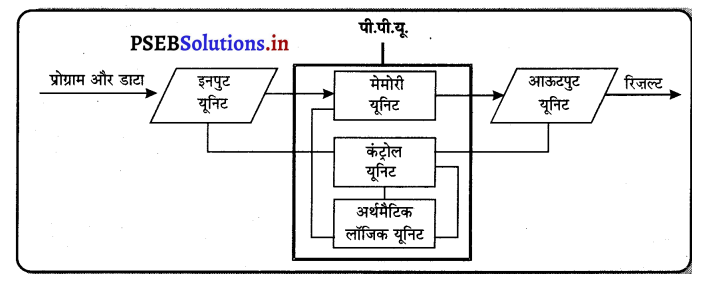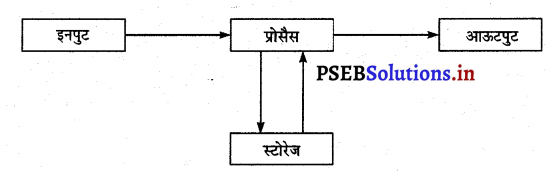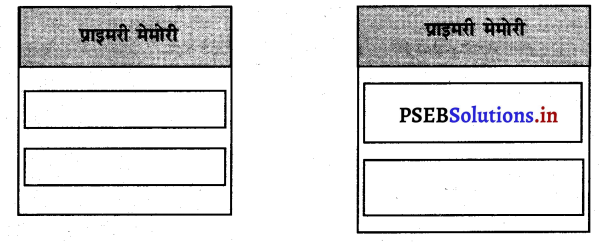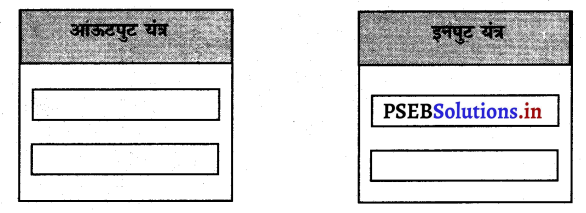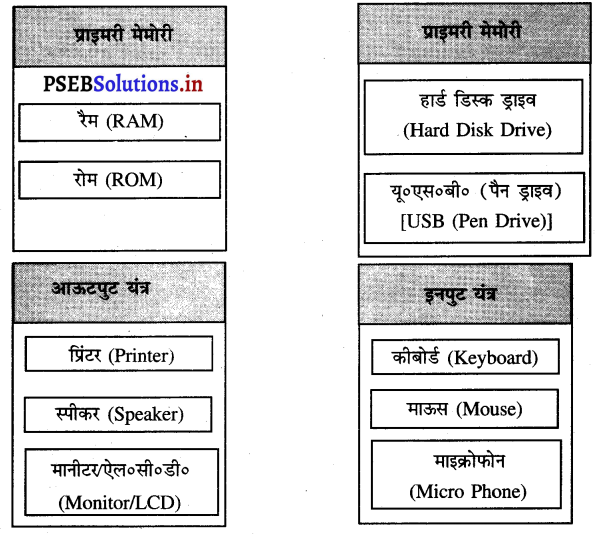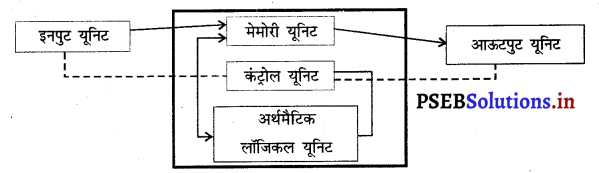This PSEB 6th Class Science Notes Chapter 11 प्रकाश, छायाएँ और परावर्तन will help you in revision during exams.
PSEB 6th Class Science Notes Chapter 11 प्रकाश, छायाएँ और परावर्तन
→ प्रकाश ऊर्जा का एक ऐसा रूप है जो हमें आस-पास की वस्तुएँ देखने में सहायता करता है।
→ प्रकाश का स्त्रोत प्राकृतिक या कृत्रिम हो सकता है, जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे, सी. एफ. एल., मोमबत्ती तथा एल. ई. डी.।
→ प्रकाश साधारणतया सीधी रेखा में चलता है।
→ अपारदर्शी वस्तुएँ अपने में से प्रकाश नहीं निकलने देती हैं और न ही इनके दूसरी ओर पड़ी वस्तुओं को देखा जा सकता है।
→ पारदर्शी वस्तुएँ अपने में से प्रकाश नहीं निकलने देती हैं और न ही इनके दूसरी ओर पड़ी वस्तुओं को देखा जा सकता है।
→ अल्पपारदर्शी वस्तुओं में से प्रकाश पूर्णरूप से नहीं गुज़र सकता है और न ही दूसरी और पड़ी वस्तुएँ स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं।
![]()
→ जब कोई अपारदर्शी वस्तु प्रकाश के पथ में आ जाती है तो इस अपारदर्शी के दूसरी ओर परछाईं बनती है।
→ चंद्रमा प्रकाशहीन है। यह सूर्य द्वारा अपने ऊपर पड़ रहे प्रकाश को परावर्तित करता है।
→ असमतल/खुरदरी सतह जैसे कपड़ा, किताब आदि द्वारा प्रकाश परावर्तन अनियमित परावर्तन होता है। इसके द्वारा किए परावर्तन के पश्चात् प्रकाश किरणें बिखर जाती हैं।
→ पिनहोल कैमरे को साधारण सामान से बनाया जा सकता है। इसके द्वारा सूर्य तथा प्रकाशमान वस्तुओं का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। यह प्रतिबिंब, उल्टा, वास्तविक तथा आकार में वस्तु से छोटा होता है।
→ दर्पण द्वारा परावर्तन होने के कारण स्पष्ट प्रतिबिंब बनते हैं।
→ प्रकाशमान वस्तुएँ-वे वस्तुएँ जिनके पास अपना स्वयं का प्रकाश होता है और वे प्रकाश को उत्सर्जित करती हैं।
→ प्रकाशहीन वस्तुएँ-वे वस्तुएँ जिनके पास अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है परंतु अन्य प्रकाशमान वस्तुओं द्वारा उत्सर्जित प्रकाश से प्रकाशमान हो जाती हैं।
→ प्रकाश- यह ऊर्जा का एक ऐसा रूप है जो हमें आस-पास की वस्तुओं को देखने में सहायता करता है।
→ प्रकाश स्त्रोत-ऐसी प्रकाशमान वस्तुएँ जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, जैसे—सूर्य, मोमबत्ती, सी. एफ. एल. आदि। ये प्रकाश स्त्रोत प्राकृतिक तथा कृत्रिम दोनों प्रकार के हो सकते हैं।
→ पारदर्शी वस्तुएँ-ऐसी वस्तुएँ जिनमें से प्रकाश नहीं गुजर सकता है तथा इसके दूसरी तरफ पड़ी वस्तुएँ स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, पारदर्शी वस्तुएँ कहलाती हैं।
→ अपारदर्शी वस्तुएँ-वे वस्तुएँ जो अपने में से प्रकाश को नहीं निकलने देती हैं और इनके दूसरी ओर पड़ी वस्तुएँ दिखाई नहीं देती हैं, को अपारदर्शी वस्तुएँ कहते हैं जैसे-गत्ते की शीट, लकड़ी, धातु तथा रबड़ आदि।
→ अल्पपारदर्शी वस्तुएँ-वे वस्तुएँ जो अपने में से प्रकाश को पूर्ण रूप से नहीं निकलने देती हैं अर्थात् अल्पमात्रा में प्रकाश को निकलने देती हैं तथा जिनके दूसरी तरफ पड़ी वस्तुएँ स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, को अल्पपारदर्शी वस्तुएँ कहते हैं। जैसे टिशू पेपर, पतला कपड़ा, तेल लगा हुआ कागज़ आदि।
→ परछाई-जब किसी प्रकाश स्त्रोत से आ रही प्रकाश किरणों के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु रूकावट बन जाती है, तो प्रकाश उस में से नहीं गुज़र सकता है तथा अपारदर्शी वस्तु की दूसरी तरफ एक काला धब्बा (क्षेत्र) बन जाता है। जिसकी बनावट अपारदर्शी वस्तु जैसी होती है, को वस्तु की परछाई कहते हैं। परछाई का आकार अपारदर्शी वस्तु से बड़ा या छोटा हो सकता है।
→ सूरज घड़ी-यह एक ऐसा यंत्र है, जो सूरज की रोशनी के साथ बनने वाली परछाई द्वारा दिन में समय दर्शाता है।
→ सूरज ग्रहण-जब धरती के ईद-गिर्द चक्कर लगाते समय ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि चंद्रमा, धरती तथा सूरज के बीच आ जाए और तीनों एक सीधी रेखा में हों तब सूरज की परछाई धरती पर बन जाती है, जिसे सूरज ग्रहण कहते हैं।
![]()
→ चंद्रग्रहण-जब धरती, सूरज तथा चंद्रमा के बीच स्थित हो तथा तीनों एक सीधी रेखा में हो तो चंद्रमा की परछाई धरती पर बनती है जिसे चंद्र ग्रहण कहते हैं।
→ पिनहोल कैमरा-एक ऐसा यंत्र जिसके द्वारा किसी स्थिर वस्तु का वास्तविक, उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है। यह प्रकाश के इस गण पर आधारित है कि प्रकाश सीधी (सरल) रेखा में चलता है।
→ दर्पण-कोई पॉलिश की गई एक समान समतल सतह जिससे उस पर पड़ रहे प्रकाश की दिशा में परिवर्तन हो जाता है, दर्पण कहलाती है।
→ प्रकाश परावर्तन-जब प्रकाश किसी चमकदार अर्थात् पॉलिश की गई सतह पर पड़ता है, तो प्रकाश का प्रसार एक विशेष दिशा में पहले माध्यम में होता है। इस प्रकाश के प्रसार की दिशा परिवर्तन की प्रक्रिया को प्रकाश परावर्तन कहते हैं। प्रकाश परावर्तन दो प्रकार का होता है ।
→ नियमित परावर्तन-जब प्रकाश किसी समतल दर्पण या चमकदार धातु की सतह पर पड़ता है तो यह नियमित रूप से प्रकाश को परावर्तित कर देती है। प्रकाश के इस परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं।
→ अनियमित परावर्तन-जब प्रकाश किसी खुरदरी या असमतल सतह पर पड़ता है तो इससे प्रकाश का दिशा परिवर्तन होने के बाद प्रकाश का बिखराव (प्रकीर्णन) हो जाता है। ऐसे प्रकाश परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के ऐसे परावर्तन के कारण हम अपने ईद गिर्द की वस्तुओं को देख पाते हैं।