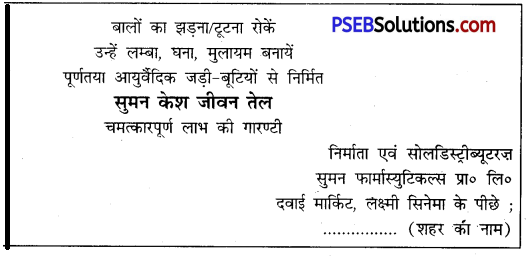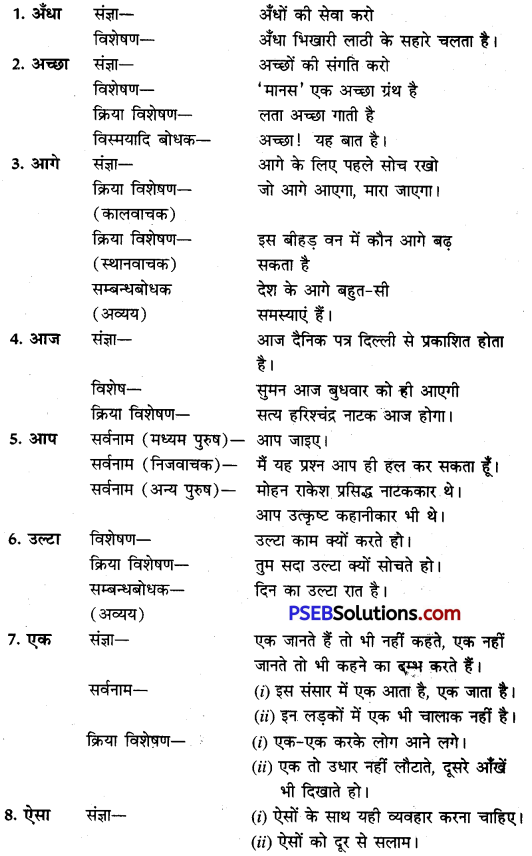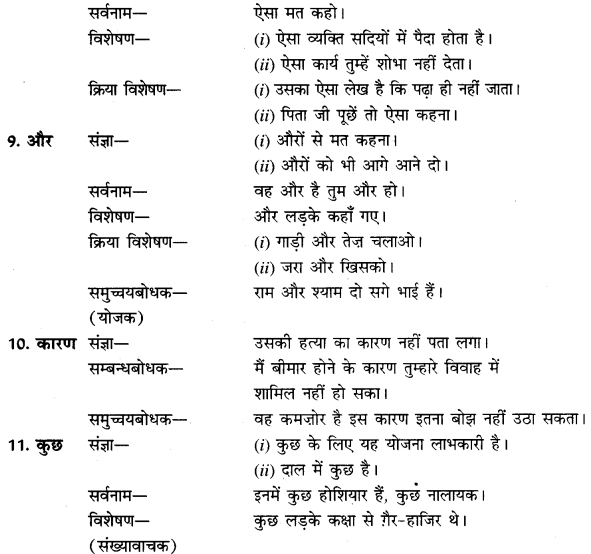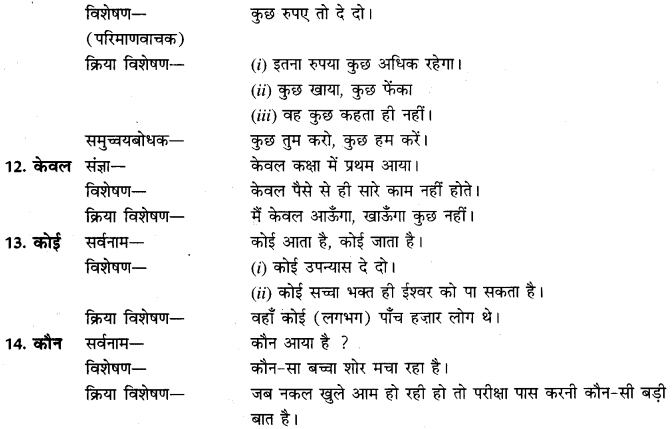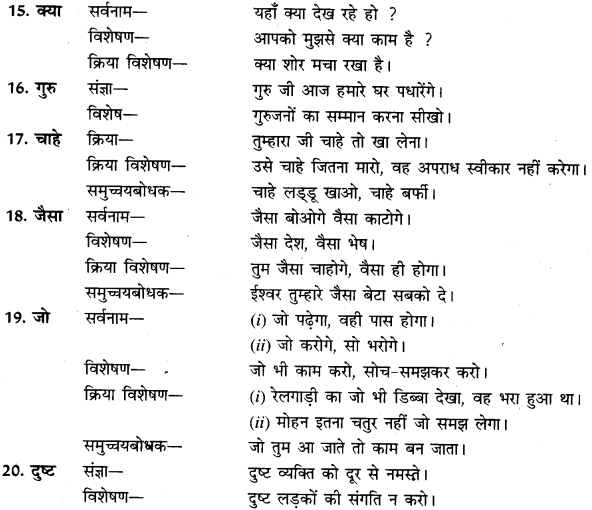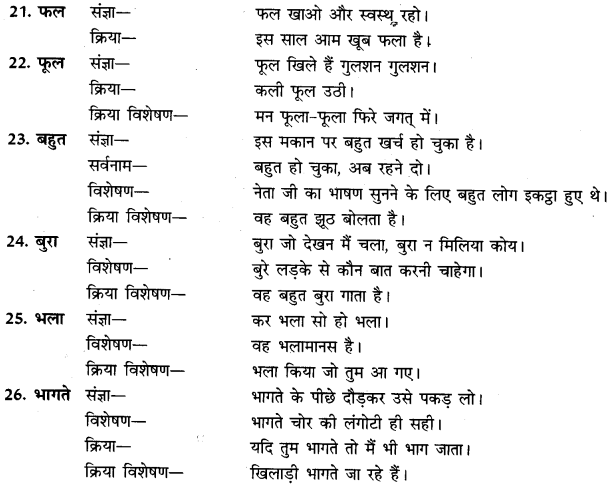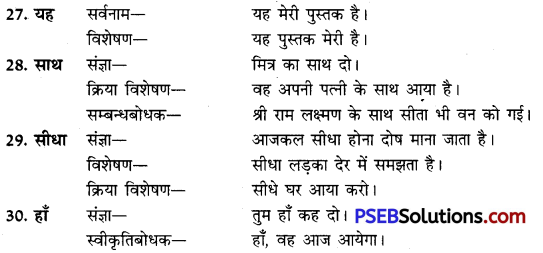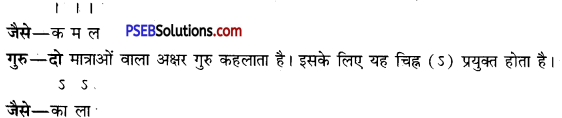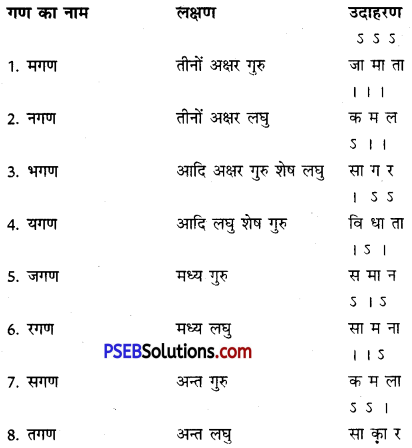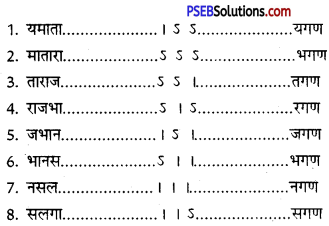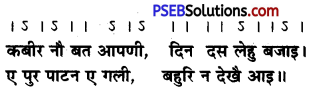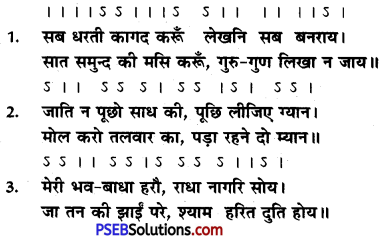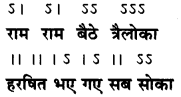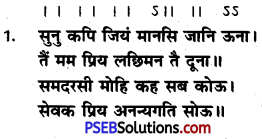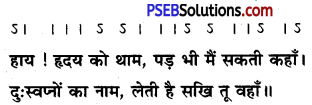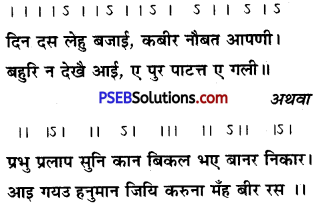Punjab State Board PSEB 12th Class Hindi Book Solutions Rachana निबंध-लेखन Questions and Answers, Notes.
PSEB 12th Class Hindi रचना निबंध-लेखन
1. मेरे जीवन का लक्ष्य
संसार में जितने भी प्राणी जन्म लेते हैं सब का कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है। मनुष्य प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है तब उसके जीवन का कोई लक्ष्य क्यों न होगा ? अवश्य है। शास्त्रों में लिखा है कि मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है अतः इसी जन्म में व्यक्ति अपने आध्यात्मिक लक्ष्य अर्थात् ईश्वर प्राप्ति के लक्ष्य को पूरा कर सकता है। किन्तु भूखे पेट तो भजन भी नहीं होता है। अतः पेट पालने के लिए प्रत्येक मनुष्य को कुछ न कुछ करना ही पड़ता है। इसी को हम भौतिक लक्ष्य की प्राप्ति करना कहते हैं।
भौतिक लक्ष्य की प्राप्ति का अर्थ है कि जीवन जीने के लिए किया जाने वाला ऐसा काम-काज कि जिसे करने से उचित आर्थिक लाभ प्राप्त हो सके। ऐसा धन्धा, जिससे प्राप्त होने वाले लाभ से जीविका चल सके, घर-परिवार का लालन-पालन सम्भव हो सके तथा सभी प्रकार के भौतिक सुख प्राप्त हो सकें।
आज जीवन मूल्य बड़ी तेजी से बदल रहे हैं। समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद ने हमारे जैसे मध्यवर्गीय परिवारों के युवकों को बहुत गम्भीरता से अपने भौतिक लक्ष्य पर विचार और निर्णय करने पर विवश कर दिया है। वह युग बीत गया जब सुनार का बेटा सुनार बनता था किन्तु आज तो विज्ञान की और उद्योग-धन्धों की उन्नति ने सारी वस्तु स्थिति ही बदल दी है। अंग्रेजों की चलाई शिक्षा नीति के अनुसार आज स्वतन्त्रता के साठ वर्ष बाद भी शिक्षा केवल नौकरी प्राप्त करने के लिए प्राप्त की जाती है। देश की जनसंख्या इतनी तीव्र गति से बढी है कि नौकरी पाना सब के लिए सम्भव नहीं है। आज नौकरी पाने के लिए कई तरह के पापड़ बेलने पड़ते हैं। रिश्वत हर कोई नहीं दे सकता तथा सिफ़ारिश हर किसी के पास नहीं होती। अत: नौकरी मिले तो कैसे ?
इन्हीं कारणों को ध्यान में रखकर मैंने निर्णय किया है कि मैं नौकरी नहीं करूँगा। बारहवीं की परीक्षा पास करके मैं कोई तकनीकी कोर्स करूँगा। ऐसा कोर्स जिसको पास करके मैं कोई अपना काम-धन्धा शुरू कर सकूँ। सरकार ने जवाहर रोज़गार योजना चला रखी है जिसके अन्तर्गत मुझे सरकारी सहायता मिल सकेगी। दूसरे आजकल बैंकों से भी आसान शर्तों और कम ब्याज पर रुपया उधार मिल जाता है। मेरा विचार है कि मैं अपने गाँव में ही किसी छोटी-मोटी चीज़ को बनाने का काम शुरू करूँ। आजकल वस्तु निर्माण के साथ-साथ उसकी मार्कीटिंग करना भी कोई सरल काम नहीं है। इस काम के लिए मैं अपने ही गाँव के कुछ पढ़े-लिखे बेरोज़गार नवयुवकों को लगाऊँगा। इस तरह वे युवक पैसा भी कमाने लगेंगे और अपने माता-पिता के साथ रहकर उनकी सेवा भी कर सकेंगे। नौकरी करने बाहर जाने वाले अपने बूढ़े माता-पिता को घर पर अकेले रहने के लिए छोड़ जाते हैं।
यह भी आजकल की एक नई समस्या बन गई बचपन से ही मेरी यह इच्छा रही है कि मैं कोई ऐसा व्यवसाय चुनूं जिसमें मुझे पूर्ण स्वतन्त्रता रहे। मुझे भी सुख मिले और राष्ट्र और समाज का भी कल्याण हो। काम चाहे कितना ही छोटा क्यों न हो उसे दिल लगाकर करना चाहिए। महात्मा गाँधी ने हमें यही शिक्षा दी है। मैं समझता हूँ मेरे उद्देश्य की पूर्ति में यदि बाधाएँ भी आएँ तो भी घबराऊँगा नहीं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर और बड़ों के आशीर्वाद से मुझे अपने उद्देश्य में अवश्य सफलता मिलेगी और मैं अपने माता-पिता, अपने समाज और अपने राष्ट्र की सेवा कर सकूँगा। प्रसिद्ध कवि मिर्जा गालिब ने ठीक ही लिखा है कदम चूम लेती है खुद आके मंज़िल, मगर जब मुसाफिर हिम्मत न हारे।

2. विद्यार्थी और अनुशासन
अनुशासन का अर्थ है नियन्त्रण में रहकर नियमों का पालन करना। विद्यार्थी जीवन में तो अनुशासन का सर्वाधिक महत्त्व है क्योंकि विद्यार्थी जीवन मनुष्य के जीवन का ऐसा भाग है जिसमें व्यक्ति नए जीवन में प्रवेश करता है। इस जीवन में नए जोश और उमंग के साथ-साथ चंचलता और चपलता उस पक्षी की भान्ति होती है जो उन्मुक्त व्योम में उड़ता है। वैसे तो अनुशासन का व्यक्ति को प्रत्येक भाग में पालन करना चाहिए, किन्तु विद्यार्थी काल में तो इसकी अधिक आवश्यकता है। विद्यार्थी काल में अनुशासन उसे भावी जीवन में सफल बनाने के सहायक होता है। गुरुसेवा, माता-पिता की आज्ञा का पालन करना और उनकी सेवा करना, छोटों के प्रति स्नेह और बड़ों के प्रति आदर भाव रखना। ये सभी अनुशासन के अन्तर्गत आते हैं। जो विद्यार्थी अपने विद्यार्थी जीवन में इस अनुशासन का पालन करता है वह सारा . . जीवन सुखी रहता है और उन्नति करता है।
अनुशासन एक ऐसी वस्तु है जिसकी अवहेलना कभी भी कहीं भी सहन नहीं की गई। आज का विद्यार्थी कल का नेता एवं शासक होगा। देश की बागडोर उसी के हाथों में होगी। इसलिए जो विद्यार्थी जीवन में ही अनुशासन नहीं सीखता उस पर देश का भविष्य उज्ज्वल कैसे रह सकता। अनुशासन का व्यक्ति के जीवन और व्यवहार से गहरा सम्बन्ध है। अपने अध्यापकों का, माता-पिता का, बड़े-बुजुर्गों का मान करना, आदर सत्कार करना, उन्हें प्रणाम करना अनुशासन का ही एक अंग है। जो विद्यार्थी इस प्रकार के अनुशासन का पालन करता है वह समाज के दूषित वातावरण के प्रभाव से बचा रहता है तथा बुरी आदतों व विचारों से अपनी रक्षा कर पाता है। अनुशासन ही विद्यार्थी के भावी जीवन को आदर्श जीवन बना सकता है।
यह कहना गलत होगा कि विद्यार्थी को अनुशासन का पाठ केवल स्कूल या कॉलेज में ही पढ़ाया जाता है। स्कूल या कॉलेज में तो विद्यार्थी मात्र चार से छ: घंटे ही रहता है। शेष समय तो वह अपने माता-पिता या समाज में रहकर ही बिताता है। यदि घर या समाज में विद्यार्थी को अनुशासनहीनता का सामना करना पड़ता है तो स्कूल/कॉलेज में उसे सिखाये, ये अनुशासन के पाठ पर पानी फिर जाता है। अतः विद्यार्थी को अनुशासन का पाठ सबसे पहले उसके मातापिता से ही मिलता है। जो माता-पिता अपने बच्चों को कुछ नहीं कहते, उनका ध्यान नहीं रखते, वे अपने बच्चों को अनुशासनहीन बना देते हैं। ऐसे बच्चे माता-पिता का आदर नहीं करते, उनके सामने चपड़-चपड़ बोलते हैं।
परिणामस्वरूप वे स्कूल या कॉलेज में भी अपने अध्यापकों का सम्मान नहीं करते। हमें यह जानकर अत्यन्त हैरानी हुई कि पंजाब में एक ऐसा शिक्षा संस्थान है जहाँ विद्यार्थी अपने अध्यापकों को विश (Wish) नहीं करते। पुराने विद्यार्थी सदा अपने अध्यापकों के चरण छूते थे किन्तु आज के विद्यार्थी ‘How do you do’ कहकर हाथ आगे बढ़ाते हैं। कुछ तथाकथित सभ्य लोग इसे विकास की संज्ञा देते हैं जबकि यह विकास नहीं ह्रास की अवस्था है। जो माता-पिता अपने बच्चों के सामने गन्दी-गन्दी गालियाँ निकालते हैं, सिगरेट, शराब पीते हैं वे अपने बच्चों को कैसे रोक सकते हैं। यह भी माना कि अध्यापकों में आज कई बटुकनाथ पैदा हो गए हैं। किन्तु विश्वास मानिए आज भी अध्यापक जी-जान से बच्चों को अनुशासन का पाठ पढ़ाने वाले ही हैं। अध्यापकों को चाहिए कि कक्षा में अपने विद्यार्थियों को अनुशासन की महत्ता पर अवश्य बताएँ।
विद्यार्थी में उत्तरदायित्व की भावना पैदा करें। उन्हें स्कूल या कॉलेज के प्रबन्ध में अथवा वहाँ मनाए जा रहे समारोहों में सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर दें। ऐसा विद्यार्थी अपने आप अनुशासन की महत्ता को समझने लगेगा। विद्यार्थी को उसके धर्म के विषय में पूरी जानकारी अवश्य दें क्योंकि धार्मिक शिक्षा अनुशासन पैदा करने का सबसे बड़ा साधन है। हमारा ऐसा मानना है कि विद्यार्थी को यदि कोई अनुशासन का प्रशिक्षण दे सकता है तो वह अध्यापक ही है।
3. समय का सदुपयोग
कहा जाता है कि आज का काम कल पर मत छोड़ो। जिस किसी ने भी यह बात कही है उसने समय के महत्त्व को ध्यान में रखकर ही कही है। समय सबसे मूल्यवान् वस्तु है। खोया हुआ धन फिर प्राप्त हो सकता है किंतु खोया हुआ समय फिर लौट कर नहीं आता। इसीलिए कहा गया है ‘The Time is Gold’ क्योंकि समय बीत जाने पर सिवाय पछतावे के कुछ हाथ नहीं आता फिर तो वही बात होती है कि ‘औसर चूकि डोमनी गावे ताल-बेताल।’ किसी चित्रकार ने समय का चित्र बनाते हुए उसके माथे पर बालों का गुच्छा दिखाया है और पीछे से उसका सिर गंजा दिखाया है। जो व्यक्ति समय को सामने से पकड़ता है, समय उसी के काबू में आता है, बीत जाने पर तो हाथ उसके गंजे सिर पर ही पड़ता है और हाथ कुछ नहीं आता। कछुआ और खरगोश की कहानी में भी कछुआ दौड़ इसलिए जीत गया था कि उसने समय के मूल्य को समझ लिया था। इसीलिए वह दौड़ जीत पाया। विद्यार्थी जीवन में भी समय के महत्त्व को एवं उसके सदुपयोग को जो नहीं समझता और विद्यार्थी जीवन आवारागर्दी और ऐशो आराम से जीवन व्यतीत कर देता है वह जीवन भर पछताता रहता है।
इतिहास साक्षी है कि संसार में जिन लोगों ने भी समय के महत्त्व को समझा वे जीवन में सफल रहे। पृथ्वी राज चौहान समय के मूल्य को न समझने के कारण ही गौरी से पराजित हुआ। नेपोलियन भी वाटरलू के युद्ध में पाँच मिनटों के महत्त्व को न समझ पाने के कारण पराजित हुआ। इसके विपरीत जर्मनी के महान् दार्शनिक कांट ने जो अपना जीवन समय के बंधन में बाँधकर कुछ इस तरह बिताते थे कि लोग उन्हें दफ्तर जाते देख अपनी घड़ियाँ मिलाया करते थे।
आधुनिक जीवन में तो समय का महत्त्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। आज जीवन में भागम-भाग और जटिलता इतनी अधिक बढ़ गई है कि यदि हम समय के साथ-साथ कदम मिलाकर न चलें तो जीवन की दौड़ में पिछड़ जाएँगे। शायद इसी कारण आज कलाई घड़ियां प्रत्येक की कलाइयों पर बँधी दिखाई देती हैं। आज सभी समय के प्रति बहुत जागरूक दिखाई देते हैं। आज के युग को प्रतिस्पर्धा का युग भी कहा जाता है। इसलिए हर कोई समय का सदुपयोग करना चाहता है। क्योंकि चिड़ियाँ खेत चुग गईं तो फिर पछताने का लाभ न होगा। आज समय का सदुपयोग करते हुए सही समय पर सही काम करना हमारे जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है।
विद्यार्थी जीवन में समय का सदुपयोग करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि विद्यार्थी जीवन बहुत छोटा होता है। इस जीवन में प्राप्त होने वाले समय का जो विद्यार्थी सही सदुपयोग कर लेते हैं वे ही भविष्य में सफलता की सीढियाँ चढते हैं और जो समय को नष्ट करते हैं, वे स्वयं नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमारे दार्शनिकों, संतों आदि ने अपने काम को तुरन्त मनोयोग से करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि ‘काल करे सो आज कर आज करे सो अब।’ कल किसने देखा है अतः दृष्टि वर्तमान पर रखो और उसका भरपूर प्रयोग करो। कर्मयोगी की यही पहचान है। पूर्व राष्ट्रपति डॉ० ए० पी० जे० अब्दुल कलाम का उदाहरण हमारे सामने है। समय का उचित सदुपयोग करके ही पहले वे मिसाइल मैन कहलाए फिर देश के राष्ट्रपति बने। जीवन दुर्लभ ही नहीं क्षणभंगुर भी है अतः जब तक सांस है तब तक समय का सदुपयोग करके हमें अपना जीवन सुखी बनाना चाहिए।
4. खेलों का जीवन में महत्त्व
खेल-कूद हमारे जीवन की एक महत्त्वपूर्ण आवश्यकता है। ये हमारे मनोरंजन का प्रमुख साधन भी हैं। पुराने जमाने में जो लोग व्यायाम नहीं कर सकते थे अथवा खेल-कूद में भाग नहीं ले सकते थे वे शतरंज, ताश जैसे खेलों से अपना मनोरंजन कर लिया करते थे। किन्तु जो लोग स्कूल या कॉलेज में पढ़ा करते थे वे स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई के पश्चात् कुछ देर खेल-कूद में भाग लेकर पढ़ाई की थकावट को दूर कर लिया करते थे। दौड़ना भागना, कूदना इत्यादि भी खेलों का ही एक अंग है। ऐसी खेलों में भाग लेकर हमारे शरीर की मांसपेशियाँ तथा शरीर के दूसरे अंग स्वस्थ हो जाया करते हैं। खेल-कूद में भाग लेकर व्यक्ति की मानसिक थकावट दूर हो जाती है।
अंग्रेज़ी की एक प्रसिद्ध कहावत है कि All work and no play makes jack a dull boy. इस कहावत का अर्थ यह है कि यदि कोई सारा दिन काम में जुटा रहेगा, खेल-कूद या मनोरंजन के लिए समय नहीं निकालेगा तो वह कुंठित हो जाएगा उसका शरीर रोगी बन जाएगा तथा वह निराशा का शिकार हो जाएगा। अतः स्वस्थ जीवन के लिए खेलों में भाग लेना अत्यावश्यक है। इस तरह व्यक्ति का मन भी स्वस्थ होता है। उसकी पाचन शक्ति भी ठीक रहती है, भूख खुलकर लगती है, नींद डटकर आती है, परिणामस्वरूप कोई भी बीमारी ऐसे व्यक्ति के पास आते डरती है।
खेलों से अनुशासन और आत्म-नियन्त्रण भी पैदा होता है और अनुशासन जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यक है। बिना अनुशासन के व्यक्ति जीवन में उन्नति और विकास नहीं कर सकता। खेल हमें अनुशासन का प्रशिक्षण देते हैं। किसी भी खेल में रैफ्री या अंपायर नियमों का उल्लंघन करने वाले खिलाड़ी को दंडित भी करता है। इसलिए हर खिलाड़ी खेल के नियमों का पालन कड़ाई से करता है। खेल के मैदान में सीखा गया यह अनुशासन व्यक्ति को आगे चलकर जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी काम आता है। देखा गया है कि खिलाड़ी सामान्य लोगों से अधिक अनुशासित होते हैं।
खेलों से सहयोग और सहकार की भावना भी उत्पन्न होती है। इसे Team Spirit या Sportsmanship भी कहा जाता है। केवल खेल ही ऐसी क्रिया है जिसमें सीखे गए उपर्युक्त गुण व्यक्ति के व्यावहारिक जीवन में बहुत काम आते हैं। आने वाले जीवन में व्यक्ति सब प्रकार की स्थितियों, परिस्थितियों और व्यक्तियों के साथ काम करने में सक्षम हो जाता है। Team spirit से काम करने वाला व्यक्ति दूसरों से अधिक सामाजिक होता है। वह दूसरों में जल्दी घुलमिल जाता है। उसमें सहन शक्ति और त्याग भावना दूसरों से अधिक मात्रा में पाई जाती है।
खेल-कूद में भाग लेना व्यक्ति के चारित्रिक गुणों का भी विकास करता है। खिलाड़ी चाहे किसी भी खेल का हो अनुशासनप्रिय होता है। क्रोध, ईर्ष्या, घृणा आदि हानिकारक भावनाओं का वह शिकार नहीं होता। खेलों से ही उसे देश प्रेम और एकता की शिक्षा मिलती है। एक टीम में अलग-अलग धर्म, सम्प्रदाय, जाति, वर्ग आदि के खिलाड़ी होते हैं। वे सब मिलकर अपने देश के लिए खेलते हैं।
इससे स्पष्ट है कि खेल जीवन की वह चेतन शक्ति है जो दिव्य ज्योति से साक्षात्कार करवाती है। अत: उम्र और शारीरिक शक्ति के अनुसार कोई न कोई खेल अवश्य खेलना चाहिए। खेल ही हमारे जीवन में एक नई आशा, महत्त्वाकांक्षा और ऊर्जा का संचार करते हैं। खेलों के द्वारा ही जीवन में नए-नए रंग भरे जा सकते हैं, उसे इंद्रधनुषी सुन्दर या मनोरम बनाया जा सकता है।
5. राष्ट्र भाषा हिंदी
भारत 15 अगस्त, सन् 1947 को स्वतन्त्र हुआ और 26 जनवरी, सन् 1950 से अपना संविधान लागू हुआ। भारतीय संविधान के सत्रहवें अध्याय की धारा 343 (1) के अनुसार ‘देवनागरी लिपि में हिंदी’ को भारतीय संघ की राजभाषा और देश की राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई थी सन् 1965 से देश के सभी कार्यालयों, बैंकों, आदि में सारा काम-काज हिंदी में होगा। किन्तु खेद का विषय है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के साठ वर्ष बाद भी सारा काम-काज अंग्रेज़ी में ही हो रहा है। देश का प्रत्येक व्यक्ति यह बात जानता है कि अंग्रेज़ी एक विदेशी भाषा है और हिंदी हमारी अपनी भाषा है।
महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने भी हिंदी भाषा को ही अपनाया था हालांकि उनकी अपनी मातृ भाषा गुजराती थी। उन्होंने हिंदी के प्रचार के लिए ही ‘दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा’ प्रारंभ की थी। उन्हीं के प्रयास का यह परिणाम है कि आज तमिलनाडु में हिंदी भाषा पढ़ाई जाती है, लिखी और बोली जाती है। वास्तव में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा इसलिए दिया गया क्योंकि यह भाषा देश के अधिकांश भाग में लिखी-पढ़ी और बोली जाती है। इसकी लिपि और वर्णमाला वैज्ञानिक और सरल है। आज हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान की राजभाषा हिंदी घोषित हो चुकी है।
हिंदी भाषा का विकास उस युग में भी होता रहा जब भारत की राजभाषा हिंदी नहीं थी। मुगलकाल में राजभाषा फ़ारसी थी, तब भी सूर, तुलसी, आदि कवियों ने श्रेष्ठ हिंदी साहित्य की रचना की। उन्नीसवीं शताब्दी में अंग्रेज़ी शासन के दौरान अंग्रेज़ी राजभाषा रही तब भी भारतेन्दु, मैथिलीशरण गुप्त और प्रसाद जी आदि कवियों ने उच्चकोटि का साहित्य रचा। इसका एक कारण यह भी था कि हिंदी सर्वांगीण रूप से हमारे धर्म, संस्कृति और सभ्यता और नीति की परिचायक है। भारतेन्दु हरिशचन्द्र जी ने आज से 150 साल से भी पहले ठीक ही कहा था
निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल।
बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय को शूल।।
कहा जाता है कि भारत एक बहु-भाषायी देश है। अतः इसकी एक राष्ट्रभाषा कैसे हो सकती है। ऐसा तर्क देने वाले यह भूल जाते हैं कि रूस में 33 भाषाएँ बोली जाती हैं जबकि उनकी राष्ट्र भाषा रूसी है। हिंदी भाषा का विरोध करने वाले यह भूल जाते हैं कि हिंदी भाषा विश्व की सब भाषाओं में से सरल भाषा है और उसका उच्चारण भी सरल है। तभी तो अंग्रेजों ने भारत में आने के बाद इस भाषा को आसानी से सीख लिया था। हिंदी भाषा की एक विशेषता यह भी है कि इसमें अन्य भाषाओं के शब्द आसानी से समा जाते हैं और जंचने भी लगते हैं। आज उर्दू फ़ारसी के अनेक शब्द हिंदी भाषा में समा चुके हैं। हिंदी भाषा का क्षेत्र अन्य प्रान्तीय भाषाओं से अधिक विस्तृत है। इस पर उच्चारण की दृष्टि से भी हिंदी संसार की सरलतम भाषा है। यह भाषा अपने उच्चारण के अनुसार ही लिखी जाती है जबकि अन्य भाषाओं में उच्चारण के अनुसार नहीं लिखा जा सकता। डॉ० सुनीति कुमार चैटर्जी ने ठीक ही कहा है कि समग्र भारत के सांस्कृतिक एकता की प्रतीक हिंदी है। व्यवहार करने वालों और बोलने वालों की संख्या के क्रम के अनुसार चीनी, अंग्रेज़ी के बाद इसका तीसरा स्थान है।
लेकिन खेद का विषय है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के इतने वर्ष बाद भी हिंदी के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। अपने विभिन्न राजनीतिक स्वार्थों के कारण विभिन्न राजनेता इसके वांछित और स्वाभाविक विकास में रोड़े अटका रहे हैं। अंग्रेज़ों की विभाजन करो और राज करो की नीति पर आज हमारी सरकार भी चल रही है जो देश की विभिन्न जातियों, सम्प्रदायों और वर्गों के साथ-साथ भाषाओं में जनता को बाँट रही है ऐसा वह अपने वोट बैंक को ध्यान में रख कर कर रही है। यह मानसिकता हानिकारक है और इसे दूर किया जाना चाहिए। हमें अंग्रेज़ी की दासता से मुक्त होना चाहिए।
हिंदी के प्रचार-प्रसार में लोगों को खुलकर सामने आना चाहिए। हिंदी का विकास जनवादी रूप में ही होना चाहिए। ऐसा करके उसका शब्द भंडार बढ़ेगा और वैज्ञानिक आविष्कारों को व्यक्त करने वाली पदावली का अभाव नहीं रहेगा। हिंदी की क्षमता का यथासंभव विकास करना हमारा कर्तव्य है। इसे सच्चे अर्थों में राष्ट्र की भाषा बनाने के लिए प्रयास किये जाने चाहिएं। हिंदी में ही भारतीय संस्कृति का उन्नत रूप विद्यमान है अतः देश, संस्कृति और एकता की रक्षा के लिए राष्ट्रभाषा का समुचित विकास आवश्यक है।

6. राष्ट्रीय एकता
भारत 125 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाला एक विशाल देश है। इसमें विभिन्न जातियों, धर्मों, सम्प्रदायों के लोग रहते हैं। कई प्रदेशों की अलग-अलग भाषाएँ हैं। लोगों के अलग-अलग रीति रिवाज हैं, अलग-अलग वेश-भूषा है किन्तु इस अनेकता में भी एकता है जैसे किसी माला में पिरोये अलग अलग रंगों के फूल। इसी को सरल शब्दों में राष्ट्रीय एकता कहते हैं। डॉ० धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार-राष्ट्र उस जन समुदाय का नाम है जिसमें लोगों की स्वाभाविक समानताओं के बन्धन ऐसे दृढ़ और सच्चे हों कि वे एकत्र रहने से सुखी और अलग-अलग रहने से असन्तुष्ट रहें और समानताओं के बन्धन से सम्बद्ध अन्य लोगों की पराधीनता को सहन न कर सकें।” हमारा राष्ट्र एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ सभी धर्मालम्बियों को अपने-अपने धर्म का पालन व प्रचार करने की खुली छूट है। हमारी राष्ट्रभाषा एक है तथा हमारी राजभाषा भी एक है। देश के सब प्राणियों को समान अधिकार प्राप्त हैं। यहाँ वर्ण, जाति अथवा लिंग के आधार पर किसी से कोई भेद नहीं किया जाता।
लगता है हमारी राष्ट्रीय एकता के वट वृक्ष पर कुछ बाहरी शक्तियों और कुछ भीतरी शक्तियों रूपी कीटाणुओं ने आक्रमण किया है। कुछ देश हमारे राष्ट्र की उन्नति से जलते हैं। वे देश के शान्त वातावरण और साम्प्रदायिक सौहार्द को खण्डित करने का प्रयास करते हैं। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान को ही लें वह अपने देश की कमजोरियों और अभावों को छिपाने के लिए हमारे देश में आतंक फैलाने का यत्न कर रहा है। किन्तु वह पाण्डवों की उक्ति को भूल गया है कि पाण्डव पाँच हैं और कौरव 100 किन्तु किसी बाहरी शत्रु के लिए एक सौ पाँच हैं। पाकिस्तान ने अक्टूबर 1948 में कबायलियों के भेष में कश्मीर में घुसपैट करने की कोशिश की। सन् 1965, सन् 1971 और सन् 1999 में कारगिल क्षेत्र में भारत पर आक्रमण कर देश की एकता को खण्डित करने की कोशिश की किन्तु हर बार हमारे वीर सैनिकों ने युद्ध के मोर्चे पर और हमारी जनता ने घरेलू मोर्चे पर उसे मुँह तोड़ जवाब दिया। देश की जनता ने सोचा कि भले ही हमारी घरेलू समस्याएँ अनेक हैं, हम उसका निपटारा स्वयं कर लेंगे किन्तु किसी बाहरी शक्ति को अपने देश की अखंडता और राष्ट्रीय एकता को भंग नहीं करने देंगे।
हमारी राष्ट्रीय एकता को खण्डित करने में कुछ भीतरी शक्तियाँ भी काम कर रही हैं । इन शक्तियों के कारण देश की प्रगति और विकास उतनी गति से नहीं हो पा रहा जितनी गति से होनी चाहिए। हमारी राष्ट्रीय एकता को सबसे बड़ा खतरा क्षेत्रवाद की भावना से है। इसी भावना के अन्तर्गत पहले पूर्वी पंजाब कहे जाने वाले पंजाब के हरियाणा और हिमाचल भाग कर दिये गये। बिहार से झारखंड, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड नए राज्य बना दिये गए। यहीं बस नहीं अब राज्यों को विशेषाधिकार दिये जाने की माँग उठ रही है। जम्मू-कश्मीर में भी जम्मू को नया राज्य बनाए जाने की माँग उठ रही है। शायद विभाजन के समर्थक यह दावा कर रहे हों कि ऐसा प्रशासन की सहूलियत के लिए किया जा रहा है किन्तु यह दलील गले नहीं उतरती। विभाजन से पूर्व पंजाब राज्य के 29 ज़िले थे और उनका प्रशासन केवल सात मंत्री चला रहे थे। जबकि पंजाब, हरियाणा और हिमाचल को मिलाकर कहे जाने वाले पूर्वी पंजाब में अब सैंकड़ों मंत्री हैं।
क्या यह जनता के पैसे का दुरुपयोग नहीं है। हमें तो लगता है पहले प्रशासन अब से अधिक सुचारु ढंग से चल रहा था। प्रान्तवाद की इस भावना को बढ़ाने में टेलिविज़न पर दिखाई जाने वाली गीतों की प्रतियोगिताओं ने बड़ा योगदान दिया है। इन प्रतियोगिताओं में दर्शक अपने-अपने प्रान्त के प्रतियोगी को ही वोट देते हैं। जब तक हम ‘धर्म अनेक पर देश एक’ के साथ-साथ यह नारा नहीं देते कि ‘प्रान्त अनेक पर देश एक’ तब तक राष्ट्रीय एकता की रक्षा न हो सकेगी।
हमारी राष्ट्रीय एकता को दूसरा बड़ा खतरा भाषावाद से है। सरकार ने भाषा के आधार पर प्रान्तों का गठन करके इस भावना को और भी बढ़ावा दिया है। आज हम पंजाबी, बंगाली, या गुजराती होने का गौरव अधिक भारतीय होने का गौरव कम अनुभव करते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि गर्व से कहो कि हम भारतीय हैं। तमिलनाडु में हिंदी भाषा का विरोध इसी भाषावाद का परिणाम है।
हमारी राष्ट्रीय एकता को साम्प्रदायिकता की भावना भी हानि पहुँचा रही है। आज लोग अपनी जाति, धर्म और सम्प्रदाय के बारे में ही सोचते हैं देश के बारे में कम। छोटी-सी बात को लेकर साम्प्रदायिक दंगे भड़क उठते हैं। यदि उपर्युक्त बाधाओं को ईमानदारी से दूर करने का प्रयत्न किया जाए तो राष्ट्रीय एकता के बलबूते देश विकसित देशों में शामिल हो सकता है।
7. साम्प्रदायिक सद्भाव
साम्प्रदायिक एकता के प्रथम दर्शन हमें सन् 1857 के स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान देखने को मिला। उस समय हिन्दूमुसलमानों ने कंधा से कंधा मिलाकर अंग्रेजों से टक्कर ली थी। यह दूसरी बात है कि कुछ देशद्रोहियों और अंग्रेज़ों के पिओं के कारण यह आन्दोलन सफल न हो सका था। अंग्रेज़ बड़ी चालाक कौम थी। उन्होंने सन् 1857 के बाद देश के शासन को कम्पनी सरकार से विकटोरिया सरकार में बदल दिया। साथ ही बाँटो और शासन करो (Devide & Rule) की नीति के अनुसार हिन्दू और मुसलमानों को बाँटने का काम भी किया। उन्होंने हिन्दुओं को रायसाहब, रायबहादुर और मुसलमानों को खाँ साहब और खाँ बहादुर की उपाधियाँ प्रदान करके साम्प्रदायिकता की इस खाई को ओर भी चौड़ा कर दिया। अंग्रेजों ने शिक्षा नीति भी ऐसी बनाई जिससे दोनों सम्प्रदाय दूर हो जाएँ। अंग्रेज़ की चालाकी से ही मुहम्मद अली जिन्ना ने सन् 1940 में पाकिस्तान की माँग की और अंग्रेजों ने देश छोड़ने से पहले साम्प्रदायिक आधार पर देश के दो टुकड़े कर दिये। विश्व में पहली बार आबादी का इतना बड़ा आदान-प्रदान हुआ। हिन्दू-मुस्लिम दंगे हुए जिसमें लाखों लोग मारे गए।
सन् 1950 में देश का संविधान बना और भारत को एक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र घोषित किया गया। प्रत्येक जाति, धर्म, सम्प्रदाय को पूर्ण स्वतन्त्रता दी गई और सब धर्मों को समान सम्मान दिया गया। आप जानकर शायद हैरान होंगे कि विश्व में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या भारत में ही है। बहुत से देशभक्त मुसलमान पाकिस्तान नहीं गए। लेकिन पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान में स्वतन्त्रता के साठ वर्ष बाद भी जनतान्त्रिक प्रणाली लागू नहीं हो सकी और भारत विश्व का सबसे बड़ा जनतान्त्रिक देश बन गया है। पाकिस्तान ने इसी झेंप को मिटाने के लिए पहले 1965 में फिर 1971 में और अभी हाल ही में 1999 में कारगिल पहाड़ियों पर आक्रमण किया पर हमारे वीर सैनिकों ने उसे मुँह तोड़ जबाव दिया। पाकिस्तान इस पर भी बाज़ नहीं आया उसकी अपनी गुप्तचर एजेंसी आई० एस० आई० ने देश में साम्प्रदायिक दंगे भड़काने के लिए आतंकवादियों को हमारे देश में भेजना शुरू किया। कई जगह बम विस्फोट किये गए। कई धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया गया। जब हिन्दुओं के धार्मिक स्थलों पर किये जाने वाले बम विस्फोटों से भी देश की साम्प्रदायिक एकता को भंग न किया जा सका तो मुस्लिम धार्मिक स्थलों पर हैदराबाद और राजस्थान में बम विस्फोट किये गए किन्तु देश की सूझवान जनता ने शत्रु की सारी कोशिशों के बावजूद साम्प्रदायिक सौहार्द को नष्ट नहीं होने दिया।
हम यह जानते हैं कि कोई भी धर्म हिंसा, घृणा या द्वेष नहीं सिखाता। सभी धर्म या सम्प्रदाय मनुष्य को नैतिकता, सहिष्णुता और शान्ति का पाठ पढ़ाते हैं किन्तु कुछ कट्टरपंथी धार्मिक नेता अपने स्वार्थ के लिए लोगों में धार्मिक भावनाएँ भड़काकर देश में अशान्ति और अराजकता फैलाने का यत्न करते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि-
मज़हब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना,
हिन्दी हैं हम वतन है हिन्दोस्तां हमारा।
साम्प्रदायिक सद्भाव बनाए रखने पर ही हम विकासशील देशों की सूची से निकल कर विकसित देशों में शामिल हो सकते हैं। साम्प्रदायिक सद्भाव बनाए रखकर ही हम तीव्र गति से उन्नति कर सकते हैं। हमें महात्मा गाँधी जी की सर्वधर्म सद्भाव नीति को अपनाना चाहिए और उनके इस भजन को याद रखना चाहिए कि, “ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान।”
हमारी सरकार भले ही धर्मनिरपेक्ष होने का दावा करती है किन्तु वोट बैंक की राजनीति को ध्यान में रखकर वह एक ही धर्म की तुष्टिकरण के लिए जो कुछ कर रही है उसके कारण धर्मों और जातियों में दूरी कम होने की बजाए और भी बढ़ रही है। धर्मनिरपेक्षता को यदि सही अर्थों में लागू किया जाए तो कोई कारण नहीं कि धार्मिक एवं साम्प्रदायिक सद्भाव न बन सके। जनता को भी चाहिए कि वह साम्प्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाले नेताओं से चाहे वे धार्मिक हों या राजनीतिक, बचकर रहे, उनकी बातों में न आएँ।
8. आतंकवाद की समस्या
आज यदि हम भारत की विभिन्न समस्याओं पर विचार करें तो हमें लगता है कि हमारा देश अनेक समस्याओं के चक्रव्यहू में घिरा हुआ है। एक ओर भुखमरी, दूसरी ओर बेरोजगारी, कहीं अकाल तो कहीं बाढ़ का प्रकोप है। इन सबसे भयानक समस्या आतंकवाद की समस्या विकट है जो देश रूपी वट वृक्ष को दीमक के समान चाट-चाट कर खोखला कर रही है। कुछ अलगाववादी शक्तियां तथा पथ-भ्रष्ट नवयुवक हिंसात्मक रूप से देश के विभिन्न क्षेत्रों में दंगा फसाद करा कर अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए हैं।
आतंकवाद से तात्पर्य “देश में आतंक की स्थिति उत्पन्न करना” है। इसके लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों में निरन्तर हिंसात्मक उत्पात मचाए जाते हैं जिससे सरकार उनमें उलझ कर सामाजिक जीवन के विकास के लिए कोई कार्य न कर सके। कुछ विदेशी शक्तियां भारत की विकास दर को देख कर जलने लगी थीं। वे ही भारत के कुछ स्वार्थी लोगों को धन-दौलत का लालच देकर उनसे उपद्रव कराती हैं जिससे भारत विकसित न हो सके। आतंकवादी रेल पटरियां उखाड़ कर, बस यात्रियों को मार कर, बैंकों को लूट कर, सार्वजनिक स्थलों पर बम फेंक कर आदि कार्यों द्वारा आतंक फैलाने में सफल होते हैं।
भारत में आतंकवाद के विकसित होने के अनेक कारण हैं जिनमें से प्रमुख ग़रीबी, बेरोज़गारी, भुखमरी तथा धार्मिक उन्माद हैं। इनमें से धार्मिक कट्टरता आतंकवादी गतिविधियों को अधिक प्रोत्साहित कर रही हैं। लोग धर्म के नाम पर एक-दूसरे का गला घोंटने के लिए तैयार हो जाते हैं। धार्मिक उन्माद अपने विरोधी धर्मावलम्बी को सहन नहीं कर पाता। परिणामस्वरूप धर्म के नाम पर अनेक दंगे भड़क उठते हैं। इतना ही नहीं धर्म के नाम पर अलगाववादी अलग राष्ट्र की मांग भी करने लगते हैं। इससे देश भी खतरे में पड़ जाता है।।
भारत सरकार को आतंकवादी गतिविधियों को कुचलने के लिए कठोर पग उठाने चाहिएं। इसके लिए सर्वप्रथम कानून एवं व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना चाहिए। जहां-जहां अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारे देश की सीमा को छू रही है उस समस्त क्षेत्र की पूरी नाकाबंदी की जानी चाहिए जिससे आतंकवादियों को सीमा पार से हथियार, गोला-बारूद तथा प्रशिक्षण न प्राप्त हो सके। पथ-भ्रष्ट युवक-युवतियों को समुचित प्रशिक्षण देकर उनके लिए रोज़गार के पर्याप्त अवसर जुटाये जाने चाहिएं। यदि युवा-वर्ग को व्यस्त रखने तथा उन्हें उनकी योग्यता के अनुरूप कार्य दे दिया जाए तो वे पथ-भ्रष्ट नहीं होंगे इससे आतंकवादियों को अपना षड्यंत्र पूरा करने के लिए जन-शक्ति नहीं मिलेगी तथा वे स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे।
जनता को भी सरकार से सहयोग करना चाहिए। कहीं भी किसी संदिग्ध व्यक्ति अथवा वस्तु को देखते ही उसकी सूचना निकट के पुलिस थाने में देनी चाहिए। बस अथवा रेलगाड़ी में बैठते समय आस-पास अवश्य देख लेना चाहिए कि कहीं कोई लावारिस वस्तु तो नहीं है। अपरिचित व्यक्ति को कुछ उपहार आदि नहीं लेना चाहिए तथा सार्वजनिक स्थल पर भी संदेहास्पद आचरण वाले व्यक्तियों से बच कर रहना चाहिए। इस प्रकार जागरूक रहने से भी हम आतंकवादियों को आतंक फैलाने से रोक सकते हैं।
कोई भी धर्म किसी की भी निर्मम हत्या की आज्ञा नहीं देता है। प्रत्येक धर्म ‘मानव’ ही नहीं अपितु प्राणिमात्र से प्रेम करना सिखाता है। अतः धार्मिक संकीर्णता से ग्रस्त व्यक्तियों का समाजिक बहिष्कार किया जाना चाहिए तथा धार्मिक स्थानों की पवित्रता को अपने स्वार्थ के लिए नष्ट करने वाले लोगों के विरुद्ध सभी धर्मावलम्बियों को एक साथ मिलकर प्रयास करने चाहिएं। इससे धर्म की आड़ लेकर आतंकवाद को प्रोत्साहित करने वाले लोगों पर अंकुश लगा सकेगा। सरकार को भी धार्मिक स्थलों के राजनीतिक उपयोगों पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिए।
यदि आतंकवाद की समस्या का गम्भीरता से समाधान न किया गया तो देश का अस्तित्व खतरे में पड़ जायेगा। सभी परस्पर लड़ कर समाप्त हो जाएंगे। जिस आज़ादी को हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर प्राप्त किया था उसे हम आपसी वैर-भाव से समाप्त कर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेंगे। देश पुनः परतन्त्रता के बन्धनों से जकड़ा जायेगा। आतंकवादी हिंसा के बल से हमारा मनोबल तोड़ रहे हैं। हमें संगठित होकर उनकी ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए जिससे उनका मनोबल समाप्त हो जाये तथा वे जान सकें कि उन्होंने एक गलत मार्ग अपनाया है। वे आत्मग्लानि के वशीभूत होकर जब अपने किए पर पश्चात्ताप करेंगे तभी उन्हें देश की मुख्याधारा में सम्मिलित किया जा सकता है। अत: आतंकवाद की समस्या का समाधान जनता एवं सरकार दोनों के मिले-जुले प्रयासों से ही सम्भव हो सकता है।

9. बढ़ती बेरोज़गारी की समस्या और समाधान
बेरोज़गारी की समस्या आज भारत की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। इतिहास साक्षी है कि बेरोज़गारी की समस्या अंग्रेज़ी शासन की देन है। जब अंग्रेज़ों ने भारतीय गाँवों की स्वतन्त्र इकाई को समाप्त करने के साथ-साथ गाँवों के अपने लघु एवं कुटीर उद्योग भी नष्ट कर दिये। वे भारत से कच्चा माल ले जाकर इंग्लैण्ड में अपने कारखानों में माल बनाकर महँगे दामों पर यहाँ बेचने लगे। तभी तो भारतेन्दु हरिश्चन्द्र जैसे कवियों को यह कहना पडा-‘पै धन विदेश चलिजात यहै अति ख्वारी’ गाँव के कारीगर बेकार हो गए और उन्होंने आजीविका की तलाश में शहरों का रुख किया। देश तब वर्गों में नहीं व्यवसायों में बँट गया। अंग्रेजों ने शासन चलाने के लिए शिक्षा नीति ऐसी लागू की कि हर पढ़ा-लिखा युवक सरकारी नौकरी पाने की होड़ में लग गया। सभी बाबू बनना चाहते थे। उन लोगों ने अपने पुश्तैनी धंधे छोड़ दिये या अंग्रेज़ की नीति से भुला दिये। नौकरियाँ कम और पाने वाले दिनों-दिन बढ़ते गए। फलस्वरूप देश को बेरोज़गारी की समस्या का सामना करना पड़ा।
देश स्वतन्त्र हुआ। बेरोज़गारी दूर करने के लिए सरकार ने बड़े-बड़े उद्योग-धन्धे स्थापित किये। किन्तु खेद का विषय है कि बेरोज़गारी दूर करने वाले कुटीर और लघु उद्योगों के विकास के लिए स्वतन्त्रता प्राप्ति के 60 वर्ष बाद भी ध्यान नहीं दिया गया। इस पर सोने पर सुहागे का काम जनसंख्या में वृद्धि ने किया। – कोई ज़माना था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। कहते हैं यहाँ दूध, घी की नदियाँ बहा करती थीं किन्तु अंग्रेज़ जाते-जाते साम्प्रदायिकता, भ्रष्टाचार, आपसी फूट और बेकारी यहाँ छोड़ गए। इन सभी समस्याओं से हम अभी तक पीछा नहीं छुड़ा पाये हैं।
हमारी गलत शिक्षा नीतियों ने बेरोजगारों की संख्या में काफ़ी वृद्धि कर दी है। आज अशिक्षित ही नहीं पढ़े-लिखे नौजवान भी नौकरी पाने के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में 65.8% शिक्षित वर्ग के लोग बेरोज़गार हैं। पढ़ाई करने वाले नौजवानों को यह भरोसा नहीं कि पढ़-लिखकर उन्हें नौकरी मिलेगी भी या नहीं इसका परिणाम यह हो रहा है कि युवा पीढ़ी में असंतोष और आक्रोश बढ़ रहा है। लूटपाट या चेन झपटने जैसी घटनाओं में वृद्धि का कारण इसी बेरोज़गारी को माना जा रहा है। युवा वर्ग को आरक्षण की मार ने भी सताया हुआ है।
भारत सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से बेरोज़गारी दूर करने का थोड़ा बहुत प्रयास अवश्य किया है किन्तु वह भी ऊँट के मुँह में जीरा वाली बात हुई है। सरकार ने देश में बड़े-छोटे उद्योग भी इसी उद्देश्य से स्थापित किये हैं कि इनमें युवा वर्ग को रोजगार प्राप्त हो पर इन संस्थानों में भी भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद का बोलबाला है और प्रतिभावान युवक मुँह बनाए दूर खड़ा देखता रह जाता है, कर कुछ नहीं सकता। सरकार को चाहिए कि वह ऐसी शिक्षा नीति अपनाए जिससे पढ़ाई पूरी करने के बाद युवक नौकरी के पीछे न भागें। अपना काम धन्धा शुरू करे। इस सम्बन्ध में सरकार को नष्ट हुए लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास की ओर ध्यान देना होगा। देखने में आया है कृषि विज्ञान में स्नातक की डिग्री लेने वाला युवक खेत में काम कर हज़ारों रुपए नहीं बल्कि कुछ सौ की कृषि इन्सपेक्टर की नौकरी चाहता है।
लोगों को भी अपनी सोच को बदलना होगा। पढ़ाई केवल नौकरी पाने के लिए नहीं होनी चाहिए। डेयरी, मुर्गी पालन, मछली पालन, मुशरूम उगाने आदि अनेक धंधे हैं, जिन्हें आज का नौजवान अपना सकता है। सरकार और जनता यदि चाहे तो बेरोज़गारी के भूत को इस देश से शीघ्र भगाया जा सकता है।
10. भ्रष्टाचार की समस्या
भ्रष्टाचार का अर्थ किसी जमाने में बड़ा व्यापक हुआ करता था अर्थात् हर उस आचरण को जो अनैतिक हो, सामाजिक नियमों के विरुद्ध हो, भ्रष्टाचार कहा जाता था किन्तु आज भ्रष्टाचार केवल रिश्वतखोरी के अर्थ में ही सीमित होकर रह गया है। वर्तमान भ्रष्टाचार कब और कैसे उत्पन्न हुआ इस प्रश्न पर विचार करते समय हमें पता चलता है कि यह समस्या भी बेरोज़गारी, महंगाई और साम्प्रदायिकता की तरह अंग्रेजों की देन है। अंग्रेज़ अफ़सर स्वयं तो रिश्वत न लेते थे पर अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को चाय पानी के नाम पर रिश्वत दिलाते थे। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद यही चाय पानी की आदत छोटे-बड़े अफसरों को पड़ गई। अन्तर केवल इतना था कि चपरासी या क्लर्क तो चाय पानी के लिए दो-चार रुपए प्राप्त करते थे, अफसर लोग सैंकड़ों में पाने की इच्छा करने लगे और बीसवीं शताब्दी के अन्त तक पहुँचते-पहुँचते यह चाय पानी का पैसा हज़ारों लाखों तक जा पहुँचा। सरकारी अफ़सरों और कर्मचारियों के साथ-साथ चाय-पानी का यह चस्का एम० एल० ए०, एम० पी० और मन्त्रियों तक को लग गया। संसद् में प्रश्न पूछे जाने को लेकर कितने सांसद रिश्वत लेते पकड़े गए यह हर कोई जानता है।
भ्रष्टाचार के पैर इस कदर पसर चुके हैं कि आज आदमी को अपना काम करवाने के लिए चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो चाय पानी के पैसे देने पड़ते हैं। पकड़ में आती है तो केवल छोटी मछलियाँ बड़ी मछली पकड़ी भी जाती है तो कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सभी जानते हैं कि बीसवीं शताब्दी में कितने घोटाले पकड़े गए जिनमें करोड़ों का लेन-देन हुआ है किन्तु यह सभी घोटाले दफतरी फाइलों में ही दब कर रह गए हैं। कोई छोटा सरकारी कर्मचारी रिश्वत लेता पकड़ा जाता है तो उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है किन्तु क्या कोई बताएगा कि कितने मन्त्री या राजनीतिज्ञ हैं जो करोड़ों के घोटाले में लिप्त हैं और उन्हें कोई दण्ड दिया गया हो।
भ्रष्टाचार की इस बीमारी को बढ़ाने के लिए हमारा व्यापारी वर्ग भी ज़िम्मेदार है। अपने आयकर या दूसरे करों के केसों के निपटारे के लिए अपना काम तुरन्त करवाने के चक्कर में वे सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत देते हैं। इस भ्रष्टाचार के रोग से हमारा शिक्षा विभाग बचा हुआ था किन्तु सुनने में आया है कि इस रोग ने भी शिक्षा विभाग में पैर पसारने शुरू कर दिये हैं। आज अध्यापक भी विद्यार्थी को नकल करवाने के लिए उसे अच्छे अंक देने के लिए या फिर किसी प्रकाशक विशेष की पुस्तकें लगवाने के लिए पैसे लेने लगे हैं। शिक्षकों की भान्ति ही डॉक्टरी पेशा भी जनसेवा का पेशा था किन्तु जो डॉक्टर लाखों की रिश्वत देकर डॉक्टर बना है वह क्यों न एक ही साल में रिश्वत में दिये पैसों की वसूली न कर लेगा। इस तरह धीरे-धीरे यह रोग प्रत्येक विभाग में फैलने लगा है।
आज हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि इस समस्या का कोई समाधान नज़र नहीं आ रहा फिर भी हिम्मत करे. इन्सान तो क्या हो नहीं सकता के अनुरूप जनता यदि चाहे तो देश से भ्रष्टाचार को मिटाया नहीं जा सकेगा या कमसे-कम तो किया ही जा सकता है। पहला कदम जनता को यह उठाना चाहिए कि भ्रष्ट राजनीतिज्ञों को चुनाव के समय मुँह न लगाएं। भ्रष्ट अफ़सरों और कर्मचारियों की पोल खोलते हुए उन्हें किसी भी हालत में रिश्वत न दें, चाहे वे उसकी फाइलों पर कितनी देर तक बैठे रहें। कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना तो पड़ेगा ही। सरकार को चाहिए कि वह ऐसे कानून बनाए जिससे भ्रष्ट लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जा सके। हमारी न्याय व्यवस्था को चाहिए कि भ्रष्ट लोगों के मामले जल्द से जल्द निपटाये। यदि हमारा चुनाव आयोग कोई ऐसा कानून बना दे कि भ्रष्ट और दागी व्यक्ति मन्त्री पद या कोई अन्य महत्त्वपूर्ण पद न ग्रहण कर सके। इन सभी सुधारों के लिए हमारी युवा पीढ़ी को ही पहल करनी पड़ेगी। तब यह आशा की जा सकती है कि भ्रष्टाचार के भूत से हम छुटकारा पा सकें।
11. बढ़ते प्रदूषण की समस्या
सम्पूर्ण ब्रह्मांड में पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जहाँ अनेक प्रकार के प्राणी जीव-जन्तु और वनस्पति विद्यमान है। पृथ्वी का वातावरण नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइ-ऑक्साइड 0.3% तथा अन्य गैसीय तत्व 0.7% से मिल कर बना है। इन तत्त्वों की यह आनुपातिक मात्रा ही पृथ्वी के वातावरण को स्वच्छ रख कर उसे जीवधारियों के लिए अनुकूल बनाए रखती है। इस अनुपात के घटने-बढ़ने से ही वातावरण दूषित हो जाता है और इसी से प्रदूषण की समस्या जन्म लेती है।
आज भारत में प्रदूषण की समस्या बड़ा गम्भीर और भयंकर रूप धारण करती जा रही है। प्रदूषण की समस्या से जनता अनेक नई-नई बीमारियों का शिकार हो रही है। हमारे देश में प्रदूषण चार प्रकार का है-जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण तथा भूमि प्रदूषण। नगरों में शुद्ध पेयजल, शुद्ध वायु, शांत वायुमंडल तथा भूमि की उर्वरा शक्ति का ह्रास हो रहा है।
नगरों में भूमिगत जल-निकासी का प्रबन्ध होता है। किन्तु यह सारा जल सीवरेज़ के नालों के द्वारा पास की नदी में डाल दिया जाता है जिससे नदियों का पानी प्रदूषण युक्त हो गया है। गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए सरकार हज़ारों करोड़ खर्च कर रही है। फिर भी उसे प्रदूषण मुक्त करने में असफल रही है। देश की अन्य नदियों की हालत भी इसी तरह की है किन्तु उसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता। देश की बढ़ती जनसंख्या और शहरीकरण ने इस समस्या को और भी गम्भीर बना दिया है।
दूसरा प्रदूषण वायु प्रदूषण है। शुद्ध वायु जीवन के लिए अनिवार्य तत्व है। शुद्ध वायु हमें वृक्षों, वनों या पेड़-पौधों से मिलती है। क्योंकि वृक्ष कार्बन-डाइआक्साइड को लेकर हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। पीपल जैसे कई वृक्ष हैं जो हमें चौबीस घंटे ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। शहरीकरण और औद्योगीकरण के कारण हमने वृक्षों की बेहिसाब कटाई कर दी है। इससे वायु तो प्रदूषित हुई ही है साथ ही भूस्खलन की समस्या खड़ी हो गई है। उत्तराखंड प्रदेश में भूस्खलन की अनेक घटनाओं से अनेक गाँव उजड़ चुके हैं और असंख्य प्राणियों की जान गई है। वायु प्रदूषण का एक दूसरा कारण है कल कारखानों, ईंटों के भट्टों की चिमनियों से उठने वाला धुआँ। रही-सही कसर शहरों में चलने वाले वाहनों से उठने वाले धुएँ ने पूरी कर दी है। वायु प्रदूषण हृदय रोग एवं अस्थमा जैसी बीमारियों में वृद्धि कर रहा है।
जल और वायु प्रदूषण के अतिरिक्त शहरों में लोगों को एक और तरह के प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है। वह है ध्वनि प्रदूषण। ब्रह्म मुहूर्त में ही सभी धार्मिक स्थानों पर ऊँची आवाज़ में लाउडस्पीकर बजने शुरू हो जाते हैं। . दिन चढ़ते ही वाहनों का शोर ध्वनि को प्रदूषित करने लगता है। इस प्रदूषण से लोगों में बहरेपन, उच्च रक्त चाप, मानसिक तनाव, हृद्य रोग, अनिद्रा आदि बीमारियाँ पैदा होती हैं।
कहा जाता है कि शहरों की अपेक्षा गाँवों का वातावरण अधिक प्रदूषण मुक्त है किन्तु यह बात सच नहीं है। गाँवों के निकट बनी फैक्टरियों का प्रदूषण युक्त पानी जब खेतों में जाता है तो वह फसलों को नष्ट करने का कारण बनता है। इस पर हमारे किसान भाई अच्छी फसल प्राप्त करने के लालच में अधिकाधिक कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करते हैं जिससे जो सब्ज़ियाँ और फल पैदा होते हैं, वे प्रदूषण युक्त होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। आज के युग में नकली दूध, नकली घी, नकली खोया आदि ने हमारे स्वास्थ्य को पहले ही प्रभावित कर रखा है ऊपर से भूमि प्रदूषण ने हमारे स्वास्थ्य को और भी खराब कर रखा है।
यदि हमने बढ़ते प्रदूषण को रोकने का कोई उपाय न किया तो आने वाला समय अत्यन्त भयानक हो जाएगा। कल कारखानों एवं सीवरेज़ के गन्दे पानी को नदियों में डालने से रोकना होगा। नगरों में वाहनों से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए सी०जी० एन० जैसे प्रदूषण मुक्त पेट्रोल का प्रयोग अनिवार्य बना दिया जाना चाहिए। कृषि के क्षेत्र में कीटनाशक दवाइयों के अधिक प्रयोग पर रोक लगानी होगी।
12. युवा वर्ग में बढ़ता नशीले पदार्थों का सेवन
वर्तमान युग में देश और समाज के लिए जो समस्या चिंता का कारण बनी हुई है वह है युवा वर्ग का नशीली दवाइयों के चक्रव्यूह में उलझना। आज दिल्ली समेत सभी महानगर विशेषकर पंजाब प्रदेश में लाखों युवक नशीले पदार्थों के प्रयोग के कारण अपना भविष्य अंधकारमय बना रहे हैं। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले लड़के-लड़कियाँ समान रूप से इनका शिकार होते जा रहे हैं। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी ने एक जगह लिखा है कि जिस देश में करोड़ों लोग भूखों मरते हैं वहाँ शराब पीना, गरीबों का रक्त पीने के बराबर है। किंतु आज शराब ही नहीं अफीम, गांजा, चरस, समैक, हशीश, एल० एस० डी०, परॉक्सीवन, डेक्साड्रिन जैसे नशे, सारे समाज को दीमक की भांति भीतर ही भीतर खोखला करते जा रहे हैं।
मद्यपान के अनेक आदी और समर्थक बड़े गर्व के साथ शराब को सोमरस का नाम देते हैं। वे यह नहीं समझते कि सोमरस एक लता से प्राप्त किया गया स्वास्थ्यवर्धक टॉनिक था जिसे आर्य लोग स्वस्थ रहने के उद्देश्य से पिया करते थे। किंतु आजकल शराब को जिसे दारू या दवाई कहा जाता है बोतलों की बोतलें चढ़ाई जाती हैं। खुशी का मौका हो या गम का पीने वाले पीने का बहाना ढूँढ़ ही लेते हैं। कितने ही राज्यों की सरकारों ने शराब की ब्रिकी पर रोक लगाने का प्रयास किया किन्तु वे विफल रहीं। एक तो इस कारण से नकली शराब बनाने वालों की चाँदी हो गई दूसरे सरकार की हजारों करोड़ की आय बन्द हो गई। कुछ वर्ष पहले हरियाणा सरकार ने अपने राज्य में पूर्ण नशाबन्दी लागू कर दी। कितने ही होटल बंद हो गए किन्तु शराब की अवैध तस्करी और नकली शराब के धंधे ने सरकार को विवश कर दिया कि वह यह रोक हटा ले। पंजाब में भी सन् 1964 में जस्टिस टेक चन्द कमेटी ने पंजाब में नशाबन्दी लागू करने की सिफारिश की थी किन्तु फिर भी सरकार इसे लागू करने का साहस न कर सकी। कौन चाहेगा कि हज़ारों करोड़ों की आय से हाथ धोए जाएँ। जनता नशे की गुलाम होती है तो होती रहे राजनीतिज्ञों की बला से।
कुछ लोगों का मानना है कि शराब महँगी होने के कारण लोग दूसरे नशों की तरफ मुड़ रहे हैं। इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। क्या कोकीन कोई सस्ता नशा है। पर देखने में आया है कि हमारा युवा वर्ग इन नशों का गुलाम बनता जा रहा है। कुछ लोग पाकिस्तान की आई०एस०आई० को इस के लिए दोषी मानते हैं किन्तु जब हमारे नौजवान नशा लेने या करने को तैयार हों तो,बेचने वालों को तो अपना माल बेचना ही है।
हमारा युवा वर्ग इस बात को भूल जाता है कि नशा करने से किसी तरह की कोई राहत नहीं मिलती है। उल्टे नशा उनके स्वास्थ्य, चरित्र का नाश करता है। देश में चोरी, डकैती अथवा अन्य अपराधों की संख्या में वृद्धि इन्हीं नशाखोर युवाओं के कारण हो रही है। आज देखने में आ रहा है कि स्कूलों के छात्र भी नशा करने लगे हैं। उन्हें और कुछ नहीं मिलता तो कोरक्स जैसे सिरप पीकर ही नशे का अनुभव कर लेते हैं। नशे की लत का शिकार युवक- युवतियाँ अनैतिक कार्य करने को भी तैयार हो जाते हैं, जो समाज के लिए अत्यन्त घातक है। सबसे बढ़कर चिंता की बात यह है कि नशों की यह लत युवा वर्ग के साथ-साथ झुग्गी झोपड़ी में भी जा पहुँचो है।
हमारा युवा वर्ग इस बात को भूल रहा है नशाखोरी की यह आदत उनमें नपुंसकता ला देती है तथा टी० बी० और अन्य संक्रामक रोग लगने का भय बना रहता है। नशा करके वाहन चलाने पर दुर्घटना की आशंका अधिक बढ़ जाती है। सरकार ने भले ही अनेक नशा छुड़ाओ केन्द्र खोल रखे हैं। शराब की बिक्री सम्बन्धी विज्ञापनों पर रोक लगा दी है किन्तु शराब निर्माता सोडा की आड़ में अपने ब्रांड का प्रचार कर रहे हैं।
युवा वर्ग को नशाखोरी की आदत से मुक्ति दिलाने के लिए ठोस उपायों की ज़रूरत है नहीं तो आने वाली पीढ़ी नशेड़ी होने के साथ-साथ आलसी और निकम्मी भी होगी ऐसे में देश के भविष्य को उज्ज्वल देखने के सपने धूमिल हो जाएंगे। इस सम्बन्ध में समाज सेवी संस्थाओं और सरकार को मिलकर काम करना होगा।

13. साक्षरता अभियान
भारत जब स्वतंत्र हुआ तब देश का साक्षरता प्रतिशत 20% से भी कम था। देश में निरक्षरता एक तो गरीबी के कारण थी दूसरे अन्धविश्वासों के कारण। लड़कियों को शिक्षा न देना एक तरह का अन्धविश्वास ही था। कहा जाता था कि लड़कियों ने पढ़-लिख कर कौन-सी नौकरी करनी है। गरीब लोग एक तो गरीबी के कारण अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं, दूसरे आर्थिक कारणों से भी अपने बच्चों को शिक्षा से वंचित रखते थे। गरीबों का मानना था कि उनके बाल-बच्चे अब तो रोज़ी-रोटी के कमाने में उनका हाथ बटा रहे हैं, पढ़-लिख जाने पर वे किसी काम के नहीं रहेंगे।
देश की स्वतंत्रता के बाद हमारे नेताओं का ध्यान इस ओर गया कि देश को विकासशील देश से विकसित देश बनाना है तो देश की जनसंख्या को शिक्षित करना ज़रूरी है। इसके लिए सरकार ने सन् 1996 से प्रौढ़ शिक्षा, सर्वशिक्षा तथा साक्षरता का अभियान चलाया। सभी जानते और मानते हैं कि अशिक्षा अन्धविश्वासों और कुरीतियों को जन्म देती है और शोषण का शिकार लोग अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ सकते। अशिक्षा व्यक्ति को भले-बुरे की पहचान करने से वंचित रखती है।
हमारी सरकार ने शिक्षा के प्रसार को प्राथमिकता दी। बीसवीं शताब्दी के अन्त तक। मिडल हाई स्कूलों की संख्या दो लाख तथा कॉलेजों की संख्या दस हज़ार से भी ऊपर जा पहुँची है। स्त्री को पुरुष के बराबर ही अधिकार दिये गए और शिक्षा के दरवाज़े उस पर खोल दिये गए। यह इसी नीति का परिणाम है कि आज आप जिस किसी भी बोर्ड या विश्वविद्यालय के परिणामों को देखें तो लड़कियाँ आप को ऊपर ही नज़र आएँगी।
यह माना कि सरकार साक्षरता अभियान के लिए बहुत बड़ी धनराशि खर्च कर रही है परन्तु इसके वांछित परिणाम हमारे सामने नहीं आ रहे। 14 दिसंबर, सन् 2007 के समाचार के अनुसार पंजाब में यह अभियान धनाभाव के कारण दम तोड़ चुका है। एक तो साक्षरता अभियान के लिए आबंटित धनराशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़कर अधिकारियों की जेबों में जा रही है। दूसरे निम्नवर्ग की अरुचि भी इस अभियान की सफलता में बाधा बन रही है। तीसरे बढ़ती हुई जनसंख्या भी आड़े आ रही है। लगता है इस पूरे अभियान पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। इसकी दशा और दिशा का फिर से निर्धारण ज़रूरी है।
सर्वशिक्षा और साक्षरता अभियान में सफलता समाज और जनता के सहयोग के बिना नहीं मिल सकती। इसके लिए कुछ समाज सेवी संस्थाओं को कुछ प्रतिबद्ध, जागरूक नागरिकों की ज़रूरत है। व्यापारी वर्ग धन देकर सहायता कर सकता है तो अध्यापक और विद्यार्थी इस अभियान की सफलता को निश्चित बना सकते हैं। उनके पास समय भी है और योग्यता भी, शिक्षा दान से बढ़कर कोई दान नहीं है। सरकार को भी चाहिए कि साक्षरता अभियान में सक्रिय सहयोग देने वालों को किसी-न-किसी रूप में पुरस्कृत करें। इस अभियान में भाग लेने वालों को यदि कुछ आर्थिक लाभ प्राप्त होगा तो अधिक रुचि से इस अभियान में भाग लेंगे। इसे किसी प्रकार का बोझ नहीं समझेंगे। सरकार को चाहिए कि वह प्रत्येक अध्यापक पर अनिवार्यता न डंडा न लगाए बल्कि इस काम के लिए अपनी मर्जी से काम करने वालों को उत्साहित करे। वैसे चाहिए तो यह है कि हर पढ़ा-लिखा व्यक्ति कम-से-कम एक व्यक्ति को साक्षर अवश्य बनाए।
साक्षरता अभियान को रोजगार और बेहतर जीवन सुविधाओं से जोड़कर देखा जाना चाहिए। पाठ्य सामग्री, पुस्तकें आदि मुफ्त दी जानी चाहिएँ। मज़दूरों और किसानों को यह समझाना चाहिए कि अंगूठा लगाना पाप है। शिक्षा के अभाव में वे खेती के आधुनिक साधनों व तकनीकों को समझ नहीं पाएँगे। शिक्षित होकर किसान और मज़दूर सेठ साहूकारों के शोषण से भी बच जाएँगे और अन्धविश्वासों से भी छुटकारा पा सकेंगे।
सरकार को भी चाहिए कि इस अभियान के लिए खर्च किया जाने वाला पैसा अशिक्षितों तक ही पहुँचे न कि अधिकारियों की जेबों में चला जाए। साक्षरता अभियान एक राष्ट्रीय अभियान है। इस की सफलता के लिए हर पढ़ेलिखे व्यक्ति को सहयोग देना चाहिए। साक्षरता प्रतिशत में वृद्धि ही हमारे देश की उन्नति और विकास का एक मात्र कारण बन सकती है।
14. बाल मजदूरी की समस्या
बाल मज़दूरी हमारे देश में पिछली कई सदियों से चल रही है। हिमाचल प्रदेश में जब तक शिक्षा का प्रसार नहीं. हुआ था, रोज़गार के साधनों की कमी थी तब हिमाचल के बहुत से क्षेत्रों से छोटे-छोटे बालक शहरों में या कहीं मैदानी इलाकों में नौकरी के लिए जाया करते थे। तब उन्हें घरेलू नौकर या मुंडू कहा जाता था। इन घरेलू नौकरों को बहुत कम वेतन दिया जाता था। ईश्वर की कृपा से आज हिमाचल प्रदेश मुंडू संस्कृति से मुक्त हो चुका है। किन्तु आज भी बिहार, उत्तर-प्रदेश और बंगाल के अनेक लड़के-लड़कियाँ छोटे-बड़े शहरों में घरेलू नौकर के तौर पर काम कर रहे हैं। इनमें से कई तो यौन शोषण का भी शिकार हो रहे हैं।
घरेलू नौकरों के अतिरिक्त अनेक ढाबे वालों ने, हलवाइयों ने और किरयाना दुकानदारों के अतिरिक्त कालीन बनाने वाले कारखानों, माचिस और पटाखे बनाने वाले कारखानों और बीड़ी बनाने वाले कारखानों में छोटे-छोटे बालक मज़दूरी करते देखे जा सकते हैं। इन बाल मजदूरों को वेतन तो कम दिया ही जाता है, इनके स्वास्थ्य का भी ध्यान नहीं रखा जाता। बीमार होने पर इनका इलाज कराना तो एक तरफ उनका वेतन भी काट लिया जाता है। कई बार तो छुट्टी कर लेने पर उन्हें अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ता है। घर, दुकान या किसी कारखाने में छोटी-मोटी चोरी हो जाए तो सबसे पहला शक बाल मज़दूरों पर ही होता है। ऐसे कई मामलों में पुलिस द्वारा बच्चों के साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता है और उन्हें तरह-तरह से प्रताड़ित किया जाता है।
आप सुनकर हैरान होंगे कि बाल मजदूरी रोकने के लिए लगभग कईं वर्ष पहले कानून बनाया गया था। लेकिन उस कानून की किस तरह धज्जियाँ उड़ रही हैं यह इसी बात से अन्दाजा लगाया जा सकता है कि अकेले पंजाब प्रदेश में ही लगभग 80 हज़ार बाल मज़दूर हैं। हालांकि बालकों से मज़दूरी करवाने वालों के लिए 10 से 25 हजार रुपए का जुर्माना और तीन महीने की कैद का प्रावधान है किंतु प्रशासन की अनदेखी के कारण दिन-ब-दिन बाल मजदूरों की संख्या में वृद्धि हो रही है। सरकार द्वारा बाल मज़दूरी विरोधी बनाए गए कानून के अन्तर्गत कई कारखानों पर छापे मार कर सैंकड़ों बच्चों को इस भयावह जीवन से मुक्ति दिलाई गई है। सरकार ने इन छुड़ाए गए बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए कई रात्रि स्कूल भी खोले हैं किन्तु इनमें अधिकतर या फण्ड के अभाव में या बच्चों के अभाव में बन्द हो चुके हैं। सरकार ने इन बच्चों के लिए या उनके अभिभावकों के लिए कोई उचित रोज़गार के साधन नहीं जुटाए हैं इस कारण ये सारी योजनाएँ बीच रास्ते में ही दम तोड़ चुकी हैं।
दिसम्बर 2007 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र ने बाल मजदूरी के सम्बन्ध में एक सर्वे करके इसके कारणों को जानने का प्रयास किया था। सर्वे में दो कारण प्रमुख रूप से उभर कर सामने आए। पहला, बाल मज़दूर परिवार के पेट पालने के लिए मजबूर होकर मजदूरी करते हैं। वे और उनके माता-पिता चाहते हुए भी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। दूसरा, बड़ा कारण सरकार की या प्रशासनिक अधिकारियों की इस समस्या से निपटने के लिए दर्शायी जा रही उदासीनता है। साथ ही कारखानों के मालिकों की भी इस समस्या को दूर न करने में असहयोग भी शामिल है। इसमें मालिकों का अपना हित भी शामिल है क्योंकि बाल मज़दूर उन्हें सस्ते में मिल जाते हैं। दूसरे इन बाल मजूदरों के माँ-बाप भी परिवार की आय को देखते हुए उसे दूर करने में सहयोग नहीं दे रहें।
बाल मज़दूरी हमारे समाज के लिए एक नासूर है जिसका कोई उचित इलाज होना चाहिए। कुछ गैर-सरकारी समाज सेवी संगठनों में बचपन बचाओ’ का अभियान अवश्य छेड़ रखा है। इसी समस्या के कारण सरकार की अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की योजना भी सिरे नहीं चढ़ रही है। अबोध बच्चों का भविष्य अन्धकारमय बना हुआ है। आवश्यकता है कि सरकार और जनता मिलकर इस कलंक को धोने का प्रयास करें। नहीं तो आज के ये बच्चे कल के अपराधी, नशीले पदार्थों के तस्कर बन जाएँगे।
15. स्वतन्त्रता दिवस-15 अगस्त
15 अगस्त भारत के राष्ट्रीय त्योहारों में से एक है। इस दिन भारत को स्वतन्त्रता प्राप्त हुई थी। लगभग डेढ़ सौ वर्षों की अंग्रेजों की गुलामी से भारत मुक्त हुआ था। राष्ट्र के स्वतन्त्रता संग्राम में अनेक युवाओं ने बलिदान दिए थे। नेता जी सुभाष चन्द्र बोस का लाल किले पर तिरंगा फहराने का सपना इसी दिन सच हुआ था। अंग्रेज़ों से पहले भारत पर मुसलमानों का शासन रहा था। इसी कारण भारत को एक धर्म निरपेक्ष गणतन्त्र घोषित किया गया।
देश में स्वतन्त्रता दिवस सभी भारतवासी बिना किसी प्रकार के भेदभाव के अपने-अपने ढंग से प्रायः हर नगर, गाँव में तो मनाते ही हैं, विदेशों में रहने वाले भारतवासी भी इस दिन को बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर स्वतन्त्रता दिवस का मुख्य कार्यक्रम दिल्ली के लाल किले पर होता है। लाल किले के सामने का मैदान और सड़कें दर्शकों से खचाखच भरी होती हैं। 15 अगस्त की सुबह देश के प्रधानमन्त्री पहले राजघाट पर जाकर महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं फिर लाल किले के सामने पहुँच सेना के तीनों अंगों तथा अन्य बलों की परेड का निरीक्षण करते हैं।
उन्हें सलामी दी जाती है और फिर प्रधानमन्त्री लाल किले की प्राचीर पर जाकर तिरंगा फहराते हैं, राष्ट्रगान गाया जाता है और राष्ट्र ध्वज को 31 तोपों से सलामी दी जाती है। ध्वजारोहण के पश्चात् प्रधामन्त्री राष्ट्र को सम्बोधित करते हुए एक भाषण देते हैं। अपने इस भाषण में प्रधानमन्त्री देश के कष्टों, कठिनाइयों, विपदाओं की चर्चा कर उनसे राष्ट्र को मुक्त करवाने का संकल्प करते हैं। देश की भावी योजनाओं पर प्रकाश डालते हैं। अपने भाषण के अन्त में प्रधानमन्त्री तीन बार जयहिंद का घोष करते हैं। प्रधानमन्त्री के साथ एकत्रित जनसमूह जयहिंद का नारा लगाते हैं। अन्त में राष्ट्रीय गीत के साथ प्रातःकालीन समारोह समाप्त हो जाता है।
सायंकाल में सरकारी भवनों पर विशेषकर लाल किले में रोशनी की जाती है। प्रधानमन्त्री दिल्ली के प्रमुख नागरिकों, सभी राजनीतिक दलों के नेताओं, विभिन्न धर्मों के आचार्यों और विदेशी राजदूतों एवं कूटनीतिज्ञों को सरकारी भोज पर आमन्त्रित करते हैं।
मुख्यमन्त्री पुलिस गार्ड की सलामी लेते हैं। सरकारी भवनों, स्कूल और कॉलेजों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। प्रदेशों में इस दिन स्कूल एवं कॉलेज के छात्र-छात्राओं द्वारा अनेक प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाते हैं। कुछ प्रदेशों में इस दिन नगरों में जुलूस भी निकाले जाते हैं। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् इस दिन प्रत्येक नागरिक को अपने घर पर तिरंगा लहराने का अधिकार प्राप्त था, किंतु राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की रक्षा करना भी प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य समझा जाता था। अर्थात् घर पर या किसी भी भवन पर लहराया जाने वाला तिरंगा सूरज अस्त होने के साथ ही उतार लेना चाहिए। ऐसा न करना आज भी दण्डनीय अपराध माना जाता है।
15 अगस्त राष्ट्र की स्वतन्त्रता के लिए शहीद होने वाले वीरों को याद करने का दिन भी है। इस दिन शहीदों की समाधियों पर माल्यार्पण किया जाता है।
15 अगस्त अन्य कारणों से भी महत्त्वपूर्ण है। यह दिन पुडूचेरी के सन्त महर्षि अरविन्द का जन्मदिन है तथा स्वामी विवेकानन्द के गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस की पुण्यतिथि है। इस दिन हमें अपने राष्ट्र ध्वज को नमस्कार कर यह संकल्प दोहराना चाहिए कि हम अपने तन, मन, धन से अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा करेंगे।
16. गणतन्त्र दिवस-26 जनवरी
भारत के राष्ट्रीय पर्यों में 26 जनवरी को मनाया जाने वाला गणतन्त्र दिवस विशेष महत्त्व रखता है। हमारा देश 15. अगस्त, सन् 1947 को अनेक बलिदान देने के बाद, अनेक कष्ट सहने के बाद स्वतन्त्र हुआ था। किन्तु स्वतन्त्रता के पश्चात् भी हमारे देश में ब्रिटिश संविधान ही लागू था। अतः हमारे नेताओं ने देश को गणतन्त्र बनाने के लिए अपना संविधान बनाने का निर्णय किया। देश का अपना संविधान 26 जनवरी, सन् 1950 के दिन लागू किया गया। संविधान लागू करने की तिथि 26 जनवरी ही क्यों रखी गई इसकी भी एक पृष्ठभूमि है। 26 जनवरी, सन् 1930 को पं० जवाहर लाल नेहरू ने अपनी दृढ़ता एवं ओजस्विता का परिचय देते हुए पूर्ण स्वतन्त्रता के समर्थन में जुलूस निकाले, सभाएं की। अतः संविधान लागू करने की तिथि भी 26 जनवरी ही रखी गई।
26 नवम्बर, सन् 1949 के दिन लगभग तीन वर्षों के निरन्तर परिश्रम के बाद डॉ० बी० आर० अम्बेदकर, श्री के० एम० मुन्शी आदि गणमान्य महानुभावों ने संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया। 26 जनवरी को प्रातः 10 बजकर 11 मिनट पर मांगलिक शंख ध्वनि से भारत के गणराज्य बनने की घोषणा की गई। डॉ० राजेन्द्र प्रसाद को सर्वसम्मति से देश का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। राष्ट्रपति भवन जाने से पूर्व डॉ० राजेन्द्र प्रसाद ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। उस दिन संसार भर के देशों से भारत को गणराज्य बनने पर शुभकामनाओं के सन्देश प्राप्त हुए। जैसा समारोह उस दिन दिल्ली में प्रस्तुत किया गया था, वैसा ही दूसरे प्रान्तों की राजधानियों और प्रमुख नगरों ने भी वैसे ही यह दिन आनन्द और उल्लास के साथ मनाया। हमारे दादा जी बताते हैं कि 26 जनवरी, सन् 1950 को जो हमारे नगर में कार्यक्रम हुआ था वैसा कार्यक्रम आज तक नहीं हुआ है।
गणतन्त्र दिवस का मुख्य समारोह देश की राजधानी दिल्ली में मनाया जाता है। सबसे पहले देश के प्रधानमन्त्री इण्डिया गेट पर प्रज्जवलित अमर ज्योति जलाकर राष्ट्र की ओर से शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मुख्य समारोह विजय चौंक पर मनाया जाता है। यहाँ सड़क के दोनों ओर अपार जन समूह गणतन्त्र के कार्यक्रमों को देखने के लिए एकत्रित होते हैं। शुरू-शुरू में राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रपति की सवारी छ: घोड़ों की बग्गी पर चला करती थी। किन्तु सुरक्षात्मक कारणों से सन् 1999 से राष्ट्रपति गणतन्त्र दिवस समारोह में बग्धी में नहीं कार में पधारते हैं। परम्परानुसार किसी अन्य राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति अतिथि रूप में उनके साथ होते हैं। तीनों सेनाध्यक्ष राष्ट्रपति का स्वागत करते हैं। तत्पश्चात् राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री का अभिवादन स्वीकार आसन ग्रहण करते हैं।
इसके बाद शुरू होती है गणतन्त्र दिवस की परेड। सबसे पहले सैनिकों की टुकड़ियाँ होती हैं, उसके बाद घोड़ों, ऊँटों पर सवार सैन्य दस्तों की टुकड़ियाँ होती हैं। सैनिक परेड के पश्चात् युद्ध में प्रयुक्त होने वाले अस्त्र-शस्त्रों का प्रदर्शन होता है। इस प्रदर्शन से दर्शकों में सुरक्षा और आत्मविश्वास की भावना पैदा होती है। सैन्य प्रदर्शन के पश्चात् विविधता में एकता दर्शाने वाली विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक झांकियाँ एवं लोक नृतक मण्डलियाँ इस परेड में शामिल होती हैं।
सायंकाल को सरकारी भवनों पर रोशनी की जाती है तथा रंग-बिरंगी आतिशबाजी छोड़ी जाती है। इस प्रकार सभी तरह के आयोजन भारतीय गणतन्त्र की गरिमा और गौरव के अनुरूप ही होते हैं जिन्हें देखकर प्रत्येक भारतीय यह प्रार्थना करता है कि अमर रहे गणतन्त्र हमारा।
17. पंजाब
पौराणिक ग्रंथों में पंजाब का पुराना नाम ‘पंचनद’ मिलता है। उस समय इस क्षेत्र में सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और जेहलम नामक पाँच नदियाँ बहती थीं। इसी कारण इसे ‘पंचनद’ कहा जाता था। फ़ारसी में पंच का अर्थ है ‘पाँच’ और आब का अर्थ है ‘पानी”अर्थात् पाँच पानियों की धरती। पंचनद से पंजाब नाम मुसलमानी प्रभाव के कारण प्रसिद्ध हुआ।
स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पाँच ही नदियाँ बहा करती थीं, किन्तु देश के विभाजन के पश्चात् इसमें अब तीन ही नदियाँ-सतलुज, ब्यास और रावी ही रह गई हैं। 15 अगस्त, सन् 1947 के बाद भारतीय पंजाब को पूर्वी पंजाब की संज्ञा दी गई। किन्तु नवम्बर 1966 में पंजाब और भी छोटा हो गया। इसमें से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश निकाल कर अलग राज्य बना दिए गए। आज जो पंजाब है उसका क्षेत्रफल 50,362 वर्ग किलोमीटर है तथा 2001 की जनगणना के बाद इसकी जनसंख्या 2.42 करोड़ है।
इतिहास इस बात का साक्षी है कि सिकन्दर से मुहम्मद गौरी तक जब-जब भी भारत पर विदेशी आक्रमण हुए तबतब सदा आक्रमणकारियों ने सबसे पहले पंजाब की धरती को ही रौंदा। सिकन्दर महान् को राजा पोरस ने नाकों चने चबबाए तो मुहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने। यह दूसरी बात है कि उस युग में भारतीय राजाओं में एक-जुटता और राष्ट्रीयता की कमी थी जिस कारण देश पर मुसलमानी शासन स्थापित हुआ। किन्तु शूरवीरता तथा देशभक्ति पंजाबवासियों की रग-रग में भरी है। प्रथम तथा द्वितीय महायुद्ध के समय अनेक पंजाबियों ने अपनी वीरता का लोहा शत्रुओं को मानने पर विवश किया। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भी पाकिस्तान के साथ हुए 1948, 1965, 1971 और 1999 के कारगिल युद्ध में पंजाब के वीर सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुती देकर देश की रक्षा की है।
पंजाब के लोग बड़े परिश्रमी हैं। वे दुनिया में जिस भी देश में गए वहाँ अपने झंडे गाड़ दिए। पंजाब प्रदेश मुख्यत: कृषि प्रधान देश है। इसी कारण इसे भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। देश के अन्न भंडार के लिए सबसे अधिक अनाज पंजाब ही देता है। इसका कारण यहाँ की उपजाऊ भूमि, आधुनिक कृषि तकनीक, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार आदि है। किसानों के कठोर परिश्रम का भी इसमें भारी योगदान है। यहाँ की मुख्य उपज गेहूँ, चावल, कपास, गन्ना, मक्की, मूंगफली आदि हैं।
पंजाब ने औद्योगिक क्षेत्र में भी काफी उन्नति की है। यहाँ का लुधियाना अपने हौजरी के सामान के लिए, जालन्धर अपने खेलों के सामान के लिए तथा अमृतसर ऊनी व सूती कपड़े के उत्पादन के लिए विख्यात है। मण्डी गोबिन्दगढ़ इस्पात उद्योग का सबसे बड़ा केन्द्र है। नंगल और भटिण्डा में रासायनिक खाद बनाने के कारखाने हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश भर में कोई दस चीनी मिलें हैं।
पंजाब प्रदेश में अनेक कुटीर उद्योग भी विकसित हुए हैं। अमृतसर के खड्डी उद्योग की दरियाँ, चादरें विदेश में भी लोकप्रिय हैं। पटियाले की जूतियों और परांदों की माँग विदेशों में भी है।
पंजाब का प्रत्येक गाँव पक्की सड़क से जुड़ा है। हर गाँव तक बस सेवा है। लगभग प्रत्येक गाँव में डाकघर और चिकित्सालय है। शिक्षा के प्रसार के क्षेत्र में भी पंजाब प्रदेश केरल के बाद दूसरे नम्बर पर आता है। प्रदेश में छ: विश्वविद्यालय हैं जो क्रमश: चण्डीगढ़, पटियाला, अमृतसर, लुधियाना, फरीदकोट और जालन्धर में स्थित हैं। पंजाब की इस प्रगति के परिणामस्वरूप आज इस प्रदेश की प्रतिव्यक्ति वार्षिक औसत आय 20,000 से 30,000 रुपए के बीच है। गुरुओं, पीरों और वीरों की धरती पंजाब आज उन्नति के नए शिखरों को छू रही है।

18. कम्प्यूटर का आधुनिक जीवन में महत्त्व
कम्प्यूटर आधुनिक युग का नया आविष्कार ही नहीं एक अद्भुत करिश्मा भी है। कम्प्यूटर आज जीवन का एक अंग बन चुका है। स्कूल-कॉलेजों से लेकर हर सरकारी या ग़ैर-सरकारी कार्यालय, संस्थान, होटलों, रेलवे स्टेशनों, हवाई कम्पनियों में इसका प्रयोग होने लगा है। यहाँ तक कि अब तो कम्प्यूटर का प्रवेश आम घरों में भी हो गया है।
कम्प्यूटर निर्माण के सिद्धान्त का श्रेय इंग्लैण्ड के एक वैज्ञानिक चार्ल्स वैबेज को जाता है। इसी सिद्धान्त का उपयोग कर अमरीका के हावर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने 1937-1944 के मध्य एक प्रारम्भिक कम्प्यूटर का निर्माण किया था किन्तु यह एक भारी भरकम मशीन थी। इन्टिग्रेटेड सर्किट या एकीकृत परिपथ प्रणाली पर निर्मित पहला कम्प्यूटर सन् 1965 में आया। भारत में कम्प्यूटर के प्रयोग का आरम्भ 1961 से ही हो गया था किन्तु तब कम्प्यूटर विदेशों से मंगवाए जाते थे। अब ये भारत में ही बनने लगे हैं।
आज का व्यक्ति श्रम और समय की बचत चाहता है साथ ही काम में पूर्णता और शुद्धता अर्थात् ‘एक्युरेसी’ भी चाहता है। कम्प्यूटर मानव इच्छा का साकार रूप है। कम्प्यूटर का मस्तिष्क दैवी मस्तिष्क है। उससे गलती, भूल या अशुद्धि की सम्भावना ही नहीं हो सकती। देरी कम्प्यूटर के शब्दकोष में नहीं है। कम्प्यूटर का प्रयोग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लाभकारी सिद्ध हो रहा है। बैंकों में कम्प्यूटर के प्रयोग ने खाताधारियों और बैंक कर्मचारियों को अनेक सुविधाएँ प्रदान की हैं। सभी खातों का कम्प्यूटीकरण होने से अब बैंकों से राशि निकलवाना पहले से बहुत आसान हो गया है। ज़मीनों के रिकार्ड, जमाबन्दी आदि भी आजकल कम्प्यूटरीकरण किये जा रहे हैं। रेलवे तथा हवाई सेवा में आरक्षण की सुविधा भी कम्प्यूटर के कारण अधिक सरल और सुविधाजनक हो गई है।
कम्प्यूटर के प्रयोग का सबसे बड़ा लाभ शिक्षा विभाग और चुनाव आयोग को हुआ है शिक्षा विभाग कम्प्यूटर की सहायता से वार्षिक परिक्षाओं के परिणाम को शीघ्र अतिशीघ्र प्रकाशित करने में सक्षम हो सका है। कम्प्यूटर के प्रयोग से मतदान और मतगणना का काम भी आसान हो गया है। पुस्तकों के प्रकाशन का काम भी आसान हो गया है। पहले हाथ से एक-एक शब्द जोड़ा जाता था। अब कम्प्यूटर की सहायता से पूरी की पूरी पुस्तक घण्टों में कम्पोज़ होकर तैयार हो जाती है। आज जीवन का कोई भी क्षेत्र बचा नहीं है, जहाँ कम्प्यूटर का प्रयोग न होता हो। स्कूलों और कॉलेजों में भी इसी कारण कम्प्यूटर विज्ञान के नए विषय शुरू किये गए हैं और छोटी श्रेणियों से लेकर स्नातक स्तर पर विद्यार्थियों को कम्प्यूटर के प्रयोग का प्रशिक्षण दिया जाता है।
कम्प्यूटर की एक अन्य चमत्कारी सुविधा इंटरनैट के उपयोग की है। भारत में इंटरनेट का उपयोग बड़ी तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है। इंटरनेट पर हमें विविध विषयों की तो जानकारी प्राप्त होती ही है, हमें अपने मित्रों, रिश्तेदारों को ई-मेल, बधाई-पत्र आदि भेजने की भी सुविधा प्राप्त है।
प्रकृति का यह नियम है कि जो वस्तु मनुष्य के लिए लाभकारी होती है उसकी कई हानियाँ भी होती हैं। कम्प्यूटर जहाँ हमारे जीवन का ज़रूरी अंग भी बन गया है वहाँ उसकी कई हानियाँ भी हैं। इंटरनैट सम्बन्धी अपराधों में दिनोंदिन वृद्धि होना चिन्ता का कारण भी है। कुछ मनचले युवक या अपराधी प्रवृत्ति के लोग मनमाने ढंग से इंटरनेट का प्रयोग करते हुए दूसरे लोगों को अश्लील चित्र, सन्देश भेजते हैं। कुछ अपराधिक छवि वाले व्यक्ति बैंक खातों के लगाते हैं। कम्प्यूटर पर इंटरनैट का प्रयोग बच्चों को भी बिगाड़ रहा है। वैसे भी कम्प्यूटर पर अधिक देर तक काम करना नेत्र ज्योति को तो प्रभावित करता ही है शरीर में बहुत से रोग भी पैदा करता है। अतः हमें चाहिए कि कम्प्यूटर के गुणों को ध्यान में रखकर ही उसका प्रयोग करना चाहिए।
19. लोहड़ी
लोहड़ी मुख्यतः पंजाब और हरियाणा में मनाया जाने वाला त्योहार है। वैसे देश-विदेश में जहाँ भी पंजाबी बसे हैं, वे इस त्योहार को मनाते हैं। यह त्योहार पंजाब की संस्कृति, प्रेम और भाईचारे का त्योहार माना जाता है। __ लोहड़ी का त्योहार विक्रमी संवत् के पौष मास के अन्तिम दिन अर्थात् मकर संक्रान्ति से एक दिन पहले मनाया जाता है। अंग्रेज़ी महीनों के हिसाब से यह दिन प्रायः 13 जनवरी और कभी-कभी 14 जनवरी को ही पड़ा करता है। सभी जानते हैं कि इन दिनों सर्दी अपने पूरे यौवन पर होती है। लगता है सर्दी के इस प्रकोप से बचने के लिए इस दिन प्रत्येक घर में वैयक्तिक तौर पर और गली-मुहल्ले में सामूहिक स्तर पर आग जला कर उसकी आरती-पूजा करके रेवड़ी, फूलमखाने, मूंगफली की आहूतियाँ डालते हैं तथा लोक गीतों की धुनों पर नाचते-गाते हुए आग तापते हैं। इस त्योहार पर लोग एक-दूसरे को तिल-गुड़, रेवड़ी, मूंगफली, मकई के उबले दाने आदि गर्म माने जाने वाले पदार्थ बाँटते हैं, खाते हैं और खिलाते हैं।
इस त्योहार वाले दिन माता-पिता अपनी विवाहिता बेटियों के घर उपर्युक्त चीजें वस्त्र-भूषण सहित भेजते हैं। इसे लोहड़ी का त्योहार कहा जाता है। जिनके घर लड़के की शादी हुई हो या लड़का पैदा हुआ हो, वे लोग भी अपने-अपने घरों में नाते-रिश्तेदारों को घर बुलाकर मिलकर लोहड़ी का त्योहार मनाते हैं। . पुराने ज़माने में लड़के-लड़कियाँ समूह में घर-घर लोहड़ी माँगने जाते थे। वे आग जलाने के लिए उपले और लकड़ियाँ एकत्र करते थे। साथ ही वे ‘दे माई लोहड़ी-तेरी जीवे जोड़ी’, ‘गीगा जम्याँ परात गुड़ बण्डिया’ तथा ‘सुन्दरमुन्दरी-ए हो’ जैसे लोक गीत भी गाया करते थे। किन्तु युग और परिस्थितियाँ बदलने के साथ-साथ यह परम्परा प्रायः लुप्त ही हो गई है। आजकल सामूहिक लोहड़ी जलाने के लिए चन्दा इकट्ठा कर लिया जाता है। लोग लोहड़ी मनाने के लिए लोगों को अपने घरों में नहीं बल्कि होटलों आदि में बुलाने लगे हैं।
कुछ लोग लोहड़ी के त्योहार को फ़सल की कटाई के साथ भी जोड़ते हैं। इस मौसम में गन्ने की फ़सल काटकर गुड़-शक्कर तैयार किया जाता है। अब तक सरसों की फ़सल भी पककर तैयार हो चुकी होती है। मकई की फ़सल भी घरों में आ चुकी होती है। शायद यही कारण है कि लोहड़ी के अवसर पर पंजाब और हरियाणा के घरों में गन्ने के रस की खीर बनाई जाती है और सरसों का साग अवश्य बनाया जाता है। यह परम्परा अभी तक चली आ रही है। गुड़, रेवड़ी, मूंगफली खाने का अर्थ शरीर को सर्दी से बचाए रखना और हृष्ट-पुष्ट बनाए रखना भी है। लोहड़ी के दिन से कुछ दिन पूर्व ही लड़के-लड़कियों के समूह यह लोकगीत गाते नज़र आते हैं-
सुन्दर मुन्दरी-ए-हो, तेरा कौन बेचारा-हो
दुल्ला भट्टी वाला-हो,
दुल्ले धी व्याही-हो, सेर शक्कर पाई-हो ……
इस गीत से जुड़ी एक लोक कथा प्रचलित है। बहुत पहले की बात है, पंजाब के गंजीवार के इलाके में एक ब्राह्मण युवती सुन्दरी से नवाब का बेटा जबरदस्ती ब्याह करना चाहता था। इससे डर कर युवती और उसके पिता ‘पिंडी भट्टियां’ नामक स्थान के जंगल के रहने वाले दुल्ला भट्टी डाकू की शरण में जा पहुँचे। सुन्दरी को अपनी बेटी मान कर दुल्ले ने आग के अलाव के पास एक ब्राह्मण युवक से फेरे करवा कर उसका विवाह करवा दिया। दैव योग से उस रात दुल्ले के पास अपनी धर्म पुत्री को विदाई के समय देने को कुछ न था। थोड़े से तिल-गुड़ या शक्कर ही था वही उसने सुन्दरी के पल्ले बाँध पति के साथ विदा कर दिया। तभी से दुल्ला भट्टी के इस पुण्य कार्य के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए लोग उपर्युक्त लोक गीत गा कर लोहड़ी का त्योहार मनाते आ रहे हैं।
कारण चाहे जो भी रहा हो इतना निश्चित है कि लोहड़ी पंजाबी संस्कृति के साँझेपन का, प्रेम और भाईचारे का त्योहार है। यह त्योहार सर्दी की चरम अवस्था में मनाया जाता है (पोह-माघ दे पाले)। अतः इस त्योहार में जो कुछ भी खाया जाता है उसकी तासीर तो गर्म होती ही है वह स्वस्थ एवं युवा बने रहने में भी सहायक होता है। इस दृष्टि से हम इस त्योहार को मानवीय गरिमा बढ़ाने वाला त्योहार भी कह सकते हैं।
20. वसाखी
भारत में जितने प्रदेश एवं जातियाँ हैं, उनसे कई गुणा अधिक उनके भिन्न-भिन्न पर्व हैं। समय व्यतीत होने के साथ ही साथ कई पर्व जाति एवं प्रदेश सीमा से निकल कर ऐतिहासिक घटनाओं से ओत-प्रोत हो, अनेकता का जामा पहन लेते हैं और वे सम्पूर्ण मानव समाज के लिए एक से हो जाते हैं।
कहते हैं वैसाखी का पर्व पहले केवल उत्तर भारत में ही मनाया जाता था किन्तु सन् 1919 में जलियाँवाला बाग़ के नरसंहार की घटना के बाद यह त्योहार सम्पूर्ण भारत में मनाया जाने लगा। आज वैसाखी का त्योहार देश के सभी भागों में समान रूप से मनाया जाता है।
नवीन विक्रम वर्ष का प्रारम्भ भी वैसाखी के दिन से ही माना जाता है, इसी दिन कई जगहों पर साहूकार अपने नए खाते खोलते हैं और मनौतियाँ मनाते हैं। उत्तरी भारत में वैसाखी मास के पहले दिन से शीत ऋतु का प्रस्थान तथा ग्रीष्म ऋतु का आगमन माना जाता है। वैसाखी वाले दिन किसान आपनी गेहूँ की फ़सल की कटाई आरम्भ करते थे (परन्तु आजकल ऐसा नहीं होता) फ़सल पकने की खुशी में ‘जट्टा आई वैसाखी’ गाते हुए किसान लोक नृत्य भांगड़ा डालते थे। इस दिन किसानों की स्त्रियाँ भी पीछे न रहती थीं। वे एक स्थान पर एकत्र हो गिद्धा डालती थीं।।
वैसाखी का त्योहार केवल किसान ही नहीं मनाते हैं बल्कि समाज के दूसरे वर्ग भी इसे भरपूर उत्साह और उमंग के साथ मनाते हैं। अगर अच्छी फ़सल किसान को पर्याप्त खुशियाँ देती हैं तो मजदूरों की बेकारी दूर होने के साथसाथ दुकानदारों की भी चारों अँगुलियाँ घी में हो जाती हैं। हमारे देश की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या वैसाखी मास में होने वाली रबी की फ़सल पर आश्रित रहती है। इसी कारण वैसाखी, के इस पुण्य पर्व की प्रतीक्षा बड़ी बेकरारी से की जाती है।
वैसाखी का यह पर्व ही हमें सन् 1699 ई० की उस संगत की याद दिला देता है, जब आनन्दपुर साहब में गुरु गोबिन्द सिंह जी ने खालसा पंथ का सृजन किया था। वह यही तो कहा करते थे-“जब शान्ति एवं समझौते के तरीके असफल हो जाते हैं तब तलवार उठाने में नहीं झिझकना चाहिए।” इसी दिन तो उन्होंने पाँच प्यारों से स्वयं अमृत छका था। तभी तो कहा जाने लगा था-वाह-वाह गुरु गोबिन्द सिंह आपे गुरु-आपे चेला। इसी दिन गुरु गोबिन्द सिंह जी ने जातिभेद, रंग, लिंग आदि को दर-किनार कर अमृत छकाने की रसम चलाई थी। अमृत छकने के बाद न कोई छोटा रहता है, न बड़ा। इसी दिन गुरु गोबिन्द सिंह जी ने यह कहा था कि सवा लाख से एक लड़ाऊँ तभी गोबिन्द सिंह नाम कहाऊँ तथा उन्होंने अपने सभी शिष्यों को अपने नाम के साथ ‘सिंह’ लगाने का आदेश दिया था।
इन सब ऐतिहासिक तथ्यों को याद कर किस का हृदय रोमांचित न हो उठेगा। वैसाखी का पवित्र पर्व हमें अद्भुत शान्ति और स्फूर्ति प्रदान करता है। इसी कारण आज देश में ही नहीं विदेश में भी विशेषकर पंजाबियों द्वारा यह पर्व बड़ी धूम-धाम से मनाया जाता है।

21. रक्षा-बन्धन
त्योहार मनाने की प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है। त्योहार जाति के स्मृति चिह्न होते हैं। रक्षा बन्धन का त्योहार पुराने जमाने में ब्राह्मणों का त्योहार माना जाता था। इस दिन ब्राह्मण अपनी रक्षा के लिए क्षत्रियों की कलाई पर सूत्र बाँधकर उनसे अपनी रक्षा का वरदान माँगते थे। कालान्तर में जब क्षत्रिय लोग युद्ध भूमि में जाया करते थे, तब उनकी माताएँ, बहनें और पत्नियाँ उनके माथे पर अक्षत, कुमकुम का तिलक लगाकर उनकी विजय एवं मंगल कामना करते हुए रक्षा-सूत्र बाँधा करती थीं। यह त्योहार भाई-बहन का त्योहार कैसे बन गया। इसके विषय में इतिहास मौन है।
रक्षा-बन्धन का त्योहार प्रत्येक वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसी कारण कोई-कोई इसे श्रावणी पर्व के नाम से भी पुकारते हैं। इसी त्योहार वाले दिन से कार्तिक शुक्ला एकादशी तक चुतर्मास भी मनाया जाता है। ब्राह्मण और ऋषि-मुनि इस अवधि में अपने-अपने आश्रमों में लौट आया करते थे और उनके रहने-खाने का प्रबन्ध राज्य की ओर से किया जाता है। यज्ञ आदि का विधान होता था जिसकी पूर्ण आहुति श्रावणी के दिन होती थी। यज्ञ की समाप्ति पर राजा लोग आश्रम-अध्यक्ष की पूजा करते थे और उनके हाथों में पीले रंग का सूत्र बाँधते थे जिसका तात्पर्य यह होता था कि बँधवाने वाले व्यक्ति की रक्षा का भार उठवाना राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया है।
समय के परिवर्तन के साथ-साथ ब्राह्मणों के साथ स्त्री भी रक्षा बन्धन की अधिकारिणी हो गई। स्त्रियाँ प्राय: अपने भाइयों के ही रक्षा बन्धन करती थीं किन्तु अन्य व्यक्ति भी राखी बाँधे जाने पर अपने को उस स्त्री का भाई समझते थे। मध्यकालीन इतिहास में ऐसी ही एक घटना का उल्लेख मिलता है। चित्तौड़ की महारानी करमवती ने अपने को नितान्त असहाय मानकर मुग़ल सम्राट् हुमायूँ को राखी भिजवाकर अपने राज्य की रक्षा के लिए मौन निमन्त्रण दिया। राखी की पवित्रता और महत्त्व को समझने वाले हुमायूँ ने चित्तौड़ पर आक्रमण करने आए गुजरात के मुसलमान शासक पर आक्रमण करके उसके दाँत खट्टे किए थे और अपनी मुँहबोली बहन करमवती की तथा उसके राज्य की रक्षा की थी।
आधुनिक युग में इस प्रथा का इतना महत्त्व नहीं रह गया जितना पहले हुआ करता था। रक्षा-बन्धन का त्योहार आने पर बाज़ार रंग-बिरंगी राखियों से भर जाते हैं। राखी खरीदने वाली बहनों की बाजारों में भीड़ लगी रहती है। पुराने जमाने में बहन अपने भाई के लिए राखी स्वयं बनाया करती थी, लेकिन आज बाज़ार में महंगी से महंगी राखी खरीदने वालों की कमी नहीं है। देखा जाए तो आज यह त्योहार मात्र एक परम्परा का निर्वाह, एक औपचारिकता बनकर ही रह गया
है।
पुराने ज़माने में स्त्रियाँ इसी बहाने अपने मायके चली जाती थीं। वहाँ वह अपनी सहेलियों से मिलती, झूला झूलती तथा आमोद-प्रमोद में दिन बिताती। सम्भवतः बड़े बुजुर्गों ने श्रावण मास में सास और बहू के इक्ट्ठा रहने पर इसीलिए रोक लगा दी हो। किन्तु यह सब बातें बीते समय की बातें होकर रह गई हैं। आज कोई भी लड़की श्रावण मास में अपने मायके जाना पसन्द नहीं करती।
जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि आज के युग में अन्य त्योहारों की तरह यह त्योहार भी श्रद्धा रहित हो गया है। रक्षा बन्धन के अवसर पर भाई-बहन के प्रति रक्षा की प्रतिज्ञा कैसे कर सकता है जबकि उसकी बहन मन्त्री, जिलाधीश, मैजिस्ट्रेट, वकील और अध्यापक है। उसकी बहन आज अबला नहीं सबला है। फिर उसकी रक्षा का भार या रक्षा की प्रतिज्ञा का क्या महत्त्व रह जाता है। इस प्रकार इन त्योहारों की उपयोगिता के साथ-साथ जाति गौरव परम्परा आदि का भी ध्यान रखना चाहिए। त्योहार मनाने के पुराने ढंग में उचित सुधार कर उसमें परिस्थितियों और समयानुसार तबदीली कर लेनी चाहिए।
22. विजयदशमी (दशहरा)
त्योहार मनाने की प्रथा प्रत्येक सभ्य जाति में प्राचीन काल से चली आ रही है। भारतवर्ष में ऐसे त्योहारों की संख्या सैंकड़ों हैं किन्तु इनमें से चार-होली, रक्षा-बन्धन, दशहरा तथा दीपावली प्रमुख त्योहार माने जाते हैं। पुराने ज़माने में दशहरा केवल क्षत्रियों का त्योहार माना जाता था किन्तु आजकल सभी वर्गों के लोग मिलजुल कर इस त्योहार को मनाते हैं। इस त्योहार को मनाने के कारणों में भगवान राम की लंका विजय और रावण वध से हैं। कहा जाता है कि इस दिन धर्म की अधर्म पर और सत्य की असत्य पर विजय मानी जाती है। करोड़ों की संख्या में स्त्री-पुरुष प्रति वर्ष रामलीला देखते हैं किन्तु उनमें से कितने ऐसे लोग हैं जो इस दिन के महत्त्व को आत्मसात करने का प्रयत्न करते हैं। देश भर में करोड़ों रुपए इस उत्सव को मनाने पर खर्च कर दिए जाते हैं। हमारा विचार है कि दशहरे का त्योहार अत्यन्त सादगी से मनाया जाना चाहिए।
बंगाल में लोग इस त्योहार को दुर्गा-पूजा के त्योहार के रूप में मनाते हैं। पौराणिक गाथाओं के अनुसार महिषासुर नामक असुर के साथ देवी दुर्गा ने लगातार नौ दिन तक घमासान युद्ध किया था। दसवें दिन अर्थात् दशमी तिथि के दिन उस राक्षस का वध किया था। सो इस विजय को स्मरण करने के लिए बंगाल में माँ दुर्गा की उपासना की जाती है। बंगाली लोग काली देवी के उपासक हैं, इसलिए वे विजयदशमी के अवसर पर सैंकड़ों भैंसों या बकरों की बलि दिया करते थे। किन्तु आज के युग में बलि की यह प्रथा समाप्त कर दी गई है।
महाराष्ट्र में लोग शमी वृक्ष की पूजा करते हैं और इस वृक्ष के पत्तों को शुभ मानकर अपने सगे-सम्बन्धियों और परिचित मित्रों से आदान-प्रदान किया करते हैं। एक तरह से इस कहानी के पीछे भी विजय का उत्सव मनाने की बात ही प्रकट होती है। कुछ लोग विजयदशमी के त्योहार के साथ एक अन्य पौराणिक कथा भी जोड़ते हैं। किसी गुरुकुल में किसी गरीब छात्र द्वारा गुरु दक्षिणा माँगने के लिए ज़िद करने पर उसे कई लाख स्वर्ण मुद्राएँ भेंट करने का आदेश दिया। निर्धन छात्र घबराया नहीं। वह राजा के पास गया। राजा ने आए याचक को खाली हाथ लौटाना उचित न समझते हुए धन देवता कुबेर पर आक्रमण कर दिया। नौ दिन तक राजा की सेनाओं ने कुबेर को घेरे में रखा। दसवें दिन कुबेर ने रात के समय शमी के वृक्ष से स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा कर दी। दसवीं सुबह राजा ने उस निर्धन विद्यार्थी से सारी मुद्राएँ उठा ले जाने के लिए कहा। पर वह उतनी ही मुद्राएँ उठाकर ले गया जितनी उसने अपने गुरु को दक्षिणा में देनी थीं। इस तरह यह कहानी भी विजय का उत्सव मनाने की बात ही प्रकट करती है।
उपर्युक्त सभी उदाहरण इस तथ्य की ओर संकेत करते हैं कि विजयदशमी विजय का उत्सव है। मुख्य रूप से इसे रामकथा के साथ ही जोड़कर मनाया जाता है। पूरे दस दिनों तक छोटे-बड़े स्तर पर राम जीवन की सम्पूर्ण लीला प्रस्तुत की जाती है। दशहरे वाले दिन शहर के खुले मैदान में रावण, कुम्भकरण, मेघनाद के पुतले जलाए जाते हैं। रावण पर श्रीराम की विजय के साथ ही विजयदशमी का त्योहार सम्पन्न हो जाता है।
आजकल एक नई कुरीति देखने में आई है। रामलीला खेलने वाले अनेक पात्र नशा करके अभिनय करते हैं। कहना न होगा कि ऐसा करके प्रबन्धक या आयोजक कोई ऊँचा या पवित्र कार्य नहीं करते। देश के चरित्रवान एवं विद्वान् सुधारकों को ऐसी कुप्रथाओं के प्रचलन पर रोक लगाने के लिए उचित कदम उठाना चाहिए।
23. दीपावली.
यूँ तो प्रायः सभी देशों और जातियों के अपने त्योहार और पर्व होते हैं परन्तु भारतवर्ष त्योहारों का देश माना जाता है। भारतवर्ष में त्योहार उसके राष्ट्रीय जीवन में एक नया उल्लास और आशा लेकर आते हैं। दीपावली भी इन त्योहारों में एक है। दीपावली शब्द का अर्थ है-‘दीपकों की पंक्ति’। दीपावली के अवसर पर जलते हए दीपकों की सुन्दर पंक्तियाँ बड़ी आकर्षक प्रतीत होती हैं। दीपावली का यह त्योहार हमारे इतिहास, पुराण तथा कई प्रसिद्ध महापुरुषों के जीवन से जुड़ा है। कहते हैं कि इसी दिन भगवान् श्री राम चौदह वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापिस आए थे। अयोध्यावासियों ने उनका स्वागत घी के दिए जलाकर किया था। इसी दिन भक्त वत्सल नृसिंह भगवान् ने हिरण्यकश्यपु का वध कर अपने भक्त प्रह्लाद की रक्षा की थी। इसी दिन भगवान् श्रीकृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध करके उसके बंदीगृह से अनेक कन्याओं को मुक्त करवाया था। कहते हैं इसी दिन लक्ष्मी जी समुद्र-मंथन के समय समुद्र से प्रकट हुई थीं। इसी दिन सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद सिंह को औरंगजेब के कारागार से मुक्ति मिली थी। इसी दिन आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानन्द सरस्वती, जैनियों के चौबीसवें तीर्थंकर महावीर स्वामी तथा स्वामी रामतीर्थ बैकुण्ठ धाम सिधारे थे।
दीपावली का त्योहार किसानों के लिए भी सुख समृद्धि का संदेश लेकर आता है। उनकी खरीफ़ की फसल काटकर घर आ जाती है। वे प्रसन्न होकर गा उठते हैं-
‘होली लाई पूरी दीवाली लाई भात’
अर्थात् होली गेहूँ की फसल लेकर आती है और दीवाली धान की। दीवाली का त्योहार वर्षा ऋतु की समाप्ति पर शरद् ऋतु के आरम्भ होने पर विजयदशमी के बीस दिन बाद आता है। वर्षा ऋतु में उत्पन्न होने वाली गंदगी से मुक्त होने के लिए लोग अपने घरों की विशेष सफाई कर दरवाज़ों पर बंदनवार सजाते हैं। घरबार की नहीं बाज़ार, दुकानें, कारखाने और दूसरे सभी स्थानों पर सफाई की जाती है। बाजारों में चहल-पहल बढ़ जाती है। लोग शुभकामनाओं और उपहारों का आदान-प्रदान करते हैं। घरों को नए और रंग-बिरंगे चित्रों से सजाते हैं।
दीपावली का यह त्योहार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से शुक्ल द्वितीया तक बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। दीपावली से दो दिन पूर्व त्रयोदशी को धनतेरस कहा जाता है। इस दिन लोग बर्तन या गहने खरीदना शुभ समझते हैं। इससे अगला दिन नरक चौदस अथवा छोटी दीवाली के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि इन दिन भगवान् श्रीकृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। अमावस्या की रात्रि को दीवाली का मुख्य पर्व होता है। लोग धन की देवी लक्ष्मी के साथ-साथ अन्य देवी-देवताओं की पूजा भी करते हैं। दीपावली विशेषकर व्यापारियों का त्योहार माना जाता है। इस दिन वे दिन में लक्ष्मी पूजन करके नए बही खाते आरम्भ करते हैं और ईश्वर से अपने कल्याण, समृद्धि व शुभ लाभ की प्रार्थना करते हैं।
किसान लोग इस दिन नए अन्न के आने की खुशी मनाते हैं। पहले वे भगवान् को भोग लगाते हैं तब वे नए अन्न को प्रयोग में लाते हैं। महाराष्ट्र में इस नए अन्न से पहले कुछ कड़वी चीज़ खाई जाती है। गोवा में इस दिन चिउरी की मिठाई खाने का रिवाज है।
दीपावली के इस त्योहार पर जुआ खेलने की कुप्रथा भी प्रचलित है। जो एक अवांछनीय प्रवृत्ति है तथा यह अपराध जैसा ही है। दीपावली के अवसर पर पटाखे और आतिशबाजी पर करोड़ों रुपया नष्ट किए जाने की प्रथा भी कोई अच्छी प्रथा नहीं है। सन् 2007 की दीपावली में 40 करोड़ रुपए के पटाखे फोड़े गए थे। यही 40 करोड़ रुपए कम से कम 40 लाख भूखे लोगों को रोटी दे सकते थे। वर्तमान में यह अपव्यय एक सौ करोड़ से कहीं अधिक हो चुका है। दीपावली का यह पर्व नवरात्र पूजा से आरम्भ होकर भैय्या दूज के दिन समाप्त हो जाता है।
24. राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी
महात्मा गाँधी जी का पूरा नाम मोहनदास कर्मचंद गाँधी था। इनका जन्म 2 अक्तूबर, सन् 1869 को गुजरात प्रान्त के पोरबन्दर नामक स्थान पर हुआ। गाँधी जी के पिता कर्मचन्द किसी समय पोरबन्दर के दीवान थे, फिर बाद में राजकोट के दीवान रहे। सात वर्ष की अवस्था में इन्हें राजकोट की देहाती पाठशाला में दाखिल करवाया गया। सन् 1887 में आपने मैट्रिक परीक्षा पास की। सन् 1888 में आप बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए। बैरिस्ट्री पास करके लौटने पर आपने पोरबन्दर में ही वकालत शुरू की किन्तु सफलता न मिली। इसी दौरान उन्हें अफ्रीका एक मुकद्दमे के सिलसिले में जाना पड़ा। वहाँ उन्होंने भारतीयों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को देखा। गाँधी जी ने अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों को साथ लेकर आन्दोलन चलाया जिसमें उन्हें सफलता प्राप्त हुई और अफ्रीका में भारतीयों के सम्मान की रक्षा होने लगी।
भारतवर्ष लौटकर गाँधी जी ने देश की राजनीति में भाग लेना आरम्भ किया। सन् 1914 के प्रथम महायुद्ध में गाँधी जी ने अंग्रेज़ों की सहायता की। क्योंकि अंग्रेज़ों ने यह वचन दिया था कि युद्ध में विजयी होने पर भारत को स्वतन्त्र कर दिया जाएगा किन्तु बात इसके विपरीत हुई, अंग्रेजों ने युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद भारत को रौलट-एक्ट तथा पंजाब की रोमांचकारी जलियाँवाला बाग नरसंहार की घटना पुरस्कार के रूप में प्रदान की।
सन् 1920 में गाँधी जी ने असहयोग आन्दोलन आरम्भ किया परिणामस्वरूप उन्हें जेल में डाल दिया गया। सन् 1930 में गाँधी जी ने देशव्यापी नमक आन्दोलन का संचालन किया। सन् 1931 में गाँधी जी को लन्दन में गोलमेज कांफ्रेंस में भाग लेने के लिए आमन्त्रित किया गया। वहाँ गाँधी जी ने बड़ी विद्वता से भारत के पक्ष का समर्थन किया। सन् 1939 में अंग्रेज़ों ने भारतीयों की राय लिए बिना ही भारत को महायुद्ध में शामिल राष्ट्र घोषित कर दिया। किन्तु गाँधी जी ने इस महायुद्ध में अंग्रेज़ों की किसी किस्म की कोई सहायता करने से इन्कार कर दिया। सन् 1942 में गाँधी ने भारत छोड़ो आन्दोलन का संचालन किया। इसी अवधि में नेता जी सुभाष चन्द्र बोस तथा उनकी आज़ाद हिन्द सेना के बलिदान के फलस्वरूप देश की जनता में राजनीतिक जागृति पैदा हो गई। अंग्रेज़ी सरकार ने सन् 1942 के आन्दोलन में भाग लेने वाले सभी नेताओं को जेल में डाल दिया। इस बात ने आग में घी डालने का काम किया। भारतवासियों का जोश और क्रोध देखकर अंग्रेज़ों को भारत छोड़कर जाना ही पड़ा।
15 अगस्त, सन् 1947 को भारतवर्ष को स्वाधीन राष्ट्र घोषित कर दिया गया, किन्तु अंग्रेज़ जाता-जाता यह चालाकी कर गया कि उसने देश को दो टुकड़ों में बाँट दिया। देश के विभाजन के फलस्व रूप देश में साम्प्रदायिक दंगे भड़क उठे। महात्मा गाँधी ने इन साम्प्रदायिक दंगों को शान्त करने के लिए भरसक प्रयत्न किया। 30 जनवरी सन् 1948 की शाम 6 बजे जब गाँधी जी अपनी प्रार्थना सभा में जा रहे थे तब नत्थूराम गोडसे नामक एक व्यक्ति ने पिस्तौल की तीन गोलियाँ चलाकर गाँधी जी की हत्या कर दी। सारा देश शोकाकुल हो उठा। संसार के सभी देशों में राष्ट्रध्वज झुका दिए गए।
गाँधी जी भारतवर्ष के महान् नेता थे, स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने भारतीय जनता का नेतृत्व किया। उन्होंने समाज की अनेक कमियों को दूर करने का प्रयत्न किया। सत्य, अहिंसा और अछूतोद्धार के पवित्र नियमों का पालन स्वयं भी किया और दूसरों को भी इसका पालन करने की प्रेरणा दी। नि:संदेह भारतवर्ष गाँधी जी का ऋणी है और सदा ही ऋणी रहेगा।
25. पंजाब केसरी लाला लाजपत राय
पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी का जन्म 28 जनवरी, सन् 1865 ई० पंजाब के जिला फिरोज़पुर के गाँव दुडिके में हुआ। इन के पिता श्री राधाकृष्ण अग्रवाल विद्वान् एवं धार्मिक विचारों के व्यक्ति थे। लुधियाना के मिशन हाई स्कूल से सन् 1880 में मैट्रिक तथा लाहौर से एफ० ए० तथा मुख्तारी की परीक्षा पास की। इन्होंने हिसार में 6 वर्ष तक वकालत की। फिर सन् 1892 में लाहौर चले गए। वहाँ कई वर्षों तक बिना वेतन लिए डी० ए० वी० कॉलेज में अध्यापन कार्य किया। इन्होंने अपने गाँव ढुडिके में राधा कृष्ण हाई स्कूल खोला तथा पंजाब के अनेक नगरों में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की।
लाला जी का राजनीति में प्रवेश भी अनोखे ढंग से हुआ।
उन दिनों सर सैय्यद अहमद मुस्लिम समाज को भड़काने और बरगलाने के लिए और मुसलमानों को भारतीय राष्ट्रीयता से अलग करने के लिए अंधाधुंध लेख लिख रहे थे। लाला जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसके विरोध में आवाज़ उठाई और सर सैय्यद अहमद खाँ की पोल खोल दी। लाला जी के इस काम ने उन्हें भारतीय नेताओं की पंक्ति में ला खड़ा किया। सन् 1888 में इलाहाबाद में हुए काँग्रेस अधिवेशन में इनका जोरदार स्वागत हुआ और उनके जोश भरे भाषण सुनकर सभी प्रभावित हुए। सन् 1893 के कांग्रेस अधिवेशन में भी उन्होंने ओजपूर्ण भाषण दिए। लाला जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस की समस्त कार्रवाई अंग्रेज़ी से हिन्दुस्तानी भाषा में करवाई।
सन् 1902, सन् 1908 और सन् 1913 में तीन बार लाला जी कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल में शामिल होकर इंग्लैण्ड गये। इंग्लैण्ड में उन्होंने अनेक जनसभाओं में व्याख्यान दिये और अनेक लेख लिखकर वहाँ की जनता को भारत की वास्तविक दशा का ज्ञान करवाया। सन् 1914 में प्रथम महायुद्ध छिड़ने पर अंग्रेज़ी शासन ने लाला जी को भारत नहीं लौटने दिया। लाला जी इंग्लैण्ड से अमरीका चले गये। वहाँ उन्होंने ‘इंडियन होम रूल लीग’ की स्थापना की और ‘यंग इंडिया’ नामक साप्ताहिक पत्र भी निकाला। उन्होंने हिन्दुस्तान के विषय में बहुत-सी पुस्तकें भी लिखीं। अमरीका में रहते हुए लाला जी ने गदर पार्टी को संगठित किया और भारत को शस्त्रास्त्रों के जहाज़ भेजने की योजना बनाई जो सिरे न चढ़ सकी। इसके बाद लाला जी सैनिक सहायता प्राप्त करने के लिए जर्मनी और जापान भी गए। इन देशों की सरकारों ने हिन्दुस्तान की सहायता का भरोसा भी दिलाया। इस प्रकार लाला जी ने विदेशों में एक सच्चे राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत के हितों की रक्षा की।
देश में वापस आने पर सन् 1921 में लाला जी कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। सन् 1920 में गाँधी जी का असहयोग आन्दोलन शुरू हो चुका था। इस में लाला जी ने सक्रिय भूमिका निभाई। फलस्वरूप लाला जी को कई बार जेल जाना पड़ा। सन् 1926 में लाला जी ने मदनमोहन मालवीय जी के साथ मिलकर कांग्रेस नैशनलिस्ट पार्टी की स्थापना की और इस पार्टी की ओर से असैम्बली के सदस्य चुने गए।
सन् 1928 में अंग्रेज़ी शासन ने साइमन कमीशन का गठन किया। इस कमीशन के सदस्यों में कोई भी भारतीय शामिल न किया गया। देश भर में इस कमीशन का विरोध किया गया। 30 अक्टूबर को साइमन कमीशन लाहौर पहुँचा। लाला जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा जुलूस निकला। अंग्रेज़ जिलाधीश स्काट ने जुलूस पर लाठी चार्ज करने की आज्ञा दी। लाला जी की छाती पर कई लाठियाँ लगीं। लाला जी गम्भीर रूप से घायल हो गए। फलस्वरूप 17 नवम्बर, सन् 1928 को प्रात: सात बजे उन का निधन हो गया। मरने से पूर्व लाला जी ने कहा था-मेरे शरीर पर पड़ी एक-एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील साबित होगी।
आज लाला जी हमारे बीच नहीं हैं किंतु उनका बलिदान हमें सदा प्रेरणा देता रहेगा। उनकी याद को बनाये रखने के लिए पंजाब में अनेक शहरों में शिक्षण संस्थाएँ चलाई जा रही हैं तथा चण्डीगढ़ के सैक्टर 15 में लाला लाजपत राय भवन का निर्माण किया गया है।

26. शहीदे आजम सरदार भगत सिंह
भारत की आज़ादी के संग्राम में शहीद होने वालों में सरदार भगत सिंह का नाम भारत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा हुआ है। सरदार भगत सिंह का जन्म 28 सितम्बर, सन् 1907 को जिला लायलपुर (अब पाकिस्तान में) के गाँव बंगा, चक्क नं० 105 तहसील जंडावाला में हुआ था। उनके पूर्वज जालंधर जिले के (अब नवांशहर ज़िला) गाँव खटकड़ कलां से उधर गए थे। सरदार भगत सिंह को देशभक्ति और क्रांतिकारी भावना अपने परिवार से विरासत में मिली थी। उनके जन्म के समय उनके पिता सरदार किशन सिंह नेपाल से तथा चाचा अजीत सिंह मांडले की जेल से छूटकर आए थे। इसलिए उनकी माता विद्यावती उन्हें ‘भागांवाला’ के नाम से पुकारती थीं। सरदार भगत सिंह की आरम्भिक शिक्षा गाँव बंगा में ही हुई, फिर वे लाहौर के डी० ए० वी० स्कूल में दाखिल हुए। हाई स्कूल की परीक्षा पास करने के बाद सरदार भगत सिंह डी० ए० वी० कॉलेज में दाखिल हुए किंतु क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने के कारण पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। इसका एक कारण यह भी था कि उन दिनों महात्मा गाँधी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन चल रहा था।
सरदार भगत सिंह बचपन से ही तलवार और बंदूक से प्यार करते थे। लाहौर में पढ़ाई छोड़ने के बाद उन्होंने नौजवान भारत सभा का संगठन किया। इस सभा का मनोरथ देश के युवकों को उत्साहित कर स्वतंत्रता संग्राम के लिए तैयार करना था। सरकार भी इनकी गतिविधियों पर विशेष ध्यान रखने लगी। तब सरदार भगत सिंह कुछ दिनों तक दिल्ली में अर्जुन सिंह बनकर और कानपुर में बलवंत नाम से प्रताप नामक दैनिक समाचार-पत्र में काम करते रहे। कानपुर में ही इनकी मुलाकात गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे क्रांतिकारी से हुई।
सरदार भगत सिंह महात्मा गांधी की अहिंसावादी नीति को पसन्द नहीं करते थे। क्योंकि उनका विचार था कि अहिंसात्मक आंदोलन से देश को आजादी नहीं मिल पाएगी यदि मिली भी तो बड़ी देर बाद मिलेगी और सरदार भगत सिंह जैसे नवयुवकों का गर्म खून इतनी देर प्रतीक्षा नहीं कर सकता था। सन् 1928 में फिरोजशाह कोटला दिल्ली में इंकलाबी युवकों की गोष्ठी हुई और उन्होंने अपनी पार्टी का नाम समाजवादी प्रजातंत्र सेना रखा। इस पार्टी का आदर्श इंकलाब लाना और लोगों को इसके लिए तैयार करना था।
उन दिनों अंग्रेज़ी सरकार ने भारतवासियों की स्वतंत्रता के लिए उत्सुकता को देखकर एक कमीशन नियुक्त किया। इस कमीशन में किसी भी हिंदुस्तानी को नहीं लिया गया था। 30 अक्तूबर, सन् 1928 को साईमन कमीशन लाहौर पहुँचा। इसके विरोध में नौजवान भारत सभा के लाला लाजपतराय के नेतृत्त्व में एक बड़ा जुलूस निकाला, जिस पर लाहौर के जिलाधीश पी०साण्ड्रस की आज्ञा से लाठियाँ बरसाई गईं। इस लाठीचार्ज में लाला लाजपतराय गम्भीर रूप से घायल हो गए परिणामस्वरूप 17 नवम्बर, सन् 1928 को उनका निधन हो गया। सरदार भगत सिंह और उनके साथियों ने साण्ड्रस की हत्या करके लाला जी की मौत का बदला ले लिया। गिरफ्तारी से बचने के लिए आप भेष बदलकर रातोरात लाहौर से निकल कर बंगाल चले गए।
विदेशी सरकार की गलत नीतियों के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल, सन् 1929 को केन्द्रीय विधानसभा में एक धमाके वाला खाली बम गिराकर ‘इंकलाब जिंदाबाद’ का नारा लगाकर अपनी गिरफ्तारियाँ दीं। सरदार भगत सिंह जानते थे कि इस अपराध के लिए उन्हें फाँसी की सजा मिलेगी किंतु वे अपने बलिदान से सोई हुई जनता को जगाना चाहते थे। इसलिए भागने की अपेक्षा उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी। 17 अक्तूबर, सन् 1930 को सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फाँसी की सजा सुना दी गई। कहते हैं कि फाँसी की सज़ा सुनते ही सरदार भगत सिंह और उनके साथियों के चेहरों पर लाली छा गई। उन्होंने जमकर इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। भगत सिंह और उनके साथियों को 24 मार्च, सन् 1931 को फाँसी दी जानी थी किंतु कायर अंग्रेजी सरकार ने नियत दिन से एक दिन पहले ही अर्थात् 23 मार्च, सन् 1931 को सायंकाल के समय उनको फाँसी लगा दी। शहीदों के शव उनके सम्बन्धियों को देने की बजाए जेल की पिछली दीवार तोड़कर फिरोजपुर पहुँचाये गए, सतलुज के किनारे उनकी लाशों के टुकड़े-टुकड़े कर जला दिया गया, फिर दरिया में फेंक दिया। आज भी फिरोज़पुर के हुसैनीवाला स्थान पर उनका शहीद स्मारक विद्यमान है।
हमारी आज़ादी के इतिहास में सरदार भगत सिंह और उनके साथियों की कुर्बानी पर पंजाब को ही नहीं समस्त भारत को गौरव प्राप्त है। पंजाब सरकार ने उनकी माता विद्यावती को ‘पंजाब माता’ का सम्मान देकर अपना कर्तव्य निभाया है और सन् 2007 में सरकारी स्तर पर पंजाब के नगर-नगर में उनकी जन्मशताब्दी मनाकर शहीदे आज़म सरदार भगत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की।
27. श्री गुरु नानक देव जी .
सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी का जन्म सन् 1469 ई० में लाहौर के निकट स्थित राय भोए की तलवंडी नामक गाँव में हुआ। (यह स्थान अब पाकिस्तान में है तथा ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है।) इनकी माता का नाम तृप्ता देवी जी तथा पिता का नाम मेहता कालू जी था।
गुरु नानक देव जी बाल्यकाल में ही ध्यान मग्न होकर आत्म चिंतन में लीन रहते थे। बचपन में ही इनके हृदय में ईश्वर भक्ति की लग्न थी। साधु संतों की सेवा में इनकी विशेष प्रवृत्ति थी। एक दिन इनके पिता ने इनको कुछ रुपये देकर सौदा करने के लिए बाजार भेजा। उन्होंने वह रुपये भूखे साधु-सन्तों को भोजन कराने पर खर्च कर दिए। इस घटना को इतिहास में सच्चा सौदा कहते हैं। गुरु नानक देव जी का अन्तर्व्यक्तित्व किसी अपूर्व ज्योति से उद्भासित रहा करता था। उनका बाह्य व्यक्तित्व भी उतना ही प्रखर और अद्भुत था। सचमुच गुरु नानक देव जी का जीवन एक कर्मठ तथा क्रियाशील व्यक्ति का जीवन रहा है। गुरु नानक देव जी एक महान् व्यक्तित्व के स्वामी और क्रांतिदर्शी व्यक्ति थे। उनकी जीवनचर्या को ध्यान में रखते हुए हम उनके जीवन को चार विभिन्न युगों में बाँट सकते हैं यथा-
- चिंतन युग
- साक्षात्कार युग
- भ्रमण युग
- स्थापना युग।
तलवंडी का निवास चिंतन युग में आता है। यहाँ उन्होंने ध्यान मग्न होकर परमसत्य, सृष्टि सत्य, समाज सत्य और व्यक्ति सत्य का चिंतन किया। तलवंडी बाल गुरु की क्रीड़ा स्थली है। यहाँ उनके बालोचित किंतु अद्भुत कार्यों के दर्शन होते हैं। वे बालसुलभ लीला करते हैं, पाठशाला में पढ़ना आरम्भ करते हैं-आपको पंडित गोपाल के पास हिंदी, पंडित. ब्रजलाल के पास संस्कृत तथा मौलवी कुतबद्दीन के पास फ़ारसी पढ़ने के लिए भेजा जाता है तो आप अपने आध्यात्मिक ज्ञान से अपने शिक्षकों को हैरान कर देते हैं। सर्प की छाया, वृक्ष की छाया, खेतों का हरे-भरे होना, इत्यादि घटनाएँ यद्यपि श्रद्धा की दृष्टि से घटित हुई मानी जा सकती हैं, तो भी इनका लाक्षणिक मूल्य अवश्य है।
इसी युग में गुरु नानक देव जी का विवाह बटाला के वासी मूलचंद की पुत्री सुलक्षणी जी के साथ हुआ जिनसे इन्हें दो पुत्र रत्न प्राप्त हुए जिनके नाम श्रीचंद और लखमी दास थे।
20 वर्ष की आयु में गुरु नानक देव जी ज़िला कपूरथला में स्थित सुल्तानपुर लोधी में अपनी बहन नानकी जी के पास आ गए वहाँ उनके बहनोई ने इन्हें दौलत खां लोधी के यहाँ अन्न भण्डार में नौकरी दिलवा दी। यहीं गुरु जी के तोलने और तेरह के स्थान पर ‘तेरा-तेरा’ रटने की कथा भी विख्यात है। यहीं इनके बेईं नदी में प्रवेश करने, तीन दिन तक अदृश्य रहने की घटना घटी। लोगों ने समझा वे डूब गए। किंतु इनकी बहन नानकी ने कहा- “मेरा भाई डूबने वाला नहीं, वह तो दूसरों को तारने वाला है। वास्तव में गुरु नानक देव जी डूबे न थे बल्कि आत्म स्वरूप में लीन होकर ‘सचखंड’ में पहुँच गए थे। बेईं में प्रवेश के समय आपको परम ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ। यहीं इन्होंने ‘न कोअ हिंदू न कोअ मुसलमान’ की घोषणा की। जीवन के इस भाग में गुरु नानक देव जी ने जिन अद्भुत कार्यों का संपादन किया, उनमें लोगों को आध्यात्मिक, नैतिक संदेश देना प्रमुख है।
सन् 1500 से 1521 तक गुरु नानक देव जी ने चार यात्राएँ की जिनमें आपने अनेक देशों एवं प्रांतों में अपने मानवतावादी विचारों का प्रचार किया। वे हिंदुओं के लगभग सभी तीर्थस्थानों पर गए और वहाँ के पंडितों को रागात्मक भक्ति का उपदेश देकर उनका हृदय परिवर्तन किया। वे मुसलमानों के तीर्थ स्थानों मक्का, मदीना, बगदाद, बलख बुखारा आदि स्थानों पर भी गए।
जीवन के अंतिम भाग में सन् 1521 से 1539 ई० तक गुरु जी करतारपुर (पाकिस्तान) में ही रहे। यहीं आपने अनेक रचनाएं रचीं। जिनमें जपुजी साहिब, आसा दी वार, सिद्ध गोष्ठी तथा पट्टी आदि हैं। यहीं आप सन् 1539 ई० में गुरु गद्दी भाई लहना जी, जो गुरु अंगद देव जी के नाम से जाने जाते हैं, को सौंपकर ईश्वरी ज्योति में विलीन हो गए।
28. गुरु गोबिन्द सिंह जी
कहते हैं जब संसार में अत्याचार बढ़ता है तब उसे दूर करने और धर्म की पुनः स्थापना के लिए कोई न कोई महापुरुष जन्म लेता है। सत्रहवीं शताब्दी में भी औरंगजेब के अत्याचारों से जब सारी भारतीय जनता दुःखी थी, तब उसका उद्धार करने के लिए तथा हिन्दू धर्म की रक्षा करने के लिए गुरु गोबिन्द सिंह जी ने जन्म लिया। गुरु गोबिन्द सिंह जी सिखों के दशम गुरु और अन्तिम गुरु हैं। आपका जन्म 22 दिसम्बर, सन् 1666 ई० को नवम् गुरु, गुरु तेग बहादुर जी के घर पटना (बिहार प्रांत) में हुआ। आपकी माता का नाम गुजरी था। 6 वर्ष की अवस्था तक आप पटना में ही रहे फिर आप अपने पिता द्वारा बसाए नगर आनन्दपुर साहिब (ज़िला रोपड़) में आ गए।
उन दिनों मुग़ल शासकों के हिन्दुओं पर अत्याचार बढ़ रहे थे। कश्मीरी पंडित गुरु तेग़ बहादुर जी के पास आये और अपनी दुःख भरी फरियाद उनको सुनाई। गुरु जी ने कहा इस समय किसी महापुरुष के बलिदान की आवश्यकता है। उनकी बात सुनकर बालक गोबिन्द जी ने कहा कि पिता जी इस समय आपसे बढ़कर महापुरुष और कौन हो सकता है। यह सुनकर गुरु जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना बलिदान देने का निश्चय कर लिया और गोबिन्द राय जी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया।
पिता के बलिदान के साथ ही नौ वर्ष की अवस्था में ही बालक गोबिन्द राय गुरु गद्दी पर बैठे। गुरु गद्दी पर आसीन होते ही गोबिन्द राय जी ने अपनी शक्ति को बढ़ाना आरम्भ कर दिया। गुरु जी के बढ़ते प्रभाव को देखकर पहाड़ी राजाओं में ईर्ष्या बढ़ने लगी। इसी ईर्ष्या के फलस्वरूप गुरु जी को पांवटा से छः मील दूर भंगानी नामक स्थान पर कहलूर के राजा भीमचंद से युद्ध करना पड़ा। उस युद्ध में गुरु जी को पहली जीत प्राप्त हुई। आगे चलकर गुरु जी को जम्मू के सूबेदार तथा पहाड़ी राजाओं के बीच नादौन में होने वाले युद्ध में पहाड़ी राजाओं की ओर से युद्ध करना पड़ा। इस युद्ध में भी गुरु जी को विजय प्राप्त हुई और पहाड़ी राजाओं को गुरु जी की शक्ति का पता लग गया।
गुरु गोबिन्द सिंह जी के जीवन की सबसे महान् घटना है-खालसा पंथ सजाना। सन् 1699 को बैसाखी के दिन आनन्दपुर साहिब में खालसा को सजाया, अमृत छका और छकाया। इस अवसर पर गुरु जी ने अपना नाम भी गोबिन्द राय से गोबिन्द सिंह कर लिया और अपने सब शिष्यों को भी अपने नाम के साथ सिंह लगाने का आदेश दिया।
गुरु गोबिन्द सिंह जी ने अपनी शक्ति को बढ़ाना शुरू कर दिया। औरंगज़ेब ने गुरु जी की शक्ति समाप्त करने का निश्चय कर लिया। औरंगजेब के आदेश से लाहौर तथा सरहिंद के सूबेदारों ने गुरु जी पर आक्रमण कर दिया। उनका घेरा आनन्दपुर साहब पर कई महीने तक चलता रहा। आठ महीने के घेरे से तंग आकर दिसम्बर सन् 1704 की एक रात को परिवार सहित आनन्दपुर साहिब छोड़ दिया। किन्तु सरसा नदी पर पहुँचते ही मुग़ल सैनिकों ने अपने वचन के विरुद्ध उन पर आक्रमण कर दिया। इस अफरा-तफरी में गुरु जी अपने दो छोटे-छोटे साहिबजादों और अपनी माता गुजरी. जी से बिछुड़ गए। गुरु जी किसी तरह नदी पार कर चमकौर की गढ़ी में पहुँच गए। मुट्ठी भर सिखों ने मुग़लों का डटकर मुकाबला किया। इस युद्ध में गुरु जी के दोनों बड़े साहिबजादे अजीत सिंह और जुझार सिंह वीरतापूर्वक लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। उधर गुरु जी के दोनों छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह विश्वासघाती रसोइए गंग के कारण सरहिंद के नवाब वज़ीर खाँ द्वारा जिंदा ही दीवारों में चिनवा दिए गए। अपने चारों पुत्रों की कुर्बानी पर भी गुरु जी विचलित नहीं हुए। उन्होंने कहा-
इन पुत्रन के सीस पर वार दिए गए सुत चार।
चार गए तो क्या हुआ, जब जीवित कई हज़ार॥
“गुरु जी का कालान्तर में दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह के साथ बढ़ता प्रेम देखकर सरहिंद का नवाब उनका जानी दुश्मन बन गया था। उसने दो पठानों को गुरु जी की हत्या करने के लिए उनके पीछे लगा दिया। जब गुरु जी दक्षिण में नांदेड़ पहुँचे तो उन पठानों में से एक ने उनके पेट में छुरा घोंप दिया। इस जख्म के कारण गुरु गोबिन्द सिंह जी 7 अक्तूबर, सन् 1708 ई० को ज्योति-जोत समा गये। ज्योति-जोत समाने से पूर्व अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए अपने शिष्यों को यह आदेश दे गए-
आज्ञा भई अकाल की, तभी चलायो पंथ॥
सब सिखन को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रन्थ॥
29. परिश्रम सफलता की कुंजी है
मनुष्य अपनी बुद्धि और परिश्रम से जो चाहे प्राप्त कर सकता है। परिश्रम करना मनुष्य के अपने हाथ में होता है और सफलता भी उसी को मिलती है जो परिश्रम करता है। परिश्रम ही सफलता की वह कुंजी है जिससे समृद्धि, यश और महानता के खजाने खोले जा सकते हैं। यह परिश्रम की कसौटी पर कसा गया सत्य है। एक साधारण से साधारण किसान भी अपने परिश्रम के बल पर अच्छी फसल प्राप्त करता है। एक विद्यार्थी भी अपने परिश्रम के बलबूते पर परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करता है।
कहते हैं कि कुछ लोग पैदा होते ही महान् होते हैं, कुछ अपने परिश्रम से महान् बनते हैं। वास्तविक महानता वही कहलाती जो परिश्रम से प्राप्त की जाती है। महान् कवि कालिदास का उदाहरण हमारे सामने है। आरम्भ में वह इतना मूर्ख था कि जिस डाली पर बैठा था उसे ही काट रहा था। कुछ लोगों ने ईर्ष्यावश चालाकी से उसका विवाह प्रतिभा सम्पन्न और विदुषी राजकुमारी विद्योत्तमा से करवा दिया। विवाहोपरान्त जब राजकुमारी को कालिदास की मूर्खता का पता चला तो उसने उसे घर से निकाल दिया। इस पर कालिदास ने परिश्रम कर कुछ बनने की ठानी और इतिहास साक्षी है कि वही मूर्ख कालिदास अपने परिश्रम के बल पर संस्कृत का महान् कवि बना।
भारतीय इतिहास में भी देश के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री भी अपने परिश्रम के बल पर ही प्रधानमन्त्री के उच्च पद तक पहुँचे। इसी प्रकार हमारे पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर ए० पी० जे० अब्दुल कलाम का उदाहरण दिया जा सकता है जो देश के राष्ट्रपति पद पर अपने परिश्रम के बल से ही पहुँचे। ये दोनों महापुरुष अत्यन्त निर्धन परिवारों में जन्मे थे।
लोग प्रतिभा की बात करते हैं परन्तु परिश्रम के अभाव में प्रतिभा का भी कोई महत्त्व नहीं होता। प्रतिभावान व्यक्ति को भी परिश्रम और पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। किसी भी व्यक्ति की सफलता में 90% भाग उसके परिश्रम का होता है। परिश्रम ही प्रतिभा कहलाती है। परिश्रम रूपी कुंजी को लेकर मनुष्य उन रहस्यों का ताला खोल सकता है जिन में न जाने कितनी अमूल्य निधियाँ भरी पड़ी हैं।
कहते हैं मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता होता है। गृह नक्षत्र हमारे भाग्य विधाता नहीं होते। कर्मवीर व्यक्ति अपने भाग्य का स्वयं निर्माता होता है। वह अपना भाग्य निर्माण करने के लिए परिश्रम करता है। परिश्रम से मुँह मोड़ने वाला व्यक्ति कायर या आलसी कहलाता है। वह जीवन में असन्तोष, असफलता, निराशा और अपमान का भागी बनता है। जबकि परिश्रमी व्यक्ति सफलता की सीढ़ियाँ निरन्तर चढ़ता जाता है। किन्तु परिश्रम का रास्ता फूलों का नहीं काँटों भरा रास्ता होता है। इस रास्ते पर चलने के लिए दृढ़ संकल्प और पक्की लगन की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति परिश्रम को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेता है वही जीवन में सफलता भी प्राप्त करता है।
मानव जीवन ही संघर्ष का दूसरा नाम है। यह संघर्ष ही परिश्रम का दूसरा नाम है। कविवर पन्त जी ने चींटी का उदाहरण देकर मनुष्य को जीवन में संघर्षरत रहने की सलाह दी है। संघर्ष से ही जीवन में गति आती है। अपने परिश्रम से कमाए हुए धन में जो सुख और आनन्द प्राप्त होता है वह भीख में पाये धन में नहीं होता। जीवन में वास्तविक सुख और आनन्द व्यक्ति को अपने परिश्रम से ही प्राप्त होता है। परिश्रम करने वाले व्यक्ति के लिए कोई बात असंभव नहीं होती। फिर परिश्रम मनुष्य के अन्तः करण को शुद्ध और पवित्र भी तो करता है इसलिए परिश्रम को सफलता की कुंजी कहा जाता है। आज के विद्यार्थी को यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए।
30. जैसी संगति बैठिए तैसोई फल देत
अथवा
सठ सुधरहिं सत्संगति पाये
अथवा
सत्संगति
अंग्रेज़ी में एक कहावत है कि ‘A man is known by the company he keeps’ अर्थात् मनुष्य अपनी संगति से पहचाना जाता है। सत्संगति का अर्थ है ‘श्रेष्ठ पुरुषों की संगति’। मनुष्य जब अपने से अधिक बुद्धिमान, विद्वान्, गुणवान एवं योग्य व्यक्ति के सम्पर्क में आता है, तब उसमें स्वयं ही अच्छे गुणों का उदय होता है और उसके दुर्गुण नष्ट हो जाते हैं। सत्संगति से मनुष्य की कलुषित वासनाएँ, कुबुद्धि और मूर्खता दूर हो जाते हैं। जीवन में मनुष्य को सुख और शांति प्राप्त होती है। समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। नीच से नीच व्यक्ति भी सत्पुरुषों की संगति में रहने से सज्जन व्यक्तियों की श्रेणी में माना जाता है। कबीर जी ने ठीक ही लिखा है-
कबीरा संगति साधु की, हरै और की व्याधि।
ओछी संगति नीच की, आठों पहर उपाधि॥
मनुष्य अच्छा है या बुरा है इसकी पहचान हमें उसकी संगति से हो जाती है। कोयलों की दलाली में सदा मुँह ही काला होता है। संगति के कारण ही साधारण कीड़ा भी फूल के साथ देवताओं पर चढ़ाया जाता है। इसी कारण कबीर जी ने कहा है-
जैसी संगति बैठिए तैसोई फल देत।
मनुष्य बचपन से ही अपने चारों ओर के वातावरण से प्रभावित होता है। सर्वप्रथम वह अपने माता-पिता, बहनभाईयों की संगति में रहकर उनके गुण-दोषों को सीखता है। देखने में आया है कि जिन बच्चों के माँ-बाप गालियाँ निकालते हैं, बच्चे भी शीघ्र ही गालियाँ निकालनी सीख जाते हैं। बहुत से बच्चे सिगरेट, शराब आदि पीना अपने माँबाप से ही सीखते हैं। कुछ बुरी आदतें बच्चे अपने साथियों से सीखते हैं। सेबों की पेटी में एक सड़ा हुआ सेब सारे सेबों को ख़राब कर देता है। एक मछली सारे तालाब को गन्दा कर देती है। ठीक इसी प्रकार बुरी संगति भी व्यक्ति को बुरा बना देती है।
संगति के कारण ही वर्षा की एक बूंद केले के पेड़ में पड़ने पर कपूर, सीप के मुँह में पड़ने पर मोती और सर्प के मुख में पड़ने पर विष बन जाती है।
सीप गयो मोती भयो कदली भयों कपूर।
अहिमुख गयो तो विष भयो, संगत के फल सूर॥
नीतिशतक में लिखा है कि सत्संगति बुद्धि की जड़ता को दूर करती है, वाणी में सच्चाई लाती है, सम्मान तथा उन्नति दिलाती है और कीर्ति का चारों दिशाओं में विस्तार करती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है
सठ सुधरहिं सत्संगति पाई। पारसपरसि कुधातु सुहाई अर्थात् सत्संगति से दुष्ट आदमी उसी तरह सुधर जाता है जैसे-लोहा पारस के स्पर्श से सोना बन जाता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा है ‘बिनु सत्संग विवेक न होई।’ अर्थात् बिना सत्संगति के मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। सज्जन पुरुषों की संगति हमारे आचरण को भी प्रभावित करती है। हमारा चरित्र उच्च और निर्मल हो जाता है।
कुसंगति से हर किसी को बचना चाहिए। गंगा जब सागर में जा मिलती है तो अपनी पवित्रता और महत्ता खो देती है। केले और बेर के वृक्ष की. कुसंगति के बारे में ठीक ही कहा गया है-
मारी मरे कुसंग की केरा के ढिग बेर।
वह हाले वह अंगचिरे, विधिना संग निबेर॥
इसी तरह कुसंगति के कारण लोहे के संग अग्नि को भी पीटा जाता है। इसके विपरीत सत्संगति मनुष्य को सच्चरित्र और उच्च विचारों वाला बनाती है। चन्दन का वृक्ष अपने आस-पास के सभी वृक्षों को भी सुगन्धि युक्त बना देता है। गुरु गोबिन्द सिंह जी अपनी रचना बिचित्र नाटक में लिखते हैं-
जो साधुन सरणी परे तिनके कथन विचार।
देत जीभ जिमि राखि है, दुष्ट अरिष्ट संहार॥
गर्ग संहिता में लिखा है कि गंगा पाप का, चन्द्रमा ताप का तथा कल्पवृक्ष दीनता को दूर करते हैं किन्तु सत्संगति पाप, ताप और दीनता तीनों को तुरन्त नाश कर देती है। अतः कहना न होगा कि व्यक्ति को सदा साधुजनों की, सज्जनों की संगति ही करनी चाहिए।

31. तेते पाँव पसारिये जेती लम्बी सौर
जब किसी की आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया हो तब उसे सलाह देते हुए बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि तेते पाँव पसारिये जेती लम्बी सौर। अर्थात् व्यक्ति को अपनी सीमा और सामर्थ्य के अनुसार ही कार्य अथवा खर्च करना चाहिए। अपनी आमदन से बाहर खर्च करने वाला सदा दुःखी ही होता है। किन्तु आजकल हर कोई अपनी चादर से बाहर पैर पसारने की कोशिश कर रहा है। इसके पीछे लोगों में बढ़ती दिखावे की भावना है। मध्यम वर्ग इसका विशेष रूप से शिकार हो रहा है। वह अमीरों की नकल करना चाहता है। अमीर वह बन नहीं पाता और ग़रीब वह बनना नहीं चाहता और न ही कहलाना चाहता है। परिणामस्वरूप मध्यम वर्ग अपनी नाक रखने के चक्कर में अमीर और ग़रीब रूपी दो चक्की के पाटों में पिस रहा है।
इतिहास साक्षी है कि भारत में कोई जमाना था जब शासन की बागडोर मध्यम वर्ग के हाथ में ही थी। तब मध्यम वर्ग आत्मसंतोषी था। अपनी कमाई और मेहनत पर विश्वास करता था। किन्तु आज उसके संतोष का बाँध टूट गया है। तब एक कमाता था और दस खाते थे किन्तु आज दस के दस ही कमाते हैं। फिर भी गुजारा नहीं होता। इसका कारण यही है कि आज हमने अपनी चादर से बाहर पैर फैलाने शुरू कर दिये हैं।
अमीरों की नकल करते हुए आज मध्यम वर्ग ब्याह-शादी पर अधिक-से-अधिक खर्चा करना चाहता है। समाज में अपनी नाक रखने के लिए उसने आखा, ठाका, सगाई आदि अनेक नए-नए खर्चीले रिवाज गढ़ लिए हैं या अपना लिये हैं। आज विवाह पर खर्च होने वाला पैसा पहले से कई गुणा बढ़ गया है। आम आदमी भी आजकल ब्याह शादी होटल या मैरिज पैलेस में करता है। दलील यह दी जाती है कि इस तरह काम की ज़िम्मेदारी घट जाती है।
चादर से बाहर पैर फैलाने का एक रूप हम विवाहावसर पर दिये जाने वाले प्रीति भोज को देखते हैं। पुराने ज़माने में लड़की की शादी होने पर लड़की की तरफ से आने वाले मेहमान खाना नहीं खाया करते थे। मिलनी होने के बाद बेटी को आशीर्वाद देकर चले जाते थे। किन्तु आज लड़की की तरफ से आने वाले मेहमान बारात आने से पहले ही खाना खा लेते हैं। शगुन में वे सौ-ढेड़-सौ देते हैं और खाना खाते हैं पाँच-छ: सौ का। सारा बोझ लड़की वालों पर पड़ता है। इसी को कहते हैं चादर के बाहर पैर पसारना।
लोग भूल जाते हैं कि चादर से बाहर पैर पसारने की इस प्रवृत्ति से समाज में महँगाई, भ्रष्टाचार तथा दहेज जैसी कई समस्याएँ पैदा होती जा रही हैं। लोग विवाह में अधिक-से-अधिक खर्चा करने लगे हैं। इससे महँगाई तो बढ़ती ही है दहेज के लालची लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। दहेज के इसी लालच के कारण कई नवविवाहिताओं को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता है। आए दिन समाचार-पत्रों में दहेज के लोभियों द्वारा अपनी बहू को जलाने की घटनाएँ प्रकाशित होती रहती हैं। आप जानकर शायद हैरान होंगे कि बहू की जलाने की घटनाएँ मध्यवर्गीय परिवारों में ही होती हैं क्योंकि मध्यमवर्ग ने अपने पैर चादर से बाहर पसारने शुरू कर दिये हैं।
समाज में भ्रष्टाचार की समस्या का पैदा होने का कारण भी लोगों के चादर से बाहर पैर पसारने की प्रवृत्ति ही आम रही है। जब हमने अपने खर्चे बढ़ा लिए हैं तो उन्हें पूरा करने के लिए रिश्वत ही एकमात्र साधन बचता है जिसे लोग बेधड़क अपना रहे हैं।
यदि दिखावे की इस प्रवृत्ति पर रोक न लगाई गई ओर मध्यम वर्ग ने अपनी चादर से बाहर पैर पसारने की आदत नहीं छोड़ी तो वह दिन दूर नहीं जब मध्यम वर्ग, जिसे कभी समाज की रीढ़ समझा जाता था, एक दिन विलुप्त हो जाएगा। अभी भी उच्च मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग में यह वर्ग बँट गया है। उच्च मध्यम वर्ग वाले अमीर वर्ग में शामिल हो जाएंगे और निम्न मध्यम वर्ग के गरीब वर्ग में। अतः अच्छी तरह सोच-समझ कर अपनी ही चादर के अनुसार पैर पसारने की प्रवृत्ति को अपनाना होगा।
32. भारतीय समाज में नारी का स्थान
मनुस्मृति में लिखा है ‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता’ अर्थात् जहाँ नारी की पूजा होती है, वहाँ देवता निवास करते हैं। भारतीय समाज में सदियों तक मनु जी के इस कथन का पालन होता रहा। नारी को प्रत्येक क्षेत्र में पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त थी। इतिहास साक्षी है कि भारतीय समाज में नारी को अपना वर चुनने के लिए पूर्ण स्वतन्त्रता थी। स्वयंवर की प्रथा इसी तथ्य की ओर संकेत करती है। नारी को शिक्षा ग्रहण की भी पूरी छूट थी। भारतीय समाज में मैत्रेयी, गार्गी, गौतमी सरीखी अनेक विदुषी नारियाँ हुई हैं।
रामायण और महाभारत काल के आते-आते नारी की स्थिति में गिरावट आनी शुरू हुई। श्रीराम द्वारा सीता जी का बनवास तथा पाँचों पाण्डवों का जुए में द्रौपदी को हार जाना, इस गिरावट की शुरुआत थी। रही सही कसर महाभारत के युद्ध ने पूरी कर दी। इस युद्ध में हज़ारों स्त्रियाँ विधवा हो गईं जिन्हें विवश होकर अयोग्य और विधर्मियों से विवाह करना पड़ा।
मुसलमानी शासन में भारतीय समाज में पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, कन्यावध का प्रचलन शुरू हो गया। नारी की स्वतन्त्रता छीन ली गई। उसे घर की चार दीवारी में कैद कर दिया गया। कबीर जैसे समाज सुधारक ने भी ‘नारी की झांई परत अंधा होता भुजंग’ जैसे दोहे लिखें। आर्थिक दृष्टि से नारी पुरुष के अधीन होकर रह गई। हिन्दी साहित्य में रीतिकाल के आते-आते नारी को मात्र भोग विलास की सामग्री समझा जाने लगा।
अंग्रेज़ी शासन में झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से लोहा लेते हुए वीरता के वे जौहर दिखाये कि अंग्रेज़ों को दाँतों तले उंगली दबानी पड़ी। सन् 1857 के प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम में नारी शक्ति ने अपना लोहा मनवाया। अंग्रेज़ों को सती प्रथा पर कानूनी पाबंदी लगाने पर विवश कर दिया हालांकि कृष्णभक्त कवयित्री मीराबाई इसका श्री गणेश पहले ही कर चुकी थी। इसी युग में आर्यसमाज का उदय हुआ। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह के पक्ष में आन्दोलन चलाया। महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले ने स्त्री शिक्षा के लिए साहसिक कदम उठाए। आज तक नारी शिक्षा से वंचित रही थी अतः अपने अधिकारों के प्रति जागरूक न हो सकी। कवि के शब्दों में नारी की स्थिति कुछ ऐसी थी-
अबला जीवन हाय। तुम्हारी यही कहानी।
आँचल में है दूध और आंखों में पानी।
देश स्वतन्त्र होने से पूर्व भारतीय समाज में दहेज की प्रथा नारी के लिए एक अभिशाप बन चुकी थी। इस प्रथा के अन्तर्गत नारी का क्रय-विक्रय होने लगा। इसीलिए देश के विभिन्न प्रदेशों में कन्याओं को जन्म लेते ही मार दिया जाने लगा। विवाह के उपरान्त भी कई लड़कियाँ दहेज रूपी राक्षस की भेंट चढ़ गईं।
15 अगस्त, सन् 1947 को देश स्वतन्त्र हुआ। स्वामी दयानन्द सरस्वती का नारी शिक्षा का आन्दोलन रंग लाया। नारी शिक्षा का प्रसार हुआ। नारी में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता आई। उचित अवसर प्राप्त होने पर नारी ने समाज में अपनी प्रतिभा का अहसास दिलाया। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद नारी ने राजनीति, प्रशासन, अंतरिक्ष विज्ञान इत्यादि सभी क्षेत्रों में अपना लोहा मनवाया। इनमें कुछ उल्लेखनीय नाम हैं श्रीमती प्रतिभा पाटिल (भारत की राष्ट्रपति) श्रीमती इन्दिरा गाँधी, श्रीमती किरण बेदी, कु० कल्पना चावला, श्रीमती सुनीता विलियमस। तीस वर्षीय एम० बी० ए० छवि राजवत (सोढा गाँव की सरपंच)। इससे यह सिद्ध होता है कि अपने संवैधानिक अधिकार के प्रति महिलाएँ कितनी जागरूक हैं।
परन्तु खेद का विषय यह है कि महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का विधेयक संसद् में पिछले एक दशक से लटका हुआ है। विभिन्न राजनीतिक दलों के राजनीतिक स्वार्थ इसके पारित होने में बाधा बने हुए हैं। इक्कीसवीं सदी तक आते-आते नारी ने अभूतपूर्व उन्नति की है किन्तु अभी तक पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता नहीं बदली। नित्य बलात्कार, शोषण की घटनाएँ पढ़ने को मिलती हैं। ऐसी घटनाओं की रोकथाम की जानी चाहिए। नारी के बढ़ते कदमों को कोई रोक नहीं सकता।
33. मानवाधिकार
मानवाधिकार वह अधिकार है जो प्रत्येक मनुष्य का संवैधानिक अधिकार है। सभी मनुष्य जन्म से समान हैं, इसलिए नसल, लिंग, भाषा, राष्ट्रीयता के भेद भाव के बिना सभी इन अधिकारों के लिए समान रूप से अधिकृत हैं। मानवाधिकार विश्व के सभी मनुष्यों को समान रूप से प्राप्त करने का अधिकार है। इन अधिकारों का सम्बन्ध प्रत्येक व्यक्ति की स्वतन्त्रता, समानता के अधिकारों से है। ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के अस्तित्व, विकास और कल्याण के लिए ज़रूरी भी हैं।
उन्नीसवीं शताब्दी में स्वामी दयानन्द सरस्वती सरीखे कुछ समाज सुधारकों ने सती प्रथा को बन्द करने, लड़कियों के पैदा होते ही मारने को बन्द करने और स्त्रीशिक्षा के पक्ष में मानवाधिकारों के संरक्षण सम्बन्धी आन्दोलन चलाया। लोक मान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा पूर्ण स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा लगा कर इसी दिशा में उठाया गया कदम था। सन् 1927 में मद्रास अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों की दृढ़तापूर्वक मांग की और अधिकारों की घोषणा के आधार पर भारत के लिए एक स्वराज्य संविधान’ बनाने का निर्णय लिया। सन् 1931 के कराची अधिवेशन में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अधिकारों को स्वतन्त्र भारत के संविधान में सम्मिलित करने की पहली महत्त्वपूर्ण घोषणा हुई थी।
सन् 1916 और सन् 1939 में हुए दो विश्वयुद्धों की विभीषका झेल चुके विश्व के सभी देश तीसरे विश्वयुद्ध के संकट से बचने के उपाय सोचने लगे। इसी उद्देश्य से 24 अगस्त, 1945 ई० को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। इसमें सन् 1946 में एलोनोर रूजवेल्ट की अध्यक्षता में एक मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया जिसने जून, 1946 ई० में विश्वव्यापी मानवाधिकारों की घोषणा का एक प्रारूप तैयार किया जिसे उसी वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा 10 दिसम्बर को स्वीकार कर लिया गया। इसीलिए हर वर्ष 10 दिसम्बर को ‘मानवाधिकार दिवस’ के रूप में माना जाता है।
26 जनवरी, सन् 1950 से लागू भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में संयुक्त राष्ट्रसंघ की मानवाधिकार सम्बन्धी घोषणाओं को शामिल किया गया। इनके अन्तर्गत प्रत्येक नागरिक को मानवीय गरिमा से जीने का अधिकार दिया है। साथ ही, मौलिक अधिकारों के रूप में उसके इन्हीं मानवाधिकारों का संरक्षण प्रदान किया गया है।
भारतीय संविधान में छः मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। यथा : (1) समानता का अधिकार (2) स्वतन्त्रता का अधिकार (3) शोषण के विरुद्ध अधिकार (4) धर्म की स्वतन्त्रता का अधिकार (5) सांस्कृतिक
और शैक्षिक अधिकार तथा (6) संवैधानिक उपचार के अधिकार। ये सभी अधिकार न्यायोचित हैं। ये अधिकार व्यापक मानवीय मूल्यों पर आधारित हैं तथा सामाजिक एवं आर्थिक न्याय इनका लक्ष्य है। कहना न होगा कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा को भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों के माध्यम से लागू किया गया है।
मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए सन् 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। यह आयोग समाज के विभिन्न वर्गों के मानवाधिकारों का संरक्षण करता है किन्तु खेद का विषय है कि बड़े व्यापक स्तर पर पूरे विश्व में मानवाधिकारों का हनन किया जा रहा है। भारत में भी आयोग के सामने सैंकड़ों शिकायतें हर माह पेश की जाती हैं। वास्तव में स्वार्थपूर्ण भोगवादी दृष्टि के व्यापक प्रसार ने जीवन मूल्यों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। जब तक प्रत्येक मानव आपसी प्रेम, सहयोग और मैत्री का पालन नहीं करेगा व्यक्ति ही व्यक्ति का शत्रु बना रहेगा। हमें ईश्वर से यही प्रार्थना करनी चाहिए-
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःखभाग भवेत्।

34. सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा/मेरा भारत महान्
उर्दू के प्रसिद्ध कवि मुहम्मद इकबाल ने कभी लिखा था।
सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा
हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्तां हमारा।
सच है, हम भारतीय जननी और जन्मभूमि को स्वर्ग समान मानते हैं। भारत देश हमारी जन्मभूमि है अतः हमें यह जननी के समान प्यारा है। राजा दुष्यन्त और शकुन्तला के पुत्र भरत के नाम से विख्यात भारत देश पहले आर्यावर्त कहलाया करता था। मुस्लिम शासक के कारण इस देश को हिन्दोस्तां कहा जाने लगा।
हमारा यह भारत देश विविधाओं से भरा है फिर भी एक है जैसे अनेक फूलों से बनी एक माला। जहाँ अनेक जातियों, धर्मों, सम्प्रदाओं, भाषा-भाषियों के लोग रहते हैं। मेरे इस देश की खूबी यह है कि जो भी यहाँ आया यहीं का होकर रह कर रह गया। हूण आए, शक आए, पठान आए, मुग़ल आए सभी यहाँ के होकर रह गए। आज सभी अपने को भारतीय कहने में गौरव अनुभव करते हैं।
मेरे देश भारत की एक बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ छ: की छः ऋतुएँ क्रम से आती हैं। वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमन्त और शिशिर यहाँ बारी-बारी से अपनी छटा बिखेरती हैं। यहाँ की नदियों का जल पवित्र होने के साथ-साथ बारहों महीने बहता रहता है। यहाँ के पर्वत अनेक वनोषधियों के निर्माता हैं। कहते हैं कि इन्हीं पर्वतों में कहीं संजीवनी बूटी पायी जाती है जिसे रामायण युग में हनुमान जी लेकर लंका पहुँचे थे।
मेरा यह देश भारत संसार की प्राचीनतम सभ्यता वाला देश है। यहाँ स्थित तक्षशिला और नालन्दा विश्वविद्यालय में संसार भर से लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करने आया करते थे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला यह देश तीन ओर से समुद्र से घिरा है तो उत्तर दिशा में विशाल हिमालय इसका प्रहरी बना खड़ा है। धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक दृष्टि से यह देश महान् है।
भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ के 80% लोग गाँवों में बसते हैं। आधुनिक युग का किसान शिक्षित है। वह विज्ञान की सहायता से खेती के नए, नए उपकरणों का प्रयोग कर रहा है। भारतीय किसान की मेहनत का यह फल है कि हमारा देश खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया है। यही नहीं अपने उत्पाद की बहुत-सी वस्तुओं को निर्यात कर धन भी अर्जित कर रहा है। इसी कारण प्रसाद जी ने अपने नाटक ‘चन्द्रगुप्त’ में युनानी सुन्दरी कार्नेलिया के मुख से यह कहलाया है-
अरुण यह मधुमय देश हमारा।
जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा।
भारत देश अनेक महात्माओं, ऋषि-मुनियों, तपस्वियों, योद्धाओं, संतों की जन्मभूमि है। इसी देश में श्रीराम, श्रीकृष्ण, महात्मा बुद्ध, महावीर, गुरु नानक देव जी जैसे अवतारी पुरुषों का जन्म हुआ। इसी देश में वेदों, पुराणों की रचना हुई। इसी देश में रामायण और महाभारत जैसे चिरंजीवी ग्रन्थ रचे गए। इसी देश में महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, गुरु गोबिन्द सिंह जैसे वीर पुरुष पैदा हुए। इसी देश में स्वामी दयानन्द, विवेकानन्द और बालगंगाधर तिलक जैसे विचारक पैदा हुए। इसी देश में रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पाण्डे, चन्द्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह, लाला लाजपत राय जैसे देश पर मर मिटने वाले महापुरुष हुए। इसी देश में महात्मा गाँधी, पं० जवाहर लाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, जयप्रकाश नारायण जैसे नेता पैदा हुए।
आज. भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। सन् 2009 तक 15 बार लोक सभा के लिए चुनाव हो चुके हैं। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् हमारा देश प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति कर रहा है। उद्योग के क्षेत्र में भी वह किसी बडे देश से पीछे नहीं है। अन्तरिक्ष विज्ञान में यह बड़े-बड़े देशों से टक्कर ले रहा है। ईश्वर से प्रार्थना है कि हमारा यह देश दिन दुगुनी रात चौगुनी उन्नति करे और एक दिन विश्व की सबसे बड़ी ताकत बन जाए।
35. मनोविनोद के साधन
मनोरंजन मानव जीवन का अनिवार्य अंग है। केवल काम जीवन में नीरसता लाता है। कार्य के साथ-साथ यदि मनोरंजन के लिए भी अवसर रहे तो काम में और गति आ जाती है। मनुष्य प्रतिदिन आजीविका कमाने के लिए कई प्रकार के काम करते हैं। उन्हें बहुत श्रम करना पड़ता है। काम करते-करते उनका मस्तिष्क, मन, शरीर, अंग-अंग थक जाता है। उन्हें अनेक प्रकार की चिन्ताएं भी घेरे रहती हैं। एक ही काम में निरन्तर लगे रहने से जी उक्ता जाता है। अतः जी बहलाने तथा थकान मिटाने के लिए किसी-न-किसी साधन को ढूंढा जाता है। इसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए मनोरंजन के साधन बने हैं।
जब से मनुष्य ने इस पृथ्वी पर पदार्पण किया है तभी से वह किसी-न-किसी साधन द्वारा मनोरंजन का आश्रय लेता रहा है।
सदा मनोरंजन देता है, मन को शान्ति वितान।
कांटों के पथ पर ज्यों मिलती फूलों की मनहर छाया॥
प्राचीनकाल में मनोरंजन के अनेक साधन थे। पक्षियों को लड़ाना, भैंसे की लड़ाई, रथों की दौड़, धनुषबाण से निशाना लगाना, लाठी-तलवार का मुकाबला, दौड़, तैरना, वृक्ष पर चढ़ने का खेल, गुल्ली-डंडा, कबड्डी, गुड़िया का विवाह, रस्सी कूदना, रस्सा खिंचाई, चौपट, गाना-बजाना, नाचना, नाटक, प्रहसन, नौका-विहार, भाला चलाना, शिकार आदि। फिर शतरंज, गंजफा आदि खेलें आरम्भ हुईं। सभ्यता एवं संस्कृति विकास के साथ-साथ मनोरंजन के साधनों में परिवर्तन आता रहा है।
आधुनिक युग में मनोरंजन के अनेक नये साधन उपलब्ध हैं। आज मनुष्य अपनी रुचि एवं सामर्थ्य के अनुरूप मनोरंजन का आश्रय ले सकता है। विज्ञान ने हमारी मनोवृत्ति को बहुत बदल दिया है। आज के मनोरंजन के साधनों में मुख्य हैं-ताश, शतरंज, रेडियो, सर्कस, चित्रपट, नाटक, प्रदर्शनी, कॉर्निवल, रेस, गोल्फ, रग्बी, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, वालीबाल, बास्कटबाल, टेनिस, बेडमिन्टन, शिकार आदि। इनमें से कई साधनों से मनोरंजन के साथ-साथ पर्याप्त व्यायाम भी होता है।
वर्तमान समय में ताश, शतरंज, चित्रपट और रेडियो, संगीत सम्मेलन, कवि-सम्मेलन, मैच देखना, सर्कस देखना मनोरंजन के सर्वप्रिय साधन हैं। इनसे आबाल वृद्ध लाभ उठाते हैं। खाली समय में ही नहीं, अपितु कार्य के लिए आवश्यक समय को भी अनावश्यक बनाकर लोग इनमें रमे रहते हैं। बच्चे, युवक, बूढ़े जब देखो तब ताश खेलते दिखाई देंगे। शतरंज खेलने का भी कइयों को शौक है। चित्रपट तो मनोरंजन का विशेष सांधन बन गया है। मज़दूर चाहे थोड़ा कमाये, तो भी चित्रपट देखने अवश्य जाएंगे। युवक-युवतियों और विद्यार्थियों के लिए तो यह एक व्यसन बन गया है। कई लड़के पैसे चुराकर चित्रपट देखते हैं। माता-पिता बाल-बच्चों को लेकर चित्रपट देखने जाते हैं और अपनी चिन्ता तथा थकावट दूर करने का प्रयत्न करते हैं।
इस समय मनोरंजन के साधनों में रेडियो प्रमुख साधन है। इससे घर बैठे ही समाचार, संगीत, भाषण, चर्चा, लोकसभा या विधानसभा की समीक्षा, वाद-विवाद, नाटक, रूपक, प्रहसन आदि सुनकर लोग अपना मनोरंजन प्रतिदिन करते हैं। स्त्रियां घर का काम कर रही हैं साथ ही उन्होंने रेडियो चलाया हुआ है। बहुत-से लोग प्रतिदिन प्रहसन अवश्य सुनेंगे। कई विद्यार्थी कहते हैं कि एक ओर रेडियो से गाने सुनाई दे रहे हों तो पढ़ाई में हमारा मन खूब लगता है। कुछ तो यहां तक कहते हैं कि रेडियो चलाए बिना हम तो पढ़ नहीं सकते। टेलीविज़न और कम्प्यूटर तो निश्चय ही मनोरंजन का सर्वश्रेष्ठ साधन है। संगीत-सम्मेलनों और कवि-सम्मेलनों में भी बड़ा मनोरंजन होता है। नृत्य आदि भी होते हैं। सर्कस देखना भी मनोरंजन का अच्छा साधन है।
मनोरंजन के साधनों से मनुष्य के मन का बोझ हल्का होता है तथा मस्तिष्क और नसों का तनाव दूर होता है। इससे नवजीवन का संचार होता है। पाचन-क्रिया भी ठीक होती है। देह को रक्त संचार में सहायता मिलती है। कहते हैं कि सरस संगीत सुनकर गौएं प्रसन्न होकर अधिक दूध देती हैं। हरिण अपना आप भूल जाते हैं। बैजू बावरे का संगीत सुनकर . मृग जंगल से दौड़ आए थे।
परन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि अति सर्वत्र बुरी होती है। यदि विद्यार्थी अपना मुख्य अध्ययन कार्य भूलकर, दिनरात मनोरंजन में लगे रहें तो उससे हानि होगी। सारा दिन ताश खेलते रहने वाले लोग अपना व्यापार चौपट कर लेते हैं। इसलिए समयानुसार ही मनोरंजन व साधनों से लाभ उठाना चाहिए। मनोरंजन के साथ-साथ ज्ञानार्जन भी होना चाहिए। हमें ऐसे मनोरंजन का आश्रय लेना चाहिए जिससे हमारे ज्ञान में वृद्धि हो। सस्ता मनोरंजन बहुमूल्य समय को नष्ट करता है। कवि एवं कलाकारों को भी ऐसी कला कृतियां प्रस्तुत करनी चाहिएं जो मनोरंजन के साथ-साथ ज्ञानवर्द्धन में भी सहायता करें। राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त ने ठीक ही कहा है-
केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए,
उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए।
एक बात और विचारणीय है। कुछ लोग ताश आदि से जुआ खेलते हैं। आजकल यह बीमारी बहुत बढ़ती जा रही है। रेलगाड़ी में, तीर्थों पर, वृक्षों के नीचे, जंगल में, बैठक में, क्लबों में जुए के दाव चलते हैं। कई लोगों ने शराब पीना तथा दुराचार के गड्ढे में गिरना भी मनोरंजन का साधन बनाया हुआ है। विनाश और पतन की ओर ले जाने वाले ऐसे मनोरंजनों से अवश्य बचना चाहिए। मनोरंजन के साधन के चयन से हमारी रुचि, दृष्टिकोण एवं स्तर का पता चलता है। अतः हम मनोरंजन के ऐसे साधन को अपनाएं जो हमारे ज्ञान एवं चरित्र बल को विकसित करें।
36. वर्षा ऋतु
मानव जीवन के समान ही प्रकृति में भी परिवर्तन आता रहता है। जिस प्रकार जीवन में सुख-दुःख, आशा निराशा की विपरीत धाराएं बहती रहती हैं, उसी प्रकार प्रकृति भी कभी सुखद रूप को प्रकट करती है तो कभी दुःखद। सुख के बाद दुःख का प्रवेश कुछ अधिक कष्टकारी होता है। बसन्त ऋतु की मादकता के बाद ग्रीष्म का आगमन होता है। ग्रीष्म ऋतु में प्रकृति का दृश्य बदल जाता है। बसन्त ऋतु की सारी मधुरता न जाने कहां चली जाती है। फूल-मुरझा जाते हैं। बाग-बगीचों से उनकी बहारें रूठ जाती हैं। गर्म लुएं सबको व्याकुल कर देती हैं। ग्रीष्म ऋतु के भयंकर ताप के पश्चात् वर्षा का आगमन होता है। वर्षा ऋतु प्राणी जगत् में नये प्राणों का संचार करती है। बागों की रूठी बहारें लौट आती हैं। सर्वत्र हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है।
धानी चनर ओढ धरा की दलहिन जैसे मस्कराती है।
नई उमंगें, नई तरंगें, लेकर वर्षा ऋतु आती है।
वैसे तो आषाढ़ मास से वर्षा ऋतु का आरम्भ हो जाता है लेकिन इसके असली महीने सावन तथा भादों हैं। धरती का ‘शस्य श्यामलाम् सुफलाम्’ नाम सार्थक हो जाता है। इस ऋतु में किसानों की आशा-लता लहलहा उठती है। नईनई सब्जियां एवं फल बाज़ार में आ जाते हैं। लहलहाते धान के खेत हृदय को आनन्द प्रदान करते हैं। नदियों, सरोवरों एवं नालों के सूखे हृदय प्रसन्नता के जल से भर जाते हैं। वर्षा ऋतु में प्रकृति मोहक रूप धारण कर लेती है। इस ऋतु में मोर नाचते हैं । औषधियां-वनस्पतियां लहलहा उठती हैं। खेती हरी-भरी हो जाती है। किसान खुशी में झूमने लगते हैं। पशु-पक्षी आनन्द-मग्न हो उठते हैं। बच्चे किलकारियां मारते हुए इधर से उधर दौड़ते-भागते, खेलतेकूदते हैं। स्त्री-पुरुष हर्षित हो जाते हैं। वर्षा की पहली बूंदों का स्वागत होता है।
वर्षा प्राणी मात्र के लिये जीवन लाती है। जीवन का अर्थ पानी भी है। वर्षा होने पर नदी-नाले, तालाब, झीलें, कुएं पानी से भर जाते हैं। अधिक वर्षा होने पर चारों ओर जल ही जल दिखाई देता है। कई बार भयंकर बाढ़ आ जाती है, जिससे बड़ी हानि होती है। पुल टूट जाते हैं, खेती तबाह हो जाती है, सच है कि अति प्रत्येक वस्तु की बुरी होती है। वर्षा न होने को ‘अनावृष्टि’ कहते हैं, बहुत वर्षा होने को ‘अतिवृष्टि’ कहते हैं। दोनों ही हानिकारक हैं। जब वर्षा न होने से सूखा पड़ता है तब अकाल पड़ जाता है। वर्षा से अन्न, चारा, घास, फल आदि पैदा होते हैं जिससे मनुष्यों तथा पशुओं का जीवन-निर्वाह होता है। सभी भाषाओं के कवियों ने ‘बादल’ और ‘वर्षा’ पर बड़ी सुन्दर-सुन्दर कविताएं रची हैं, अनोखी कल्पनाएं की हैं। संस्कृत, हिन्दी आदि के कवियों ने सभी ऋतुओं के वर्णन किए हैं। ऋतु-वर्णन की पद्धति बड़ी लोकप्रिय हो रही है। महाकवि तुलसीदास ने वर्षा ऋतु का बड़ा सुहावना वर्णन किया है। वन में सीता हरण के बाद उन्हें ढूंढ़ते हुए भगवान् श्री रामचन्द्र जी लक्ष्मण जी के साथ ऋष्यमूक पर्वत पर ठहरते हैं। वहां लक्ष्मण से कहते है
वर्षा काल मेघ नभ छाये देखो लागत परम सुहाये।
दामिनी दमक रही धन माहीं। खल की प्रीति जथा थिर नाहीं॥
कवि लोग वर्णन करते हैं कि वर्षा ऋतु में वियोगियों की विरह-वेदना बढ़ जाती है। अर्थात् बादल जीवन (पानी) देने आए थे किन्तु वे वियोगिनी का जीवन (प्राण) लेने लगे हैं। मीरा का हृदय भी पुकार उठता है-
सावण आवण कह गया रे।
हरि आवण की आस
रैण अंधेरी बिजरी चमकै,
तारा गिणत निरास।
कहते हैं कि प्राचीन काल में एक बार बारह वर्ष तक वर्षा नहीं हुई थी। त्राहि-त्राहि मच गई थी। जगह-जगह प्यास के मारे मुर्दा शरीर पड़े थे। लोगों ने कहा कि यदि नरबली दी जाए तो इन्द्र देवता प्रसन्न हो सकते हैं, पर कोई भी जान देने के लिए तैयार न हुआ। तब दस-बारह साल का बालक शतमन्य अपनी बलि देने के लिए तैयार हो गया। बलि वेदी पर उसने सिर रखा, बधिक उसका सिर काटने के लिए तैयार था। इतने में बादल उमड़ आए और वर्षा की झड़ी लग गई। बिना बलि दिए ही संसार तृप्त हो गया।
वर्षा में जुगनू चमकते हैं। वीर बहूटियां हरी-हरी घास पर लहू की बूंदों की तरह दिखाई देती हैं। वर्षा कई प्रकार की होती है-रिमझिम, मूसलाधार, रुक-रुककर होने वाली, लगातार होने वाली। आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन-इन चार महीनों में साधु-संन्यासी यात्रा नहीं करते। एक स्थान पर टिक कर सत्संग आदि करके चौमासा बिताते हैं। श्रावण की पूर्णमासी को मनाया जाने वाला रक्षाबन्धन वर्षा ऋतु का प्रसिद्ध त्योहार है।
वर्षा में कीट-पतंग मच्छर बहुत बढ़ जाते हैं। सांप आदि जीव बिलों से बाहर निकल आते हैं। वर्षा होते हुए कई दिन हो जाएं तो लोग तंग आ जाते हैं। रास्ते रुक जाते हैं। गाड़ियां बन्द हो जाती हैं। वर्षा की अधिकता कभी-कभी बाढ़ का रूप धारण कर जन-जीवन के लिए अभिशाप बन जाती है। निर्धन व्यक्ति का जीवन तो दुःख की दृश्यावली बन जाता है।
इन दोषों के होते हुए भी वर्षा का अपना महत्त्व है। यदि वर्षा न होती तो इस संसार में कुछ भी न होता। न आकाश में इन्द्रधनुष की शोभा दिखाई देती और न प्रकृति का ही मधुर संगीत सुनाई देता। यह पृथ्वी की प्यास बुझाकर उसे तृप्त करती है। प्रसाद जी ने बादलों का आह्वान करते हुए कहा है-
शीघ्र आ जाओ जलद, स्वागत तुम्हारा हम करें।
ग्रीष्म से संतप्त मन के, ताप को कुछ कम करें।

37. परोपकार
औरों को हँसते देखो मनु,
हँसी और सुख पाओ।
अपनी सुख को विस्तृत कर लो,
सबको सुखी बनाओ।
आदिकाल से ही मानव-जीवन में दो प्रकार की प्रवृत्तियां काम करती रही हैं। कुछ लोग स्वार्थ-भावना से प्रेरित होकर अपना ही हित-साधन करते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरों के हित में ही अपना जीवन लक्ष्य स्वीकार करते हैं। परोपकार की भावना दूसरों के लिये अपना सब कुछ त्यागने के लिए प्रोत्साहित करती है। यदि संसार में स्वार्थभावना ही प्रबल हो जाए तो जीवन की गति के आगे विराम लग जाए। समाज सद्गुणों से शून्य हो जाए। धर्म, सदाचार और सहानुभूति का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। परोपकार जीवन का मूलमन्त्र तथा भावना विश्व की प्रगति का आधार है, समाज की गति है और जीवन का संगीत परोपकार से पुण्य होता है और परपीड़न से पाप। गोस्वामी तुलसीदास ने इस भावना को इस प्रकार व्यक्त किया है-
परहित सरिस धर्म नहिं भाई। परपीड़ा सम नहिं अधमाई।
दूसरों की नि:स्वार्थ भाव से सेवा करने से बड़ा कार्य दूसरा नहीं हो सकता। अपने लिए तो पशु-पक्षी और कीड़ेमकौड़े भी जी लेते हैं। यदि मनुष्य ने भी यह किया तो क्या किया? अपने लिए हंसना और रोना तो सामान्य बात है जो दूसरे के दुःख को देखकर रोता है उसी की आंखों से गिरने वाले आंसू मोती के समान हैं। गुप्त जी ने कहा भी है-
गौरव क्या है, जनभार सहन करना ही।
सुख क्या है, बढ़कर दुःख सहन करना ही॥
परहित का प्रत्यक्ष दर्शन करना हो तो प्रकृति पर दृष्टिपात कीजिए। फूल विकसित होकर संसार को सुगन्धि प्रदान करता है। वृक्ष स्वयं अग्नि वर्षा पीकर पथिक को छाया प्रदान करते हैं। पर्वतों से करुणा के झरने और सरिताएं प्रवाहित होती हैं जो संतप्त धरा को शीतलता और हरियाली प्रदान करती हैं। धरती जब कष्टों को सहन करके भी हमारा पालनपोषण करती है। सूर्य स्वयं तपकर संसार को नव-जीवन प्रदान करता है। संध्या दिन-भर की थकान का हरण कर लेती है। चांद अपनी चांदनी का खजाना लुटाकर प्राणी-जगत् को निद्रा के मधुर लोक में ले जाकर सारे शोक-संताप को भुला देता है। प्रकृति का पल-पल, कण-कण परोपकार में लीन है। यह व्यक्ति को भी अपने समान परहित के लिए प्रेरित करती है-
वृक्ष कबहुं नहिं फल भखै, नदी संचै नीर।
परमारथ के कारने, साधन धरा शरीर॥
स्वार्थ में लिप्त रहना पशुता का प्रतीक नहीं तो क्या है
यही पशु प्रवृत्ति है कि आप आप ही चरे।
वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे॥
परोपकार सर्वोच्च धर्म है जो इस धर्म का पालन करता है, वह वन्दनीय बन जाता है। इसी धर्म के निर्वाह के लिए राम वन-वन भटके, ईसा सलीब पर चढ़े, सुकरात को विष-पान करना पड़ा। गांधी जी को गोलियों की बौछार सहन करनी पड़ी। स्वतंत्रता के यज्ञ में अनेक देश-भक्तों को आत्मार्पण करना पड़ा। उन्हीं वीर रत्नों के जलते अंगार से ही आज का स्वातन्त्र्य उठा है। कोई शिव ही दूसरों के लिए हलाहल पान करता है-
मनुष्य दुग्ध से दनुज रुधिर से अगर सुधा से जीते हैं,
किन्तु हलाहल भवसागर का शिव शंकर ही पीते हैं।
परोपकार अथवा परहित से बढ़कर न कोई पुण्य है और न कोई धर्म। व्यक्ति, जाति और राष्ट्र तथा विश्व की उन्नति, प्रगति और शान्ति के लक्ष्य को प्राप्त करने का इससे बड़ा उपकरण दूसरा नहीं। आज के वैज्ञानिक युग में मनुष्य से लेकर राष्ट्र तक स्वार्थ केन्द्रित हो गए हैं। यही कारण है कि सब कुछ होते हुए भी क्लेश एवं अशान्ति का बोल-बाला है। यदि मनुष्य सूक्ष्म दृष्टि से विचार करे तो इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि परोपकार के द्वारा वह व्यक्तिगत तथा सामाजिक दोनों क्षेत्रों में प्रगति कर सकता है। स्वार्थ में और परोपकार में समन्वय एवं सन्तुलन की आवश्यकता है। सामाजिक दृष्टि से परोपकार लोकमंगल का साधक है तो व्यक्तिगत दृष्टि से आत्मोन्नति का संबल है पर उपकार का अर्थ यह कदापि नहीं है कि व्यक्ति अपने लिए जिए ही नहीं। वह अपने लिए जीवन जीता हुआ भी दूसरों के आंसू पोंछ सकता है, किसी दुःखी के अधरों पर मुस्कान ला सकता है। किसी गिरते को सम्भाल कर खुदा के नाम से विभूषित हो सकता है-
आदमी लाख संभलने पै भी गिरता है मगर
झुक के उसको जो उठा ले वो खुदा होता है।
जो दूसरों का भला करता है, ईश्वर उसका भला करता है। कहा भी है, ‘कर भला हो भला’ तथा ‘सेवा का फल मीठा होता है’। परोपकार की भावना से मनुष्य की आत्मा का विस्तार होता है तथा धीरे-धीरे उसमें विश्व बन्धुत्व की भावना का उदय होता है। परोपकारी व्यक्ति का हृदय मक्खन से भी कोमल होता है। मक्खन तो ताप (गर्मी) पाकर पिघलता है परन्तु सन्तु दूसरों के ताप अर्थात् दुःख से ही द्रवीभूत हो जाता है। महात्मा बुद्ध को कोई दुःख न था पर दूसरों के रोग, बुढ़ापे एवं मौत ने उन्हें संसार का सबसे बड़े दुःखी बना दिया था। ऐसी कितनी ही विभूतियों के नाम गिनवाए जा सकते हैं जिन्होंने स्वयं कांटों के पथ पर चलकर संसार को सुखद पुष्प प्रदान किए।
आज विज्ञान की शक्ति से मत्त होकर शक्तिशाली राष्ट्र कमज़ोर राष्ट्रों को डरा रहे हैं। ऐसे अन्धकारपूर्ण वातावरण को लोकमंगल की भावना का उदय ही दूर कर सकता है। भारतीय संस्कृति आदि काल से ही विश्व-कल्याण की भावना से प्रेरित रही है। धन-दौलत का महत्त्व इसी में है कि वह गंगा के प्रवाह की तरह सब का हित करे। सागर की उस महानता और जल राशि का क्या महत्त्व जिसके रहते संसार प्यासा जा रहा है। अन्त में पन्त जी के शब्दों में कहा जा सकता है-
आज त्याग तप संयम साधन
सार्थक हों पूजन आराधन,
नीरस दर्शनीयमानव
वप् पाकर मुग्ध करे भव
38. सिनेमा (चलचित्र) के हानि-लाभ
विज्ञान के आधुनिक जीवन में क्रान्ति उत्पन्न कर दी है। मानव जीवन से सम्बद्ध कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जिसको विज्ञान ने प्रभावित न किया हो। आज मानव का जीवन अत्यन्त व्यस्त है। उसे एक मशीन की तरह ही निरन्तर काम में लीन रहना पड़ता है। भले ही यह काम मशीन चलाने का हो, मशीन निरीक्षण का हो अथवा उसकी देखभाल करने का हो। अभिप्राय यह है कि मनुष्य किसी न किसी रूप में इसके साथ जुड़ा हुआ है। आज के व्यस्त जीवन को देखकर ही कहा गया-
बोझ बनी जीवन की गाड़ी बैल बना इन्सान
अतः मनुष्य को अपनी शारीरिक एवं मानसिक थकान मिटाने के लिए मनोरंजन की आवश्यकता है। मनोरंजन के क्षेत्र में रेडियो, ग्रामोफोन, टेलीविज़न आदि अनेक आविष्कारों में चलचित्र या सिनेमा मनोरंजन का सर्वश्रेष्ठ साधन है।
सिनेमा या चित्रपट शब्द सुनते ही लोगों के, विशेषतः युवकों और विद्यार्थियों के मन में एक लहर सी हिलोरें लेने लगती है। इस युग में सिनेमा देखना जीवन का एक अनिवार्य अंग बन गया है। जब कोई आनन्द मनाने का अवसर हो, कोई घरेलू उत्सव हो, या कोई मंगल कार्य हो तब भी सिनेमा देखने की योजना बीच में आ धमकती है। यही कारण है कि उत्सवों के दिनों में मंगलपर्व के अवसर पर तथा परीक्षा परिणाम की घोषणा के अवसरों पर चलचित्र देखने वालों की प्रायः भीड़ रहती है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब चित्रपट देखने के लिए लालायित रहते हैं। आज कोई विरला ही व्यक्ति होगा जिसने कभी सिनेमा न देखा हो। तभी तो कहा गया है-
चमत्कार विज्ञान जगत् का,
और मनोरंजन जन साधन
चारों ओर हो रहा जग में,
आज सिनेमा का अभिनन्दन।
आज सिनेमा मनोरंजन का बहुत बड़ा साधन है। दिन-भर के काम-धन्धों, झंझटों और चिंताओं से अकुलाया हुआ मनुष्य जब सिनेमा देखने जाता है तब पहले तो जाने की उमंग से ही उसकी चिन्ता और थकान लुप्त-सी हो जाती है। सिनेमा भवन में जाकर जब वह सामने सफ़ेद पर्दे पर चलती-फिरती, दौड़ती-भागती, बातें करती, नाचती गाती, हाव-भाव दिखाती, लड़ाई तथा संघर्ष से जूझती एवं रोती-हंसती तस्वीरें देखता है तो वह यह भूल जाता है कि वह सिनेमा हाल में कुर्सी पर बैठा कोई चित्र देख रहा है, बल्कि यह अनुभव करता है कि सारी घटनाएं प्रत्यक्ष देख रहा है। इससे उसका हृदय आनंद में झूम उठता है।
किसी भी दृश्य अथवा प्राणी का चित्र लेकर उसे सजीव रूप में प्रस्तुत करना सिनेमा कला है। चलचित्र का अर्थ है गतिशील चित्र। चलचित्रों के लिए असाधारण एवं विशेष शक्तिशाली कैमरों का प्रयोग किया जाता है। चलचित्र प्रस्तुत करने के लिए विशिष्ट भवन बनाया जाता है। सिनेमा हाल में एक विशेष प्रकार का पर्दा होता है जिस पर मशीन द्वारा प्रकाश फेंक कर चित्र दिखाया जाता है।
चलचित्र का प्रचार दिन-प्रतिदिन बढ़ता जाता है। बड़े-बड़े देशों में तो फिल्म उद्योग स्थापित हो गए हैं। फिल्मनिर्माण के क्षेत्र में आज भारत दूसरे स्थान पर है। बम्बई (मुम्बई) और मद्रास (चेन्नई) चित्र-निर्माण के क्षेत्र में विश्व भर में विख्यात है। आरम्भ में हमारे यहां मूक चित्रों का प्रदर्शन होता था। धीरे-धीरे सवाक् चित्र भी बनने लगे। आलमआरा पहला सवाक् चित्र था जिसे रजत पट पर प्रस्तुत किया गया धीरे-धीरे चलचित्रों का स्तर बढ़ता गया। आज चलचित्र का प्रत्येक अंग विकसित दिखाई देता है। हमारे यहां कई भाषाओं के चित्र बनते हैं। तकनीक एवं कला की दृष्टि से भारतीय चलचित्रों ने पर्याप्त उन्नति की है। हमारे कई चित्र तो अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। संसार में प्रायः अधिकांश वस्तुएं ऐसी हैं जिनमें गुण एवं दोष दोनों होते हैं। सिनेमा भी इस तथ्य का अपवाद नहीं। चलचित्रों से यहां अनेक लाभ हैं वहां उनमें कुछ दोष भी हैं-
देश-विदेश के दृश्य और आचरण सिनेमा द्वारा पता चलते हैं। भूगोल की शिक्षा का यह एक बड़ा साधन है। चित्रपट में दिखाए गए कथानकों का लोगों के मन पर गहरा असर पड़ता है। वे उनसे अपने जीवन को सामाजिक बनाने की शिक्षा लेते हैं। सिनेमा में करुणा-भरे प्रसंगों और दीन-दुःखी व्यक्तियों को देखकर दर्शकों के दिल में सहानुभूति के भाव उत्पन्न होते हैं। बच्चों, युवकों और विद्यार्थियों का ज्ञान बढ़ाने के लिए सिनेमा एक उपयोगी कला है। बड़े-बड़े कलकारखानों और सबके द्वारा आसानी से न देखे जा सकने वाले स्थानों को सब लोग सिनेमा द्वारा सहज ही देख लेते हैं। विद्यार्थियों को नाना प्रकार की ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा सिनेमा द्वारा दी जा सकती है। सिनेमा एक उपयोगी आविष्कार है। सिनेमा द्वारा भूगोल, इतिहास आदि विषयों को शिक्षा छात्र को सरलता से दी जा सकती है। देश में भावनात्मक एकता उत्पन्न करने और राष्ट्रीयता का विकास करने में भी चलचित्र सहायता प्रदान कर सकते हैं। सिनेमा स्लाइड्स के द्वारा व्यापार को भी उन्नत बनाया जा सकता है। ये शांति एवं मनोरंजन का दूत है। इनके द्वारा हमारी सौन्दर्यनुभूति का विकास होता है। हमारे मन में अनेक कोमल भावनाएं प्रकट होती हैं। अनेक प्रकार के चित्र अनेक प्रकार के भावों को उत्तेजित करते हैं।
सिनेमा की हानियां भी कम नहीं है। चित्रपटों के कथानक अधिकतया शृंगार-प्रधान होते हैं। उनमें कामुकता वाले अश्लील चित्र, सम्वाद और गीत होते हैं। इन बातों का विशेषतः युवकों और विद्यार्थियों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। उनमें संयम घटता है। उनकी एकाग्रता नष्ट होती है। पढ़ने तथा कार्य करने से उनका मन हटता है। उनके चरित्र की हानि होती है। वे दिन-रात परस्पर स्त्री-पुरुष कलाकारों तथा कथानकों की ही चर्चा और विवेचना किया करते हैं। वे दृश्यों और गीतों का अनुकरण करते हैं। उनका मन अशान्त और अस्थिर हो जाता है। बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। कई लोग धोखा देने, डाका डालने, बैंक लूटने, स्त्रियों का अपहरण, बलात्कार, नैतिक पतन, भ्रष्टाचार, शराब पीने आदि की शिक्षा सिनेमा से ही लेते हैं। सिनेमा देखना एक दुर्व्यसन हो जाता है। यह घुन की तरह युवकों को अन्दर से खोखला करता जाता है। चरित्र की हानि के साथ-साथ धन, समय और शक्ति का भी नाश होता है। स्वास्थ्य बिगड़ता है।
आंखों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। विद्यार्थियों में अनुशासन-हीनता उच्छृखलता और लम्पटता पैदा करने में सिनेमा का विशेष हाथ है। छात्र-छात्राएं सस्ते संगीत एवं गीतों के उपासक बन जाते हैं। वे हाव-भाव और अन्य अनेक बातों में अभिनेता तथा अभिनेत्रियों का अनुकरण करते हैं। फैशन एवं विलास भावना को बढ़ाने में भी सिनेमा का ही हाथ रहा है। निर्धन वर्ग इस पर विशेष लट्ट हैं। अत: उसका आर्थिक संकट और भी बढ़ जाता है। युवक-युवतियां सिनेमा से प्रभावित होकर भारतीयता से रिक्त एवं सौन्दर्य के उपासक बनते जा रहे हैं।
इस प्रकार सिनेमा के कुछ लाभ भी हैं और हानियां भी हैं। यदि कामुकता-पूर्ण अश्लील दृश्य, गीत, सम्वाद की जगह ज्ञान वर्द्धक दृश्य आदि अधिक हों, विद्यार्थियों को शृंगार-प्रधान सिनेमा देखने की मनाही हो, सैंसर को और कठोर किया जाए, तो हानि की मात्रा काफ़ी घट सकती है। इसे वरदान या अभिशाप बनाना हमारे हाथ में है। यदि भारतीय आदर्शों के अनुरूप चलचित्रों का निर्माण किया जाए तो यह निश्चय ही वरदान सिद्ध हो सकते हैं।
39. बसन्त ऋतु
भारत अपनी प्राकृतिक शोभा के लिए विश्व-विख्यात है। इसे ऋतुओं का देश कहा जाता है। ऋतु-परिवर्तन का जो सुन्दर क्रम हमारे देश में है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। प्रत्येक ऋतु की अपनी छटा और अपना आकर्षण है। बसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद्, हेमन्त, शिशिर इन सबका अपना महत्त्व है। इनमें से बसन्त ऋतु की शोभा सबसे निराली है। वैसे तो बसन्त ऋतु फाल्गुन मास से शुरू हो जाती है। इसके असली महीने चैत्र और वैसाख हैं। बसन्त ऋतु को ऋतुराज कहते हैं, क्योंकि यह ऋतु सबसे सुहावनी, अद्भुत आकर्षक और मन में उमंग भर देने वाली है। इस ऋतु में पौधों, वृक्षों, लताओं पर नए-नए पत्ते निकलते हैं, सुन्दर-सुन्दर फूल खिलते हैं। सचमुच बसन्त की बासन्ती दुनिया की शोभा ही निराली होती है। बसन्त ऋतु प्रकृति के लिए वरदान बन कर आती है।
बागों में, वाटिकाओं में, वनों में सर्वत्र नव जीवन आ जाता है। पृथ्वी का कण-कण एक नये आनन्द, उत्साह एवं संगीत का अनुभव करता है। ऐसा लगता है जैसे मूक वीणा ध्वनित हो उठी हो, बांसुरी को होठों से लगातार किसी ने मधुर तान छेड़ दी हो। शिशिर से ठिठुरे हुए वृक्ष मानो निद्रा से जाग उठे हों और प्रसन्नता से झूमने लगे हों। शाखाओं एवं पत्तों पर उत्साह नज़र आता है। कलियां अपना बूंघट खोलकर अपने प्रेमी भंवरों से मिलने के लिए उतावली हो जाती हैं। चारों ओर रंग-बिरंगी तितलियों की अनोखी शोभा दिखाई देती है। प्रकृति में सर्वत्र यौवन के दर्शन होते हैं, सारा वातावरण सुवासित हो उठता है। चंपा, माधवी, गुलाब, चमेली आदि की सुन्दरता मन को मोह लेती है। कोयल की ध्वनि कानों में मिश्री घोलती है।
आम, जामुन आदि के वृक्षों पर बौर आता है और उसके बाद फल भर जाते हैं। सुगन्धित और रंग-बिरंगे फूलों पर बौर तथा मंजरियों पर भौरे गुंजारते हैं, मधुमक्खियां भिनभिनाती हैं। ये जीव उनका रस पीते हैं। बसन्त का आगमन प्राणी जगत् में परिवर्तन ला देता है। जड़ में भी चेतना आ जाती है और चेतन तो एक अद्भुत स्फूर्ति का अनुभव करता है। मनुष्य-जगत् में भी यह ऋतु विशेष उल्लास एवं उमंगों का संचार करती है। बसन्त ऋतु का प्रत्येक दिन एक उत्सव का रूप धारण कर लेता है। कवि एवं कलाकार इस ऋतु से विशेष प्रभावित होते हैं। उनकी कल्पना सजग हो उठती है। उन्हें उत्तम से उत्तम कला कृतियां रचने की प्रेरणा मिलती है।
इस ऋतु में दिशाएं साफ़ हो जाती हैं, आकाश निर्मल हो जाता है। चारों ओर स्निग्धता और प्रसन्नता फैल जाती है। हाथी, भौरे, कोयलें, चकवे विशेष रूप से ये मतवाले हो उठते हैं। मनुष्यों में मस्ती छा जाती है। कृषि के लिए भी यह ऋतु बड़ी उपयोगी है। चना, गेहूं आदि की फसल इस ऋतु में तैयार होती है। – बसन्त ऋतु में वायु प्रायः दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। क्योंकि यह वायु दक्षिण की ओर से आती है, इसलिए इसे दक्षिण पवन कहते हैं। यह शीतल, मन्द और सुगन्धित होती है। सर्दी समाप्त हो जाने के कारण बसन्त ऋतु में जीवमात्र की चहल-पहल और हलचल बढ़ जाती है। सूर्य की तीव्रता अधिक नहीं होती। दिन-रात एक समान होते हैं। जलवायु उत्तम होती है। सब जगह नवीनता, प्रकाश, उत्साह, उमंग, स्फूर्ति, नई इच्छा नया जोश तथा नया बल उमड़ आता है। लोगों के मन में आशाएं तरंगित होने लगती हैं, अपनी लहलाती खेती देखकर किसानों का मन झूम उठता है कि अब वारे-न्यारे हो जाएंगे।
इस ऋतु की एक बड़ी विशेषता यह है कि इन दोनों शरीर में नये रक्त का संचार होता है और आहार-विहार ठीक रखा जाए तो स्वास्थ्य की उन्नति होती है। स्वभावतः ही बालक-बालिकाएं, युवक-युवतियां, बड़े-बूढ़े, पशु-पक्षी सब अपने हृदय में एक विशेष प्रसन्नता और मादकता अनुभव करते हैं। इस ऋतु में बाहर खुले स्थानों, मैदानों, जंगलों, पर्वतों, नदी-नालों, बाग-बगीचों में घूमना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। कहा भी है कि, ‘बसन्ते भ्रमणं पथ्यम्’ अर्थात् बसन्त में भ्रमण करना पथ्य है। इस ऋतु में मीठी और तली हुई वस्तुएं कम खानी चाहिए। चटनी, कांजी, खटाई आदि का उपयोग लाभदायक रहता है। इसका कारण यह है कि सर्दी के बाद ऋतु-परिवर्तन से पाचन शक्ति कुछ मन्द हो जाती है। बसन्त पंचमी के दिन इतनी पतंगें उड़ती हैं कि उनसे आकाश भर जाता है। सचमुच यह ऋतु केवल प्राकृतिक आनन्द का ही स्रोत नहीं बल्कि सामाजिक आनन्द का भी स्रोत है।
बसन्त ऋतु प्रभु और प्रकृति का एक वरदान है। इसे मधु ऋतु भी कहते हैं। भगवान् श्रीकृष्ण ने गीता में कहा है कि मैं ऋतुओं में बसन्त हूं। बसन्त की महिमा का वर्णन नहीं हो सकता। इसकी शोभा अद्वितीय होती है। जिस प्रकार गुलाब का फूल पुष्पों में, हिमालय का पर्वतों में, सिंह का जानवरों में, कोयल का पक्षियों में अपना विशिष्ट स्थान है उसी प्रकार ऋतुओं में बसन्त की अपनी शोभा और महत्त्व है। कहा भी है
आ आ प्यारी बसन्त सब ऋतुओं से प्यारी। तेरा शुभागमन सुनकर फूली केसर क्यारी॥
40. समाचार-पत्रों का महत्त्व
मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जैसे-जैसे उसकी सामाजिकता में विस्तार होता जाता है, वैसे-वैसे उसकी अपनी साथियों के दुःख-सुख जानने की इच्छा भी तीव्र होती जाती है। इतना ही नहीं वह आस-पास के जगत् की गति-विधियों से परिचित रहना चाहता है। मनुष्य अपनी योग्यता तथा साधनों के अनुरूप समय-समय पर समाचार जानने के लिए प्रयत्नशील रहा है। इन प्रयत्नों में समाचार-पत्रों एवं प्रेसों का आविष्कार सबसे महत्त्वपूर्ण है। आज समाचार-पत्र सर्वसुलभ हो गए हैं। इन समाचार-पत्रों ने संसार को एक परिवार का रूप दे दिया है। एक मोहल्ले से लेकर राष्ट्र तक की ओर और राष्ट्र से लेकर विश्व तक की गतिविधि का चित्र इन पत्रों के माध्यम से हमारे सामने आ जाता है। आज समाचार-पत्र शक्ति का स्त्रोत माने जाते हैं-
झुक आते हैं उनके सम्मुख, गर्वित ऊंचे सिंहासन।
बांध न पाया उन्हें आज तक, कभी किसी का अनुशासन।
निज विचारधारा के पोषक हैं प्रचार के दूत महान्।
समाचार-पत्रों का करते, इसीलिए तो सब सम्मान॥
प्राचीन काल में समाचार जानने के साधन बड़े स्थूल थे। एक समाचार को पहुंचने में पर्याप्त समय लग जाता था। कुछ समाचार तो स्थायी से बन जाते थे। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के सिद्धान्तों को दूर तक पहुंचाने के लिए लाटें बनवाईं। साधु-महात्मा चलते-चलते समाचार पहुंचाने का कार्य करते थे, पर यह समाचार अधिकतर धर्म एवं राजनीति से सम्बन्ध रखते थे। छापेखाने के आविष्कार के साथ ही समाचार-पत्र की जन्म-कथा का प्रसंग आता है। मुगल काल में ‘अखबारात-इ-मुअल्ले’ नाम से समाचार-पत्र चलता था। अंग्रेज़ों के आगमन के साथ-साथ हमारे देश में समाचारपत्रों का विकास हुआ। सर्वप्रथम 20 जनवरी, सन् 1780 ई० में वारेन हेस्टिग्ज़ ने ‘इण्डियन गजट’ नामक समाचारपत्र निकाला।
इसके बाद ईसाई प्रचारकों ने ‘समाज दर्पण’ नामक अखबार प्रारम्भ किया। राजा राममोहन राय ने सतीप्रथा के विरोध में ‘कौमुदी’ तथा ‘चन्द्रिका’ नामक अखबार निकाले। ईश्वर चन्द्र ने ‘प्रभाकर’ नाम से एक समाचारपत्र प्रकाशित किया। हिन्दी के साहित्यकारों ने भी समाचार-पत्रों के विकास में अपना महत्त्वपूर्ण सहयोग दिया। भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। स्वाधीनता से पूर्व निकलने वाले समाचार-पत्रों ने स्वाधीनता संग्राम में जो भूमिका निभाई, वह सराहनीय है। उन्होंने भारतीय जीवन में जागरण एवं क्रान्ति का शंख बजा दिया। लोकमान्य तिलक का ‘केसरी’ वास्तव में सिंह-गर्जना के समान था।
समाचार-पत्र अपने विषय के अनुरूप कई प्रकार के होते हैं। इनमें सबसे महत्त्वपूर्ण समाचार-पत्र दैनिक समाचारपत्र हैं। ये प्रतिदिन छपते हैं और संसार भर के समाचारों का दूत बनकर प्रातः घर-घर पहुंच जाते हैं। हिन्दी दैनिक समाचारपत्रों में नवभारत टाइम्स, हिन्दुस्तान, आज, विश्वमित्र, वीर अर्जुन, पंजाब केसरी, वीर प्रताप, दैनिक ट्रिब्यून का बोलबाला है। साप्ताहिक-पत्रों में विभिन्न विषयों पर लेख, सरस कहानियां, मधुर कविताएं तथा साप्ताहिक घटनाओं तक का विवरण रहता है। पाक्षिक पत्र भी विषय की दृष्टि से साप्ताहिक पत्रों के ही अनुसार होते हैं। मासिक पत्रों में अपेक्षाकृत जीवनोपयोगी अनेक विषयों की विस्तार से चर्चा रहती है। वे साहित्यिक अधिक होते हैं जिनमें साहित्य के विभिन्न अंगों पर भाव एवं कला की दृष्टि से प्रकाश डाला जाता है। इनमें विद्वत्तापूर्ण लेख, उत्कृष्ट कहानियां, सरस गीत, विज्ञान की उपलब्धियां, राजनीतिक दृष्टिकोण, सामायिक विषयों पर आलोचना एवं पुस्तक समीक्षा आदि सब कुछ होता है।
उपर्युक्त पत्रिकाओं के अतिरिक्त त्रैमासिक, अर्द्ध-वार्षिक आदि पत्रिकाएं भी छपती हैं। ये भिन्न-भिन्न विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। विषय की दृष्टि से राजनीतिक, साहित्यिक, व्यापारिक, सामाजिक, धार्मिक आदि विभाग हैं। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र आदि विषयों पर भी पत्रिकाएं निकालती हैं। धार्मिक, मासिक पत्रों में कल्याण विशेष लोकप्रिय है।
समाचार-पत्रों से अनेक लाभ हैं। आज के युग में इनकी उपयोगिता दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इनका सबसे बड़ा लाभ यह है कि विश्व भर में घटित घटनाओं का परिचय हम घर बैठे प्राप्त कर लेते हैं। यह ठीक है कि रेडियो इनसे भी पूर्व समाचारों की घोषणा कर देता है, पर रेडियो पर केवल संकेत होता है उसकी सचित्र झांकी तो अखबारों द्वारा ही देखी जा सकती है। यदि समाचार-पत्रों को विश्व जीवन का दर्पण कहें तो अत्युक्ति न होगी। जीवन के विभिन्न दृष्टिकोण, विभिन्न विचारधाराएं हमारे सामने आ जाती हैं। प्रत्येक पत्र का सम्पादकीय विशेष महत्त्वपूर्ण होता है। आज का युग इतना तीव्रगामी है कि यदि हम दो दिन अखबार न पढ़ें तो हम ज्ञान-विज्ञान में बहुत पीछे रह जाएं।
इनसे पाठक का मानसिक विकास होता है। उसकी जिज्ञासा शांत होती है और साथ ही ज्ञान-पिपासा बढ़ जाती है। समाचार-पत्र एक व्यक्ति से लेकर सारे देश की आवाज़ है जो दूसरे देशों तक पहुंचती है जिससे भावना एवं चिन्तन के क्षेत्र का विकास होता है। व्यापारियों के लिए ये विशेष लाभदायक हैं। वे विज्ञापन द्वारा वस्तुओं की बिक्री में वृद्धि करते हैं। इनमें रिक्त स्थानों की सूचना, सिनेमा-जगत् के समाचार, क्रीड़ा जगत् की गतिविधि, परीक्षाओं के परिणाम, वैज्ञानिक उपलब्धियां, वस्तुओं के भावों के उतार-चढ़ाव, उत्कृष्ट कविताएं, चित्र कहानियां, धारावाहिक उपन्यास आदि प्रकाशित होते रहते हैं। समाचार-पत्रों के विशेषांक बड़े उपयोगी होते हैं। इनमें महान् व्यक्तियों की जीवन-गाथा, धार्मिक, सामाजिक आदि उत्सवों का बड़े विस्तार से परिचय रहता है। देश-विदेश के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक भवनों के चित्र पाठक के आकर्षण का केन्द्र हैं।
समाचार-पत्र अत्यन्त उपयोगी होते हुए भी कुछ कारणों से हानिकारक भी है। इस हानि का कारण इनका दुरुपयोग है। प्रायः बहुत से समाचार-पत्र किसी न किसी धार्मिक अथवा राजनीतिक पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। अखबार का आश्रय लेकर एक दल दूसरे दल पर कीचड़ उछालता है। अनेक सम्पादक सत्ताधीशों की चापलूसी करके सत्य को छिपा रहे हैं। कुछ समाचार-पत्र व्यावसायिक दृष्टि को प्राथमिकता देते हुए इनमें कामुकता एवं विलासिता को बढ़ाने वाले नग्न चित्र प्रकाशित करते हैं। कभी-कभी अश्लील कहानियां एवं कविताएं भी देखने को मिल जाती हैं। साम्प्रदायिक समाचार-पत्र पाठक के दृष्टिकोण को संकीर्ण बनाते हैं तथा राष्ट्र में अनावश्यक एवं ग़लत उत्तेजना उत्पन्न करते हैं। पक्षपात पूर्ण ढंग से और बढ़ा-चढ़ाकर प्रकाशित किए गए समाचार-पत्र जनता में भ्रांति उत्पन्न करते हैं। झूठे विज्ञापनों से लोग गुमराह होते हैं। इस प्रकार इस प्रभावशाली साधन का दुरुपयोग कभीकभी देश के लिए अभिशाप बन जाता है।
सच्चा समाचार-पत्र वह है जो निष्पक्ष होकर राष्ट्र के प्रति अपना कर्त्तव्य निभाए। वह जनता के हित को सामने रखे और लोगों को वास्तविकता का ज्ञान कराए। वह दूध का दूध और पानी का पानी कर दे। वह सच्चे न्यायाधीश के समान हो। उसमें हंस का-सा विवेक हो जो दूध को एक तरफ तथा पानी को दूसरी तरफ कर दे। वह दुराचारियों एवं देश के छिपे शत्रुओं की पोल खोले। एक ज़माना था जब सम्पादकों को जेलों में डालकर अनेक प्रकार की यातनाएं दी जाती थीं। उनके समाचार-पत्र अंग्रेज़ सरकार बन्द कर देती थी, प्रेसों को ताले लगा दिए जाते थे लेकिन सम्पादक सत्य के पथ से नहीं हटते थे। दुःख की बात है कि आज पैसे के लोभ में अपने ही देश का शोषण किया जा रहा है।
यदि समाचार-पत्र अपने कर्त्तव्य का परिचय दें तो निश्चय ही ये वरदान हैं। इसमें सेवा-भाव है। इनका मूल्य कम हो ताकि सर्वसाधारण भी इन्हें खरीद सके। ये देश के चरित्र को ऊपर उठाने वाले हों, न्याय का पक्ष लेने वाले तथा अत्याचार का विरोध करने वाले हों। ये राष्ट्र भाषा के विकास में सहायक हों। भाषा को परिष्कृत करें, नवीन साहित्य को प्रकाश में लाने वाले हों, नर्वोदित साहित्यकारों को प्रोत्साहन देने वाले हों, समाज तथा राष्ट्र को जगाने वाले हों तथा उनमें देश की संसद् तथा राज्य सभाओं की आवाज़ हो तो निश्चय हो यह देश की काया पलट करने में समर्थ हो सकते हैं।

41. ग्राम्य जीवन
अंग्रेज़ी में एक कहावत प्रचलित है “God made the country and man made the town”. अर्थात् गांव को ईश्वर ने बनाया है और नगर को मनुष्य ने बनाया है। ग्राम का अर्थ समूह है-उसमें कुछ एक घरों और नरनारियों का समूह रहता है। नगर का सम्बन्ध नागरिकता से है जिसका अर्थ है कौशल से रचाया हुआ। ग्राम कृषि और नगर व्यापार के कार्य क्षेत्र हैं। एक में जीवन सरल एवं सात्विक है तो दूसरे में तड़क-भड़कमय और कृत्रिम। गांव प्रकृति की शांत गोद है पर उसमें अभावों का बोलबाला है। शहर में व्यस्तता है, रोगों का भण्डार है, कोलाहल है, किन्तु लक्ष्मी का साम्राज्य होने के कारण आमोद-प्रमोद के राग-रंग की ज्योति जगमगाती रहती है।
ग्रामीण व्यक्तियों का स्वास्थ्य अच्छा होता है। इसका कारण यह है कि उन्हें स्वस्थ वातावरण में रहना पड़ता है। खुले मैदान में सारा दिवस व्यतीत करना पड़ता है। अत्यन्त परिश्रम करना पड़ता है। स्वास्थ्यप्रद कुओं का पानी पीने को मिलता है। प्राकृतिक सौन्दर्य का पूर्ण आनन्द ग्राम के लोग ही ले सकते हैं। अधिकतर नगरों में देखा जाता है कि लोग प्रकृति के सौन्दर्य को देखने के लिए तरसते रहते हैं। ग्रामों की जनसंख्या थोड़ी होती है। वे एक-दूसरे से खूब परिचित होते हैं। एक-दूसरे के सुख-दुःख में सम्मिलित होते हैं। इनका जीवन सीधा-सादा तथा सात्विक होता है। नगरों में रहने वालों की भांति वे बाह्य आडम्बरों में नहीं फंसते।
ग्रामवासियों को कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। ग्रामों में स्वच्छता की अत्यन्त कमी होती है। घरों में। गंदा पानी निकालने का उचित प्रबन्ध नहीं होता। अशिक्षा के कारण ग्रामवासी अपनी समस्याओं का समाधान भी पुरी तरह नहीं कर पाते। अधिकतर लोग वहां निर्धनता में जकड़े रहते हैं जिसके कारण वे जीवन-निर्वाह भी पूरी तरह से नहीं कर पाते। जीवन की आवश्यकताएं अधूरी ही रहती हैं। पुस्तकालय तथा वाचनालय का कोई प्रबन्ध नहीं होता। बाहरी वातावरण से वे पूर्णतया अपरिचित होते हैं। छोटी-छोटी बीमारी के लिए उन्हें शहर भागना पड़ता है। शहर की तरफ प्रत्येक वस्तु नहीं मिलती, प्रत्येक आवश्यकता के लिए शहर जाना पड़ता है।
नगर शिक्षा के केन्द्र होते हैं। प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक नगर में हम प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा से नगर निवासियों में विचार-शक्ति की वृद्धि होती है। जीविकोपार्जन के अनेक साधन होते हैं। प्रत्येक वस्तु हर समय मिल सकती है। यात्रियों के लिए भोजन, निवास-स्थान, विश्रामगृह तथा दवाखानों का तो पूछना ही क्या है। गली में डॉक्टर और वैद्य बैठे रहते हैं। डाकखाना, पुलिस स्टेशन आदि का प्रबन्ध प्रत्येक शहर में होता है। वकील, बैरिस्टर और अदालतें शहरों में होती हैं। इस प्रकार नगर का जीवन बड़ा सुखमय है, परन्तु इस जीवन में भी अनेक कठिनाइयां होती नगरवासियों को प्राकृतिक सौन्दर्य का अनुभव तो होता ही नहीं। नगरों में सभी व्यक्ति इतने व्यस्त रहते हैं कि एकदूसरे से सहानुभूति प्रकट करने का अवसर भी प्राप्त नहीं होता। अक्सर देखा जाता है कि कई वर्षों तक बगल के कमरे में रहने वाले को हम पहचान ही नहीं पाते, उनसे परिचय की बात तो दूर रही।
किसी भी देश की उन्नति के लिए यह परम आवश्यक है कि उसके नगरों और ग्रामों का सन्तुलित विकास हो। यह तभी सम्भव हो सकता है जब नगरों और ग्रामों की कमियों को दूर किया जाए। नगरों की विशेषताएं ग्राम वालों को उपलब्ध हों और ग्रामों में प्राप्त शुद्ध खाद्य सामग्री नगर वालों तक पहुंचाई जा सके। ग्रामों में शिक्षा का प्रसार हो। लड़ाईझगड़ों और कुरीतियों का निराकरण हो।
ग्राम जीवन तथा नगर जीवन दोनों दोषों एवं गुणों से परिपूर्ण हैं। इनके दोषों को सुधारने की आवश्यकता है। गांवों में शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। सरकार की ओर से इस सन्दर्भ में महत्त्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। नगर निवासियों का यह कर्त्तव्य है कि वे ग्रामों के उत्थान में अपना योगदान दें। ग्राम भारत की आत्मा हैं। शहरों की सुख-सुविधा ग्रामों की उन्नति पर ही निर्भर करती है। दोनों में उचित समन्वय की आवश्यकता है।
चुनना तुम्हें नगर का जीवन, या चुनना है ग्राम निवास,
करना होगा श्रेष्ठ समन्वय, होगा तब सम्पूर्ण विकास।
42. टेलीविज़न (दूरदर्शन)
टेलीविज़न महत्त्वपूर्ण आधुनिक आविष्कार है। यह मनोरंजन का साधन भी है और शिक्षा ग्रहण करने का सशक्त उपकरण ही। मनुष्य के मन में दूर की चीज़ों को देखने की प्रबल इच्छा रहती है चित्र-कला, फोटोग्राफी और छपाई के विकास से दूरस्थ वस्तुओं, स्थानों, व्यक्तियों के चित्र सुलभ होने लगे। परन्तु इनके दर्शनीय स्थान की आंशिक जानकारी ही मिल सकती है। टेलीविज़न के आविष्कार ने अब यह सम्भव बना दिया है। दूर की घटनाएं हमारी आंखों के सामने उपस्थित हो जाती हैं।
टेलीविज़न का सिद्धान्त रेडियो के सिद्धान्त से बहुत अंशों में मिलता-जुलता है। रेडियो प्रसारण में वक्ता या गायक स्टूडियो में अपनी वार्ता या गायन प्रस्तुत करता है। उसकी आवाज़ से हवा में तरंगें उत्पन्न होती हैं जिन्हें उसके सामने रखा हुआ माइक्रोफोन बिजली की तरंगों में बदल देता है। इन बिजली की तरंगों को भूमिगत तारों के द्वारा शक्तिशाली ट्रांसमीटर तक पहुंचाया जाता है जो उन्हें रेडियो तरंगों में बदल देता है। इन तरंगों को टेलीविज़न एरियल पकड़ लेता है। टेलीविज़न के पुर्जे इन्हें बिजली तरंगों में बदल देते हैं। फिर उसमें लगे लाउडस्पीकर से ध्वनि आने लगती है जिसे हम सुन सकते हैं। टेलीविज़न कैमरे में कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले चित्र आने लगते हैं।
टेलीविज़न के पर्दे पर हम वे ही दृश्य देख सकते हैं जिन्हें किसी स्थान पर टेलीविज़न कैमरे द्वारा चित्रित किया जा रहा हो और उनके चित्रों को रेडियो तरंगों के द्वारा दूर स्थानों पर भेजा रहा हो। इसके लिए टेलीविज़न के विशेष स्टूडियो बनाए जाते हैं, जहां वक्ता, गायक, नर्तक आदि अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। टेलीविज़न के कैमरामैन उनके चित्र विभिन्न कोणों से प्रतिक्षण उतारते रहते हैं । स्टूडियो में जिसका चित्र जिस कोण से लिया जाएगा टेलीविज़न सैट के पर्दे पर उसका चित्र वैसा ही दिखाई पड़ेगा। प्रत्येक वस्तु के दो पहलू होते हैं। जहां फूल हैं वहां कांटे भी अपना स्थान बना लेते हैं। टेलीविज़न भी इसका अपवाद नहीं है। छात्र तो टेलीविज़न पर लटू दिखाई देता है। कोई भी और कैसा भी कार्यक्रम क्यों न हो, वे अवश्य देखेंगे। दीर्घ समय तक टेलीविज़न के आगे बैठे रहने के कारण उनके अध्ययन में बाधा पड़ती है। उनका शेष समय कार्यक्रमों की विवेचना करने में निकल जाता है।
रात को देर तक जागते रहने के कारण प्रातः देर से उठना, विद्यालय में विलम्ब से पहुंचना, सहपाठियों से कार्यक्रमों की चर्चा करना, श्रेणी में ऊंघते रहना आदि उनके जीवन के सामान्य दोष बन गए हैं। टेलीविज़न कुछ महंगा भी है। यह अभी तक अधिकांश मध्यम वर्ग और धनियों के घरों की ही शोभा है। अधिकांश लोग मनोरंजन के इस सर्वश्रेष्ठ साधन से वंचित हैं। यदि टेलीविज़न पर मनोरंजनात्मक कार्यक्रमों के साथ-साथ शिक्षात्मक कार्यक्रम भी दिखाए जाएं तो यह विशेष उपयोगी बन सकता है। पाठ्यक्रम को चित्रों द्वारा समझाया जा सकता है। आशा है, भविष्य में कुछ सुधार अवश्य हो सकेंगे।
टेलीविज़न का पहला प्रयोग सन् 1925 ई० में ब्रिटेन के जान एल० बेयर्ड ने किया था। इतने थोड़े समय में संसार के विकसित देशों में टेलीविज़न का प्रचार इतना अधिक बढ़ गया है वहां प्रत्येक सम्पन्न घर में टेलीविज़न सैट रहना आम बात हो गई है। भारत में टेलीविज़न का प्रसार 15 दिसम्बर, सन् 1959 ई० से तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्र प्रसाद द्वारा प्रारम्भ किया गया था। अब देश के कोने-कोने में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित हो गए हैं, जिनसे घर-घर तक दूरदर्शन के कार्यक्रम देखे जा सकते हैं।
टेलीविज़न के अनेक उपयोग हैं-लगभग उतने ही जितने हमारी आंखों के नाटक, संगीत सभा, खेलकूद आदि के दृश्य टेलीविज़न के पर्दे पर देखकर हम अपना मनोरंजन कर सकते हैं। राजनीतिक नेता टेलीविज़न के द्वारा अपना सन्देश अधिक प्रभावशाली ढंग से जनता तक पहुंचा सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी टेलीविज़न का प्रयोग सफलता से किया जा रहा है कुछ देशों में टेलीविज़न के द्वारा किसानों को खेती की नई-नई विधियां दिखाई जाती हैं।
समुद्र के अन्दर खोज करने के लिए टेलीविज़न का प्रयोग होता है। यदि किसी डूबे हुए जहाज़ की स्थिति का सहीसही पता लगाना हो तो जंजीर के सहारे टेलीविज़न कैमरे को समुद्र के जल के अन्दर उतारते हैं। उसके द्वारा भेजे गये चित्रों से समुद्र तक की जानकारी ऊपर के लोगों को मिल जाती है। टेलीविज़न का सबसे आश्चर्यजनक चमत्कार तब सामने आया जब रूस के उपग्रह में रखे गए टेलीविज़न कैमरे ने चन्द्रमा की सतह के चित्र ढाई लाख मील दूर से पृथ्वी पर भेजे । इन चित्रों से मनुष्य को पहली बार चन्द्रमा के दूसरी ओर उस तल की जानकारी मिली जो हमें कभी दिखाई नहीं देती। जब रूस और अमेरिका चन्द्रमा पर मनुष्य को भेजने की तैयारी कर रहे थे तो इसके लिए चन्द्रमा की सतह के सम्बन्ध में सभी उपयोगी जानकारी टेलीविज़न कैमरों द्वारा पहले ही प्राप्त कर ली गई थी।
निश्चय ही टेलीविज़न आज के युग का एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण मनोरंजन का साधन है। इसका उपयोग देश की प्रगति के लिए किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में भारत की कांग्रेस सरकार ने बहुत ही प्रशंसनीय पग उठाए। यह कहना उपयुक्त ही होगा की निकट भविष्य में भारत के प्रत्येक क्षेत्र में टेलीविज़न कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाने लगेंगे।
43. मेरी प्रिय पुस्तक
महात्मा गांधी के मन में राम-राज्य स्थापित करने की उच्च भावना जगाने वाली प्रेरणा शक्ति रामचरितमानस थी और बही मेरी प्रिय पुस्तक है। यह पुस्तक महाकवि तुलसीदास का अमर स्मारक है। तुलसीदास ही क्यों-वास्तव में इससे हिन्दी-साहित्य समृद्ध होकर समस्त जगत् को आलोक दे रहा है। इसकी श्रेष्ठता का अनुमान इस बात से ही लगाया जा सकता है कि यह कृति संसार की प्रायः सभी समृद्ध भाषाओं में अनूदित हो चुकी है।
रामचरितमानस, मानव-जीवन के लिए मूल्य निधि है। पत्नी का पति के प्रति, भाई का भाई के प्रति, बहू का सासससुर के प्रति, पुत्र का माता-पिता के प्रति क्या कर्त्तव्य होना चाहिए आदि इस कृति का मूल सन्देश है। इसके अतिरिक्त साहित्यिक दृष्टि से यह कृति हिन्दी-साहित्य उपवन का वह कुसुमित फूल है, जिसे सूंघते ही तन-मन में एक अनोखी सुगन्धि का संचार हो जाता है। यह ग्रन्थ दोहा-चौपाई छंदों में लिखा महाकाव्य है।
ग्रन्थ में सात कांड हैं जो इस प्रकार हैं-बाल-कांड, अयोध्या कांड, अरण्य-कांड, किष्किधाकांड, सुन्दर-कांड, लंका-कांड तथा उत्तर-कांड। हर कांड, भाषा भाव आदि की दृष्टि से पुष्ट और उत्कृष्ट है और हर कांड के आरम्भ में संस्कृत के श्लोक है। तत्पश्चात् कथा फलागम की ओर बढ़ती है।-
यह ग्रन्थ अवधी भाषा में लिखा हुआ है।
इसकी भाषा में प्रांजलता के साथ-साथ
प्रवाह तथा सजीवता दोनों हैं। इसे अलंकार स्वाभाविक रूप में आने के कारण सौन्दर्य प्रदत्त है। उनके कारण कथा का प्रवाह रुकता नहीं, स्वच्छन्द रूप से बहता चला जाता है। इसमें रूपक तथा अनुप्रास अलंकार मुख्य रूप में मिलते हैं। इसके मुख्य छन्द हैं-दोहा और चौपाई। शैली वर्णनात्मक होकर भी बीच-बीच में मार्मिक व्यंजना-शक्ति लिए हुए हैं।
इसमें प्रायः समस्त रसों का यथास्थान समावेश है। वीभत्स रस लंका में उभर कर आया है। चरित्रों का चित्रण जितना प्रभावशाली तथा सफल इसमें हुआ है उतना हिन्दी के अन्य किसी महाकाव्य में नहीं हुआ। राम, सीता, लक्ष्मण, रावण, दशरथ, भरत आदि के चरित्र विशेषकर उल्लेखनीय तथा प्रशंसनीय हैं।
इस ग्रंथ को पढ़ने से प्रतिदिन की पारिवारिक, सामाजिक आदि समस्याओं को दूर करने की प्रेरणा मिलती है। परलोक के साथ-साथ इस लोक में कल्याण का मार्ग दिखाई देता है और मन में शान्ति का सागर उमड़ पड़ता है। बारबार पढ़ने को मन चाहता है।
रामचरितमानस हमारे सामने समन्वय का दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। इसमें भक्ति और ज्ञान का, शैवों और वैष्णवों का तथा निराकार और साकार का समन्वय मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास ज्ञान और भक्ति में कोई भेद नहीं मानते।
रामचरितमानस में नीति, धर्म का उपदेश जिस रूप में दिया गया है। वह वास्तव में प्रशंसनीय है। “राम-भक्ति का इतना विराट् तथा प्रभावी निरूपण और राम-कथा का इतना सरस तथा धार्मिक कीर्तन किसी और जगह मिलता अति दुर्लभ है।” इसमें जीवन के मार्मिक चित्र का विशद चित्रण किया गया है। जीवन के प्रत्येक रस का संचार किया है और लोकमंगल की उच्च भावना का समावेश भी किया गया है। यह वह पतित पावनी गंगा है जिसमें डुबकी लगाते ही सारा शरीर शुद्धमय हो उठता है तथा एक मधुर रस का संचार होता है। सहृदय भक्तों के लिए यह दिव्य तथा अमर वाणी है।
उपर्युक्त विवेचन के अनुसार अन्त में हम कह सकते हैं। ‘रामचरित मानस साहित्यिक तथा धार्मिक दृष्टि से उच्चकोटि की रचना है जो अपनी उच्चता तथा भव्यता की कहानी स्वयं कहती है इसलिए मैं इसे अपनी प्रिय पुस्तक मानता हूं।
44. आज का भारतीय किसान
भारतीय किसान परिश्रम, सेवा और त्याग की सजीव मूर्ति है। उसकी सादगी, सरलता तथा दुबलापन उसके सात्विक जीवन को प्रकट करती है। उसकी प्रशंसा में ठीक ही कहा गया गया है-
नगरों से ऐसे पाखण्डों से दूर,
साधना-निरत, सात्विक जीवन के महासत्य
तू वन्दनीय जग का, चाहे रह छिपा नित्य
इतिहास करेगा. तेरे श्रम में रहा सत्य।
किसान संसार का अन्नदाता कहा जाता है। उसे अपने इस नाम को सार्थक बनाने के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ता है। वह बहुत सवेरे ही अपने खेत में कार्य शूरू कर देता है। दोपहर तक लगातार परिश्रम करता है। वह खेतों के हवन में अपने पसीने की आहुति डालता है। इस आहुति के परिणाम स्वरूप ही खेतों में हरियाली छा जाती है। दोपहर के भोजन के बाद वह फिर अपने काम में डट जाता है। सूर्यास्त तक लगातार काम करता है। ग्रीष्म ऋतु की कड़कती धूप हो या हाड़ काया देने वाला जाड़ा हो, दोनों स्थितियों में किसान अपने काम पर दिखाई देता है। इतना कठोर परिश्रम करने के बाद भी कई बार उसकी झोंपड़ी में अकाल का तांडव नृत्य दिखाई देता है। संकट में भी वह किसी से शिकायत नहीं करता। दुःख के बूंट पी कर रह जाता है।
भारतीय किसान के रहन-सहन में बड़ी सादगी और सरलता होती है। उसके जीवन पर बदलती हुई परिस्थितियों का कुछ असर नहीं पड़ता। वह फैशन और आडम्बर की दुनिया से हमेश दूर रहता है। उसका जीवन अनेक प्रकार के अभावों से घिरा रहता है।
अशिक्षा के कारण भारतीय किसान अनेक बातों में पिछड़ जाता है। उसका मानसिक विकास नहीं हो पाता। यही कारण है कि उसके जीवन में अन्धविश्वास सरलता से अपना स्थान बना लेते हैं। इन अन्धविश्वासों पर वह अपने खूनपसीने की कमाई का अपव्यय करता है। अपनी सरलता और सीधेपन के कारण वह सेठ-साहूकारों तथा ज़मींदारों के चंगुल में फंस जाता है। वह इनके शोषण की चक्की में पिसता हुआ दम तोड़ देता है। मुंशी प्रेमचन्द ने अपने उपन्यास गोदान में किसान जीवन की शोचनीय दशा का मार्मिक चित्रण किया है। किसानों में प्राय: ललित कलाओं एवं उद्योगों में भी रुचि नहीं होती। वे बहुत परिश्रमी है तो बहुत आलसी भी बन जाते हैं। साल के आठ महीने तो वह खूब काम करता है पर चार महीने वह हाथ पर हाथ धर कर बैठता है। नशा तो उसके जीवन का अंग बन जाता है। हिंसक घटनाएं, लड़ाई-झगड़ों के भयंकर परिणाम तो उसके जीवन को बर्बाद कर देते हैं।
किसान कुछ दोषों के होने पर भी दैवी गुणों से युक्त है। वह परिश्रम, बलिदान, त्याग और सेवा के आदर्श द्वारा संसार का उपकार करता है। ईश्वर के प्रति वह आस्थावान् है। प्रकृति का वह पुजारी तथा धरती माँ का उपासक है। धन से गरीब होने पर भी मन का अमीर और उदार है। अतिथि का सत्कार करना वह अपना परम धर्म मानता है।
स्वतन्त्रता के बाद भारतीय किसान के जीवन में बड़ा परिवर्तन आया है। सरकार ने इसे अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान की हैं। अब उसका जीवन बहुत नगर-जीवन के समान बनता जा रहा है। वह उत्तम बीजों के महत्त्व तथा आधुनिक मशीनों का प्रयोग करना सीख गया है। शिक्षा के प्रति भी उसकी रुचि बढ़ी है। अब उसकी सन्तान देश में ही नहीं विदेश में भी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त कर रही हैं। अब सेठ-साहूकार भी उसे शीघ्र अपना शिकार नहीं बना सकते। ग्राम पंचायतें भी उसे जागृति प्रदान कर रही हैं।
किसान अन्नदाता है। वह समाज का हितैषी है। उसके सुख में ही देश का सुख है। उसकी समृद्धि में ही देश की समृद्धि है। आशा है कि भविष्य में किसान भरपूर उन्नति करेगा। शिक्षा उसके जीवन में नया चमक लाएगी। देश को उस पर गर्व है।
45. पेड़-पौधे और हम
आदि काल से ही प्रकृति के साथ मनुष्य का गहरा सम्बन्ध आ रहा है। मनुष्य ने प्रकृति की गोद में ही जन्म लिया और उसी ने अपने भरण-पोषण की सामग्री प्राप्त की। प्रकृति ने ही मानव जीवन को संरक्षण प्रदान किया। हिंसक पशुओं की मार से बचने के लिए उसने ऊंचे-ऊंचे वृक्षों का सहारा लिया। वृक्षों के मीठे फलों को खा कर अपनी भूख को मिटाया। सूर्य की तीव्र गर्मी से बचने के लिए उसने शीतल छाया प्रदान करने वाले वृक्षों का सहारा लिया। घने वृक्षों के नीचे झोपड़ी बना कर मनुष्य ने अपनी तथा अपने परिवार को आंधी, वर्षा, शीत के संकट से बचाया। श्री राम चन्द्र, सीता तथा लक्ष्मण ने भी पंचवटी नामक स्थान पर कुटिया बना कर बनवास का लम्बा जीवन व्यतीत किया था। पंचवटी की शोभा ने कुटिया की शोभा को द्विगुणित कर दिया था। गुप्त जी ने शब्दों में-‘पंचवटी की छाया में है सुन्दर पर्ण कुटीर बना’।
वृक्षों की लकडी से भी मनुष्य अनेक प्रकार के लाभ उठाता रहा है। जैसे-जैसे मनुष्य सभ्यता की सीढ़ियां चढ़ता गया। वैसे-वैसे वृक्षों का उपयोग भी बढ़ता गया। इनकी लकड़ी से आग जला कर भोजन पकाया। मकान और झोंपड़ियां बनाईं। नावें बनीं, मकानों की छतों के लिए शहतीर बने, दरवाजे और खिड़कियां बनीं। वर्तमान युग में लकड़ी का जिन रूपों में उपयोग बढ़ा है, उसका वर्णन करना सरल काम नहीं। संक्षेप में कहा जा सकता है कि कोई ऐसा भवन नहीं जहां लकड़ी की वस्तुओं का उपयोग न होता हो। वृक्षों की उपयोगिता का सब से बड़ा प्रमाण यह है कि अगर वृक्ष न होते तो संसार में कुछ भी न होता।
वृक्षों के महत्त्व एवं गौरव को समझते हुए ही हमारे पूर्व पुरुषों ने इनकी आराधना पर बल दिया। पीपल की पूजा इस तथ्य का प्रमाण है। आज भी यह प्रथा प्रचलित है। पीपल को काटना पाप की कोटि में आता है। इससे वृक्ष-सम्पत्ति की रक्षा का भाव प्रकट होता है। पृथ्वी को हरा-भरा, सुन्दर तथा आकर्षक बनाने में वृक्षों का बहुत बड़ा योगदान है। इस हरियाली के कारण ही बाग-बगीचों का महत्त्व है।
वृक्षों की अधिकता पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को भी बढ़ाती है। मरुस्थल के विकास को रोकने के लिए वृक्षारोपण की बड़ी आवश्यकता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहां का जीवन खेती पर ही निर्भर करता है। खेतों के लिए जल की आवश्यकता है। सिंचाई का सबसे उत्तम स्रोत वर्षा है। वर्षा के जल की तुलना में नदियों, नालों, झरनों तथा ट्यूबवैलों के जल का कोई महत्त्व नहीं। इनके अभाव की पूर्ति भी वर्षा ही करती है। वर्षा न हो तो इनका अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाता है। अनुकूल वर्षा तो उस प्रभु का प्रसाद है, जिसे पा कर चराचर को तृप्ति का अनुभव होता है। आकाश में चलती हुई मानसून हवाओं को वृक्ष अपनी ओर खींचते हैं। वे वर्षा के पानी को चूसकर उसे धरा की भीतरी परतों तक पहुंचा देते हैं जिसके परिणामस्वरूप पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति में वृद्धि होती है।
वृक्षों से हमारे स्वास्थ्य को भी लाभ पहुंचता है, हम अपनी सांस के द्वारा जी विषैली हवा बाहर निकालते हैं, उसे वृक्ष ग्रहण कर लेते हैं और बदले में हमें स्वच्छ और स्वास्थ्यप्रद वायु प्रदान करते हैं। वृक्ष एक प्रकार से हवा को स्वच्छ रखने में सहायता देते हैं। आँखों के लिए हरियाली अत्यन्त लाभकारी होती है। इससे आँखों की ज्योति बढ़ती है। यही कारण है कि जीवन में हरे रंग का बड़ा महत्त्व दिया जाता है। वृक्षों की छाल तथा जड़ें दवाइयों के निर्माण में भी प्रयुक्त होती है।
वृक्षों की शोभा नयनाभिराम होती है। तभी तो हम अपने घरों में भी छोटे-छोटे पेड़-पौधे लगवाते हैं. उनकी हरियाली और कोमलता हमें मन्त्र-मुग्ध कर देती है। वृक्षों पर वास करने वाले पक्षियों की मधुर ध्वनियां वातावरण में संगीत भर देती हैं। वृक्षों से प्राप्त होने वाले फल, आदि खाद्य समस्या के समाधान में सहायता करते हैं। कुछ पशु ऐसे हैं जो वृक्षों से ही अपना आहार प्राप्त करते हैं। ये पशु हमारे लिए बड़े उपयोगी हैं।
वृक्षों की वृद्धि के लिए ही वन महोत्सव का आन्दोलन प्रारम्भ हुआ। वन सुरक्षा तथा उसकी उन्नति के सम्बन्ध में सन् 1952 में एक प्रस्ताव पास कर के यह मांग की गई थी कि समस्त क्षेत्रफल के एक तिहाई भाग में वनों एवं वृक्ष को लगाया जाए। वृक्षों का अभाव जीवन में व्याप्त अभावों की खाई को गहरा करता है। प्राकृतिक सभ्यता को मनमाने ढंग से नष्ट करने का अभिप्राय सभ्यता को ह्रास की ओर ले जाना है। भारत में 15,000 विभिन्न जातियों के पेड़-पौधों पाए जाते हैं। यहां लगभग 7 करोड़, 53 लाख हेक्टेयर भूमि वनों से ढकी हुई है। इस प्रकार पूरे क्षेत्रफल के 23 प्रतिशत भाग में वन-भूमि है। आवश्यकता वनों को बढ़ाने के लिए है। सभी प्रदेशों की सरकारें इस दिशा में जागरूक हैं।
देश के विद्वान् तथा वैज्ञानिक यह अनुभव करने लगे हैं कि वन-सम्पदा की वृद्धि भी उतनी ज़रूरी है जितनी अन्य प्रकार के उत्पादनों की वृद्धि की आवश्यकता है। अतः जनता का तथा सरकार का यह कर्त्तव्य है कि पेड़-पौधों की संख्या बढ़ाई जाए। सूने तथा उजाड़ स्थानों पर वृक्ष लगाए जाएं। नदी नालों पर वृक्ष लगाने से उनकी प्रवाह-दिशाओं को स्थिर किया जा सकता है। वृक्षों की लकड़ी से अनेक उद्योग-धन्धों को विकसित किया जा सकता है। अनेक प्रकार की औषधियों के लिए जड़ी-बूटियां प्राप्त की जा सकती हैं।
स्पष्ट हो जाता है कि वृक्ष हमारे जीवन के लिए अत्यधिक उपयोगी हैं, अत: उनके संरक्षण एवं उनकी वृद्धि में प्रत्येक भारतवासी को सहयोग देना चाहिए। वृक्ष हमारा जीवन हैं। इसके लिए अभाव में हमारे जीवन की गाड़ी नहीं चल सकती। वृक्षों को काटे बिना गुज़ारा नहीं पर उनको काटने के साथ-साथ नये वृक्ष लगाने की योजना भी बनानी चाहिए। जितने वृक्ष काटे जाएं, उससे अधिक लगाए जाएं। वृक्षारोपण की प्रवृत्ति को प्रबल बना कर ही हम अकाल तथा महामारी जैसे प्रकोपों से मुक्त हो सकते हैं।

46. प्रभात का भ्रमण
किसी विद्वान् ने संच ही कहा है कि शीघ्र सोने और शीघ्र उठने से व्यक्ति स्वस्थ, सम्पन्न और बुद्धिमान बनता है। (Early to bed and early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise.) यदि कोई देर से सोयेगा तो उसे सुबह सवेरे उठने में कष्ट अनुभव होगा। अतः समय पर सोकर प्रात: बेला में उठना (जगाना) आसान होता है। सुबह सवेरे उठने से मनुष्य स्वस्थ रहता है। स्वस्थ मनुष्य ही अच्छी तरह काम कर सकता है, पढ़ सकता है, कमा सकता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क की बात तो बहुत पुराने समय से मानी आ रही है।
प्रातःकाल का समय बहुत सुहावना होता है। रात बीत जाने की सूचना हमें पक्षियों की चहचहाट सुन कर मिलती है। उस समय शीतल, मन्द और सुगन्धित तीनों ही तरह की हवा बहती है। सुबह सवेरे फूलों पर पड़ी हुई ओस की बूंदें बड़ी लुभावनी प्रतीत होती हैं। हरी-हरी घास पर पड़ी ओस की बूंदें ऐसे प्रतीत होती हैं मानो रात्रि ने जाते समय अपनी झोली के सारे मोती धरती पर बिखेर दिये हों। प्रकृति का कण-कण सचेत हो उठता है। कविवर प्रसाद भी लिखते हैं-
खग-कुल कुल-कुल सा बोल रहा,
किसलय का आंचल डोल रहा,
लो यह लतिका भी भर लाई,
मधु मुकुल नवल रस गागरी।
प्रभात का समय अति श्रेष्ठ समय है, इसी कारण हमारे शास्त्रों में इस काल को देवताओं का समय कहा जाता है। प्राचीनकाल में ऋषि मुनि से लेकर गृहस्थी लोग तक इस समय में जाग जाया करते थे। सूर्योदय से पूर्व ही वे लोग पूजा : पाठ आदि नित्यकर्म से निवृत हो जाया करते थे। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि व्यक्ति को प्रातःकाल में भ्रमण के लिए जाना चाहिए इससे स्वास्थ्य लाभ होने के साथ-साथ व्यक्ति प्राकृतिक सुषमा का भी अवलोकन कर सकता है।
प्रातःभ्रमण के अनेक लाभ हैं, जिन्हें आज के युग के वैज्ञानिकों ने भी स्वीकारा है। प्रात: बेला में वायु अत्यन्त स्वच्छ एवं स्वास्थ्यवर्धक होती है। उस समय वायु प्रदूषण रहित होती है। अतः उस वातावरण में भ्रमण करने से (सैर करने से) मनुष्य कई प्रकार के रोगों से सुरक्षित रहता है। शरीर में चुस्ती और फुर्ती आती है जिसकी सहायता से मनुष्य सारा दिन अपने काम काज में रुचि लेता है।
प्रातः भ्रमण से मस्तिष्क को शक्ति और शान्ति मिलती है। व्यक्ति की स्मरण शक्ति बढ़ती है और मन ईश्वर की भक्ति की ओर प्रवृत्त होता है। प्रात:कालीन भ्रमण विद्यार्थियों के लिए तो लाभकारी है ही अन्य सभी वर्गों के स्त्री-पुरुषों के लिए भी लाभकारी है। आधुनिक वैज्ञानिक खोज ने हमारे शास्त्रों की इस बात को मान लिया है कि पीपल का वृक्ष यों तो चौबीसों घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है परन्तु प्रात: बेला में वह वृक्ष दुगुनी ऑक्सीजन छोड़ता है और गायत्री मन्त्र का यदि सही ढंग से उच्चारण किया जाए तो ऑक्सीजन हमारे शरीर के प्रत्येक अंग में प्रवाहित हो जाती है। ऐसा करके मनुष्य को ऐसे लगता है मानो किसी ने उसकी बैटरी चार्ज कर दी हो।
आज के प्रदूषण युक्त वातावरण में तो प्रातः भ्रमण स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रातः भ्रमण के समय हमारी गति मन्द-मन्द हो। प्रातः भ्रमण हमें नियमित रूप से करना चाहिए तभी उसका यथेष्ठ लाभ होगा। यदि प्रातः भ्रमण के समय आपका कोई साथी, मित्र या भाई बहन आदि हो तो सोने पर सुहागा हो जाता है। प्रातः भ्रमण से आनन्द अनुभव होता है। विद्यार्थी के लिए तो विशेषकर लाभकारी है। प्रातःकाल में पढ़ा हुआ याद रहता है जबकि रात को जाग जाग कर पढ़ा शीघ्र भूल जाता है। आप को यदि अपने स्वास्थ्य से प्यार है तो प्रातः भ्रमण अवश्य करें और परिमाण स्वयं भी देखें और दूसरे को भी बताएं।
47. मित्रता
जब से मनुष्य ने समाज का निर्माण किया है, उसने दूसरों से मिल-जुल कर रहना सीखना शुरू किया। इस मेल-जोल में मनुष्य को एक ऐसे साथी की आवश्यकता अनुभव हुई जिसके साथ वह अपने सुख-दु:ख सांझे कर सके, अपने मन की बात कह सके। अतः वह किसी न किसी साथी को चुनता है जो उसके सुख-दुःख को बांट सके तथा मुसीबत के समय उसके काम आए। उस साथी को ही हम ‘मित्र’ की संज्ञा से याद करते हैं। प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु (Aristotle) ने मित्रता की परिभाषा देते हुए कहा है ‘A single soul dwelling in two bodies’ अर्थात् मित्रता दो शरीर एक प्राण का नाम है। अंग्रेजी की एक सूक्ति है ‘A friend in need is a friend indeed’ अर्थात् मित्र वही है जो मुसीबत के समय काम आए। वास्तव में सच्चे मित्र की पहचान या परख ही मुसीबत के दिनों में होती है। बाइबल में कहा गया है कि ‘सच्चा मित्र’ जीवन में एक दवाई की तरह काम करता है जो व्यक्ति के प्रत्येक रोग का निदान करता है।
होश सम्भालते ही मनुष्य को किसी मित्र की आवश्यकता अनुभव होती है किन्तु उसे मित्र चुनने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यह कठिनाई व्यक्ति के सामने युवावस्था में अधिक आती है क्योंकि तब उसे जीवन में प्रवेश करना होता है। यों तो जवानी तक पहुंचते-पहुंचते व्यक्ति अनेक लोगों से सम्पर्क में आता है। कुछ से तो उसकी जानपहचान भी घनिष्ठ हो जाती है परन्तु उन्हें मित्र बनाया जा सकता है या नहीं, यही समस्या व्यक्ति के सामने आती है। सही मित्र का चुनाव व्यक्ति के जीवन को स्वर्ग और गलत मित्र का चुनाव नरक भी बना सकता है।
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल का कहना है कि “आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसके गुण-दोष को कितना परख कर लेते हैं, पर किसी को मित्र बनाने में उसके पूर्व आचरण और प्रकृति आदि का कुछ भी विचार और अन्वेषण नहीं करते।” किसी व्यक्ति का हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई और साहस ये ही दो चार बातें देखकर लोग झटपट किसी को अपना मित्र बना लेते हैं, वे यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है तथा जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। एक प्रसिद्ध विद्वान् ने कहा है-“विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है, जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खज़ाना मिल गया। ऐसी ही मित्रता करने का हमें यत्न करना चाहिए।”
विद्यार्थी जीवन में तो छात्रों को मित्र बनाने की धुन सवार रहती है। अनेक सहपाठी उसके मित्र बनते हैं किन्तु तब वे दुनिया के कड़े संघर्ष से बेखबर होते हैं किन्तु कभी-कभी बचपन की मित्रता स्थायी सिद्ध होती है। बचपन की मित्रता में एक खूबी यह है कि दोनों मित्रों के भविष्य में प्रतिकूल परिस्थितियों में होने पर भी उनकी मित्रता में कोई अन्तर नहीं आता। बचपन की मित्रता में अमीरी-गरीबी या छोटे-बड़े का अन्तर नहीं देखा जाता है। भगवान् श्रीकृष्ण की निर्धन ब्राह्मण सुदामा से मित्रता बचपन की ही तो मित्रता थी, जिसे आज भी हम आदर्श मित्रता मानते हैं। उदार तथा उच्चाश्य कर्ण की लोभी दुर्योधन से मित्रता की नींव भी तो बचपन में ही पड़ी थी। किन्तु आजकल के सहपाठी की मित्रता स्थायी नहीं होती क्योंकि उसका आधार स्वार्थ पर टिका होता है और स्वार्थ को ध्यान में रख कर किया गया कोई भी कार्य टिकाऊ नहीं होता।
संसार के अनेक महान् महापुरुष मित्रों के कारण ही बड़े-बड़े कार्य करने में समर्थ हुए हैं।
सच्चा मित्र व्यक्ति टूटने नहीं देता। वह उसे जोड़ने का काम करता है, उसके लड़खड़ाते पांवों को सहारा देता है। संकट और विपत्ति के दिनों में सहारा देता है, हमारे सुख-दुःख में हमारा साथ देता है। कर्त्तव्य से विमुख होने की नहीं कर्त्तव्य का पालन करने की सलाह देता है। जान-पहचान बढ़ाना और बात है मित्रता बढ़ाना और। जान-पहचान बढ़ाने से कुछ हानि होगी न लाभ किन्तु यदि हानि होगी तो बहुत भारी होगी। अतः हमें मित्र चुनते समय बड़ी सावधानी एवं सोच-विचार से काम लेना चाहिए ताकि बाद में हमें पछताना न पड़े। अंग्रेज़ी के प्रसिद्ध कवि औलिवर गोल्ड स्मिथ ने ठीक ही कहा है-
“And what is friendship but a name
A charm that lulls to sleep
A shade that follows wealth or fame
But leake the wretch to weep ?”
48. महंगाई/महंगाई की समस्या और समाधान
आज विश्व के देशों के सामने दो समस्याएँ प्रमुख हैं-मुद्रा स्फीति तथा महँगाई। जनता अपनी सरकार से माँग करती है कि उसे कम दामों पर दैनिक उपभोग की वस्तुएँ उपलब्ध करवाई जाएँ। विशेषकर विकासशील देश अपनी आर्थिक कठिनाइयों के कारण ऐसा करने में असफल हो रहे हैं। लोग आय में वृद्धि की मांग करते हैं। देश के पास धन नहीं। फलस्वरूप मुद्रा का फैलाव बढ़ता है, सिक्के की कीमत घटती है, महँगाई और बढ़ती है।
भारत की प्रत्येक सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की कीमतें कम करने के आश्वासन दिए, किन्तु कीमतें बढ़ती ही चली गई। इस कमर तोड़ महँगाई के अनेक कारण हैं। महँगाई का सबसे बड़ा कारण होता है, उपज में कमी। सूखा पड़ने, बाढ़ आने अथवा किसी कारण से उपज में कमी हो जाए तो वस्तुओं के दाम बढ़ना स्वाभाविक है।
उपज जब मंडियों में आती है, अमीर व्यापारी भारी मात्रा में अनाज एवं अन्य वस्तुएं खरीदकर अपने गोदाम भर लेता है जिससे बाज़ार में वस्तुओं की कमी हो जाती है। व्यापारी अपने गोदामों की वस्तुएँ तभी निकालता है। जब उसे कई गुना अधिक कीमत प्राप्त होती है।
अन्य सरकारों की भांति वर्तमान सरकार ने भी महँगाई कम करने का आश्वासन दिया है, किन्तु प्रश्न यह है कि महँगाई कम कैसे हो ? उपज में बढ़ोत्तरी हो यह आवश्यक है, किन्तु हम देख चुके हैं कि उपज बढ़ने का भी कोई बहुत अनुकूल प्रभाव कीमतों पर नहीं पड़ता। वस्तुतः हमारी वितरण प्रणाली में ऐसा दोष है जो उपभोक्ताओं की कठिनाइयां बढ़ा देता है।
आपात् स्थिति के प्रारम्भिक दिनों में वस्तुओं के दाम नियत करने की परिपाटी चली थी, किन्तु शीघ्र ही व्यापारियों ने पुनः मनमानी आरम्भ कर दी। तेल-उत्पादक देशों द्वारा तेल की कीमत बढ़ा देने से भी महँगाई बढ़ी है। वस्तुतः अफसरशाही, लालफीताशाही तथा नेताओं की शुतुर्मुर्गीय नींद महँगाई के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है।
देश का कितना दुर्भाग्य है कि स्वतन्त्रता के इतने वर्ष पश्चात् भी किसानों को सिंचाई की पूर्ण सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं। बड़े-बड़े नुमायशी भवन बनाने की अपेक्षा सिंचाई की चोटी योजनाएं बनाना और क्रियान्वित करना बहुत ज़रूरी है। हमारे सामने ऐसे भी उदाहरण आ चुके हैं जब सरकारी कागज़ों में कुएँ खुदवाने के लिए धन-राशि का व्यय दिखाया गया, किन्तु वे कुएँ कभी खोदे ही नहीं गए।
बढ़ती महँगाई पर अंकुश रखने के लिए सक्रिय राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता है। यदि निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों को उचित दाम पर आवश्यक वस्तुएँ नहीं मिलेंगी तो असंतोष बढ़ेगा और हमारी स्वतन्त्रता के लिए पुनः खतरा उत्पन्न हो जाएगा।
49. पॉलीथीन से बचें
बहुत कुछ दिया है विज्ञान ने हमें सुख भी, दुःख भी। सुविधा से भरा जीवन हमारे लिए अनिवार्यता-सी बन गई है। बाज़ार से सामान खरीदने के लिए हम घर से बाहर निकलते हैं। अपना पर्स तो जेब में डाल लेते हैं पर सामान घर लाने के लिए कोई थैला या टोकरी साथ लेने की सोचते भी नहीं। क्या करना है उसका ? फालतू का बोझ। लौटती बार तो सामान उठाकर लाना ही है तो जाती बार बेकार का बोझा क्यों ढोएं। जो दुकानदार सामान देगा वह उसे किसी पॉलीथीन के थैले या लिफाफे में भी डाल देगा। हमें उसे लानी में आसानी-न तो रास्ते में फटेगा और न ही बारिश में गीला होने से गलेगा। घर आते ही हम सामान निकाल लेंगे और पॉलीथीन डस्टबिन में या घर से बाहर नाली में। किसी भी छोटे कस्बे या नगर के हर मुहल्ले से प्रतिदिन सौ-दो सौ पॉलीथीन के थैले या लिफाफे तो घर से बाहर कूड़े के रूप में जाते ही हैं। वे नालियों में बहते हुए नालों में चले जाते हैं और फिर वे बिना बाढ़ के मुहल्लों में बाढ़ का दृश्य दिखा देते हैं।
पानी में उन्हें गलना तो है नहीं। वे बहते पानी को रोक देते हैं। उनके पीछे कूड़ा इकट्ठा हो जाता है और फिर वह नालियों-नालों के किनारों से बाहर आना आरंभ हो जाता है। गंदा पानी वातावरण को प्रदूषित करता है। वह मलेरिया फैलने का कारण बनता है। हम यह सब देखते हैं. लोगों को दोष देते हैं, जिस महल्ले में पानी भरता है उसमें रहने वालों को गंवार की उपाधि से विभूषित करते हैं और अपने घर लौट आते हैं और फिर से पॉलीथीन की थैलियां नाली में बिना किसी संकोच बहा देते हैं। क्यों न बहाएं-हमारे मुहल्ले में पानी थोड़े ही भरा है।’
पॉलीथीन ऐसे रसायनों से बनता है जो ज़मीन में 100 वर्ष के लिए गाड़ देने से भी नष्ट नहीं होते। पूरी शताब्दी बीत जाने पर भी पॉलीथीन को मिट्टी से ज्यों का त्यों निकाला जा सकता है। ज़रा सोचिए, धरती माता दुनिया की हर चीज़ हज़म कर लेती है पर पॉलीथीन तो उसे भी हज़म नहीं होता। पॉलीथीन धरती के स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। यह पानी की राह को अवरुद्ध करता है: खनिजों का रास्ता रोक लेता है अर्थात् यह ऐसी बाधा है जो जीवन के सहज प्रवाह को रोक सकता है। यदि कोई छोटा बच्चा या मंद बुद्धि व्यक्ति अनजाने में पॉलीथीन की थैली को सिर से गर्दन तक डाल ले फिर से बाहर न निकाल पाए तो उसकी मृत्यु निश्चित है।

हम धर्म के नाम पर पुण्य कमाने के लिए गौऊओं तथा अन्य पशुओं को पॉलीथीन में लिपटी रोटी सब्जी के छिलके, फल आदि ही डाल देते हैं। वे निरीह पशु उन्हें ज्यों का त्यों निगल जाते हैं जिससे उनकी आंतों में अवरोध उत्पन्न हो जाता है और वे तड़प-तड़प कर मर जाते हैं। ऐसा करने से हमने क्या पुण्य कमाया या पाप? ज़रा सोचिए नदियों और नहरों में हम प्रायः पॉलीथीन अन्य सामग्रियों के साथ बहा देते हैं. जो उचित नहीं है। सन् 2005 में इसी पॉलीथीन और अवरुद्ध नालों के कारण वर्षा ऋतु में आधी मुम्बई पानी में डूब गई थी।
हमें पॉलीथीन से परहेज करना चाहिए। इसके स्थान पर कागज़ और कपड़े का इस्तेमाल करना अच्छा है। रंग-बिरंगे पॉलीथीन तो वैसे भी कैंसर-जनक रसायनों से बनते हैं। काले रंग के पॉलीथीन में तो सबसे अधिक हानिकारक रसायन होते हैं जो बार-बार पुराने पॉलीथीन के चक्रण से बनते हैं। अभी भी समय है कि हम पॉलीथीन के भयावह रूप से परिचित हो जाएं और इसका उपयोग नियन्त्रित रूप में ही करें।
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()