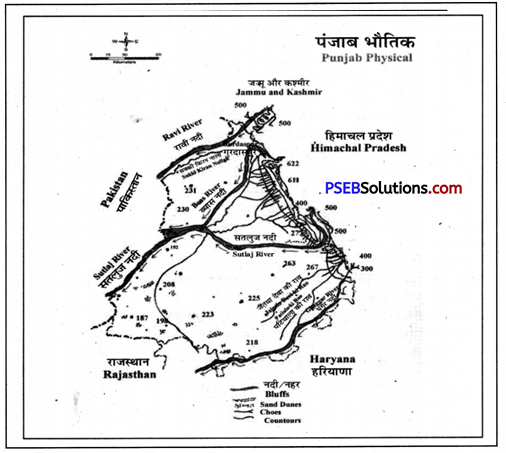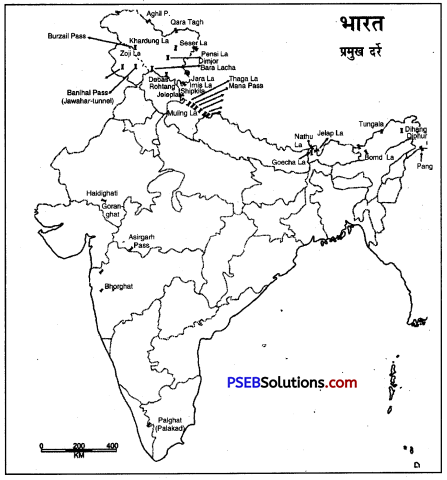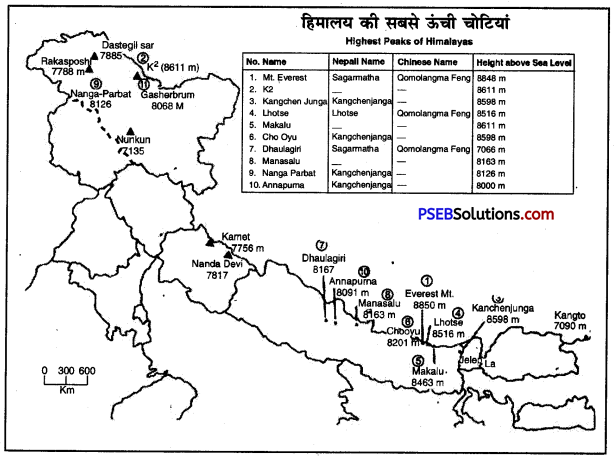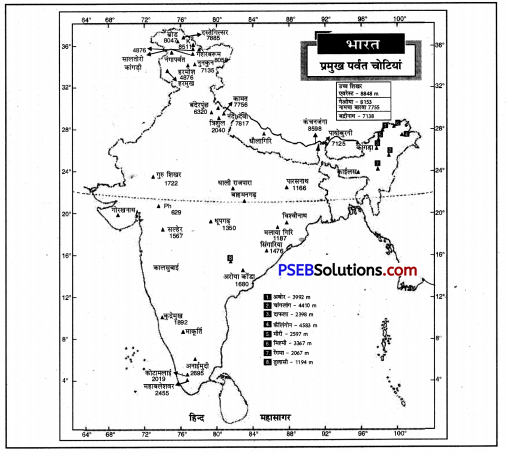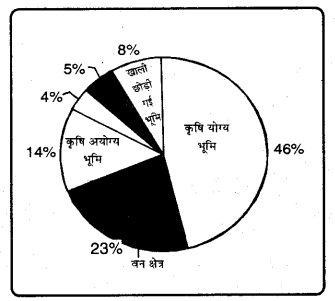Punjab State Board PSEB 11th Class Political Science Book Solutions Chapter 16 सरकारों के रूप-एकात्मक एवं संघात्मक शासन प्रणाली Textbook Exercise Questions and Answers.
PSEB Solutions for Class 11 Political Science Chapter 16 सरकारों के रूप-एकात्मक एवं संघात्मक शासन प्रणाली
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-
प्रश्न 1.
एकात्मक सरकार का अर्थ और विशेषताओं की व्याख्या करें। (Discuss the meaning and features of Unitary Government.)
उत्तर–
आधुनिक राज्य क्षेत्र व जनसंख्या में इतने विशाल हैं कि प्रत्येक राज्य को प्रान्तों अथवा इकाइयों में बांटा गया है। इन प्रान्तों अथवा इकाइयों को प्रान्तीय शासन चलाने के लिए कुछ अधिकार तथा शक्तियां प्राप्त होती हैं। इन प्रान्तीय सरकारों का केन्द्रीय सरकारों से क्या सम्बन्ध है, इस आधार पर सरकारों का वर्गीकरण एकात्मक तथा संघात्मक रूपों में किया जाता है। एकात्मक सरकार में शासन की समस्त शक्तियां अन्तिम रूप में केन्द्रीय सरकार के पास केन्द्रित होती हैं जबकि संघात्मक सरकार में शक्तियां केन्द्र तथा प्रान्तों में बंटी होती हैं।
एकात्मक सरकार की परिभाषाएं (Definitions of Unitary Government)-एकात्मक शासन वह शासन है जिसमें शासन की समस्त शक्तियां केन्द्रीय सरकार के पास केन्द्रित होती हैं। सुविधा की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार प्रान्तों की स्थापना करती है तथा उन्हें थोड़े-बहुत अधिकार प्रदान करती है। केन्द्रीय सरकार जब चाहे इन प्रान्तों की सीमाएं घटा-बढ़ा भी सकती है। एकात्मक शासन की भिन्न-भिन्न विद्वानों ने भिन्न-भिन्न परिभाषाएं दी हैं जो निम्नलिखित हैं-
- डायसी (Dicey) के अनुसार, “एक केन्द्रीय शक्ति के द्वारा सर्वोच्च शक्ति का स्वाभाविक प्रयोग किया जाना ही एकात्मक शासन है।” (“Unitary government is the habitual exercise of supreme legislative authority by one central power.”)
- डॉ० फाइनर (Finer) के अनुसार, “एकात्मक शासन वह होता है जहां एक केन्द्रीय सरकार में सम्पूर्ण शासन शक्ति निहित होती है और जिसकी इच्छा व जिसके प्रतिनिधि कानूनी दृष्टि में सर्वशक्तिमान होते हैं।”
- प्रोफेसर स्ट्रांग (Strong) के अनुसार, “एकात्मक राज्य वह है जो एक केन्द्रीय शासन के अधीन संगठित हो।” (“A unitary state is one organised under a single central government.”)
- प्रो० गार्नर (Garner) के अनुसार, “जब संविधान द्वारा सरकार की सब शक्तियां अकेले केन्द्रीय अंग तथा अन्य अंगों को दी जाएं, जिससे स्थानीय सरकारें अपनी शक्तियां और स्वतन्त्रता तथा अपना अस्तित्व तक प्राप्त करती हों, वहां एकात्मक सरकार होती है।”
इंग्लैण्ड, फ्रांस, जापान, श्रीलंका, चीन, इटली तथा जर्मनी में एकात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है।
- प्रो० गार्नर (Garner) के अनुसार, “जब संविधान द्वारा सरकार की सब शक्तियां अकेले केन्द्रीय अंग तथा अन्य अंगों को दी जाएं, जिससे स्थानीय सरकारें अपनी शक्तियां और स्वतन्त्रता तथा अपना अस्तित्व तक प्राप्त करती हों, वहां एकात्मक सरकार होती है।”

एकात्मक सरकार के लक्षण (Features of Unitary Government)-
एकात्मक शासन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं-
- शक्तियों का केन्द्रीयकरण (Centralization of Powers)—एकात्मक शासन में शासन की शक्तियां केन्द्रीय सरकार में निहित होती हैं। शासन की सुविधा के लिए राज्यों को प्रान्तों में बांटा गया होता है और उन्हें कुछ अधिकार तथा शक्तियां दी जाती हैं। केन्द्र जब चाहे प्रान्तों के अधिकारों तथा शक्तियों को छीन सकता है और उनकी शक्तियां जब चाहे घटा-बढ़ा सकता है। इन प्रान्तों अथवा इकाइयों का अस्तित्व केन्द्र के ऊपर निर्भर करता है।
- प्रभुसत्ता (Sovereignty)-एकात्मक शासन में प्रभुसत्ता केन्द्र में निहित होती है
- इकहरी नागरिकता (Single Citizenship)-एकात्मक शासन में एक ही नागरिकता होती है। इंग्लैण्ड में नागरिकों को एक ही नागरिकता प्राप्त है।
- इकहरा शासन (Single Administration)-एकात्मक शासन में इकहरी शासन व्यवस्था होती है। इसमें एक ही विधानपालिका, एक ही कार्यपालिका तथा एक ही सर्वोच्च न्यायपालिका होती है।
- लिखित अथवा अलिखित संविधान (Written or Unwritten Constitution)-एकात्मक शासन में संविधान लिखित हो सकता है और अलिखित भी। इंग्लैण्ड का संविधान अलिखित है जबकि जापान का संविधान लिखित है।
- कठोर अथवा लचीला संविधान (Rigid or Flexible Constitution) एकात्मक शासन का संविधान कठोर अथवा लचीला हो सकता है। इंग्लैण्ड का संविधान लचीला है जबकि जापान का संविधान कठोर है।
- प्रान्तों का अस्तित्व केन्द्र पर निर्भर करता है (Existence of the Provinces depends upon Centre)प्रान्तीय सरकारों का अस्तित्व और उनकी शक्तियां केन्द्रीय सरकार की इच्छा पर निर्भर होती हैं। प्रान्तों के अस्तित्व तया शक्तियों में परिवर्तन करने के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं होती।
प्रश्न 2.
एकात्मक सरकार के गुणों और दोषों की व्याख्या करें। (Discuss the merits and demerits of Unitary Government.)
उत्तर-
एकात्मक शासन के गुण (Merits of Unitary Government)-एकात्मक शासन के निम्नलिखित गुण हैं-
- शक्तिशाली शासन (Strong Administration)-एकात्मक सरकार में शासन शक्तिशाली होता है। सभी शक्तियां केन्द्र के पास होती हैं। प्रान्तीय सरकारें केन्द्रीय सरकार के आदेशानुसार कार्य करती हैं। कानूनों को बनाने तथा लागू करने की ज़िम्मेदारी केन्द्र पर होती है। इस तरह शासन शक्तिशाली होता है जिस कारण देश की विदेश नीति भी प्रभावशाली होती है।
- सादा शासन (Simple Administration)-एकात्मक सरकार में शासन का संगठन अति सरल होता है। शासन की समस्त शक्तियां केन्द्रीय सरकार के पास होती हैं जिसके कारण केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों में मतभेद उत्पन्न नहीं होते। सादा शासन होने के कारण एक अनपढ़ व्यक्ति को भी अपने देश के शासन के संगठन का ज्ञान होता है।
- लचीला प्रशासन (Flexible Government)-संविधान अधिक कठोर न होने के कारण समयानुसार आसानी से बदला जा सकता है। संकटकाल के लिए यह शासन-प्रणाली बहुत उपयुक्त है। केन्द्र को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए किसी भी समय प्रान्तों की शक्तियों को कम किया जा सकता है।
- कम खर्चीला शासन (Less Expensive)—एकात्मक शासन प्रणाली संघात्मक सरकार की अपेक्षा कम खर्चीली होती है। इसमें एक ही विधानपालिका तथा एक ही कार्यपालिका होती है जिससे खर्च कम होता है। प्रान्तों में विधानमण्डल तथा कार्यपालिका न होने के कारण धन की बचत होती है।
- शासन की एकरूपता (Uniformity in Administration)-कानून बनाने के लिए एक ही विधानपालिका होती है तथा कानूनों को लागू करने के लिए एक ही कार्यपालिका होती है। इससे सारे राज्य में शासन की एकरूपता बनी रहती है। एक नागरिक देश के किसी भी भाग में क्यों न चला जाए उसे एक ही तरह के कानूनों का पालन करना होता है।
- राष्ट्रीय एकता (National Unity)—एकात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रीय एकता की भावनाओं में वृद्धि होती है। इसका कारण यह है कि सभी नागरिकों को एक से कानून का पालन करना पड़ता है और उन्हें एक ही नागरिकता प्राप्त होती है। नागरिकों में प्रान्तीयता की भावनाएं उत्पन्न नहीं होती जिससे राष्ट्रीय एकता बनी रहती है।
- कार्यकुशल शासन (Efficient Administration)-एकात्मक शासन प्रणाली में शासन में कुशलता आ जाती है क्योंकि इस शासन व्यवस्था में केन्द्र तथा प्रान्तों में मतभेद तथा गतिरोध उत्पन्न नहीं होते। एकात्मक सरकार में शासन में कुशलता होती है क्योंकि समस्त निर्णय केन्द्र द्वारा लिए जाते हैं। केन्द्र शीघ्र निर्णय लेकर उन्हें शीघ्रता से लागू करता है। इससे शासन में कुशलता का आना स्वाभाविक है।
- संकटकाल के लिए उपयुक्त (Suitable in time of Emergency) शासन की समस्त शक्तियां केन्द्र के पास होती हैं, जिसके कारण सरकार शक्तिशाली होती है। संकट के समय केन्द्र शीघ्र निर्णय लेकर संकट का सामना दृढ़ता से कर सकता है।
- इकहरी नागरिकता (Single Citizenship) एकात्मक शासन में इकहरी नागरिकता होती है और प्रत्येक व्यक्ति समस्त देश का नागरिक होता है, किसी प्रान्त का नहीं। इससे उनकी वफ़ादारी अविभाजित रहती है और वह देश के प्रति वफ़ादार रहता है।
- छोटे-छोटे राज्यों के लिए उपयुक्त (Suitable for Small States)-एकात्मक शासन प्रणाली छोटे राज्यों के लिए उपयुक्त है। कम क्षेत्र वाले प्रदेश को छोटे-छोटे प्रान्तों में बांटना ठीक नहीं होता क्योंकि प्रत्येक छोटे क्षेत्र में अलग सरकार स्थापित करने से ख़र्च भी बहुत बढ़ जाते हैं।
- वैदेशिक सम्बन्धों में दृढ़ता (Strong and Firm in Foreign Relations)-एकात्मक सरकार दूसरे राज्यों से अपने सम्बन्ध स्थापित करने और उनके संचालन में दृढ़ता से काम ले सकती है। अन्य राज्यों से सन्धि करते समय केन्द्रीय सरकार को प्रान्तीय सरकारों से सलाह करने की आवश्यकता नहीं होती।
- उत्तरदायित्व निश्चित किया जा सकता है (Responsibility can be fixed)-सारे देश का शासन केन्द्रीय शासन के अधीन होता है जिसके कारण उत्तरदायित्व निश्चित करना आसान है।
एकात्मक शासन के दोष (Demerits of Unitary Government)-
बहुत-से राज्य एकात्मक शासन प्रणाली को अपनाए हुए हैं। एकात्मक शासन प्रणाली के बहुत-से अवगुण भी हैं जो निम्नलिखित हैं-
- केन्द्र निरंकुश बन जाता है (Centre becomes Despotic)-एकात्मक शासन में शक्तियों का केन्द्रीयकरण होता है जिसके कारण केन्द्र के निरंकुश बन जाने का सदा भय बना रहता है।
- स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती (Local needs are not fulfilled)—प्रत्येक प्रान्त की अपनी समस्याएं होती हैं जिनके लिए विशेष प्रकार के कानूनों की आवश्यकता होती है। केन्द्रीय सरकार को न तो स्थानीय आवश्यकताओं का पूरा ज्ञान होता है और न ही कानून प्रान्तों के लिए बनाए जाते हैं। वह तो एक ही कानून सब प्रान्तों के लिए बनाती है।
- बड़े राज्यों के लिए अनुपयुक्त (Unsuitable for big States)-एकात्मक सरकार उन राज्यों के लिए जिनका क्षेत्रफल तथा जनसंख्या बहुत अधिक होती है, उपयुक्त नहीं है क्योंकि केन्द्रीय सरकार दूर-दूर फैले हुए भागों में शासन की व्यवस्था अच्छी प्रकार से लागू नहीं कर सकती।
- केन्द्रीय सरकार का कार्य बढ़ जाता है (Central Government becomes over-burdened)—एकात्मक सरकार में सारे देश का शासन केन्द्र के द्वारा चलाया जाता है। जिससे केन्द्रीय सरकार का कार्य बढ़ जाता है। केन्द्रीय सरकार को ही देश की समस्याओं तथा विदेशी मामलों को सुलझाना पड़ता है। शासन के सभी निर्णय केन्द्र के द्वारा लिए जाते हैं जिससे केन्द्र का कार्यभार बहुत बढ़ जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि केन्द्र प्रत्येक कार्य को कुशलता से नहीं कर पाता और कई समस्याओं को सुलझाने के लिए केन्द्र को समय ही नहीं मिल पाता है।
- नौकरशाही का प्रभाव (Influence of Bureaucracy)-एकात्मक शासन में स्थानीय शासन नहीं होने के कारण सरकारी कर्मचारियों की शक्ति तथा प्रभाव बहुत बढ़ जाता है। प्रान्तों का शासन जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा नहीं चलाया जाता बल्कि प्रान्तों के शासन के लिए सरकारी कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं जो जनता की समस्याओं के प्रति उदासीन होते हैं। सरकारी कर्मचारी अपनी मनमानी करते हैं, क्योंकि उन पर स्थानीय नियन्त्रण नहीं होता।
- शासन में दक्षता नहीं आती (Administration does not become efficient)—एकात्मक शासन में राष्ट्रीयता तथा प्रान्तीय मामलों का प्रबन्ध केन्द्र को ही करना पड़ता है। इससे उसके काम इतने बढ़ जाते हैं कि वह कोई भी काम ठीक प्रकार से नहीं कर सकती, यहां तक कि राष्ट्रीय महत्त्व के कार्य भी ठीक समय पर और अच्छी तरह नहीं हो पाते।
- लोगों को राजनीतिक शिक्षा नहीं मिलती (People do not get Political Education)—प्रान्तों में सारा प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा होता है और वहां की जनता को शासन के साथ सम्मिलित नहीं किया जाता है। प्रान्तीय विधानमण्डलों के अभाव में समय-समय पर चुनाव आदि भी नहीं होते, इसलिए जनता को राजनीति में भाग लेने का अवसर कम मिलता है।
- नागरिकों की सार्वजनिक कार्यों में अरुचि (No interest of Citizens towards Local Affairs)एकात्मक शासन में स्थानीय समस्याओं से सम्बन्धित सभी निर्णय केन्द्रीय सरकार के द्वारा किए जाते हैं। स्थानीय समस्याओं पर विचार करने तथा उन्हें सुलझाने के लिए वहां के लोगों को स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं होती। इससे जनता में स्थानीय समस्याओं में कोई रुचि नहीं रहती और उनका उत्साह भी कम हो जाता है। प्रजातन्त्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि जनता स्वयं शासन में रुचि ले और अपनी समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न करें।
निष्कर्ष (Conclusion) एकात्मक शासन के गुण भी हैं और दोष भी। किसी देश में यह प्रणाली ठीक सिद्ध होती है और किसी देश में उचित नहीं समझी जाती।
![]()
प्रश्न 3.
संघवाद से क्या अभिप्राय है ?
(What is the meaning of federalism ?)
उत्तर-
संघात्मक शासन उसे कहते हैं जहां संविधान के द्वारा शक्तियां केन्द्र तथा प्रान्तों में बंटी होती हैं और दोनों अपने कार्यों में स्वतन्त्र होते हैं। इसका अर्थ यह है कि केन्द्रीय सरकार प्रान्तों को दी गई शक्तियों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती और न ही प्रान्त केन्द्रीय सरकार को दी गई शक्तियों में हस्तक्षेप कर सकते हैं। संघात्मक शासन में दोहरी सरकार होती है। प्रभुसत्ता न तो केन्द्रीय सरकार में निहित होती है और न ही प्रान्तीय सरकारों में और न ही प्रभुसत्ता केन्द्र तथा प्रान्तों में बंटी होती है। प्रभुसत्ता वास्तव में राज्य के पास होती है।
संघवाद को अंग्रेज़ी भाषा में ‘फेडरलिज्म’ (Federalism) कहते हैं। फेडरलिज्म शब्द लेटिन भाषा के शब्द फोईडस (Foedus) से बना है जिसका अर्थ है सन्धि अथवा समझौता। संघात्मक सरकार इस प्रकार समझौते का परिणाम होती है। जिस तरह किसी समझौते के लिए एक से अधिक पक्षों का होना आवश्यक होता है उसी तरह संघात्मक राज्य की स्थापना करने के लिए दो या दो से अधिक राज्यों के बीच समझौते की आवश्यकता होती है। उदाहरणस्वरूप प्रारम्भ में अमेरिका के 13 राज्यों ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की स्थापना की। आज अमेरिका के 50 राज्य हैं। भारत, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैण्ड, दक्षिणी अफ्रीका तथा कनाडा में संघात्मक सरकारें पाई जाती हैं।
संघात्मक सरकार की परिभाषाएं (Definitions of Federal Government)-
संघात्मक सरकार की भिन्न-भिन्न परिभाषाएं की गई हैं-
- माण्टेस्कयू (Montesquieu) के अनुसार, “संघात्मक सरकार एक ऐसा समझौता है जिसके द्वारा बहुत से एकजैसे राज्य एक बड़े राज्य के सदस्य बनने को सहमत हो जाते हैं।” (“Federal Government is a convention by which several similar states agree to become members of a large one.”)
- हैमिल्टन (Hamilton) के अनुसार, “संघात्मक शासन राज्यों का एक समुदाय है जो एक नए राज्य का निर्माण करता है।” (“Federation is an association of states that form a new one.”)
- डॉ० फाईनर (Dr. Finer) के शब्दों में, “संघात्मक राज्य वह है जिसमें अधिकार और शक्ति का कुछ भाग स्थानीय क्षेत्रों में निहित हो व दूसरा भाग एक केन्द्रीय संस्था के पास हो जिसको स्थानीय क्षेत्रों के समुदाय ने अपनी इच्छा से बनाया हो।”
- अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, “संघात्मक राज्य तोड़े न जा सकने वाले राज्यों का बना, तोड़ा जा सकने वाला संघ है।” (“Destructible union composed of indestructible states.”)
- गार्नर (Garmer) की परिभाषा स्पष्ट तथा अन्य परिभाषाओं से श्रेष्ठ है। उसके अनुसार, “संघात्मक एक ऐसी प्रणाली है जिसमें केन्द्रीय तथा स्थानीय सरकारें एक सामान्य प्रभुसत्ता के अधीन होती हैं। ये सरकारें अपने निश्चित क्षेत्र में जिसको संविधान अथवा संसद् का कोई अधिनियम निश्चित करता है, सर्वोच्च होती हैं। संघ सरकार जैसा कि प्रायः यह कह दिया जाता है कि अकेली सरकार केन्द्रीय ही नहीं होती वरन् यह केन्द्र तथा स्थानीय सरकारों को मिला कर बनती है। स्थानीय सरकार संघ का उतना ही भाग है जितना कि केन्द्रीय सरकार, यद्यपि वह न तो केन्द्र द्वारा बनाई जाती है और न ही उसके अधीन होती है।”
प्रश्न 4.
संघात्मक शासन व्यवस्था में जो तीन सामान्य सिद्धान्त अपनाये जाते हैं, उनका वर्णन कीजिए।
(Describe the three general principles that are followed in federalism.)
अथवा
संघात्मक सरकार के आवश्यक तत्त्वों की व्याख्या करें।
(Discuss the essential features of a federal government.)
उत्तर-
संघात्मक सरकार के निम्नलिखित आवश्यक तत्त्व तथा विशेषताएं होती हैं-
1. लिखित संविधान (Written Constitution)-संघात्मक सरकार का संविधान सदैव लिखित होना चाहिए ताकि केन्द्र तथा प्रान्तों के मध्य शक्तियों का विभाजन निश्चित तथा स्पष्ट किया जा सके। यदि संविधान अलिखित होगा तो दोनों सरकारों में झगड़े तथा गतिरोध उत्पन्न होते हैं क्योंकि दोनों सरकारों की शक्तियां निश्चित तथा स्पष्ट नहीं होती। अतः समझौते के अनुच्छेद लिखित होने चाहिएं अर्थात् संविधान लिखित होना चाहिए।
2. संविधान की सर्वोच्च (Supremacy of the Constitution)—संघात्मक सरकार में संविधान की सर्वोच्चता होना अति आवश्यक है। संविधान की सर्वोच्चता का अर्थ है कि समझौते की शर्ते जिसके द्वारा संघ राज्य की स्थापना की गई है, केन्द्र तथा प्रान्तीय सरकारों के ऊपर लागू होती हैं। न तो केन्द्र और न ही प्रान्त संविधान का उल्लंघन कर सकता है क्योंकि ऐसा करना समझौते का उल्लंघन करना है जिसके द्वारा संघात्मक राज्य की स्थापना की गई है। कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समुदाय या संस्था संविधान से ऊपर नहीं है। संविधान का उल्लंघन करने का अधिकार किसी को प्राप्त नहीं होता। जब कभी केन्द्र तथा प्रान्तों में गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो दोनों को संविधान की धाराओं के अनुसार कार्य करना होता है। केन्द्र तथा प्रान्त अपने अधिकार तथा शक्तियां संविधान से प्राप्त करते हैं, इसलिए संविधान का सर्वोच्च होना आवश्यक है। अमेरिका, भारत, स्विट्ज़रलैण्ड आदि संघात्मक राज्यों में संविधान सर्वोच्च है।
3. कठोर संविधान (Rigid Constitution) संविधान की सर्वोच्चता तभी कायम रह सकती है यदि संविधान कठोर हो। संविधान में संशोधन केन्द्रीय संसद् अथवा प्रान्तीय विधानमण्डल द्वारा साधारण कानून निर्माण की विधि से नहीं होना चाहिए। संविधान में संशोधन करने का अधिकार यदि केन्द्रीय सरकार को प्राप्त होगा तो केन्द्रीय सरकार अपनी इच्छानुसार संविधान में संशोधन करके प्रान्तों के अधिकारों तथा शक्तियों को छीनने की चेष्ठा करेगी और शीघ्र ही एकात्मक शासन की स्थापना हो जाएगी। संविधान में संशोधन केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों, दोनों की स्वीकृति से होना चाहिए। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैण्ड इत्यादि संघात्मक राज्यों के संविधान कठोर हैं। अमेरिका का संविधान विश्व के शेष सब संविधानों से कठोर है।
4. शक्तियों का विभाजन (Distribution of Powers)—संघात्मक सरकार का अनिवार्य तत्त्व यह है कि शासन प्रणाली में राज्य की सभी शक्तियां केन्द्रीय सरकार तथा प्रान्तीय सरकारों में बंटी होती है। शक्तियों का बंटवारा प्रायः इस तरीके से किया जाता है कि जो विषय सारे देश से सम्बन्धित होते हैं ते केन्द्रीय सरकार को सौंप दिए जाते हैं और जो विषय स्थानीय महत्त्व के होते हैं उन्हें प्रान्तीय सरकारों को सौंप दिया जाता हे।
इस प्रकार सुरक्षा, विदेशी सम्बन्ध, विदेशी व्यापार, साता भात के साधन, मुद्रा आदि महत्त्वपूर्ण विषय केन्द्रीय सरकार के पास रहते हैं और स्थानीय महत्त्व के विषय जैसे कि शिक्षा, जेल, पुलिस, कृषि, स्वास्थ्य, सफ़ाई आदि प्रान्तों के पास रहते हैं। शक्तियों के विभाजन के लिए तीन तरीके अपनाए जाते हैं-
- प्रथम, केन्द्रीय सरकार की शक्तियां निश्चित कर दी जाती हैं और शेष अधिकार (Residuary Powers) प्रान्तों तथा इकाइयों को दे दिए जाते हैं। इस प्रणाली को अमेरिका में अपनाया गया है।
- द्वितीय, प्रान्तीय सरकारों अथवा इकाइयों की शक्तियां निश्चित कर दी जाती हैं और शेष अधिकार केन्द्र को दे दिए जाते हैं। इस प्रणाली को कनाडा में अपनाया गया है।
- तृतीय, केन्द्र तथा प्रान्तों दोनों की शक्तियां निश्चित कर दी जाती हैं और शेष शक्तियों का भी वर्णन कर दिया जाता है जिन्हें समवर्ती विषय (Concurrent Subjects) कहा जाता है। समवर्ती विषयों पर केन्द्र तथा प्रान्त दोनों ही कानून बना सकते हैं और यदि किसी विषय पर केन्द्र तथा प्रान्तों के कानूनों में झगड़ा उत्पन्न हो जाए तो केन्द्र का कानून लागू होता है। भारत में इसी प्रणाली को अपनाया गया है।
5. न्यायपालिका की श्रेष्ठता (Supremacy of the Judiciary)-संघात्मक सरकार में एक स्वतन्त्र, निष्पक्ष तथा सर्वोच्च न्यायपालिका का होना आवश्यक है। संघात्मक सरकार में न्यायपालिका को तीन मुख्य कार्य करने पड़ते
- केन्द्र तथा प्रान्तों के झगड़ों को निपटाना-संघात्मक सरकार में केन्द्र तथा प्रान्तों में शक्तियों का बंटवारा होता है। इस विभाजन के कारण कई बार केन्द्र तथा प्रान्तों में अथवा दो प्रान्तों में पारस्परिक झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं। इन झगड़ों को निपटाने के लिए निष्पक्ष न्यायपालिका का होना अति आवश्यक है ताकि ऐसे झगड़ों पर निष्पक्ष निर्णय दिया जा सके।
- संविधान की व्याख्या करना-संघात्मक सरकार का संविधान लिखित होता है जिस कारण कई बार संविधान की धाराओं की व्याख्या करने की आवश्यकता पड़ जाती है। संविधान की व्याख्या करने का यह अधिकार न्यायपालिका को प्राप्त होता है और न्यायपालिका का निर्णय अन्तिम होता है।
- संविधान की रक्षा-संघात्मक सरकार में संविधान सर्वोच्च होता है। इसकी सर्वोच्चता को कायम रखने की ज़िम्मेदारी न्यायपालिका पर होती है। न्यायपालिका यह देखती है कि केन्द्रीय सरकार अथवा प्रान्तीय सरकार संविधान का उल्लंघन तो नहीं करती। यदि केन्द्र सरकार अथवा प्रान्तीय सरकारें कोई ऐसा कानून बनाती हैं जो संविधान का उल्लंघन करता हो तो न्यायपालिका इस कानून को अवैध घोषित कर सकती है। भारत तथा अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति प्राप्त है।
6. द्वि-सदनीय विधानमण्डल (Bicameral Legislature)—संघात्मक शासन प्रणाली में द्वि-सदनीय विधानमण्डल का होना आवश्यक है। एक सदन समस्त राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है जबकि दूसरा सदन प्रान्तों अथवा इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। निम्न सदन (Lower House) का कार्य सारे राष्ट्र के हितों की रक्षा करना होता है जबकि ऊपरी सदन (Upper House) का मुख्य कार्य प्रान्तों के हितों की रक्षा करना होता है। भारत में संसद् के दो सदन हैं : लोकसभा तथा राज्यसभा। अमेरिका में भी कांग्रेस के दो सदन हैं : प्रतिनिधि सदन तथा सीनेट।
7. दोहरी नागरिकता (Double Citizenship)-संघात्मक प्रणाली की एक विशेषता यह भी होती है कि इसमें नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है। नागरिकों को एक तो सारे राष्ट्र की नागरिकता प्राप्त होती है और एक उस राज्य की नागरिकता प्राप्त होती है जिसमें वे रहे होते हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने वाले व्यक्ति (विदेशियों को छोड़कर) को संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता के अतिरिक्त उस राज्य की नागरिकता भी प्राप्त होती है जिसमें उसका निवास स्थान होता है।
प्रश्न 5.
संघात्मक सरकार के गुणों और दोषों की व्याख्या करें।
(Discuss the merits and demerits of Federal Government.)
उत्तर-
संघात्मक सरकार में निम्नलिखित गुण पाये जाते हैं
संघात्मक सरकार के गुण (Merits of Federal Government)-
1. विभिन्नता में एकता (Unity in Diversity)-इस शासन व्यवस्था का मुख्य गुण यह है कि इसमें विभिन्नता में एकता की प्राप्ति की जाती है। जिन देशों में धार्मिक, भाषायी तथा जातीय विभिन्नता पाई जाती है, उन देशों में संघात्मक सरकार द्वारा राष्ट्रीय एकता को कायम रखा जा सकता है। संघात्मक सरकार में इकाइयां अपनी स्वायत्तता भी बनाए रखती हैं क्योंकि संघ की इकाइयां अपने कार्यों में स्वतन्त्र होती हैं।
2. यह निर्बल राज्यों की शक्तिशाली राज्यों से सुरक्षा करता है (It safeguards the Weak States from Stronger Ones)—संघात्मक सरकार में छोटे-छोटे राज्य मिल कर शक्तिशाली संगठन बनाकर अपनी रक्षा कर सकते हैं। बिना संघात्मक सरकार के यह सम्भव है कि छोटे-छोटे राज्य राज्यों के हाथों में स्वतन्त्रता भी खो बैठें। आज यदि अमेरिका शक्तिशाली है तो सिर्फ संघ शासन के कारण। जो सम्मान आज अमेरिका के राज्यों को प्राप्त है वह कभी उन्हें न मिलता यदि इन राज्यों ने मिलकर संघ की स्थापना न की होती। इसके अतिरिक्त आज राज्य की सुरक्षा के लिए बहुत अधिक धन ख़र्च होता है जिसे कोई भी छोटा राज्य सहन नहीं कर सकता। अतः संसदीय शासन द्वारा ही छोटे-छोटे राज्य अपनी सुरक्षा कर सकते हैं।
3. शासन में कार्यकुशलता (Efficiency in Administration) शासन की शक्तियों का केन्द्र तथा प्रान्तों में विभाजन होता है जिस कारण केन्द्र पर कार्य का बोझ नहीं बढ़ता। कार्य के विभाजन के कारण दोनों सरकारें अपना कार्य कुशलता से करती हैं। किसी के पास कार्य अधिक नहीं होता। कार्यभार अधिक न होने के कारण प्रत्येक समस्या को सुलझाने के शीघ्र निर्णय ले लिया जाता है। केन्द्रीय सरकार को छोटी-छोटी बातों की चिन्ता नहीं होती जिससे केन्द्र अपना कीमती समय बड़ी-बड़ी समस्याओं में लगा सकता है। अतः शक्तियों के इस विभाजन से कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। एकात्मक शासन में केन्द्रीय सरकार के पास कार्य-भार अधिक होने के कारण प्रत्येक निर्णय में देरी होती है। इंग्लैण्ड में संसद् के पास काम अधिक और समय कम होता है।
4. आर्थिक विकास के लिए लाभदायक (Useful for Economic Progress)—संघात्मक सरकार से अधिक आर्थिक उन्नति होती है। छोटे-छोटे राज्यों के आर्थिक साधन इतने नहीं होते कि वे उन्नति कर सकें। संघात्मक राज्य के साधन बहुत बढ़ जाते हैं जिससे समस्त देश की उन्नति होती है।
5. यह केन्द्रीय सरकार को निरंकुश बनने से रोकती है (It checks the despotism of Central Government)-संघात्मक सरकार में शक्तियों के विभाजन के कारण केन्द्र की शक्तियां सीमित होती हैं। सीमित शक्तियों के कारण केन्द्र निरंकुश नहीं बन सकता। इस तरह संघ राज्य में नागरिकों की स्वतन्त्रता सुरक्षित रहती है।
6. यह बड़े राज्यों के लिए उपयुक्त है (It is suitable for big States)-संघात्मक सरकार उन राज्यों के लिए जिनका क्षेत्रफल विशाल होता है तथा जिनकी जनसंख्या बहुत अधिक होती है, उपयुक्त है। बड़े राज्यों का शासन केन्द्र ठीक तरह से नहीं चला सकता। बड़े राज्यों को प्रान्तों में बांट कर स्थानीय शासन उन्हें सौंप दिया जाना चाहिए ताकि केन्द्र का भार हल्का हो जाए।
7. यह नागरिकों की प्रतिष्ठा बढ़ाती है (It enhances the Prestige of the Citizens)-संघ की नागरिकता से नागरिकों की प्रतिष्ठा बढ़ती है। पंजाब या असम अथवा हरियाणा जैसे छोटे राज्य का नागरिक होने की अपेक्षा भारत का नागरिक होना अधिक गौरव की बात है।
8. राजनीतिक शिक्षा (Political Education)—संघात्मक सरकार में लोगों को एकात्मक शासन की अपेक्षा राजनीतिक शिक्षा अधिक मिलती है। केन्द्र के अतिरिक्त प्रान्तों में विधानमण्डल होने के कारण बार-बार चुनाव होते हैं जिससे लोगों को राजनीतिक शिक्षा मिलती है।
9. स्थानीय मामलों में रुचि (Interest in Local Affairs)-संघात्मक सरकार में स्थानीय प्रशासन लोगों के अपने हाथों में होता है जिसके कारण लोग स्थानीय मामलों में रुचि लेते हैं। लोगों में शासन के प्रति उदासीनता समाप्त हो जाती है क्योंकि शासन उनका अपना होता है।
10. यह विश्व राज्य के लिए एक आदर्श है (It is model for the World State)-संघात्मक सरकार विश्व राज्य की स्थापना की ओर एक कदम है। जब छोटे राज्य संघ बना कर सफलता से कार्य कर सकते हैं तो संसार के सभी देश विश्व राज्य की स्थापना करके भी सफलता से कार्य कर सकते हैं।
11. अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा (International Prestige)-संघीय शासन व्यवस्था के अधीन सदस्य राज्यों की अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में मान-प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। आज संसार में अमेरिका को अधिक शक्तिशाली राष्ट्र माना जाता है, क्योंकि अमेरिका 50 राज्यों का सम्मिलित राज्य है।
12. बचत (Economy)-संघ प्रणाली का एक अन्य गुण बचत है क्योंकि इसके अनेक प्रकार के राज्य अपनी प्रभुसत्ता का त्याग करके एक बड़ा राज्य बना लेते हैं जिसके फलस्वरूप उन राज्यों की सुरक्षा के लिए सेना, पुलिस आदि पर इतना खर्च नहीं होता जितना कि उनके अलग-अलग रहने पर होता है।
संघात्मक सरकार की हानियां (Disadvantages of Federal Government)-
संघात्मक सरकार के गुणों के साथ-साथ कुछ दोष भी हैं। इसके मुख्य अवगुण वही हैं जो कि एकात्मक शासन प्रणाली के गुण हैं
1. दुर्बल शासन (Weak Government)-संघात्मक सरकार शक्तियों के विभाजन के कारण दुर्बल सरकार होती है। केन्द्रीय सरकार न तो प्रत्येक विषय पर कानून बना सकती है और न ही प्रान्तों में हस्तक्षेप कर सकती है। केन्द्र के बनाए हुए कानूनों को सर्वोच्च न्यायपालिका अवैध घोषित कर सकती है। प्रो० डायसी के मतानुसार, “संघीय संविधान एकात्मक संविधान की अपेक्षा कमज़ोर होता है।”
2. राष्ट्रीय एकता को ख़तरा (Danger to National Unity)—इस शासन प्रणाली में प्रान्तों को काफ़ी स्वतन्त्रता प्राप्त होती है जिससे नागरिकों में प्रान्तीयता की भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। नागरिक प्रान्तीय भावनाओं में फंस कर राष्ट्र के हित को भूल जाते हैं। प्रत्येक सम्प्रदाय अपना अलग प्रान्त चाहता है और उसकी प्राप्ति के लिए वह आन्दोलन भी करता है। प्रत्येक प्रान्त अपने बारे में सोचता है न कि देश के लिए। कई बार प्रान्त यह सोचने लगता है कि केन्द्रीय सरकार उनके साथ अन्याय कर रही है। वे केन्द्र से सहयोग करना छोड़ देते हैं।
3. संघ के टूटने का भय (Fear of disintegration of Federation)—संघ शासन प्रणाली में यह भय सदा बना रहता है कि कहीं एक इकाई या कुछ इकाइयां मिलकर संघ से अलग होने का प्रयास न करें। प्रान्तों की अपनी सरकार होती है और वह अपने कार्यों में स्वतन्त्र होते हैं। यदि किसी विषय पर केन्द्र तथा प्रान्त का आपस में मतभेद हो जाए तो वह संघ से अलग होने का प्रयत्न करेगा। उदाहरणस्वरूप सोवियत संघ में संघात्मक सरकार पाई जाती थी। दिसम्बर, 1991 में सोवियत संघ के 15 राज्य अलग होकर स्वतन्त्र राज्य बन गए और इस प्रकार सोवियत संघ नाम का देश ही समाप्त हो गया।
4. विदेश नीति में कमज़ोर (Weak in Foreign Policy)-अधिकांश राज्यों की सरकारें विदेशी के साथ किए गए समझौतों की शर्तों को पूरा करने में अनेक प्रकार की अड़चनें डाल कर संघात्मक सरकार के मार्ग में कठिनाई उत्पन्न कर देती हैं। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार विदेश नीति को दृढ़ता से नहीं अपना सकती क्योंकि उसे पूर्ण विश्वास नहीं होता कि राज्यों की सरकारें उसकी नीति का समर्थन करेंगी अथवा नहीं।
5. केन्द्र और राज्यों में झगड़े (Conflicts between Central and State Government)—संघात्मक शासन प्रणाली में केन्द्र और राज्यों में अधिकार क्षेत्र सम्बन्धी झगड़े प्रायः उत्पन्न हो जाते हैं। संघात्मक शासन में प्रायः राज्य की सीमाओं पर झगड़े चलते रहते हैं। भारत इस तथ्य की पुष्टि करता है।
6. खर्चीला शासन (Expensive Government)—संघात्मक शासन एक खर्चीला शासन है क्योंकि इसमें दो प्रकार की सरकारें होती हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा अलग खर्च होता है और प्रान्तीय सरकारों द्वारा अलग। दोहरे शासन के कारण खर्चा भी लगभग दोहरा होता है। जनता को अधिक कर देने पड़ते हैं जिससे तंग आकर साधारण जनता विद्रोह करने के लिए भी तैयार हो जाती है। बार-बार चुनावों पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं।
![]()
7. संविधान समय के अनुसार नहीं बदलता (Constitution does not change with Time)—संघात्मक सरकार में संविधान कठोर होता है, जिसके कारण संविधान में आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता। इसका परिणाम यह निकलता है कि कुछ देर बाद देश का संविधान समय से बहुत पीछे रह जाता है और वह समाज की आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाता। कई बार कठोर संविधान क्रान्ति का कारण बन जाता है।
8. शासन की एकरूपता का न होना (No Uniformity of Administration)—संघात्मक प्रणाली का यह अवगुण है कि समस्त देश में एक-सी शासन व्यवस्था नहीं मिलती। प्रत्येक प्रान्त एक ही विषय पर अपनी इच्छा के अनुसार कानून बनाता तथा कर लगाता है। इसका परिणाम यह होता है कि विभिन्न प्रान्तों में विभिन्न प्रकार के कानून होते हैं और कर भी अलग-अलग लगते हैं। इससे लोगों में प्रान्तीयता की भावना भी आ जाती है।
9. बुरे प्रशासन के लिए किसी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता (No body can be held responsible for bad Administration)-संघात्मक शासन में अकेले केन्द्र को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि शक्तियां केन्द्र तथा प्रान्तों में बंटी होती हैं। प्रशासनिक असफलता के लिए एक सरकार दूसरी को दोषी ठहराने का प्रयत्न करती है।
10. दोहरी नागरिकता हानिकारक है (Double Citizenship is Harmful)-संघात्मक प्रणाली में नागरिक को दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है, परन्तु दोहरी नागरिकता हानिकारक है। नागरिकों को दो सरकारों के प्रति वफादार रहना पड़ता है, जिस के कारण नागरिक दोनों के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभा सकता।
11. न्यायपालिका का अनावश्यक महत्त्व (Undue Importance of Judiciary)—संघ सरकार में संविधान की व्याख्या के लिए न्यायपालिका की आवश्यकता होती है। कई बार यह देखा गया है कि न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या कानून की भावना के अनुसार नहीं बल्कि अपनी दृष्टिकोण के अनुसार करती है। जिस न्यायपालिका के न्यायाधीश खुले रूप में ही कहें कि “हम संविधान के अधीन हैं पर संविधान क्या है यह हम बतलाएंगे” तो वहां संविधान न्यायपालिका के हाथ में खिलौना बन जाता है।
निष्कर्ष (Conclusion)—यह ठीक है कि संघ सरकार की त्रुटियां हैं। पर आधुनिक युग में अधिक-से-अधिक देशों में इसी शासन को स्थापित किया जा रहा है क्योंकि इसमें न केवल लोगों को अपने स्थानीय मामलों में आवश्यक शिक्षा मिलती है अपितु कई देशों ने इस व्यवस्था द्वारा अनुकरणीय उन्नति की है। अमेरिका तथा रूस इस बात के साक्षी हैं। लॉस्की (Laski) ने ठीक ही कहा, “क्योंकि आज का समाज संघीय है, इसलिए शक्ति की बांट भी होनी चाहिए।” (Because society is federal authority must also be federal.)
प्रश्न 6.
संघात्मक और एकात्मक सरकारों में अन्तर करें।
(Distinguish between Federal and the Unitary form of Government.)
उत्तर-
केन्द्र तथा राज्यों के आपसी सम्बन्धों और शासन की शक्तियों की अवस्थिति (Location) के आधार पर शासन एकात्मक होता है। एकात्मक या संघात्मक शासन प्रणाली में समस्त शक्तियां केन्द्र के पास होती हैं और इकाइयों पर इसका पूर्ण नियन्त्रण होता है, परन्तु संघात्मक प्रणाली में केन्द्र और इकाइयों में शक्तियां बंटी होती हैं और दोनों ही अपने क्षेत्र में स्वायत्तता से कार्य करती हैं।
एकात्मक और संघात्मक सरकारों में भिन्नता (Distinction between Unitary and Federal forms of Government) उपर्युक्त चर्चा के आधार पर दोनों सरकारों में अन्तर को विस्तारपूर्वक नीचे दर्शाया गया है : –
1. सरकारों की संख्या (Number of Governments)-एकात्मक प्रणाली के अधीन एक राज्य में एक ही सरकार होती है। नेपाल, श्रीलंका, इंग्लैण्ड और फ्रांस ऐसी प्रणाली के उदाहरण हैं। संघात्मक प्रणाली में केन्द्रीय सरकार के अतिरिक्त इकाइयों की अपनी अलग-अलग सरकार होती है।
2. शासन का संगठन (Government Set-up) -एकात्मक सरकार में शासन का संगठन इकहरा होता है। सारे राज्य में एक ही सरकार होने के नाते देश-भर में एक समान कानून होते हैं, एक जैसी कार्यपालिका और न्यायपालिका की व्यवस्था होती है। इंग्लैंड के नागरिक चाहे वे अपने देश के किसी भी भाग में रहते हों सब एक प्रकार के कानून के अधीन होते हैं। संघात्मक सरकार में शासन का संगठन दोहरा होता है। हर नागरिक का सम्बन्ध दो व्यवस्थापिकाओं, दो कार्यपालिकाओं और न्यायपालिकाओं से होता है। उदाहरणस्वरूप, पंजाब में रहने वाला व्यक्ति रेलगाड़ी, डाक व तार विषयों के लिए केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित है और पुलिस, मोटर, बस, सिनेमाघर, शिक्षा आदि विषयों के लिए पंजाब सरकार के सम्बद्ध है।
3. आपसी सम्बन्ध (Mutual Relations)-एकात्मक प्रणाली के अन्तर्गत भी एक से अधिक सरकारें होती हैं जैसे भारत में सन् 1935 से पहले थीं। परन्तु ऐसी स्थिति में प्रान्तीय सरकारों का स्तर अधीनता (Subordination) का होता है। ये सरकारें अपने हर कार्य में केन्द्रीय सरकार के अधीन होती हैं। प्रान्तीय सरकारों के पास किसी प्रकार की स्वायत्तता (Autonomy) नहीं होती। संघात्मक प्रणाली के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार और प्रान्तीय सरकारें अपने-अपने क्षेत्र में स्वतन्त्र होती हैं और एक सरकार दूसरी सरकार की शक्तियों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अमेरिका, कैनेडा और वर्तमान भारत में ऐसी ही व्यवस्था है।
4. शक्तियों का स्त्रोत (Sources of Powers) एकात्मक प्रणाली में प्रान्तीय सरकारों की शक्तियों का स्रोत केन्द्रीय सरकार होती है अर्थात् प्रान्तीय सरकारें उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करती हैं जो केन्द्र सरकार उन्हें प्रदत्त (Delegate) करती है। केन्द्रीय सरकार कभी भी इन शक्तियों को परिवर्तित कर सकती हैं। संघात्मक प्रणाली में केन्द्रीय सरकार और प्रान्तीय सरकारें अपनी-अपनी शक्तियां राज्य के संविधान से प्राप्त करती हैं। इस प्रणाली के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के पास अधिकार नहीं होता कि प्रान्तों की शक्तियों में कोई भी परिवर्तन कर सके। ऐसा परिवर्तन केवल संविधान में संशोधन द्वारा ही सम्भव है।
5. संविधान की प्रकृति (Nature of Constitution)-वैसे तो आजकल लिखित संविधान की प्रणाली लगभग हर देश में अपनाई जाती है। हां, एकात्मक प्रणाली के लिए लिखित और कठोर संविधान आवश्यक नहीं है। इंग्लैण्ड का संविधान न लिखित ही है और न ही कठोर। परन्तु संघात्मक प्रणाली के लिए संविधान का लिखित और कठोर होना अनिवार्य है।
6. नागरिकता (Citizenship)—एकात्मक प्रणाली के अन्तर्गत नागरिकों को इकहरी नागरिकता (Single Citizenship) प्राप्त होती है, जैसा कि इंग्लैंड, फ्रांस आदि राज्यों में है। संघात्मक प्रणाली के अधीन दोहरी नागरिकता (Double Citizenship) प्राप्त हो सकती है, जैसा कि अमेरिका में।
लघु उत्तरीय प्रश्न
प्रश्न 1.
एकात्मक सरकार का अर्थ एवं परिभाषा लिखें।
उत्तर-
एकात्मक शासन वह शासन है जिसमें शासन की समस्त शक्तियां केन्द्रीय सरकार के पास केन्द्रित होती हैं। सुविधा की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार प्रान्तों की स्थापना करती है तथा उन्हें थोड़े-बहुत अधिकार प्रदान करती है। केन्द्रीय सरकार जब चाहे इन प्रान्तों की सीमाएं भी घटा-बढ़ा सकती है। एकात्मक शासन की भिन्न-भिन्न विद्वानों ने भिन्न-भिन्न परिभाषाएं दी हैं जो निम्नलिखित हैं-
- डायसी के अनुसार, “एक केन्द्रीय शक्ति के द्वारा सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग किया जाना ही एकात्मक शासन है।”
- डॉ० फाइनर के मतानुसार, “एकात्मक शासन वह होता है जहां एक केन्द्रीय सरकार में सम्पूर्ण शासन निहित होता है और जिसकी इच्छा व जिसके प्रतिनिधि कानूनी दृष्टि में सर्वशक्तिमान् होते हैं।”
- प्रोफेसर स्ट्रांग के अनुसार, “एकात्मक राज्य वह राज्य है जो केन्द्रीय शासन के अधीन हो।”
प्रश्न 2.
एकात्मक सरकार की चार विशेषताएं लिखें।
उत्तर-
एकात्मक शासन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं-
- शक्तियों का केन्द्रीयकरण-एकात्मक शासन में शासन की शक्तियां केन्द्रीय सरकार में निहित होती हैं। शासन की सुविधा के लिए राज्यों को प्रान्तों में बांटा गया होता है और उन्हें कुछ अधिकार तथा शक्तियां दी जाती हैं। केन्द्र जब चाहे प्रान्तों के अधिकारों तथा शक्तियों को छीन सकता है।
- प्रभुसत्ता-एकात्मक शासन में प्रभुसत्ता केन्द्र में निहित होती है ।
- इकहरी नागरिकता-एकात्मक शासन में एक ही नागरिकता होती है। इंग्लैंड में नागरिकों को एक ही नागरिकता प्राप्त है।
- इकहरा शासन-एकात्मक शासन में इकहरी शासन व्यवस्था होती है।
प्रश्न 3.
एकात्मक सरकार के चार गुण बताइए।
उत्तर-
एकात्मक शासन के निम्नलिखित गुण हैं-
- शक्तिशाली शासन-एकात्मक सरकार में शासन शक्तिशाली होता है । सभी शक्तियां केन्द्र के पास होती हैं। प्रान्तीय सरकारें केन्द्रीय सरकार के आदेशानुसार कार्य करती हैं । कानूनों को बनाने तथा लागू करने की ज़िम्मेदारी केन्द्र पर ही होती है । इस तरह शासन शक्तिशाली होता है जिस कारण देश की विदेश नीति भी प्रभावशाली होती है ।
- सादा शासन-एकात्मक सरकार में शासन का संगठन अति सरल होता है । शासन की समस्त शक्तियां केन्द्रीय सरकार के पास होती हैं जिसके कारण केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों में मतभेद उत्पन्न नहीं होते। सादा शासन होने के कारण एक अनपढ़ व्यक्ति को भी अपने देश के शासन के संगठन का ज्ञान होता है ।
- लचीला प्रशासन-संविधान अधिक कठोर न होने के कारण समयानुसार आसानी से बदला जा सकता है । संकटकाल के लिए यह शासन प्रणाली बहुत उपयुक्त है। केन्द्र को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए किसी भी समय प्रान्तों की शक्तियों को कम किया जा सकता है।
- कम खर्चीला शासन-एकात्मक शासन प्रणाली संघात्मक सरकार की अपेक्षा कम खर्चीली होती है।
![]()
प्रश्न 4.
एकात्मक सरकार के चार दोषों का वर्णन करें।
उत्तर-
एकात्मक सरकार में निम्नलिखित दोष पाए जाते हैं-
- केन्द्र निरंकुश बन जाता है-एकात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों का केन्द्रीयकरण होता है जिसके कारण केन्द्र के निरंकुश बन जाने का भय होता है ।
- स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती–प्रत्येक प्रान्त की अपनी अलग समस्याएं होती हैं जिसके लिए उन्हें विशेष कानूनों की आवश्यकता होती है। केन्द्रीय सरकार को न तो स्थानीय आवश्यकताओं का पूर्ण ज्ञान होता है और न ही कानून प्रान्तों के लिए बनाए जाते हैं। केन्द्रीय सरकार एक ही कानून को सब प्रान्तों पर लागू कर देती है।
- बड़े राज्यों के लिए अनुपयुक्त-एकात्मक शासन प्रणाली उन राज्यों के लिए उपयुक्त नहीं है जिनका क्षेत्रफल या जनसंख्या बहुत अधिक है क्योंकि केन्द्रीय सरकार दूर-दूर तक फैले हुए भागों में शासन व्यवस्था अच्छी प्रकार से लागू नहीं कर सकती।
- कार्यभार में वृद्धि-एकात्मक सरकार में सारे देश का शासन केन्द्र द्वारा चलाया जाता है, जिससे केन्द्रीय सरकार का कार्य बढ़ जाता है।
प्रश्न 5.
संघात्मक सरकार किसे कहते हैं ?
उत्तर-
संघात्मक शासन उसे कहते हैं जहां संविधान के द्वारा शक्तियां केन्द्र तथा प्रान्तों में बंटी होती हैं और दोनों अपने कार्यों में स्वतन्त्र होते हैं। इसका अर्थ यह है कि केन्द्रीय सरकार को दी गई शक्तियों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती और न ही प्रान्त केन्द्रीय सरकार को दिए गए कार्यों में हस्तक्षेप कर सकते हैं । संघात्मक शासन में दोहरी सरकार होती है। प्रभुसत्ता न तो केन्द्रीय सरकार में निहित होती है और न ही प्रान्तीय सरकारों में और न ही प्रभुसत्ता केन्द्र तथा प्रान्तों में बंटी होती है। प्रभुसत्ता वास्तव में राज्यों के पास होती है।।
संघवाद को अंग्रेज़ी भाषा में ‘फेडरलिज्म’ (Federalism) कहते हैं। फेडरलिज्म शब्द लेटिन भाषा के शब्द फोईडस (Foedus) से बना है जिसका अर्थ है सन्धि अथवा समझौता। संघात्मक सरकार इस प्रकार समझौते का परिणाम होती है। जिस तरह किसी समझौते के लिए एक से अधिक पक्षों का होना आवश्यक होता है उसी तरह संघात्मक राज्य की स्थापना करने के लिए दो या दो से अधिक राज्यों के बीच समझौते की आवश्यकता होती है।
प्रश्न 6.
संघात्मक सरकार की कोई तीन परिभाषाएं लिखें।
उत्तर-
संघात्मक सरकार की मुख्य परिभाषाएं निम्नलिखित हैं-
- माण्टेस्क्यू के अनुसार, “संघात्मक सरकार एक ऐसा समझौता है जिसके द्वारा बहुत-से एक जैसे राज्य एक बड़े राज्य के सदस्य बनने को सहमत हो जाते हैं।”
- डॉ० फाइनर के शब्दों में, “संघात्मक राज्य वह है जिसमें अधिकार व शक्तियों का कुछ भाग स्थानीय क्षेत्रों में निहित हो व दूसरा भाग एक केन्द्रीय संस्था के पास हो जिसको स्थानीय क्षेत्रों के समुदायों ने अपनी इच्छा से बनाया हो।”
- गार्नर की परिभाषा स्पष्ट तथा अन्य परिभाषाओं से श्रेष्ठ हैं। उनके अनुसार, “संघात्मक एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें केन्द्रीय तथा स्थानीय सरकारें एक सामान्य प्रभुसत्ता के अधीन होती हैं। ये सरकारें अपने निश्चित क्षेत्र में जिसको संविधान अथवा संसद् का कोई अधिनियम निश्चित करता है, सर्वोच्च होती है। संघ सरकार जैसा कि प्रायः कह दिया जाता है कि अकेली केन्द्रीय सरकार ही नहीं होती वरन् यह केन्द्र तथा स्थानीय सरकारों को मिला कर बनती है। स्थानीय सरकार संघ का उतना ही भाग है जितना कि केन्द्रीय सरकार का यद्यपि वह न तो केन्द्र द्वारा बनाई जाती है न ही उसके अधीन होती है।
![]()
प्रश्न 7.
संघात्मक शासन की चार विशेषताएं लिखें।
उत्तर-
संघात्मक शासन प्रणाली में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं-
- लिखित संविधान-संघात्मक सरकार का संविधान सदैव लिखित होना चाहिए ताकि केन्द्र तथा प्रान्तों के मध्य शक्तियों का विभाजन स्पष्ट एवं निश्चित किया जा सके। यदि शक्तियों का विभाजन स्पष्ट नहीं होगा तो दोनों सरकारों के मध्य गतिरोध की सम्भावना रहेगी।
- संविधान की सर्वोच्चता-संघात्मक शासन प्रणाली में संविधान का सर्वोच्च होना आवश्यक है क्योंकि कभीकभी केन्द्र और राज्यों में शक्तियों के विभाजन को लेकर आपस में विवाद हो जाता है तब उस विवाद को संविधान की धाराओं के अनुसार सुलझाया जाता है।
- कठोर संविधान-संघात्मक शासन प्रणाली में संविधान का कठोर होना भी आवश्यक है ताकि केन्द्रीय सरकार उसमें आसानी से संशोधन करके राज्य सरकारों की शक्तियों को घटा-बढ़ा न सके। संविधान में संशोधन केन्द्र और राज्य सरकारों की अनुमति से होना चाहिए।
- शक्तियों का विभाजन-संघात्मक सरकार का अनिवार्य तत्त्व यह है, कि शासन प्रणाली में राज्य की सभी शक्तियां केन्द्रीय सरकार तथा प्रान्तीय सरकारों में बंटी होती हैं।
प्रश्न 8.
संघात्मक शासन प्रणाली के चार गुणों का वर्णन करें।
उत्तर-
संघात्मक सरकार में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं-
- विभिन्नता में एकता-इस शासन व्यवस्था का मुख्य गुण यह है कि इसमें विभिन्नता में एकता पाई जाती है। इस शासन प्रणाली में विभिन्न धर्मों, जातियों, भाषाओं, सम्प्रदायों आदि के राज्यों को मिला कर एक मज़बूत केन्द्रीय सरकार की स्थापना की जाती है।
- शासन में कार्य-कुशलता-शासन की शक्तियों का केन्द्र तथा राज्यों में विभाजन होता है जिस कारण केन्द्र पर कार्य का अधिक बोझ नहीं होता। कार्य में विभाजन के कारण कार्य भार कम हो जाता है तथा निर्णय शीघ्र लिए जाते हैं। शक्तियों के विभाजन से कार्य में कुशलता आती है।
- आर्थिक विकास के लिए लाभदायक-संघात्मक शासन प्रणाली में उन्नति में वृद्धि होती है। छोटे-छोटे राज्यों के पास इतने अधिक आर्थिक साधन नहीं होते कि वे अपनी उन्नति कर सकें। संघात्मक राज्य के साधन बहुत बढ़ जाते हैं जिससे समस्त देश की उन्नति होती है।
- राजनीतिक शिक्षा-संघात्मक सरकार में लोगों को एकात्मक शासन की अपेक्षा राजनीतिक शिक्षा अधिक मिलती है।
प्रश्न 9.
संघात्मक शासन प्रणाली के कोई चार दोष लिखें।
उत्तर-
संघात्मक शासन प्रणाली में निम्नलिखित मुख्य दोष पाए जाते हैं-
- दुर्बल शासन-संघात्मक सरकार शक्तियों के विभाजन के कारण दुर्बल सरकार होती है। केन्द्रीय सरकार न तो प्रत्येक विषय पर कानून बना सकती है और न ही प्रान्तों के कार्यों में हस्तक्षेप करने का अधिकार रखती है।
- राष्ट्रीय एकता को खतरा-नागरिक प्रान्तीय भावनाओं में फंस कर राष्ट्रीय हितों को भूल जाते हैं। प्रत्येक प्रान्त राष्ट्रीय हित में न सोचकर अपने हित में सोचता है। इससे राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा पैदा होता है।
- संघ के टूटने का भय-संघीय शासन प्रणाली में सदा यह भय बना रहता है कि कोई इकाई या कुछ इकाइयां मिलकर संघ से अलग होने का प्रयत्न न करें। प्रान्तों की अपनी सरकार होती है और वह अपने कार्यों में स्वतन्त्र होती है। यदि किसी विषय पर केन्द्र तथा प्रान्त में मतभेद हो जाएं तो वह संघ से अलग होने का प्रयत्न करेगा।
- केन्द्र और राज्यों में झगड़े-संघात्मक शासन प्रणाली में केन्द्र और राज्यों में अधिकार क्षेत्र सम्बन्धी झगड़े प्रायः उत्पन्न हो जाते हैं।प्रश्न 10. एकात्मक सरकार और संघात्मक सरकार में कोई चार अन्तर बताएं।
उत्तर-एकात्मक सरकार और संघात्मक सरकार में निम्नलिखित तीन मुख्य अन्तर पाए जाते हैं- - सरकारों की संख्या-एकात्मक शासन प्रणाली में केन्द्र और राज्य में एक ही सरकार होती है जबकि संघात्मक शासन प्रणाली में एक केन्द्रीय सरकार के अतिरिक्त राज्यों की सरकारें भी होती हैं।
- शासन का संगठन-एकात्मक सरकार में शासन का संगठन इकहरा होता है। परन्तु संघात्मक सरकार में दोहरी शासन व्यवस्था होती है।
- आपसी सम्बन्ध- एकात्मक प्रणाली के अन्तर्गत भी एक से अधिक सरकारें हो सकती हैं, परन्तु ऐसी स्थिति में वे पूर्णतया सरकार के अधीन होती हैं। प्रान्तीय सरकारों के पास किसी भी तरह की स्वायत्तता नहीं होती। संघात्मक शासन में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें अपने-अपने क्षेत्र में स्वतन्त्र होती हैं और एक सरकार दूसरी सरकार के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती।
- नागरिकता-एकात्मक प्रणाली के अन्तर्गत नागरिकों को इकहरी नागरिकता प्राप्त होती है, जबकि संघात्मक प्रणाली के अधीन दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है।
अति लघु उत्तरीय प्रश्न
प्रश्न 1.
एकात्मक सरकार का अर्थ लिखें।
उत्तर-
एकात्मक शासन वह शासन है जिसमें शासन की समस्त शक्तियां केन्द्रीय सरकार के पास केन्द्रित होती हैं। सुविधा की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार प्रान्तों की स्थापना करती है तथा उन्हें थोड़े-बहुत अधिकार प्रदान करती है। केन्द्रीय सरकार जब चाहे इन प्रान्तों की सीमाएं भी घटा-बढ़ा सकती है।
प्रश्न 2.
एकात्मक सरकार के दो गुण बताइए।
उत्तर-
- शक्तिशाली शासन-एकात्मक सरकार में शासन शक्तिशाली होता है । सभी शक्तियां केन्द्र के पास होती हैं।
- सादा शासन-एकात्मक सरकार में शासन का संगठन अति सरल होता है। शासन की समस्त शक्तियां केन्द्रीय सरकार के पास होती हैं जिसके कारण केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों में मतभेद उत्पन्न नहीं होते।
प्रश्न 3.
एकात्मक सरकार के दो दोषों का वर्णन करें।
उत्तर-
- केन्द्र निरंकुश बन जाता है-एकात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों का केन्द्रीयकरण होता है जिसके कारण केन्द्र के निरंकुश बन जाने का भय होता है।
- स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती–प्रत्येक प्रान्त की अपनी अलग समस्याएं होती हैं जिसके लिए उन्हें विशेष कानूनों की आवश्यकता होती है। केन्द्रीय सरकार को न तो स्थानीय आवश्यकताओं का पूर्ण ज्ञान होता है और न ही कानून प्रान्तों के लिए बनाए जाते हैं। केन्द्रीय सरकार एक ही कानून को सब प्रान्तों पर लागू कर देती है।
प्रश्न 4.
संघात्मक सरकार किसे कहते हैं ?
उत्तर-
संघात्मक शासन उसे कहते हैं जहां संविधान के द्वारा शक्तियां केन्द्र तथा प्रान्तों में बंटी होती हैं और दोनों अपने कार्यों में स्वतन्त्र होते हैं। इसका अर्थ यह है कि केन्द्रीय सरकार को दी गई शक्तियों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती और न ही प्रान्त केन्द्रीय सरकार को दिए गए कार्यों में हस्तक्षेप कर सकते हैं।
प्रश्न 5.
संघात्मक शासन प्रणाली के दो गुणों का वर्णन करें।
उत्तर-
- विभिन्नता में एकता-इस शासन व्यवस्था का मुख्य गुण यह है कि इसमें विभिन्नता में एकता पाई जाती है।
- शासन में कार्य-कुशलता-शासन की शक्तियों का केन्द्र तथा राज्यों में विभाजन होता है जिस कारण केन्द्र पर कार्य का अधिक बोझ नहीं होता। कार्य में विभाजन के कारण कार्य भार कम हो जाता है तथा निर्णय शीघ्र लिए जाते हैं। शक्तियों के विभाजन से कार्य में कुशलता आती है।
![]()
प्रश्न 6.
संघात्मक शासन प्रणाली के कोई दो दोष लिखें।
उत्तर-
- दुर्बल शासन-संघात्मक सरकार शक्तियों के विभाजन के कारण दुर्बल सरकार होती है।
- राष्ट्रीय एकता को खतरा-इस शासन प्रणाली में प्रान्तों को काफ़ी स्वतन्त्रता प्राप्त होती है जिससे नागरिकों में प्रान्तीयता की भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं।
वस्तुनिष्ठ प्रश्न
प्रश्न I. एक शब्द/वाक्य वाले प्रश्न-उत्तर-
प्रश्न 1. एकात्मक सरकार किसे कहते हैं ?
उत्तर-एकात्मक सरकार में शासन की समस्त शक्तियां केन्द्रीय सरकार के पास होती हैं।
प्रश्न 2. एकात्मक सरकार की कोई एक परिभाषा लिखें।
उत्तर-प्रो० स्ट्रांग के अनुसार, “एकात्मक राज्य वह है, जो एक केन्द्रीय शासन के अधीन संगठित हो।”
प्रश्न 3. एकात्मक सरकार का कोई एक लक्षण लिखें।
उत्तर-एकात्मक सरकार में शासन की शक्तियां केन्द्रीय सरकार में निहित होती हैं।
प्रश्न 4. एकात्मक सरकार का कोई एक गुण लिखें।
उत्तर-एकात्मक सरकार में शासन शक्तिशाली होता है।
प्रश्न 5. एकात्मक सरकार का कोई एक दोष लिखें।
उत्तर-एकात्मक सरकार में केन्द्र के निरंकुश बनने का डर बना रहता है।
प्रश्न 6. इंग्लैण्ड में किस प्रकार का शासन है?
उत्तर-इंग्लैण्ड में एकात्मक शासन है।
प्रश्न 7. अमेरिका में कैसा शासन पाया जाता है?
उत्तर-अमेरिका में संघात्मक शासन पाया जाता है।
प्रश्न 8. भारत में किस प्रकार का शासन पाया जाता है ?
उत्तर- भारत में संघात्मक शासन पाया जाता है।
प्रश्न 9. संघात्मक सरकार की कोई एक परिभाषा लिखिए।
उत्तर-हेमिल्टन के अनुसार, “कुछ राज्यों के संयोजन से बने हुए नए राज्य को संघ कहते हैं।”
प्रश्न 10. संघात्मक सरकार की कोई एक विशेषता बताओ।
उत्तर-संघीय शासन प्रणाली में संविधान लिखित होता है।
प्रश्न 11. संघात्मक सरकार का कोई एक गुण बताओ।
उत्तर-संघीय सरकार निर्बल राज्यों की शक्तिशाली राज्यों से रक्षा करती है।
प्रश्न 12. संघात्मक सरकार का कोई एक दोष बताओ।
उत्तर-इसमें सरकार दुर्बल होती है।
प्रश्न 13. संघात्मक और एकात्मक सरकार में कोई एक भेद बताओ।
उत्तर-संघात्मक सरकार का संविधान लिखित होता है, परन्तु एकात्मक सरकार का संविधान अलिखित भी हो सकता है।
प्रश्न 14. एकात्मक शासन में सभी शक्तियां कहां पर केन्द्रित होती हैं ?
उत्तर-एकात्मक शासन में शक्तियां एक केन्द्रीय सरकार में केन्द्रित होती हैं।
प्रश्न 15. संघात्मक शासन में संविधान लिखित होता है, या अलिखित?
उत्तर-संघात्मक शासन में संविधान लिखित होता है।
![]()
प्रश्न 16. फैडरलिज्म शब्द किस भाषा से निकला है?
उत्तर-फैडरलिज्म शब्द लातीनी भाषा से निकला है।
प्रश्न 17. फोइडस (Foedus) का क्या अर्थ है?
उत्तर-फोइडस का अर्थ सन्धि अथवा समझौता है।
प्रश्न II. खाली स्थान भरें-
1. एकात्मक सरकार में केन्द्र सुविधा के अनुसार ………. की स्थापना करती है।
2. ……….. सरकार जब चाहे प्रान्तों की सीमाएं घटा-बढ़ा सकती है।
3. एकात्मक सरकार ………… के समय उपयुक्त होती है।
4. आलोचकों के अनुसार केन्द्रीय सरकार में …….. आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती।
5. एकात्मक सरकार में केन्द्रीय सरकार का ………. बढ़ जाता है।
उत्तर-
- प्रान्तों
- केन्द्रीय
- संकटकाल
- स्थानीय
- कार्य।
प्रश्न III. निम्नलिखित में से सही एवं ग़लत का चुनाव करें।
1. संघवाद को अंग्रेज़ी में फेडरलिज्म (Federalism) कहते हैं।
2. फेडरलिज्म शब्द लैटिन भाषा के शब्द फोईडस (Foedus) से बना है, जिसका अर्थ है, सन्धि अथवा समझौता।
3. संघात्मक सरकार झगड़े का परिणाम होती है।
4. संघात्मक सरकार में लिखित संविधान की आवश्यकता नहीं होती।
5. संघात्मक सरकार में संविधान का सर्वोच्च होना आवश्यक है।
उत्तर-
- सही
- सही
- ग़लत
- ग़लत
- सही।
प्रश्न IV. बहुविकल्पीय प्रश्न
प्रश्न 1.
निम्नलिखित में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है ?
(क) भारत
(ख) संयुक्त राज्य अमेरिका
(ग) स्विट्ज़रलैंड
(घ) जापान।
उत्तर-
(घ) जापान।
![]()
प्रश्न 2.
निम्नलिखित में से किस देश में संघात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है ?
(क) इंग्लैंड
(ख) जापान
(ग) साम्यवादी चीन
(घ) संयुक्त राज्य अमेरिका।
उत्तर-
(घ) संयुक्त राज्य अमेरिका।
प्रश्न 3.
यह किसने कहा है, “एक केन्द्रीय शक्ति के द्वारा सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग किया जाना ही एकात्मक शासन है।”
(क) डॉ० फाइनर
(ख) लॉर्ड ब्राइस
(ग) डायसी
(घ) गैटेल।
उत्तर-
(ग) डायसी।
प्रश्न 4.
यह किसने कहा है, “संघात्मक शासन राज्यों का एक समुदाय है, जोकि नए राज्य का निर्माण करता
(क) माण्टेस्कयू
(ख) डॉ० फाइनर
(ग) जैलीनेक
(घ) हैमिल्टन।
उत्तर-
(घ) हैमिल्टन।