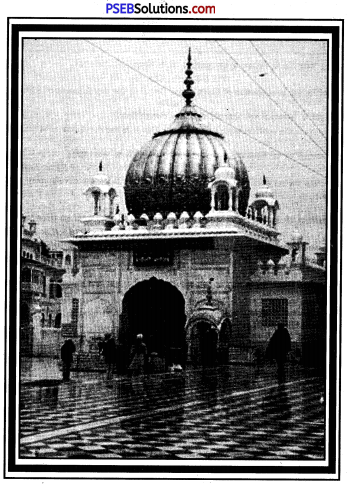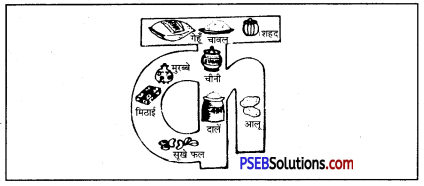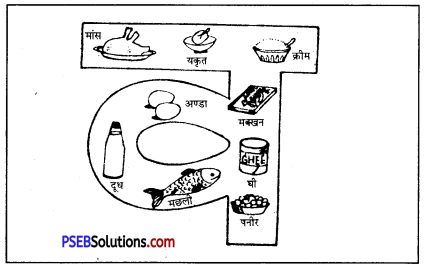Punjab State Board PSEB 12th Class History Book Solutions Chapter 5 गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी और गुरु रामदास जी के अधीन सिख धर्म का विकास Textbook Exercise Questions and Answers.
PSEB Solutions for Class 12 History Chapter 5 गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी और गुरु रामदास जी के अधीन सिख धर्म का विकास
निबंधात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)
गरु अंगद देव जी का प्रारंभिक जीवन (Early Career of Guru Angad Dev Ji)
प्रश्न 1.
गुरु अंगद देव जी के प्रारंभिक जीवन के बारे में आप क्या जानते हैं ? संक्षिप्त वर्णन करें। (What do you know about the early career of Guru Angad Dev Ji ? Explain briefly.)
उत्तर-
गुरु अंगद देव जी अथवा भाई लहणा जी सिखों के दूसरे गुरु थे। उनका गुरु काल 1539 ई० से 1552 ई० तक रहा। गुरु अंगद देव जी के प्रारंभिक जीवन का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है—
1.जन्म और माता-पिता (Birth and Parentage)-गुरु अंगद देव जी का पहला नाम भाई लहणा जी था। उनका जन्म 31 मार्च, 1504 ई० को मत्ते की सराय नामक गाँव में हुआ। आपके पिता जी का नाम फेरूमल था तथा वह क्षत्रिय परिवार से संबंध रखते थे। लहणा जी की माता जी का नाम सभराई देवी था। वह बहुत धार्मिक विचारों वाली स्त्री थी। भाई लहणा जी पर उनके धार्मिक विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा।
2. बचपन और विवाह (Childhood and Marriage)-भाई लहणा जी जब युवा हुए तो वह अपने पिता जी के कार्य में हाथ बंटाने लगें। 15 वर्ष के होने पर उनका विवाह उसी गाँव के निवासी श्री देवी चंद की सुपुत्री बीबी खीवी जी के साथ कर दिया गया। आपके घर दो पुत्रों दातू और दासू तथा दो पुत्रियों बीबी अमरो और बीबी अनोखी ने जन्म लिया। 1526 ई० में बाबर के पंजाब आक्रमण के समय फेरूमल जी अपने परिवार को लेकर खडूर साहिब नामक गाँव में आ गए। शीघ्र ही फेरूमल जी का देहांत हो गया, जिस कारण परिवार का समूचा उत्तरदायित्व भाई लहणा जी के कंधों पर आ पड़ा।
3. लहणा जी गुरु नानक देव जी के अनुयायी बने (Lehna Ji becomes the disciple of Guru Nanak Dev Ji)-भाई लहणा जी गुरु नानक देव जी से भेंट करने से पूर्व दुर्गा माता के भक्त थे। वह प्रतिवर्ष ज्वालामुखी (जिला काँगड़ा) देवी के दर्शन के लिए जाते थे। एक दिन खडूर साहिब में भाई जोधा जी के मुख से ‘आसा दी वार’ का पाठ सुना। यह पाठ सुनकर भाई लहणा जी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने गुरु नानक देव जी के दर्शन करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। आगामी वर्ष जब भाई लहणा जी ज्वालामुखी की यात्रा के लिए निकले तो वह मार्ग में करतारपुर में गुरु नानक देव जी के दर्शनों के लिए रुके। वह गुरु साहिब के महान् व्यक्तित्व और मधुर वाणी को सुनकर अत्यधिक प्रभावित हुए, इसलिए भाई लहणा जी गुरु नानक देव जी के अनुयायी बन गए और गुरु-चरणों में ही अपना जीवन व्यतीत करने का निर्णय किया।
4. गुरुगद्दी की प्राप्ति (Assumption of Guruship)-भाई लहणा जी ने पूर्ण श्रद्धा के साथ गुरु नानक साहिब की अथक सेवा की। भाई लहणा की सच्ची भक्ति और अपार प्रेम को देखकर गुरु नानक देव जी ने गुरुगद्दी उनके सुपुर्द करने का निर्णय किया। गुरु नानक साहिब ने एक नारियल और पाँच पैसे भाई लहणा जी के सम्मुख रखकर उन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। भाई लहणा को अंगद का नाम दिया गया। यह घटना 7 सितंबर, 1539 ई० की है। गुरु नानक साहिब द्वारा गुरु अंगद देव जी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करना सिख-इतिहास की एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण घटना मानी जाती है। यदि गुरु नानक साहिब अपने ज्योति-जोत समाने से पूर्व ऐसा न करते तो निस्संदेह सिख धर्म का अस्तित्व लुप्त हो जाना था। इसका कारण यह था कि सिख धर्म अभी अच्छी प्रकार से संगठित नहीं था। गुरु नानक देव जी के उपदेशों से जो लोग प्रभावित हुए थे उनकी संख्या दूसरे लोगों की अपेक्षा नगण्य थी। गुरु अंगद देव जी की नियुक्ति से सिख धर्म को एक निश्चित दिशा प्राप्त हुई तथा इसका आधार मज़बूत हुआ। जी० सी० नारंग का यह कहना पूर्णत: सही है,
“यदि गुरु नानक जी उत्तराधिकारी की नियुक्ति के बिना ही ज्योति जोत समा जाते तो आज सिख धर्म नहीं होना था।”1
गुरु अंगद देव जी के अधीन सिरव धर्म का विकास (Development of Sikhism Under Guru Angad Dev Ji)

प्रश्न 2.
सिख-धर्म के विकास में गुरु अंगद देव जी का क्या योगदान है ? वर्णन कीजिए ।
(What is the contribution of Guru Angad Dev Ji to the development of Sikhism ? Explain.)
अथवा
सिख धर्म के आरंभिक विकास में गुरु अंगद देव जी का क्या योगदान था ?
(What was the contribution of Guru Angad Dev Ji to the early development of Sikhism ?)
उत्तर-
गुरु अंगद देव जी 1539 ई० में सिखों के दूसरे गुरु बने। वह 1552 ई० तक गुरुगद्दी पर आसीन रहे। जिस समय गुरु अंगद देव जी गुरुगद्दी पर बैठे थे, उस समय सिख पंथ के सामने कई संकट विद्यमान थे। पहला सिख धर्म का हिंदू धर्म में विलीन हो जाने का खतरा था। दूसरा बड़ा ख़तरा उदासियों से था। सिख अनुयायियों की कम संख्या होने के कारण बहुत से सिख उदासी मत में शामिल होते जा रहे थे। गुरु अंगद साहिब ने अपने यत्नों से सिख पंथ के सम्मुख विद्यमान इन खतरों को दूर किया। गुरु अंगद साहिब ने सिख पंथ के विकास में जो महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई उसका वर्णन निम्नलिखित अनुसार है—
1. गुरमुखी को लोकप्रिय बनाना (Popularisation of Gurmukhi)-गुरुं अंगद देव जी ने गुरमुखी लिपि को लोकप्रिय बनाने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने इसके रूप में एक नया निखार लाया। अब इस लिपि को समझना सामान्य लोगों के लिए सरल हो गया। सिखों के सभी धार्मिक ग्रंथों की रचना इस लिपि में हुई। इस लिपि का नाम गुरमुखी [गुरुओं के मुख से निकली हुई] होने के कारण यह सिखों को गुरु के प्रति अपने कर्तव्य का स्मरण दिलाती रही। इस प्रकार यह लिपि सिखों की अपनी अलग पहचान बनाए रखने में सहायक सिद्ध हुई। इस लिपि के प्रसार के कारण सिखों में तीव्रता से विद्या का प्रसार भी होने लगा। एच० एस० भाटिया एवं एस० आर० बख्शी के अनुसार,
“गुरु अंगद देव जी ने सिखों को हिंदुओं एवं मुसलमानों से एक अलग भाषा दी तथा उन्हें यह अनुभव करवाया कि वे अलग लोग हैं।”2.
2. वाणी का संग्रह (Collection of Hymns)-गुरु अंगद देव जी का दूसरा महान् कार्य गुरु नानक देव जी की वाणी को एकत्रित करना था। यह वाणी एक स्थान पर न होकर अलग-अलग स्थानों पर बिखरी हुई थी। गुरु अंगद साहिब ने इस समूची वाणी को एकत्रित किया। सिख परंपराओं के अनुसार गुरु अंगद देव जी ने एक श्रद्धालु सिख भाई बाला जी को बुलाकर गुरु नानक साहिब के जीवन के संबंध में भाई पैड़ा मौखा जी से एक जन्म साखी लिखवाई। इस साखी को भाई बाला जी की जन्म साखी के नाम से जाना जाता है। कुछ विद्वान् इस तथ्य से सहमत नहीं हैं कि भाई बाला जी की जन्म साखी को गुरु अंगद देव जी के समय लिखा गया था। गुरु अंगद साहिब ने स्वयं ‘नानक’ के नाम से वाणी की रचना की। इस प्रकार गुरु अंगद देव जी ने वाणी के वास्तविक रूप को बिगड़ने से बचाया। दूसरा, इसने आदि ग्रंथ साहिब जी की तैयारी के लिए महत्त्वपूर्ण आधार तैयार किया।
3. लंगर प्रथा का विस्तार (Expansion of Langar System)-लंगर प्रथा के विकास का श्रेय गुरु अंगद देव जी को जाता है। लंगर का समूचा प्रबंध उनकी धर्म पत्नी बीबी खीवी जी करते थे। लंगर में सभी व्यक्ति बिना किसी ऊँच-नीच, जाति के भेदभाव के इकट्ठे मिलकर छकते थे। इस लंगर के लिए सारी माया गुरु जी के सिख देते थे। इस प्रथा के कारण सिखों में परस्पर सहयोग की भावना बढ़ी। इसने हिंदू समाज में फैली जाति-प्रथा पर कड़ा प्रहार किया। इस प्रकार इस संस्था ने सामाजिक एवं आर्थिक असमानता को दूर करने में प्रशंसनीय योगदान दिया। इसके कारण सिख धर्म की ख्याति दूर-दूर तक फैल गई। प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफैसर हरबंस सिंह का यह कहना पूर्णतः सही है, “सामाजिक क्रांति लाने में यह (लंगर) संस्था महत्त्वपूर्ण साधन सिद्ध हुई।”3
4. संगत का संगठन (Organisation of Sangat)-गुरु अंगद देव जी ने गुरु नानक देव जी द्वारा स्थापित संगत संस्था को भी संगठित किया। संगत से अभिप्राय था-एकत्रित होकर बैठना। संगत में सभी धर्मों के लोगस्त्री और पुरुष भाग ले सकते थे। यह संगत सुबह-शाम गुरु जी के उपदेशों को सुनने के लिए एकत्रित होती थी। इस संस्था ने सामाजिक असमानता को दूर करने तथा सिखों को संगठित करने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।
5. उदासी मत का खंडन (Denunciation of the Udasi Sect)-उदासी मत की स्थापना गुरु नानक देव जी के बड़े सुपुत्र बाबा श्रीचंद जी ने की थी। यह मत संन्यास अथवा त्याग के जीवन पर बल देता था। बहुत से सिख उदासी मत को मान्यता देने लग पड़े थे। ऐसी परिस्थितियों में यह संकट उत्पन्न हो गया था कि कहीं सिख गुरु नानक देव जी उपदेशों को भूल कर उदासी मत न अपना लें। अतः गुरु अंगद देव जी ने उदासी मत का कड़ा विरोध किया तथा स्पष्ट किया कि उदासी मत के सिद्धांत सिख धर्म के सिद्धांतों से.सर्वथा विपरीत हैं एवं जो सिख उदासी मत में विश्वास रखता है, वह सच्चा सिख नहीं हो सकता। इस प्रकार गुरु अंगद देव जी ने सिख मत के अस्तित्व को बनाए रखा।
6. शारीरिक शिक्षा (Physical Training)-गुरु अंगद देव जी यह मानते थे कि जिस प्रकार आत्मा की उन्नति के लिए नाम का जाप करना आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार शारीरिक स्वस्थता के लिए व्यायाम करना भी आवश्यक है। इस उद्देश्य के साथ गुरु जी ने खडूर साहिब में एक अखाड़ा बनवाया। यहाँ सिख प्रतिदिन प्रातःकाल मल्ल युद्ध तथा अन्य व्यायाम करते थे।
7. गोइंदवाल साहिब की स्थापना (Foundation of Goindwal Sahib)-गुरु अंगद देव जी ने खडूर साहिब के समीप गोइंदवाल साहिब नामक एक नए नगर की स्थापना की। इस नगर का निर्माण कार्य एक श्रद्धालु सेवक अमरदास की देख-रेख में 1546 ई० में आरंभ हुआ। यह नगर शीघ्र ही सिखों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान बन गया।
8. हुमायूँ से भेंट (Meeting with Humayun)-1540 ई० में मुग़ल बादशाह हुमायूँ शेरशाह सूरी के हाथों पराजय के पश्चात् पंजाब पहुँचा। वह खडूर साहिब गुरु अंगद देव जी से आशीर्वाद लेने के लिए पहुँचा। उस समय गुरु जी समाधि में लीन थे। हुमायूँ ने इसे अपना अपमान समझकर तलवार निकाल ली। उस समय गुरु जी ने अपनी आँखें खोली और हुमायूँ से कहा कि, “यह तलवार जिसका तुम मुझ पर प्रयोग करने लगे हो, वह तलवार शेरशाह सूरी के विरुद्ध लड़ाई करते समय कहाँ थी ?” ये शब्द सुनकर हुमायूँ अत्यंत लज्जित हुआ और उसने गुरु जी से क्षमा माँगी। गुरु जी ने हुमायूँ को आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हें कुछ समय प्रतीक्षा करने के पश्चात् राज्य सिंहासन प्राप्त होगा। गुरु जी की यह भविष्यवाणी सत्य निकली। इस भेंट के कारण सिखों तथा मुग़लों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हुए।
9. उत्तराधिकारी की नियुक्ति (Nomination of the Successor)-गुरु अंगद देव जी का सिख पंथ के विकास के लिए सबसे महान् कार्य अमरदास जी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करना था। गुरु अंगद देव जी ने काफ़ी सोच-समझकर इस उच्च पद के लिए अमरदास जी का चुनाव किया। गुरु जी ने अमरदास जी के सम्मुख एक नारियल और पाँच पैसे रखकर अपना शीश झुकाया। इस प्रकार अमरदास जी को सिखों का तीसरा गुरु नियुक्त किया गया। गुरु अंगद देव जी 29 मार्च, 1552 ई० को ज्योति जोत समा गए।
10. गुरु अंगद देव जी की सफलताओं का मूल्याँकन (Estimate of Guru Angad Dev Ji’s Achievements)-इस प्रकार हम देखते हैं कि गुरु अंगद देव जी ने अपनी गुरुगद्दी के काल में सिख पंथ के विकास में बहुत प्रशंसनीय योगदान दिया। गुरु जी ने गुरमुखी लिपि का प्रचार करके, गुरु नानक साहिब की वाणी को एकत्रित करके, संगत और पंगत संस्थाओं का विस्तार करके, सिख पंथ को उदासी मत से अलग करके, गोइंदवाल साहिब की स्थापना करके और अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करके सिख पंथ की नींव को और सुदृढ़ किया। गुरु अंगद देव जी की सफलताओं का मूल्यांकन करते हुए प्रसिद्ध इतिहासकार के० एस० दुग्गल का कहना है,
“यह आश्चर्य वाली बात है कि गुरु अंगद साहिब ने अपने अल्प समय के दौरान कितनी अधिक सफलता प्राप्त कर ली थी।”4
एक अन्य प्रसिद्ध इतिहासकार एस० एस० जौहर के अनुसार,
“गुरु अंगद देव जी का गुरु काल सिख पंथ के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण मोड़ था।”5
1. “Had Nanak died without a successor, there would have been no Sikhism today.” G.C. Narang, Transformation of Sikhism (New Delhi : 1989) p. 29.
2. “Guru Angad Dev Ji gave the Sikhs a written language different from the language of the Hindus and Muslims and thus made them realise that they were separate people.” H.S. Bhatia and S.R. Bakshi, Encyclopaedic History of the Sikhs and Sikhism (New Delhi : 1999) Vol. 1, p. 12.
3. “This served as an instrument of a far-reaching social revolution.” Prof. Harbans Singh, The Heritage of the Sikhs (Delhi : 1994) p. 31.
4. “It is amazing how much Guru Angad could achieve in the short time at his disposal.” K.S. Duggal, The Sikh Gurus : Their Lives and Teachings (New Delhi : 1993) p. 71.
5. “The pontificate of Guru Angad Dev is indeed a turning point in the history of Sikh faith.” S.S. Johar, Handbook on Sikhism (Delhi : 1979) p. 26.

प्रश्न 3.
गुरु अंगद देव जी के जीवन तथा सिख पंथ के विकास में उनके योगदान की चर्चा करें।
(Discuss the life and contribution of Guru Angad Dev Ji to the development of Sikhism.)
अथवा
गुरु अंगद देव जी के जीवन एवं सफलता का संक्षिप्त वर्णन करें। (Describe in brief, the life and achievements of Guru Angad Dev Ji.)
उत्तर-
गुरु अंगद देव जी 1539 ई० में सिखों के दूसरे गुरु बने। वह 1552 ई० तक गुरुगद्दी पर आसीन रहे। जिस समय गुरु अंगद देव जी गुरुगद्दी पर बैठे थे, उस समय सिख पंथ के सामने कई संकट विद्यमान थे। पहला सिख धर्म का हिंदू धर्म में विलीन हो जाने का खतरा था। दूसरा बड़ा ख़तरा उदासियों से था। सिख अनुयायियों की कम संख्या होने के कारण बहुत से सिख उदासी मत में शामिल होते जा रहे थे। गुरु अंगद साहिब ने अपने यत्नों से सिख पंथ के सम्मुख विद्यमान इन खतरों को दूर किया। गुरु अंगद साहिब ने सिख पंथ के विकास में जो महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई उसका वर्णन निम्नलिखित अनुसार है—
1. गुरमुखी को लोकप्रिय बनाना (Popularisation of Gurmukhi)-गुरुं अंगद देव जी ने गुरमुखी लिपि को लोकप्रिय बनाने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने इसके रूप में एक नया निखार लाया। अब इस लिपि को समझना सामान्य लोगों के लिए सरल हो गया। सिखों के सभी धार्मिक ग्रंथों की रचना इस लिपि में हुई। इस लिपि का नाम गुरमुखी [गुरुओं के मुख से निकली हुई] होने के कारण यह सिखों को गुरु के प्रति अपने कर्तव्य का स्मरण दिलाती रही। इस प्रकार यह लिपि सिखों की अपनी अलग पहचान बनाए रखने में सहायक सिद्ध हुई। इस लिपि के प्रसार के कारण सिखों में तीव्रता से विद्या का प्रसार भी होने लगा। एच० एस० भाटिया एवं एस० आर० बख्शी के अनुसार,
“गुरु अंगद देव जी ने सिखों को हिंदुओं एवं मुसलमानों से एक अलग भाषा दी तथा उन्हें यह अनुभव करवाया कि वे अलग लोग हैं।”2.
2. वाणी का संग्रह (Collection of Hymns)-गुरु अंगद देव जी का दूसरा महान् कार्य गुरु नानक देव जी की वाणी को एकत्रित करना था। यह वाणी एक स्थान पर न होकर अलग-अलग स्थानों पर बिखरी हुई थी। गुरु अंगद साहिब ने इस समूची वाणी को एकत्रित किया। सिख परंपराओं के अनुसार गुरु अंगद देव जी ने एक श्रद्धालु सिख भाई बाला जी को बुलाकर गुरु नानक साहिब के जीवन के संबंध में भाई पैड़ा मौखा जी से एक जन्म साखी लिखवाई। इस साखी को भाई बाला जी की जन्म साखी के नाम से जाना जाता है। कुछ विद्वान् इस तथ्य से सहमत नहीं हैं कि भाई बाला जी की जन्म साखी को गुरु अंगद देव जी के समय लिखा गया था। गुरु अंगद साहिब ने स्वयं ‘नानक’ के नाम से वाणी की रचना की। इस प्रकार गुरु अंगद देव जी ने वाणी के वास्तविक रूप को बिगड़ने से बचाया। दूसरा, इसने आदि ग्रंथ साहिब जी की तैयारी के लिए महत्त्वपूर्ण आधार तैयार किया।
3. लंगर प्रथा का विस्तार (Expansion of Langar System)-लंगर प्रथा के विकास का श्रेय गुरु अंगद देव जी को जाता है। लंगर का समूचा प्रबंध उनकी धर्म पत्नी बीबी खीवी जी करते थे। लंगर में सभी व्यक्ति बिना किसी ऊँच-नीच, जाति के भेदभाव के इकट्ठे मिलकर छकते थे। इस लंगर के लिए सारी माया गुरु जी के सिख देते थे। इस प्रथा के कारण सिखों में परस्पर सहयोग की भावना बढ़ी। इसने हिंदू समाज में फैली जाति-प्रथा पर कड़ा प्रहार किया। इस प्रकार इस संस्था ने सामाजिक एवं आर्थिक असमानता को दूर करने में प्रशंसनीय योगदान दिया। इसके कारण सिख धर्म की ख्याति दूर-दूर तक फैल गई। प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफैसर हरबंस सिंह का यह कहना पूर्णतः सही है, “सामाजिक क्रांति लाने में यह (लंगर) संस्था महत्त्वपूर्ण साधन सिद्ध हुई।”3
4. संगत का संगठन (Organisation of Sangat)-गुरु अंगद देव जी ने गुरु नानक देव जी द्वारा स्थापित संगत संस्था को भी संगठित किया। संगत से अभिप्राय था-एकत्रित होकर बैठना। संगत में सभी धर्मों के लोगस्त्री और पुरुष भाग ले सकते थे। यह संगत सुबह-शाम गुरु जी के उपदेशों को सुनने के लिए एकत्रित होती थी। इस संस्था ने सामाजिक असमानता को दूर करने तथा सिखों को संगठित करने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।
5. उदासी मत का खंडन (Denunciation of the Udasi Sect)-उदासी मत की स्थापना गुरु नानक देव जी के बड़े सुपुत्र बाबा श्रीचंद जी ने की थी। यह मत संन्यास अथवा त्याग के जीवन पर बल देता था। बहुत से सिख उदासी मत को मान्यता देने लग पड़े थे। ऐसी परिस्थितियों में यह संकट उत्पन्न हो गया था कि कहीं सिख गुरु नानक देव जी उपदेशों को भूल कर उदासी मत न अपना लें। अतः गुरु अंगद देव जी ने उदासी मत का कड़ा विरोध किया तथा स्पष्ट किया कि उदासी मत के सिद्धांत सिख धर्म के सिद्धांतों से.सर्वथा विपरीत हैं एवं जो सिख उदासी मत में विश्वास रखता है, वह सच्चा सिख नहीं हो सकता। इस प्रकार गुरु अंगद देव जी ने सिख मत के अस्तित्व को बनाए रखा।
6. शारीरिक शिक्षा (Physical Training)-गुरु अंगद देव जी यह मानते थे कि जिस प्रकार आत्मा की उन्नति के लिए नाम का जाप करना आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार शारीरिक स्वस्थता के लिए व्यायाम करना भी आवश्यक है। इस उद्देश्य के साथ गुरु जी ने खडूर साहिब में एक अखाड़ा बनवाया। यहाँ सिख प्रतिदिन प्रातःकाल मल्ल युद्ध तथा अन्य व्यायाम करते थे।
7. गोइंदवाल साहिब की स्थापना (Foundation of Goindwal Sahib)-गुरु अंगद देव जी ने खडूर साहिब के समीप गोइंदवाल साहिब नामक एक नए नगर की स्थापना की। इस नगर का निर्माण कार्य एक श्रद्धालु सेवक अमरदास की देख-रेख में 1546 ई० में आरंभ हुआ। यह नगर शीघ्र ही सिखों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान बन गया।
8. हुमायूँ से भेंट (Meeting with Humayun)-1540 ई० में मुग़ल बादशाह हुमायूँ शेरशाह सूरी के हाथों पराजय के पश्चात् पंजाब पहुँचा। वह खडूर साहिब गुरु अंगद देव जी से आशीर्वाद लेने के लिए पहुँचा। उस समय गुरु जी समाधि में लीन थे। हुमायूँ ने इसे अपना अपमान समझकर तलवार निकाल ली। उस समय गुरु जी ने अपनी आँखें खोली और हुमायूँ से कहा कि, “यह तलवार जिसका तुम मुझ पर प्रयोग करने लगे हो, वह तलवार शेरशाह सूरी के विरुद्ध लड़ाई करते समय कहाँ थी ?” ये शब्द सुनकर हुमायूँ अत्यंत लज्जित हुआ और उसने गुरु जी से क्षमा माँगी। गुरु जी ने हुमायूँ को आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हें कुछ समय प्रतीक्षा करने के पश्चात् राज्य सिंहासन प्राप्त होगा। गुरु जी की यह भविष्यवाणी सत्य निकली। इस भेंट के कारण सिखों तथा मुग़लों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हुए।
9. उत्तराधिकारी की नियुक्ति (Nomination of the Successor)-गुरु अंगद देव जी का सिख पंथ के विकास के लिए सबसे महान् कार्य अमरदास जी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करना था। गुरु अंगद देव जी ने काफ़ी सोच-समझकर इस उच्च पद के लिए अमरदास जी का चुनाव किया। गुरु जी ने अमरदास जी के सम्मुख एक नारियल और पाँच पैसे रखकर अपना शीश झुकाया। इस प्रकार अमरदास जी को सिखों का तीसरा गुरु नियुक्त किया गया। गुरु अंगद देव जी 29 मार्च, 1552 ई० को ज्योति जोत समा गए।
10. गुरु अंगद देव जी की सफलताओं का मूल्याँकन (Estimate of Guru Angad Dev Ji’s Achievements)-इस प्रकार हम देखते हैं कि गुरु अंगद देव जी ने अपनी गुरुगद्दी के काल में सिख पंथ के विकास में बहुत प्रशंसनीय योगदान दिया। गुरु जी ने गुरमुखी लिपि का प्रचार करके, गुरु नानक साहिब की वाणी को एकत्रित करके, संगत और पंगत संस्थाओं का विस्तार करके, सिख पंथ को उदासी मत से अलग करके, गोइंदवाल साहिब की स्थापना करके और अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करके सिख पंथ की नींव को और सुदृढ़ किया। गुरु अंगद देव जी की सफलताओं का मूल्यांकन करते हुए प्रसिद्ध इतिहासकार के० एस० दुग्गल का कहना है,
“यह आश्चर्य वाली बात है कि गुरु अंगद साहिब ने अपने अल्प समय के दौरान कितनी अधिक सफलता प्राप्त कर ली थी।”4
एक अन्य प्रसिद्ध इतिहासकार एस० एस० जौहर के अनुसार,
“गुरु अंगद देव जी का गुरु काल सिख पंथ के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण मोड़ था।”5
1. “Had Nanak died without a successor, there would have been no Sikhism today.” G.C. Narang, Transformation of Sikhism (New Delhi : 1989) p. 29.
2. “Guru Angad Dev Ji gave the Sikhs a written language different from the language of the Hindus and Muslims and thus made them realise that they were separate people.” H.S. Bhatia and S.R. Bakshi, Encyclopaedic History of the Sikhs and Sikhism (New Delhi : 1999) Vol. 1, p. 12.
3. “This served as an instrument of a far-reaching social revolution.” Prof. Harbans Singh, The Heritage of the Sikhs (Delhi : 1994) p. 31.
4. “It is amazing how much Guru Angad could achieve in the short time at his disposal.” K.S. Duggal, The Sikh Gurus : Their Lives and Teachings (New Delhi : 1993) p. 71.
5. “The pontificate of Guru Angad Dev is indeed a turning point in the history of Sikh faith.” S.S. Johar, Handbook on Sikhism (Delhi : 1979) p. 26.
गुरु अमरदास जी का आरंभिक जीवन एवं कठिनाइयाँ (Early Career and Difficulties of Guru Amar Das Ji)
प्रश्न 4.
गुरु अमरदास जी के आरंभिक जीवन एवं कठिनाइयों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। (Give a brief account of the early career and difficulties of Guru Amar Das Ji.)
उत्तर-
सिखों के तीसरे गुरु अमरदास जी के आरंभिक जीवन एवं कठिनाइयों का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है—
1. जन्म और माता-पिता (Birth and Parentage)-गुरु अमरदास जी का जन्म 5 मई, 1479 ई० को जिला अमृतसर के बासरके गाँव में हुआ। आपके पिता जी का नाम तेज भान था। वे भल्ला जाति के क्षत्रिय परिवार से संबंध रखते थे। गुरु जी के पिता जी काफ़ी धनवान थे। गुरु अमरदास जी की माता जी के नाम के संबंध में इतिहासकारों को कोई निश्चित जानकारी प्राप्त नहीं है।
2. बचपन और विवाह (Childhood and Marriage)-गुरु अमरदास जी बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। अमरदास जी ने बड़े होकर अपने पिता जी का काम संभाल लिया। क्योंकि आपके माता-पिता विष्णु के पुजारी थे, इसलिए आप भी वैष्णव मत के अनुयायी बन गए। 24 वर्ष की आयु में आपका विवाह देवी चंद की सुपुत्री, मनसा देवी से कर दिया गया। आपके घर दो पुत्रों-बाबा मोहन और बाबा मोहरी और दो पुत्रियों-बीबी दानी और बीबी भानी ने जन्म लिया।
3. गुरु अंगद देव जी का सिख बनना (To become Guru Angad Dev Ji Disciple)-एक बार जब अमरदास जी हरिद्वार यात्रा से लौट रहे थे तो वे मार्ग में एक साधु से मिले। उन दोनों ने इकट्टे भोजन किया। भोजन के पश्चात् उस साधु ने अमरदास जी से पूछा कि उनका गुरु कौन है ? अमरदास जी ने उत्तर दिया कि उनका गुरु कोई नहीं है। उस साधु ने कहा, “मैंने एक गुरु विहीन व्यक्ति के हाथों भोजन खाकर पाप किया है और अपना जन्म भ्रष्ट कर लिया है। मुझे प्रायश्चित्त के लिए पुनः गंगा में स्नान करना पड़ेगा।” इसका आपके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा तथा आपने गुरु धारण करने का दृढ़ निश्चय किया।
एक दिन अमरदास जी ने बीबी अमरो के मुख से गुरु नानक देव जी की वाणी सुनी तो बहुत प्रभावित हुए। इसलिए अमरदास जी ने गुरु अंगद देव जी के, दर्शन करने का निर्णय किया। वे गुरु जी के दर्शनों के लिए खडूर साहिब गए तथा उनके अनुयायी बन गए। उस समय गुरु जी की आयु 62 वर्ष की थी।
4. गुरुगद्दी की प्राप्ति (Assumption of Guruship)—अमरदास जी ने खडूर साहिब में रह कर 11 वर्षों तक गुरु अंगद देव जी की अथक सेवा की। वे प्रतिदिन गुरु साहिब जी के स्नान के लिए ब्यास नदी से, जो वहाँ से तीन मील की दूरी पर स्थित थी, पानी से भरा घड़ा अपने सिर पर उठाकर लाते तथा गुरु-घर में आई संगतों की तन-मन से सेवा करते। 1552 ई० की बात है कि अमरदास जी सदा की भाँति ब्यास से पानी लेकर लौट रहे थे। अंधेरा होने के कारण अमरदास जी को ठोकर लगी और वह गिर पड़े। साथ ही एक जुलाहे का घर था। आवाज़ सुनकर जुलाहा उठा और उसने पूछा कि कौन है। जुलाहिन ने कहा कि यह अवश्य अमरु निथावाँ (जिसके पास कोई स्थान न हो) होगा। धीरे-धीरे यह बात गुरु अंगद देव जी तक पहुँची। उन्होंने कहा कि आज से अमरदास ‘निथावाँ’ नहीं होगा, बल्कि निथावों को सहारा देगा। मार्च, 1552 ई० में गुरु अंगद साहिब ने अमरदास जी के सम्मुख एक नारियल और पाँच पैसे रखकर अपना शीश झुकाया और उन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इस प्रकार अमरदास जी 73 वर्ष की आयु में सिखों के तीसरे गुरु बने।
गुरु अमरदास जी की प्रारंभिक कठिनाइयाँ
(Guru Amar Das Ji’s Early Difficulties)
गुरुगद्दी प्राप्त करने के पश्चात् गुरु अमरदास जी, गुरु अंगद साहिब जी के आदेश पर खडूर साहिब से गोइंदवाल आ गए। यहाँ गुरु जी को आरंभ में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इनका संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित है—
1. दासू और दातू का विरोध (Opposition of Dasu and Datu)—गुरु अमरदास जी को अपने गुरुकाल के आरंभ में, गुरु अंगद देव जी के पुत्रों दासू और दातू के विरोध का सामना करना पड़ा। उन्होंने गुरु जी को गुरु मानने से इंकार कर दिया तथा स्वयं को असली उत्तराधिकारी घोषित किया। उनका कहना था कि कल तक हमारे घर का पानी भरने वाला आज गुरु कैसे बन सकता है। एक दिन दातू ने क्रोधित होकर गोइंदवाल साहिब जाकर भरे दरबार में गुरु जी को ठोकर मारी जिसके कारण वह गद्दी से नीचे गिर पड़े। इस पर भी गुरु साहिब ने बहुत ही नम्रता से दातू से क्षमा माँगी। इसके पश्चात् गुरु जी गोइंदवाल साहिब को छोड़कर अपने गाँव बासरके चले गए। सिख संगतों ने दातू को अपना गुरु मानने से इंकार कर दिया। अंततः निराश होकर वह खडूर साहिब लौट गया। बाबा बुड्डा जी तथा अन्य सिख संगतों के कहने पर गुरु अमरदास जी पुनः गोइंदवाल साहिब आ गए।
2. बाबा श्रीचंद का विरोध (Opposition of Baba Sri Chand)-बाबा श्रीचंद जी गुरु नानक जी के ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण गुरुगद्दी पर अपना अधिकार समझते थे। उन्होंने गुरु अंगद देव जी का विरोध इसलिए न किया क्योंकि उन्हें गुरुगद्दी गुरु नानक साहिब ने स्वयं सौंपी थी। परंतु गुरु अंगद देव जी के पश्चात् उन्होंने अपने पिता की गद्दी प्राप्त करने का प्रयत्न किया। बाबा श्रीचंद जी के अनेक समर्थक थे। गुरु अमरदास जी ने ऐसे समय में दृढ़ता से काम लेते हुए सिखों को स्पष्ट किया कि उदासी संप्रदाय के सिद्धांत गुरु नानक देव जी के उपदेशों के विपरीत हैं। उनके तर्कों से प्रभावित होकर सिखों ने बाबा श्रीचंद जी का साथ छोड़ दिया। इस प्रकार गुरु अमरदास जी ने सिखों को उदासी संप्रदाय से सदैव के लिए पृथक् कर दिया।
3. गोइंदवाल साहिब के मुसलमानों का विरोध (Opposition by the Muslims of Goindwal Sahib)–गोइंदवाल साहिब में गुरु अमरदास जी की बढ़ती हुई ख्याति देखकर वहाँ के मुसलमानों ने सिखों को तंग करना आरंभ कर दिया। वे सिखों का सामान चोरी कर लेते। वे सतलुज नदी से जल भर कर लाने वाले सिखों के घड़े पत्थर मार कर तोड़ देते थे। सिख इस संबंध में गुरु जी से शिकायत करते। अमरदास जी ने सिखों को शांत रहने का उपदेश दिया। एक बार गाँव में कुछ सशस्त्र व्यक्ति आ गए। इन मुसलमानों का उनसे किसी बात पर झगड़ा हो गया। उन्होंने बहुत से मुसलमानों को यमलोक पहुँचा दिया। लोग सोचने लगे कि मुसलमानों को परमात्मा की ओर से यह दंड मिला है। इस प्रकार उनका सिख धर्म में विश्वास और दृढ़ हो गया।
4. हिंदुओं द्वारा विरोध (Opposition by the Hindus)-इसका कारण यह था कि गुरु अमरदास जी के सामाजिक सुधारों से प्रभावित होकर बहुत से लोग सिख धर्म में शामिल होते जा रहे थे। सिख धर्म में ऊँच-नीच का भेदभाव नहीं किया जाता था। लंगर में सब एक साथ भोजन करते थे। इसके अतिरिक्त बाऊली का निर्माण होने से सिखों को एक अलग तीर्थ स्थान भी मिल गया था। गोइंदवाल साहिब के उच्च जातियों के हिंदू यह बात सहन न कर सके। उन्होंने अपने बादशाह अकबर के पास यह झूठी शिकायत की कि गुरु जी हिंदू धर्म के विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं। इस आरोप की जाँच के लिए अकबर ने गुरु साहिब को अपने दरबार में बुलाया। गुरु अमरदास जी ने अपने श्रद्धालु भाई जेठा जी को भेजा। भाई जेठा जी से मिलने के पश्चात् अकबर ने गुरु जी को निर्दोष घोषित किया। इससे सिख लहर को और उत्साह मिला।
गुरु अमरदास जी का आरंभिक जीवन एवं कठिनाइयाँ
(Early Career and Difficulties of Guru Amar Das Ji)

प्रश्न 4.
गुरु अमरदास जी के आरंभिक जीवन एवं कठिनाइयों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। (Give a brief account of the early career and difficulties of Guru Amar Das Ji.)
उत्तर-
सिखों के तीसरे गुरु अमरदास जी के आरंभिक जीवन एवं कठिनाइयों का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है—
1. जन्म और माता-पिता (Birth and Parentage)-गुरु अमरदास जी का जन्म 5 मई, 1479 ई० को जिला अमृतसर के बासरके गाँव में हुआ। आपके पिता जी का नाम तेज भान था। वे भल्ला जाति के क्षत्रिय परिवार से संबंध रखते थे। गुरु जी के पिता जी काफ़ी धनवान थे। गुरु अमरदास जी की माता जी के नाम के संबंध में इतिहासकारों को कोई निश्चित जानकारी प्राप्त नहीं है।
2. बचपन और विवाह (Childhood and Marriage)-गुरु अमरदास जी बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। अमरदास जी ने बड़े होकर अपने पिता जी का काम संभाल लिया। क्योंकि आपके माता-पिता विष्णु के पुजारी थे, इसलिए आप भी वैष्णव मत के अनुयायी बन गए। 24 वर्ष की आयु में आपका विवाह देवी चंद की सुपुत्री, मनसा देवी से कर दिया गया। आपके घर दो पुत्रों-बाबा मोहन और बाबा मोहरी और दो पुत्रियों-बीबी दानी और बीबी भानी ने जन्म लिया।
3. गुरु अंगद देव जी का सिख बनना (To become Guru Angad Dev Ji Disciple)-एक बार जब अमरदास जी हरिद्वार यात्रा से लौट रहे थे तो वे मार्ग में एक साधु से मिले। उन दोनों ने इकट्ठे भोजन किया। भोजन के पश्चात् उस साधु ने अमरदास जी से पूछा कि उनका गुरु कौन है २ अमरदास जी ने उत्तर दिया कि उनका गुरु कोई नहीं है। उस साधु ने कहा, “मैंने एक गुरु विहीन व्यक्ति के हाथों भोजन खाकर पाप किया है और अपना जन्म भ्रष्ट कर लिया है। मुझे प्रायश्चित्त के लिए पुनः गंगा में स्नान करना पड़ेगा।” इसका आपके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा तथा आपने गुरु धारण करने का दृढ़ निश्चय किया।
एक दिन अमरदास जी ने बीबी अमरो के मुख से गुरु नानक देव जी की वाणी सुनी तो बहुत प्रभावित हुए। इसलिए अमरदास जी ने गुरु अंगद देव जी के, दर्शन करने का निर्णय किया। वे गुरु जी के दर्शनों के लिए खडूर साहिब गए तथा उनके अनुयायी बन गए। उस समय गुरु जी की आयु 62 वर्ष की थी।
4. गुरुगद्दी की प्राप्ति (Assumption of Guruship)-अमरदास जी ने खडूर साहिब में रह कर 11 वर्षों तक गुरु अंगद देव जी की अथक सेवा की। वे प्रतिदिन गुरु साहिब जी के स्नान के लिए ब्यास नदी से, जो वहाँ से तीन मील की दूरी पर स्थित थी, पानी से भरा घड़ा अपने सिर पर उठाकर लाते तथा गुरु-घर में आई संगतों की तन-मन से सेवा करते। 1552 ई० की बात है कि अमरदास जी सदा की भाँति ब्यास से पानी लेकर लौट रहे थे। अंधेरा होने के कारण अमरदास जी को ठोकर लगी और वह गिर पड़े। साथ ही एक जुलाहे का घर था। आवाज़ सुनकर जुलाहा उठा और उसने पूछा कि कौन है। जुलाहिन ने कहा कि यह अवश्य अमरु निथावाँ (जिसके पास कोई स्थान न हो) होगा। धीरे-धीरे यह बात गुरु अंगद देव जी तक पहुँची। उन्होंने कहा कि आज से अमरदास ‘निथावाँ’ नहीं होगा, बल्कि निथावों को सहारा देगा। मार्च, 1552 ई० में गुरु अंगद साहिब ने अमरदास जी के सम्मुख एक नारियल और पाँच पैसे रखकर अपना शीश झुकाया और उन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इस प्रकार अमरदास जी 73 वर्ष की आयु में सिखों के तीसरे गुरु बने।
गुरु अमरदास जी की प्रारंभिक कठिनाइयाँ (Guru Amar Das Ji’s Early Difficulties)
गुरुगद्दी प्राप्त करने के पश्चात् गुरु अमरदास जी, गुरु अंगद साहिब जी के आदेश पर खडूर साहिब से गोइंदवाल आ गए। यहाँ गुरु जी को आरंभ में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इनका संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित है—
1. दासू और दातू का विरोध (Opposition of Dasu and Datu)-गुरु अमरदास जी को अपने गुरुकाल के आरंभ में, गुरु अंगद देव जी के पुत्रों दासू और दातू के विरोध का सामना करना पड़ा। उन्होंने गुरु जी को गुरु मानने से इंकार कर दिया तथा स्वयं को असली उत्तराधिकारी घोषित किया। उनका कहना था कि कल तक हमारे घर का पानी भरने वाला आज गुरु कैसे बन सकता है। एक दिन दातू ने क्रोधित होकर गोइंदवाल साहिब जाकर भरे दरबार में गुरु जी को ठोकर मारी जिसके कारण वह गद्दी से नीचे गिर पड़े। इस पर भी गुरु साहिब ने बहुत ही नम्रता से दातू से क्षमा माँगी। इसके पश्चात् गुरु जी गोइंदवाल साहिब को छोड़कर अपने गाँव बासरके चले गए। सिख संगतों ने दातू को अपना गुरु मानने से इंकार कर दिया। अंततः निराश होकर वह खडूर साहिब लौट गया। बाबा बुड्डा जी तथा अन्य सिख संगतों के कहने पर गुरु अमरदास जी पुनः गोइंदवाल साहिब आ गए।
2. बाबा श्रीचंद का विरोध (Opposition of Baba Sri Chand)-बाबा श्रीचंद जी गुरु नानक जी के ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण गुरुगद्दी पर अपना अधिकार समझते थे। उन्होंने गुरु अंगद देव जी का विरोध इसलिए न किया क्योंकि उन्हें गुरुगद्दी गुरु नानक साहिब ने स्वयं सौंपी थी। परंतु गुरु अंगद देव जी के पश्चात् उन्होंने अपने पिता की गद्दी प्राप्त करने का प्रयत्न किया। बाबा श्रीचंद जी के अनेक समर्थक थे। गुरु अमरदास जी ने ऐसे समय में दृढ़ता से काम लेते हुए सिखों को स्पष्ट किया कि उदासी संप्रदाय के सिद्धांत गुरु नानक देव जी के उपदेशों के विपरीत हैं। उनके तर्कों से प्रभावित होकर सिखों ने बाबा श्रीचंद जी का साथ छोड़ दिया। इस प्रकार गुरु अमरदास जी ने सिखों को उदासी संप्रदाय से सदैव के लिए पृथक् कर दिया।
3. गोइंदवाल साहिब के मुसलमानों का विरोध (Opposition by the Muslims of Goindwal Sahib)-गोइंदवाल साहिब में गुरु अमरदास जी की बढ़ती हुई ख्याति देखकर वहाँ के मुसलमानों ने सिखों को तंग करना आरंभ कर दिया। वे सिखों का सामान चोरी कर लेते। वे सतलुज नदी से जल भर कर लाने वाले सिखों के घड़े पत्थर मार कर तोड़ देते थे। सिख इस संबंध में गुरु जी से शिकायत करते। अमरदास जी ने सिखों को शांत रहने का उपदेश दिया। एक बार गाँव में कुछ सशस्त्र व्यक्ति आ गए। इन मुसलमानों का उनसे किसी बात पर झगड़ा हो गया। उन्होंने बहुत से मुसलमानों को यमलोक पहुँचा दिया। लोग सोचने लगे कि मुसलमानों को परमात्मा की ओर से यह दंड मिला है। इस प्रकार उनका सिख धर्म में विश्वास और दृढ़ हो गया।
4. हिंदुओं द्वारा विरोध (Opposition by the Hindus)—इसका कारण यह था कि गुरु अमरदास जी के सामाजिक सुधारों से प्रभावित होकर बहुत से लोग सिख धर्म में शामिल होते जा रहे थे। सिख धर्म में ऊँच-नीच का भेदभाव नहीं किया जाता था। लंगर में सब एक साथ भोजन करते थे। इसके अतिरिक्त बाऊली का निर्माण होने से सिखों को एक अलग तीर्थ स्थान भी मिल गया था। गोइंदवाल साहिब के उच्च जातियों के हिंदू यह बात सहन न कर सके। उन्होंने अपने बादशाह अकबर के पास यह झूठी शिकायत की कि गुरु जी हिंदू धर्म के विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं। इस आरोप की जाँच के लिए अकबर ने गुरु साहिब को अपने दरबार में बुलाया। गुरु अमरदास जी ने अपने श्रद्धालु भाई जेठा जी को भेजा। भाई जेठा जी से मिलने के पश्चात् अकबर ने गुरु जी को निर्दोष घोषित किया। इससे सिख लहर को और उत्साह मिला।
गुरु अमरदास जी के समय सिख धर्म का विकास (Development of Sikhism Under Guru Amar Das Ji)
प्रश्न 5.
सिख पंथ के विकास में गुरु अमरदास जी के योगदान का वर्णन करें।
(Describe the contribution of Guru Amar Das Ji in the development of Sikhism.)
अथवा
सिख धर्म के विकास में गुरु अमरदास जी ने क्या योगदान दिया? (What were the contribution of Guru Amar Das Ji in the development of Sikhism ?)
अथवा
गुरु अमरदास जी की सिख धर्म के विकास में की गई सेवाओं का वर्णन करो।
(Describe the services rendered by Guru Amar Das Ji for the development of Sikh Religion.) .
अथवा
गुरु अमरदास जी के सिख पंथ के संगठन तथा प्रसार के लिए किए गए कार्यों का संक्षिप्त वर्णन करें।
(Describe in brief the organisational development and spread of Sikhism by Guru Amar Das Ji.)
अथवा
सिख धर्म के संगठन एवं विकास के लिए गुरु अमरदास जी ने क्या-क्या कार्य किए ? .
(What were the measures taken by Guru Amar Das Ji for the consolidation and expansion of Sikhism ?)
उत्तर-
सिखों के तीसरे गुरु, गुरु अमरदास जी 1552 ई० से 1574 ई० तक गुरुगद्दी पर रहे। क्योंकि सिख धर्म अभी पूर्णतः संगठित नहीं हुआ था अतः गुरु जी ने इस दिशा में अनेक पग उठाए। गुरु अमरदास जी ने गुरु अंगद देव जी द्वारा आरंभ किए कार्यों को जारी रखा और बहुत-सी नई प्रथाओं तथा संस्थाओं की स्थापना की।—
1. गोइंदवाल साहिब में बाऊली का निर्माण (Construction of the Baoli at Goindwal Sahib)गुरु अमरदास जी का सिख पंथ के विकास की ओर पहला पग गोइंदवाल साहिब में एक बाऊली का निर्माण करना था। इस बाऊली का निर्माण कार्य 1552 ई० से 1559 ई० तक चला। इस बाऊली तक पहुँचने के लिए 84 सीढ़ियाँ बनाई गई थीं। गुरु जी ने यह घोषणा की कि जो यात्री प्रत्येक सीढ़ी पर शुद्ध हृदय से जपुजी साहिब का पाठ करेगा तथा पाठ के पश्चात् बाऊली में स्नान करेगा वह 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाएगा। बाऊली के निर्माण से सिख पंथ को एक पवित्र तीर्थ स्थान मिल गया। अब उन्हें हिंदुओं के तीर्थ स्थानों पर जाने की आवश्यकता न रही। इसके साथ ही वहाँ लोगों की पानी की समस्या भी हल हो गई। लोग बड़ी संख्या में गोइंदवाल साहिब आने लगे। इससे सिख धर्म के प्रसार को बल मिला। एच० एस० भाटिया तथा एस० आर० बक्शी के शब्दों में, “गुरु अमरदास जी का गुरुगद्दी काल, सिख आंदोलन के इतिहास में एक नया मोड़ प्रमाणित हुआ।”6
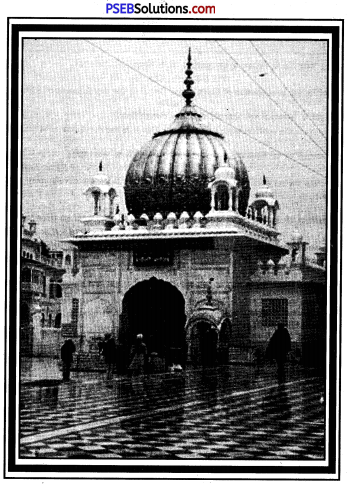
BAOLI SAHIB : GOINDWAL SAHIB
2. लंगर संस्था का विस्तार (Expansion of Langar Institution)—गुरु अमरदास जी ने, गुरु नानक देव जी द्वारा स्थापित लंगर संस्था का और विस्तार किया। गुरु जी ने यह घोषणा की कि कोई भी यात्री लंगर छके बिनां उनके दर्शन नहीं कर सकता। “पहले पंगत फिर संगत’ का नारा दिया गया। यहाँ तक कि मुग़ल बादशाह अकबर तथा हरिपुर के राजा ने भी गुरु जी से भेंट से पूर्व पंगत में बैठकर लंगर खाया था। इस लंगर में विभिन्न धर्मों और जातियों के लोग सम्मिलित होते थे। यह लंगर देर रात तक चलता रहता था। लंगर संस्था सिख धर्म के प्रचार में बड़ी सहायक प्रमाणित हुई । इससे जाति-प्रथा को गहरा आघात पहुँचा। इसने निम्न जातियों को समाज में एक नया सम्मान दिया। इससे सिखों में परस्पर भ्रातृत्व की भावना का विकास हुआ। डॉक्टर फौजा सिंह के अनुसार,
“इस (लंगर) संस्था ने जाति प्रथा को गहरी चोट पहुँचाई तथा सामाजिक एकता के लिए मार्ग साफ किया।”7
3. वाणी का संग्रह (Collection of Hymns)—गुरु अमरदास जी का दूसरा महत्त्वपूर्ण कार्य गुरु नानक देव जी तथा गुरु अंगद देव जी की वाणी का संग्रह करना था। गुरु साहिब ने स्वयं 907 शब्दों की रचना की। ऐसा करने से आदि ग्रंथ साहिब जी के संकलन के लिए आधार तैयार हो गया।
4. मंजी प्रथा (Manji System)-मंजी प्रथा की स्थापना गुरु अमरदास जी के सबसे महत्त्वपूर्ण कार्यों में से एक थी। सिखों की संख्या में वृद्धि के कारण गुरु साहिब के लिए प्रत्येक सिख तक पहुँच पाना संभव नहीं था। उन्होंने अपने उपदेश दूर-दूर के क्षेत्रों में रहने वाले सिखों तक पहुँचाने के लिए 22 मंजियों की स्थापना की। इन मंजियों की स्थापना एक ही समय पर नहीं बल्कि अलग-अलग समय पर की गई। प्रत्येक मंजी के मुखिया को मंजीदार कहते थे। ये मंजीदार अधिक-से-अधिक लोगों को सिख धर्म में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करते थे। क्योंकि मंजीदार मंजी (चारपाई) पर बैठकर प्रचार करते थे, इसलिए यह प्रथा इतिहास में मंजी प्रथा के नाम से विख्यात हुई। मंजी प्रथा की स्थापना के परिणामस्वरूप सिख धर्म की प्रसिद्धि दूर-दूर तक फैल गई। डॉक्टर डी० एस० ढिल्लों के अनुसार,
“मंजी प्रथा की स्थापना ने सिख पंथ की प्रसार गतिविधियों में उल्लेखनीय योगदान दिया।”8
5. उदासी संप्रदाय का खंडन (Denunciation of the Udasi Sect)-गुरु अमरदास जी के समय में उदासी संप्रदाय सिख संप्रदाय के अस्तित्व के लिए खतरा बना हुआ था। बहुत से सिख बाबा श्रीचंद जी से प्रभावित होकर उदासी संप्रदाय में सम्मिलित होने लगे थे। ऐसे समय गुरु अमरदास जी ने बड़े साहस से काम लिया। उन्होंने सिखों को समझाया कि सिख धर्म उदासी मत से बिल्कुल अलग है। उनका कहना था कि सिख धर्म गृहस्थ मार्ग अपनाने तथा संसार में रह कर श्रम करने की शिक्षा देता है। दूसरी ओर उदासी मत मुक्ति की खोज में वनों में मारेमारे फिरने की शिक्षा देता है। गुरु साहिब के आदेश पर सिखों ने उदासी मत से सदैव के लिए अपने संबंध तोड़ लिए। इस प्रकार गुरु अमरदास जी ने सिख धर्म को हिंदू धर्म में विलीन होने से बचा लिया।
6. सामाजिक सुधार (Social Reforms)-गुरु अमरदास जी एक महान् समाज सुधारक थे। समाज में जाति बंधन कठोर रूप धारण कर चुका था। उस समय निम्न जाति के लोगों पर बहुत अत्याचार होते थे। गुरु अमरदास जी ने जाति प्रथा का ज़ोरदार शब्दों में खंडन किया। उन्होंने जाति का अहंकार करने वाले को मूर्ख तथा गंवार बताया। गुरु अमरदास जी ने समाज में प्रचलित सती-प्रथा का डट कर विरोध किया। गुरु जी का कथन था—
सतीआ एहि न आखीअनि जो मड़ियाँ लग जलनि॥
सतीआ सेई नानका जो विरहा चोट मरनि॥
अर्थात् उस स्त्री को सती नहीं कहा जा सकता जो पति की चिता में जल कर मर जाती है। वास्तव में सती वही है जो पति के बिछोह को सहन न करती हुई विरह के आघात से मर जाए। गुरु अमरदास जी ने बाल-विवाह तथा पर्दा प्रथा का विरोध किया। उन्होंने विधवा विवाह तथा अंतर्जातीय विवाह का समर्थन किया। उन्होंने मादक द्रव्यों के सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके अतिरिक्त गुरु अमरदास जी ने सिखों के जन्म, विवाह तथा मृत्यु के अवसरों के लिए विशेष रस्में प्रचलित की। ये रस्में बिल्कुल सरल थीं। संक्षेप में गुरु अमरदास जी ने एक आदर्श-समाज का निर्माण किया।
7. अकबर का गोइंदवाल साहिब आगमन (Akbar’s visit to Goindwal Sahib)-मुग़ल सम्राट अकबर 1568 ई० में गुरु साहिब के दर्शनों के लिए गोइंदवाल साहिब आया। उसने गुरु अमरदास जी को मिलने से पूर्व संगत में बैठ कर लंगर खाया। वह गुरु जी के व्यक्तित्व और लंगर व्यवस्था से बहुत प्रभावित हुआ। उसने कुछ गाँवों की जागीर देने की गुरु जी को पेशकश की। परंतु गुरु जी ने यह जागीर लेने से इंकार कर दिया। अकबर की इस यात्रा का लोगों के दिल पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। वे भारी संख्या में सिख धर्म में सम्मिलित होने लगे। इस कारण सिख धर्म और भी लोकप्रिय हो गया।
8. उत्तराधिकारी की नियुक्ति (Nomination of the Successor)-गुरु अमरदास जी ने 1574 ई० में अपने दामाद भाई जेठा जी की नम्रता तथा सेवा भाव से प्रभावित होकर उन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने का निर्णय किया। गुरु जी ने न केवल भाई जेठा जी को अपना उत्तराधिकारी ही बनाया अपितु गुरुगद्दी उनके वंश में रहने का आशीर्वाद भी दिया। गुरु अमरदास जी 1 सितंबर, 1574 ई० को गोइंदवाल साहिब में ज्योति-जोत समा गए।
9. गुरु अमरदास जी की सफलताओं का मूल्याँकन (Estimate of Guru Amar Das Ji’s Achievements)-गुरु अमरदास जी के नेतृत्व में सिख पंथ ने महत्त्वपूर्ण विकास किया। गुरु जी ने गोइंदवाल साहिब में बाऊली का निर्माण करके, लंगर प्रथा का विस्तार करके, पूर्व गुरुओं की वाणी को एकत्र करके, सामाजिक कुरीतियों का विरोध करके, उदासी संप्रदाय का खंडन करके सिख पंथ के इतिहास में एक मील पत्थर का काम किया। प्रसिद्ध इतिहासकार संगत सिंह के अनुसार,
“गुरु अमरदास जी के अधीन सिख पंथ का तीव्र विकास हुआ।”9
एक अन्य प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर डी० एस० ढिल्लों के अनुसार,
“सिख पंथ के विकास में गुरु अमरदास जी ने प्रशंसनीय योगदान दिया।”10
6. “The pontificate of Guru Amar Das Ji is thus a turning point in the history of the Sikh movement.” H. S. Bhatia and S.R. Bakshi, Encyclopaedic History of the Sikhs and Sikhism (New Delhi : 1999) Vol. 1, p. 15.
7. “This institution gave a shattering blow to the rigidity of the caste system and paved the way for social equality.” Dr. Fauja Singh, Perspectives on Guru Amar Das (Patiala : 1982) p. 25.
8. “The establishment of Manji System gave a big thrust to the missionary activities of the Sikhs.” Dr. D.S. Dhillon, Sikhism : Origin and Development (New Delhi : 1988) p. 207.
9. “Under Guru Amar Das, Sikhism made rapid strides.” Sangat Singh, The Sikhs in History (New Delhi : 1996) p. 29. 10. “Guru Amar Das’s contribution to the growth of the Sikh Panth was great.” Dr. D.S. Dhillon, Sikhism : Origin and Development (New Delhi : 1988) p. 94.

गुरु अमरदास जी के सामाजिक सुधार (Social Reforms of Guru Amar Das Ji)
प्रश्न 6.
गुरु अमरदास जी के सामाजिक सुधारों का मूल्यांकन करें। (Examine the social reforms of Guru Amar Das Ji.)
अथवा
“गुरु अमरदास जी एक महान् समाज सुधारक थे।” बताएँ।
(“Guru Amar Das Ji was a great social reformer.” Discuss.)
उत्तर-
गुरु अमरदास जी का नाम सिख इतिहास में एक महान् समाज सुधारक के रूप में भी प्रसिद्ध है। वह सिखों की सामाजिक संरचना को एक नया रूप देना चाहते थे। वह सिखों को तात्कालीन समाज के जटिल नियमों से मुक्त करना चाहते थे ताकि उनमें आपसी भ्रातृत्व स्थापित हो। गुरु अमरदास जी के सामाजिक सुधार का संक्षिप्त वर्णन निम्न अनुसार है—
1. जातीय भेद-भाव तथा छुआ-छूत का खंडन (Denunciation of Caste Distinctions and Untouchability)—गुरु अमरदास जी ने जातीय एवं छुआ-छूत की प्रथाओं का जोरदार शब्दों में खंडन किया। उनका कथन था कि जाति पर अभिमान करने वाले मूर्ख तथा गंवार हैं। उन्होंने संगतों को यह हुक्म दिया कि जो कोई उनके दर्शन करना चाहता है उसे पहले पंगत में लंगर छकना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त गुरु जी ने कुछ कुएँ खुदवाए। इन कुओं से प्रत्येक जाति के लोगों को पानी लेने का अधिकार था। इस प्रकार गुरु अमरदास जी ने आपसी भ्रातृत्व का प्रचार किया।
2. लड़कियों की हत्या का खंडन (Denunciation of Female Infanticide)-उस समय लड़कियों के जन्म को अशुभ माना जाता था। समाज में लड़कियों के जन्म लेते ही उन्हें मार दिया जाता था। गुरु अमरदास जी ने इस कुप्रथा का जोरदार शब्दों में खंडन किया। उनका कथन था कि जो व्यक्ति ऐसा करता है वह घोर पाप का सहभागी बनता है । उन्होंने सिखों को इस अपराध से दूर रहने का उपदेश दिया।
3. बाल विवाह का खंडन (Denunciation of Child Marriage)-उस समय समाज में प्रचलित परंपराओं के अनुसार लड़कियों का विवाह छोटी आयु में ही कर दिया जाता था। इस कारण समाज में स्त्रियों की दशा बहुत दयनीय हो गई थी। गुरु अमरदास जी ने बाल विवाह के विरुद्ध प्रचार किया।
4. सती प्रथा का खंडन (Denunciation of Sati System) उस समय समाज में प्रचलित कुप्रथाओं में से सबसे घृणा योग्य कुप्रथा सती प्रथा की थी। इस अमानवीय प्रथा के अनुसार यदि किसी दुर्भाग्यशाली स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसे जबरन पति की चिता के साथ जीवित जला दिया जाता था। गुरु अमरदास जी ने शताब्दियों से चली आ रही इस कुप्रथा के विरुद्ध एक ज़ोरदार अभियान चलाया। गुरु साहिब का कथन था
सतीआ एहि न आखीअनि जो मड़ियाँ लग जलनि॥
सतीआ सेई नानका जो विरहा चोटि मरनि॥
भाव उस स्त्री को सती नहीं कहा जा सकता जो पति की चिता में जल कर मर जाती है। वास्तव में सती तो वह है जो अपने पति के वियोग की पीड़ा में प्राण त्याग दे।
5. पर्दा प्रथा का खंडन (Denunciation of Purdah System)-उसं समय समाज में पर्दा प्रथा का प्रचलन भी काफ़ी बढ़ गया था। यह प्रथा स्त्रियों के शारीरिक तथा मानसिक विकास में एक बड़ी बाधा थी। इसलिए गुरु अमरदास जी ने इस प्रथा की जोरदार शब्दों में आलोचना की। उन्होंने यह आदेश दिया कि संगत अथवा लंगर में सेवा करते समय कोई भी स्त्री पर्दा न करे।
6. नशीली वस्तुओं का विरोध (Prohibition of Intoxicants)-उस समय समाज में शराब तथा अन्य नशीले पदार्थों का प्रयोग बहुत बढ़ गया था। इस कारण समाज का दिन-प्रतिदिन नैतिक पतन होता जा रहा था। इसलिए गुरु अमरदास जी ने इन नशों के विरुद्ध जोरदार प्रचार किया। उनका कथन था कि जो मनुष्य शराब पीता है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वह अपने-पराए का भेद भूल जाता है। मनुष्य को ऐसी झूठी शराब नहीं पीनी चाहिए, जिस कारण वह परमात्मा को भूल जाए।
7. विधवा विवाह के पक्ष में (Favoured Widow Marriage)—जो स्त्रियाँ सती होने से बच जाती थीं, उन्हें सदैव विधवा का जीवन व्यतीत करना पड़ता था। समाज की ओर से विधवा विवाह पर प्रतिबंध लगा हुआ थां। विधवा का जीवन नरक के समान था। गुरु अमरदास जी ने इस प्रथा को खेदजनक बताया। उनका कथन था कि हमें विधवा का पूरा सम्मान करना चाहिए। गुरु जी ने बाल विधवा के पुनर्विवाह के पक्ष में प्रचार किया।
8. जन्म, विवाह तथा मृत्यु के समय के नवीन नियम (New Ceremonies related to Birth, Marriage and Death)-उस समय समाज में जन्म, विवाह तथा मृत्यु से संबंधित जो रीति-रिवाज प्रचलित थे, वे बहुत जटिल थे। गुरु साहिब ने सिखों के लिए इन अवसरों पर विशेष नियम बनाए। ये नियम पूर्णतः सरल थे। गुरु साहिब ने जन्म, विवाह तथा अन्य अवसरों पर गाने के लिए अनंदु साहिब की रचना की। इसमें 40 पौड़ियाँ हैं। इसके अतिरिक्त विवाह समय लावाँ की नई प्रथा आरंभ की गई।।
9. त्योहार मनाने का नवीन ढंग (New Mode of Celebrating Festivals)—गुरु अमरदास जी ने सिखों को वैसाखी, माघी तथा दीवाली के त्योहारों को नवीन ढंग से मनाने के लिए कहा। इन तीनों त्योहारों के अवसरों पर बड़ी संख्या में सिख गोइंदवाल साहिब पहुँचते थे। गुरु साहिब का यह पग सिख पंथ के प्रचार में बड़ा सहायक सिद्ध हुआ। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर बी० एस० निझर के अनुसार,
“गुरु अमरदास जी द्वारा आरंभ किए गए इन सामाजिक सुधारों को सिख पंथ के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण मोड़ लाने वाले समझे जाने चाहिएँ।”11
प्रश्न 7.
गुरु अमरदास जी के जीवन एवं सफलताओं का वर्णन कीजिए। (Describe the life and achievements of Guru Amar Das Ji.)
अथवा
गुरु अमरदास जी को गुरुगद्दी पर विराजमान होते समय किन-किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा ? सिख मत के संगठन और विस्तार के लिए उनके द्वारा उठाए गए कदमों की चर्चा कीजिए ।
(What were the difficulties faced by Guru Amar Das Ji at the time of his accession ? Discuss the steps taken by him to consolidate and expand Sikhism.)
उत्तर-
इस प्रश्न के उत्तर के लिए विद्यार्थी कृपया प्रश्न 5 एवं 6 का उत्तर संयुक्त रूप से लिखें।

प्रश्न 8.
1539 ई० से 1574 ई० तक सिख पंथ के विकास की चर्चा करें। (Examine the development of Sikhism from 1539 to 1574 A.D.)
अथवा
सिख धर्म के विकास में गुरु अंगद देव जी तथा गुरु अमरदास जी के योगदान का वर्णन करें।
(Describe the contribution of Guru Angad Dev Ji and Guru Amar Das Ji in the development of Sikhism.)
उत्तर-
सिखों के तीसरे गुरु, गुरु अमरदास जी 1552 ई० से 1574 ई० तक गुरुगद्दी पर रहे। क्योंकि सिख धर्म अभी पूर्णतः संगठित नहीं हुआ था अतः गुरु जी ने इस दिशा में अनेक पग उठाए। गुरु अमरदास जी ने गुरु अंगद देव जी द्वारा आरंभ किए कार्यों को जारी रखा और बहुत-सी नई प्रथाओं तथा संस्थाओं की स्थापना की।—
1. गोइंदवाल साहिब में बाऊली का निर्माण (Construction of the Baoli at Goindwal Sahib)गुरु अमरदास जी का सिख पंथ के विकास की ओर पहला पग गोइंदवाल साहिब में एक बाऊली का निर्माण करना था। इस बाऊली का निर्माण कार्य 1552 ई० से 1559 ई० तक चला। इस बाऊली तक पहुँचने के लिए 84 सीढ़ियाँ बनाई गई थीं। गुरु जी ने यह घोषणा की कि जो यात्री प्रत्येक सीढ़ी पर शुद्ध हृदय से जपुजी साहिब का पाठ करेगा तथा पाठ के पश्चात् बाऊली में स्नान करेगा वह 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाएगा। बाऊली के निर्माण से सिख पंथ को एक पवित्र तीर्थ स्थान मिल गया। अब उन्हें हिंदुओं के तीर्थ स्थानों पर जाने की आवश्यकता न रही। इसके साथ ही वहाँ लोगों की पानी की समस्या भी हल हो गई। लोग बड़ी संख्या में गोइंदवाल साहिब आने लगे। इससे सिख धर्म के प्रसार को बल मिला। एच० एस० भाटिया तथा एस० आर० बक्शी के शब्दों में, “गुरु अमरदास जी का गुरुगद्दी काल, सिख आंदोलन के इतिहास में एक नया मोड़ प्रमाणित हुआ।”6
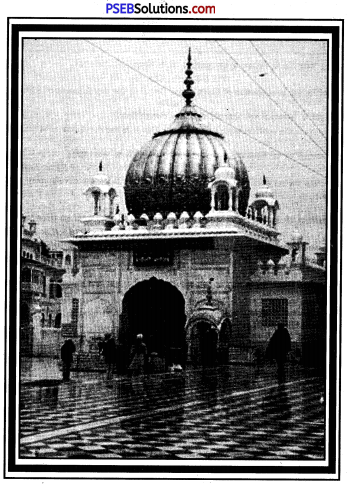
BAOLI SAHIB : GOINDWAL SAHIB
2. लंगर संस्था का विस्तार (Expansion of Langar Institution)—गुरु अमरदास जी ने, गुरु नानक देव जी द्वारा स्थापित लंगर संस्था का और विस्तार किया। गुरु जी ने यह घोषणा की कि कोई भी यात्री लंगर छके बिनां उनके दर्शन नहीं कर सकता। “पहले पंगत फिर संगत’ का नारा दिया गया। यहाँ तक कि मुग़ल बादशाह अकबर तथा हरिपुर के राजा ने भी गुरु जी से भेंट से पूर्व पंगत में बैठकर लंगर खाया था। इस लंगर में विभिन्न धर्मों और जातियों के लोग सम्मिलित होते थे। यह लंगर देर रात तक चलता रहता था। लंगर संस्था सिख धर्म के प्रचार में बड़ी सहायक प्रमाणित हुई । इससे जाति-प्रथा को गहरा आघात पहुँचा। इसने निम्न जातियों को समाज में एक नया सम्मान दिया। इससे सिखों में परस्पर भ्रातृत्व की भावना का विकास हुआ। डॉक्टर फौजा सिंह के अनुसार,
“इस (लंगर) संस्था ने जाति प्रथा को गहरी चोट पहुँचाई तथा सामाजिक एकता के लिए मार्ग साफ किया।”7
3. वाणी का संग्रह (Collection of Hymns)—गुरु अमरदास जी का दूसरा महत्त्वपूर्ण कार्य गुरु नानक देव जी तथा गुरु अंगद देव जी की वाणी का संग्रह करना था। गुरु साहिब ने स्वयं 907 शब्दों की रचना की। ऐसा करने से आदि ग्रंथ साहिब जी के संकलन के लिए आधार तैयार हो गया।
4. मंजी प्रथा (Manji System)-मंजी प्रथा की स्थापना गुरु अमरदास जी के सबसे महत्त्वपूर्ण कार्यों में से एक थी। सिखों की संख्या में वृद्धि के कारण गुरु साहिब के लिए प्रत्येक सिख तक पहुँच पाना संभव नहीं था। उन्होंने अपने उपदेश दूर-दूर के क्षेत्रों में रहने वाले सिखों तक पहुँचाने के लिए 22 मंजियों की स्थापना की। इन मंजियों की स्थापना एक ही समय पर नहीं बल्कि अलग-अलग समय पर की गई। प्रत्येक मंजी के मुखिया को मंजीदार कहते थे। ये मंजीदार अधिक-से-अधिक लोगों को सिख धर्म में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करते थे। क्योंकि मंजीदार मंजी (चारपाई) पर बैठकर प्रचार करते थे, इसलिए यह प्रथा इतिहास में मंजी प्रथा के नाम से विख्यात हुई। मंजी प्रथा की स्थापना के परिणामस्वरूप सिख धर्म की प्रसिद्धि दूर-दूर तक फैल गई। डॉक्टर डी० एस० ढिल्लों के अनुसार,
“मंजी प्रथा की स्थापना ने सिख पंथ की प्रसार गतिविधियों में उल्लेखनीय योगदान दिया।”8
5. उदासी संप्रदाय का खंडन (Denunciation of the Udasi Sect)-गुरु अमरदास जी के समय में उदासी संप्रदाय सिख संप्रदाय के अस्तित्व के लिए खतरा बना हुआ था। बहुत से सिख बाबा श्रीचंद जी से प्रभावित होकर उदासी संप्रदाय में सम्मिलित होने लगे थे। ऐसे समय गुरु अमरदास जी ने बड़े साहस से काम लिया। उन्होंने सिखों को समझाया कि सिख धर्म उदासी मत से बिल्कुल अलग है। उनका कहना था कि सिख धर्म गृहस्थ मार्ग अपनाने तथा संसार में रह कर श्रम करने की शिक्षा देता है। दूसरी ओर उदासी मत मुक्ति की खोज में वनों में मारेमारे फिरने की शिक्षा देता है। गुरु साहिब के आदेश पर सिखों ने उदासी मत से सदैव के लिए अपने संबंध तोड़ लिए। इस प्रकार गुरु अमरदास जी ने सिख धर्म को हिंदू धर्म में विलीन होने से बचा लिया।
6. सामाजिक सुधार (Social Reforms)-गुरु अमरदास जी एक महान् समाज सुधारक थे। समाज में जाति बंधन कठोर रूप धारण कर चुका था। उस समय निम्न जाति के लोगों पर बहुत अत्याचार होते थे। गुरु अमरदास जी ने जाति प्रथा का ज़ोरदार शब्दों में खंडन किया। उन्होंने जाति का अहंकार करने वाले को मूर्ख तथा गंवार बताया। गुरु अमरदास जी ने समाज में प्रचलित सती-प्रथा का डट कर विरोध किया। गुरु जी का कथन था—
सतीआ एहि न आखीअनि जो मड़ियाँ लग जलनि॥
सतीआ सेई नानका जो विरहा चोट मरनि॥
अर्थात् उस स्त्री को सती नहीं कहा जा सकता जो पति की चिता में जल कर मर जाती है। वास्तव में सती वही है जो पति के बिछोह को सहन न करती हुई विरह के आघात से मर जाए। गुरु अमरदास जी ने बाल-विवाह तथा पर्दा प्रथा का विरोध किया। उन्होंने विधवा विवाह तथा अंतर्जातीय विवाह का समर्थन किया। उन्होंने मादक द्रव्यों के सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके अतिरिक्त गुरु अमरदास जी ने सिखों के जन्म, विवाह तथा मृत्यु के अवसरों के लिए विशेष रस्में प्रचलित की। ये रस्में बिल्कुल सरल थीं। संक्षेप में गुरु अमरदास जी ने एक आदर्श-समाज का निर्माण किया।
7. अकबर का गोइंदवाल साहिब आगमन (Akbar’s visit to Goindwal Sahib)-मुग़ल सम्राट अकबर 1568 ई० में गुरु साहिब के दर्शनों के लिए गोइंदवाल साहिब आया। उसने गुरु अमरदास जी को मिलने से पूर्व संगत में बैठ कर लंगर खाया। वह गुरु जी के व्यक्तित्व और लंगर व्यवस्था से बहुत प्रभावित हुआ। उसने कुछ गाँवों की जागीर देने की गुरु जी को पेशकश की। परंतु गुरु जी ने यह जागीर लेने से इंकार कर दिया। अकबर की इस यात्रा का लोगों के दिल पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। वे भारी संख्या में सिख धर्म में सम्मिलित होने लगे। इस कारण सिख धर्म और भी लोकप्रिय हो गया।
8. उत्तराधिकारी की नियुक्ति (Nomination of the Successor)-गुरु अमरदास जी ने 1574 ई० में अपने दामाद भाई जेठा जी की नम्रता तथा सेवा भाव से प्रभावित होकर उन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने का निर्णय किया। गुरु जी ने न केवल भाई जेठा जी को अपना उत्तराधिकारी ही बनाया अपितु गुरुगद्दी उनके वंश में रहने का आशीर्वाद भी दिया। गुरु अमरदास जी 1 सितंबर, 1574 ई० को गोइंदवाल साहिब में ज्योति-जोत समा गए।
9. गुरु अमरदास जी की सफलताओं का मूल्याँकन (Estimate of Guru Amar Das Ji’s Achievements)-गुरु अमरदास जी के नेतृत्व में सिख पंथ ने महत्त्वपूर्ण विकास किया। गुरु जी ने गोइंदवाल साहिब में बाऊली का निर्माण करके, लंगर प्रथा का विस्तार करके, पूर्व गुरुओं की वाणी को एकत्र करके, सामाजिक कुरीतियों का विरोध करके, उदासी संप्रदाय का खंडन करके सिख पंथ के इतिहास में एक मील पत्थर का काम किया। प्रसिद्ध इतिहासकार संगत सिंह के अनुसार,
“गुरु अमरदास जी के अधीन सिख पंथ का तीव्र विकास हुआ।”9
एक अन्य प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर डी० एस० ढिल्लों के अनुसार,
“सिख पंथ के विकास में गुरु अमरदास जी ने प्रशंसनीय योगदान दिया।”10
6. “The pontificate of Guru Amar Das Ji is thus a turning point in the history of the Sikh movement.” H. S. Bhatia and S.R. Bakshi, Encyclopaedic History of the Sikhs and Sikhism (New Delhi : 1999) Vol. 1, p. 15.
7. “This institution gave a shattering blow to the rigidity of the caste system and paved the way for social equality.” Dr. Fauja Singh, Perspectives on Guru Amar Das (Patiala : 1982) p. 25.
8. “The establishment of Manji System gave a big thrust to the missionary activities of the Sikhs.” Dr. D.S. Dhillon, Sikhism : Origin and Development (New Delhi : 1988) p. 207.
9. “Under Guru Amar Das, Sikhism made rapid strides.” Sangat Singh, The Sikhs in History (New Delhi : 1996) p. 29. 10. “Guru Amar Das’s contribution to the growth of the Sikh Panth was great.” Dr. D.S. Dhillon, Sikhism : Origin and Development (New Delhi : 1988) p. 94.
11. “These social reforms introduced by Guru Amar Das must be regarded as a turning point in the history of Sikhism.” Dr. B.S. Nijjar, op. cit., p. 83.
“गुरु रामदास जी का जीवन तथा सफलताएँ । (Life and Achievements of Guru Ram Das JI)
प्रश्न 9.
चौथे गुरु रामदास जी के जीवन तथा उनके सिख धर्म तथा सिख पंथ के संगठन में दिए गए योगदान पर एक विस्तृत नोट लिखें।
(Write an informative note on the life history of the fourth Guru Ram Das Ji and his contribution to the Sikh faith and the organisation of the Sikh Panth.)
अथवा
गुरु रामदास जी के अधीन सिख पंथ के विकास का वर्णन करें। (Write a detailed note on the development of Sikhism under Guru Ram Das Ji.)
अथवा
गुरु रामदास जी के जीवन व सफलताओं का वर्णन करो। (Describe the life and achievements of Guru Ram Das Ji.)
अथवा
सिख पंथ में गुरु रामदास जी का क्या योगदान है ?
(Describe the contribution of Guru Ram Das Ji in the development of Sikhism.)
अथवा
सिख इतिहास में गुरु रामदास जी का क्या योगदान है ? (What was the contribution of Guru Ram Das Ji to the development of Sikh History ?)
उत्तर-
गुरु रामदास जी सिखों के चौथे गुरु थे। वह 1574 ई० से लेकर 1581 ई० तक गुरुगद्दी पर आसीन रहे। उनके गुरुकाल में सिख पंथं के संगठन और विकास में महत्त्वपूर्ण प्रगति हुई । गुरु रामदास जी के आरंभिक जीवन और उनके अधीन सिख पंथ के विकास का संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित अनुसार है—
I. गुरु रामदास जी का प्रारंभिक जीवन
(Early Career of Guru Ram Das Ji)
1. जन्म और माता-पिता (Birth and Parentage)-गुरु रामदास जी का जन्म 24 सितंबर, 1534 ई० को चूना मंडी, लाहौर में हुआ था। आपको पहले भाई जेठा जी के नाम से जाना जाता था। आपके पिता जी का नाम हरिदास तथा माता जी का नाम दया कौर था। वे सोढी जाति के क्षत्रिय परिवार से संबंध रखते थे। जेठा जी के माता-पिता बहुत निर्धन थे।
2. बचपन और विवाह (Childhood and Marriage)—भाई जेठा जी बचपन से ही धार्मिक विचारों वाले थे। एक बार आपके माता जी ने आपको उबले हुए चने बेच कर कुछ कमाने को कहा। बाहर जाते समय उन्हें कुछ भूखे साधु मिल गए। आपने सारे चने इन भूखे साधुओं को खिला दिए और स्वयं खाली हाथ लौट आए। आप लोगों की सेवा करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। एक बार आपको एक सिख जत्थे के साथ गोइंदवाल साहिब जाने का अवसर मिला। आप वहाँ पर गुरु अमरदास जी के व्यक्तित्व से इतने प्रभावित हुए कि उनके शिष्य बन गए। गुरु अमरदास जी भाई जेठा जी की भक्ति और गुणों को देखकर बहुत प्रभावित हुए। इसलिए गुरु साहिब ने 1553 ई० में अपनी छोटी लड़की बीबी भानी जी का विवाह उनके साथ कर दिया। भाई जेठा जी के घर तीन लड़कों का जन्म हुआ। उनके नाम पृथी चंद (पृथिया), महादेव और अर्जन थे।
3. गुरुगद्दी की प्राप्ति (Assumption of Guruship)—विवाह के पश्चात् भी भाई जेठा जी गोइंदवाल साहिब में ही रहे तथा पहले की तरह गुरु जी की सेवा करते रहे। भाई जेठा जी की निष्काम सेवा, नम्रता और मधुर स्वभाव ने गुरु अमरदास जी का मन मोह लिया था। इसलिए 1 सितंबर, 1574 ई० में गुरु अमरदास जी ने अपने ज्योति-जोत समाने से पूर्व भाई जेठा जी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। उस समय से भाई जेठा जी को रामदास जी कहा जाने लगा। इस प्रकार गुरु रामदास जी सिखों के चौथे गुरु बने।
II. गुरु रामदास जी के समय सिख पंथ का विकास (Development of Sikhism under Guru Ram Das Ji)
गुरु रामदास जी का गुरुकाल 1574 ई० से 1581 ई० तक था। उनका गुरुकाल का समय बहुत ही कम था। फिर भी उन्होंने सिख पंथ के विकास तथा संगठन में प्रशंसनीय योगदान दिया।—
1. रामदासपुरा की स्थापना (Foundation of Ramdaspura)-गुरु रामदास जी की सिख पंथ को सबसे महत्त्वपूर्ण देन रामदासपुरा अथवा अमृतसर की स्थापना करना था। रामदासपुरा की स्थापना 1577 ई० में हुई। इस शहर को बसाने के लिए गुरु साहिब ने यहाँ भिन्न-भिन्न व्यवसायों से संबंध रखने वाले 52 व्यापारियों को बसाया। इन व्यापारियों ने जो बाजार बसाया वह ‘गुरु का बाज़ार’ नाम से प्रसिद्ध हुआ। गुरु साहिब ने रामदासपुरा में दो सरोवरों अमृतसर एवं संतोखसर की खुदवाई का विचार बनाया। अमृतसर सरोवर के निर्माण का कार्य बाबा बुड्डा जी की देखरेख में हुआ। शीघ्र ही अमृत सरोवर के नाम पर ही रामदासपुरा का नाम अमृतसर पड़ गया। अमृतसर की स्थापना से सिखों को उनका मक्का मिल गया। यह शीघ्र ही सिखों का सर्वाधिक प्रसिद्ध धर्म-प्रचार केंद्र बन गया।
2. मसंद प्रथा का आरंभ (Introduction of Masand System)—गुरु रामदास जी को रामदासपुरा में अमृतसर एवं संतोखसर नामक दो सरोवरों की खुदवाई के लिए धन की आवश्यकता पड़ी। इसलिए गुरु साहिब ने अपने प्रतिनिधियों को अलग-अलग स्थानों पर भेजा ताकि वे सिख मत का प्रचार कर सकें और संगतों से धन एकत्रित कर सकें। यह संस्था मसंद प्रथा के नाम से प्रसिद्ध हुई। मसंद प्रथा के कारण ही सिख मत का दूर-दूर तक प्रचार हुआ। एस० एस० गाँधी के अनुसार,
“मसंद प्रथा ने सिख पंथ को संगठित करने में बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।”12
3. उदासियों से समझौता (Reconciliation With Udasis)-गुरु रामदास जी के समय की एक महत्त्वपूर्ण घटना उदासी तथा सिख संप्रदाय के मध्य समझौता था। एक बार उदासी मत के संस्थापक बाबा श्रीचंद जी गुरु रामदास जी के दर्शनों के लिए अमृतसर आए। वह गुरु साहिब की नम्रता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उस दिन के पश्चात् सिख मत का विरोध नहीं किया। यह समझौता सिख पंथ के विकास के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण प्रमाणित हुआ।
4. कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण कार्य (Some other important Works)-गुरु जी के अन्य महत्त्वपूर्ण कार्यों में वाणी की रचना (679 शब्द) करना था। उन्होंने चार लावों द्वारा विवाह प्रथा को प्रोत्साहित किया। गुरु साहिब ने पहले से चली आ रही संगत, पंगत और मंजी नामक संस्थाओं को जारी रखा। गुरु साहिब ने समाज में प्रचलित कुरीतियों जैसे-जाति प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह आदि का भी ज़ोरदार शब्दों में खंडन किया।
5. अकबर के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध (Friendly Relations with Akbar)-गुरु रामदास जी के समय में भी सिखों के मुग़ल बादशाह अकबर से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित रहे। अकबर ने गुरु रामदास जी से लाहौर में मुलाकात की थी। गुरु जी के विचारों से प्रभावित होकर उसने गुरु साहिब के कहने पर पंजाब के कृषकों का एक वर्ष के लिए लगान माफ कर दिया। फलस्वरूप गुरु साहिब की ख्याति में और वृद्धि हुई।
6. उत्तराधिकारी की नियुक्ति (Nomination of the Successor)-1581 ई० में गुरु रामदास जी ने अपने ज्योति-जोत समाने से पूर्व अपने सबसे छोटे पुत्र अर्जन देव जी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इसका कारण यह था कि गुरु साहिब के सबसे बड़े पुत्र पृथिया ने अपने षड्यंत्रों के कारण उन्हें नाराज़ कर लिया था। दूसरे पुत्र महादेव को सांसारिक कार्यों में कोई रुचि नहीं थी। अर्जन साहिब प्रत्येक पक्ष से गुरुगद्दी के योग्य थे। गुरु रामदास जी 1 सितंबर, 1581 ई० को ज्योति-जोत समा गए।
7. गुरु रामदास जी की सफलताओं का मूल्याँकन (Estimate of the Achievements of Guru Ram Das Ji)-गुरु रामदास जी अपने गुरुगद्दी काल में सिख पंथ को एक नया स्वरूप देने में सफल हुए। गुरु जी ने रामदासपुरा एवं मसंद प्रथा की स्थापना से, उदासियों के साथ समझौता करके, अपनी वाणी की रचना करके, समाज में प्रचलित कुरीतियों का खंडन करके, संगत, पंगत एवं मंजी संस्थाओं को जारी रख कर तथा अकबर के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करके सिख धर्म की नींव को और सुदृढ़ किया। अंत में हम प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर डी० एस० ढिल्लों के इन शब्दों से सहमत हैं,
“गुरु रामदास जी ने अपने लगभग 7 वर्षों के गुरुकाल में सिख पंथ को दृढ़ ढाँचा एवं दिशा प्रदान की।”13
12. “Masand System played a big role in consolidating Sikhism.” S. S. Gandhi, History of the Sikhs (Delhi : 1978) p. 209.
13. “During the short period of his guruship of about seven years, Guru Ram Das provided a well-knit community with a form and content.” Dr. D. S. Dhillon, Sikhism : Origin and Development (New Delhi : 1988) p. 100.

प्रश्न 10.
1539 ई० से 1581 ई० तक सिख पंथ के विकास का संक्षिप्त वर्णन करें।
(Describe briefly the development of Sikhism from 1539 to 1581 A.D.)
उत्तर-
गुरु अंगद देव जी 1539 ई० में सिखों के दूसरे गुरु बने। वह 1552 ई० तक गुरुगद्दी पर आसीन रहे। जिस समय गुरु अंगद देव जी गुरुगद्दी पर बैठे थे, उस समय सिख पंथ के सामने कई संकट विद्यमान थे। पहला सिख धर्म का हिंदू धर्म में विलीन हो जाने का खतरा था। दूसरा बड़ा ख़तरा उदासियों से था। सिख अनुयायियों की कम संख्या होने के कारण बहुत से सिख उदासी मत में शामिल होते जा रहे थे। गुरु अंगद साहिब ने अपने यत्नों से सिख पंथ के सम्मुख विद्यमान इन खतरों को दूर किया। गुरु अंगद साहिब ने सिख पंथ के विकास में जो महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई उसका वर्णन निम्नलिखित अनुसार है—
1. गुरमुखी को लोकप्रिय बनाना (Popularisation of Gurmukhi)-गुरुं अंगद देव जी ने गुरमुखी लिपि को लोकप्रिय बनाने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने इसके रूप में एक नया निखार लाया। अब इस लिपि को समझना सामान्य लोगों के लिए सरल हो गया। सिखों के सभी धार्मिक ग्रंथों की रचना इस लिपि में हुई। इस लिपि का नाम गुरमुखी [गुरुओं के मुख से निकली हुई] होने के कारण यह सिखों को गुरु के प्रति अपने कर्तव्य का स्मरण दिलाती रही। इस प्रकार यह लिपि सिखों की अपनी अलग पहचान बनाए रखने में सहायक सिद्ध हुई। इस लिपि के प्रसार के कारण सिखों में तीव्रता से विद्या का प्रसार भी होने लगा। एच० एस० भाटिया एवं एस० आर० बख्शी के अनुसार,
“गुरु अंगद देव जी ने सिखों को हिंदुओं एवं मुसलमानों से एक अलग भाषा दी तथा उन्हें यह अनुभव करवाया कि वे अलग लोग हैं।”2.
2. वाणी का संग्रह (Collection of Hymns)-गुरु अंगद देव जी का दूसरा महान् कार्य गुरु नानक देव जी की वाणी को एकत्रित करना था। यह वाणी एक स्थान पर न होकर अलग-अलग स्थानों पर बिखरी हुई थी। गुरु अंगद साहिब ने इस समूची वाणी को एकत्रित किया। सिख परंपराओं के अनुसार गुरु अंगद देव जी ने एक श्रद्धालु सिख भाई बाला जी को बुलाकर गुरु नानक साहिब के जीवन के संबंध में भाई पैड़ा मौखा जी से एक जन्म साखी लिखवाई। इस साखी को भाई बाला जी की जन्म साखी के नाम से जाना जाता है। कुछ विद्वान् इस तथ्य से सहमत नहीं हैं कि भाई बाला जी की जन्म साखी को गुरु अंगद देव जी के समय लिखा गया था। गुरु अंगद साहिब ने स्वयं ‘नानक’ के नाम से वाणी की रचना की। इस प्रकार गुरु अंगद देव जी ने वाणी के वास्तविक रूप को बिगड़ने से बचाया। दूसरा, इसने आदि ग्रंथ साहिब जी की तैयारी के लिए महत्त्वपूर्ण आधार तैयार किया।
3. लंगर प्रथा का विस्तार (Expansion of Langar System)-लंगर प्रथा के विकास का श्रेय गुरु अंगद देव जी को जाता है। लंगर का समूचा प्रबंध उनकी धर्म पत्नी बीबी खीवी जी करते थे। लंगर में सभी व्यक्ति बिना किसी ऊँच-नीच, जाति के भेदभाव के इकट्ठे मिलकर छकते थे। इस लंगर के लिए सारी माया गुरु जी के सिख देते थे। इस प्रथा के कारण सिखों में परस्पर सहयोग की भावना बढ़ी। इसने हिंदू समाज में फैली जाति-प्रथा पर कड़ा प्रहार किया। इस प्रकार इस संस्था ने सामाजिक एवं आर्थिक असमानता को दूर करने में प्रशंसनीय योगदान दिया। इसके कारण सिख धर्म की ख्याति दूर-दूर तक फैल गई। प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफैसर हरबंस सिंह का यह कहना पूर्णतः सही है, “सामाजिक क्रांति लाने में यह (लंगर) संस्था महत्त्वपूर्ण साधन सिद्ध हुई।”3
4. संगत का संगठन (Organisation of Sangat)-गुरु अंगद देव जी ने गुरु नानक देव जी द्वारा स्थापित संगत संस्था को भी संगठित किया। संगत से अभिप्राय था-एकत्रित होकर बैठना। संगत में सभी धर्मों के लोगस्त्री और पुरुष भाग ले सकते थे। यह संगत सुबह-शाम गुरु जी के उपदेशों को सुनने के लिए एकत्रित होती थी। इस संस्था ने सामाजिक असमानता को दूर करने तथा सिखों को संगठित करने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।
5. उदासी मत का खंडन (Denunciation of the Udasi Sect)-उदासी मत की स्थापना गुरु नानक देव जी के बड़े सुपुत्र बाबा श्रीचंद जी ने की थी। यह मत संन्यास अथवा त्याग के जीवन पर बल देता था। बहुत से सिख उदासी मत को मान्यता देने लग पड़े थे। ऐसी परिस्थितियों में यह संकट उत्पन्न हो गया था कि कहीं सिख गुरु नानक देव जी उपदेशों को भूल कर उदासी मत न अपना लें। अतः गुरु अंगद देव जी ने उदासी मत का कड़ा विरोध किया तथा स्पष्ट किया कि उदासी मत के सिद्धांत सिख धर्म के सिद्धांतों से.सर्वथा विपरीत हैं एवं जो सिख उदासी मत में विश्वास रखता है, वह सच्चा सिख नहीं हो सकता। इस प्रकार गुरु अंगद देव जी ने सिख मत के अस्तित्व को बनाए रखा।
6. शारीरिक शिक्षा (Physical Training)-गुरु अंगद देव जी यह मानते थे कि जिस प्रकार आत्मा की उन्नति के लिए नाम का जाप करना आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार शारीरिक स्वस्थता के लिए व्यायाम करना भी आवश्यक है। इस उद्देश्य के साथ गुरु जी ने खडूर साहिब में एक अखाड़ा बनवाया। यहाँ सिख प्रतिदिन प्रातःकाल मल्ल युद्ध तथा अन्य व्यायाम करते थे।
7. गोइंदवाल साहिब की स्थापना (Foundation of Goindwal Sahib)-गुरु अंगद देव जी ने खडूर साहिब के समीप गोइंदवाल साहिब नामक एक नए नगर की स्थापना की। इस नगर का निर्माण कार्य एक श्रद्धालु सेवक अमरदास की देख-रेख में 1546 ई० में आरंभ हुआ। यह नगर शीघ्र ही सिखों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान बन गया।
8. हुमायूँ से भेंट (Meeting with Humayun)-1540 ई० में मुग़ल बादशाह हुमायूँ शेरशाह सूरी के हाथों पराजय के पश्चात् पंजाब पहुँचा। वह खडूर साहिब गुरु अंगद देव जी से आशीर्वाद लेने के लिए पहुँचा। उस समय गुरु जी समाधि में लीन थे। हुमायूँ ने इसे अपना अपमान समझकर तलवार निकाल ली। उस समय गुरु जी ने अपनी आँखें खोली और हुमायूँ से कहा कि, “यह तलवार जिसका तुम मुझ पर प्रयोग करने लगे हो, वह तलवार शेरशाह सूरी के विरुद्ध लड़ाई करते समय कहाँ थी ?” ये शब्द सुनकर हुमायूँ अत्यंत लज्जित हुआ और उसने गुरु जी से क्षमा माँगी। गुरु जी ने हुमायूँ को आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हें कुछ समय प्रतीक्षा करने के पश्चात् राज्य सिंहासन प्राप्त होगा। गुरु जी की यह भविष्यवाणी सत्य निकली। इस भेंट के कारण सिखों तथा मुग़लों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हुए।
9. उत्तराधिकारी की नियुक्ति (Nomination of the Successor)-गुरु अंगद देव जी का सिख पंथ के विकास के लिए सबसे महान् कार्य अमरदास जी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करना था। गुरु अंगद देव जी ने काफ़ी सोच-समझकर इस उच्च पद के लिए अमरदास जी का चुनाव किया। गुरु जी ने अमरदास जी के सम्मुख एक नारियल और पाँच पैसे रखकर अपना शीश झुकाया। इस प्रकार अमरदास जी को सिखों का तीसरा गुरु नियुक्त किया गया। गुरु अंगद देव जी 29 मार्च, 1552 ई० को ज्योति जोत समा गए।
10. गुरु अंगद देव जी की सफलताओं का मूल्याँकन (Estimate of Guru Angad Dev Ji’s Achievements)-इस प्रकार हम देखते हैं कि गुरु अंगद देव जी ने अपनी गुरुगद्दी के काल में सिख पंथ के विकास में बहुत प्रशंसनीय योगदान दिया। गुरु जी ने गुरमुखी लिपि का प्रचार करके, गुरु नानक साहिब की वाणी को एकत्रित करके, संगत और पंगत संस्थाओं का विस्तार करके, सिख पंथ को उदासी मत से अलग करके, गोइंदवाल साहिब की स्थापना करके और अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करके सिख पंथ की नींव को और सुदृढ़ किया। गुरु अंगद देव जी की सफलताओं का मूल्यांकन करते हुए प्रसिद्ध इतिहासकार के० एस० दुग्गल का कहना है,
“यह आश्चर्य वाली बात है कि गुरु अंगद साहिब ने अपने अल्प समय के दौरान कितनी अधिक सफलता प्राप्त कर ली थी।”4
एक अन्य प्रसिद्ध इतिहासकार एस० एस० जौहर के अनुसार,
“गुरु अंगद देव जी का गुरु काल सिख पंथ के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण मोड़ था।”5
1. “Had Nanak died without a successor, there would have been no Sikhism today.” G.C. Narang, Transformation of Sikhism (New Delhi : 1989) p. 29.
2. “Guru Angad Dev Ji gave the Sikhs a written language different from the language of the Hindus and Muslims and thus made them realise that they were separate people.” H.S. Bhatia and S.R. Bakshi, Encyclopaedic History of the Sikhs and Sikhism (New Delhi : 1999) Vol. 1, p. 12.
3. “This served as an instrument of a far-reaching social revolution.” Prof. Harbans Singh, The Heritage of the Sikhs (Delhi : 1994) p. 31.
4. “It is amazing how much Guru Angad could achieve in the short time at his disposal.” K.S. Duggal, The Sikh Gurus : Their Lives and Teachings (New Delhi : 1993) p. 71.
5. “The pontificate of Guru Angad Dev is indeed a turning point in the history of Sikh faith.” S.S. Johar, Handbook on Sikhism (Delhi : 1979) p. 26.
संक्षिप्त उत्तरों वाले प्रश्न (Short Answer Type Questions)
प्रश्न 1.
गुरु अंगद देव जी का सिख पंथ के विकास में योगदान बताएँ। (Explain the contribution of Guru Angad Dev Ji to the development of Sikhism.)
अथवा
सिख पंथ के विकास में गुरु अंगद देव जी ने क्या-क्या कार्य किए ?
(What did Guru Angad Dev Ji do for the development of Sikh Panth ?)
अथवा
गुरु अंगद देव जी की किन्हीं तीन ऐसी सफलताओं का वर्णन करें जिनके कारण सिख धर्म का विकास हुआ।
(Write any three achievemnents of Guru Angad Dev Ji for the development of Sikhism.)
अथवा
सिख पंथ के विकास में गुरु अंगद देवो के कोई तीन कार्य बताएँ।
(Mention any three achievements of Guru Angad Dev Ji for the development of Sikhism.)
अथवा
गुरु अंगद देव जी पर एक संक्षिप्त नोट लिखें। (Write a short note on Guru Angad Dev Ji.)
उत्तर-
- गुरु अंगद देव जी ने खडूर साहिब को अपने प्रचार का मुख्य केंद्र बनाया।
- उन्होंने गुरमुखी लिपि को एक नया रूप प्रदान किया।
- गुरु अंगद देव जी ने संगत और पंगत संस्थाओं को अधिक विकसित किया।
- उन्होंने अपने अनुयायियों में कठोर अनुशासन लागू किया।
- उन्होंने सिख पंथ को उदासी मत से पृथक् करने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।
- उन्होंने गोइंदवाल साहिब नामक एक नए नगर की स्थापना की।

प्रश्न 2.
गुरु अंगद देव जी ने गुरमुखी लिपि को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या योगदान दिया ?
(What contribution was made by Guru Angad Dev Ji to improve Gurmukhi script ?)
अथवा
गुरमुखी लिपि को प्रचलित करने के लिए गुरु अंगद देव जी ने क्या योगदान दिया ?
(What contribution was made by Guru Angad Dev Ji to popularise Gurmukhi script ?)
उत्तर-
गुरु अंगद देव जी ने गुरमुखी लिपि को संशोधित कर नया रूप प्रदान किया। परिणामस्वरूप, इस लिपि को समझना लोगों के लिए सरल हो गया। इस लिपि में सिखों के सभी धार्मिक ग्रंथों की रचना हुई। इस लिपि के कारण ब्राह्मण वर्ग को कड़ा आघात पहुँचा क्योंकि वे संस्कृत को ही धर्म की भाषा मानते थे। इस लिपि के लोकप्रिय होने के कारण सिख मत के प्रचार में बड़ी सहायता मिली। यह लिपि विद्या के प्रसार में भी सहायक सिद्ध हुई।
प्रश्न 3.
गुरु अंगद देव जी ने उदासी मत का खंडन किस प्रकार किया ? (How did Guru Angad Dev Ji denounce the Udasi sect ?)
उत्तर-
गुरु अंगद देव जी का सिख मत के विकास की ओर एक अन्य प्रशंसनीय कार्य उदासी मत का खंडन करना था। इस मत की स्थापना गुरु नानक देव जी के बड़े सुपुत्र बाबा श्रीचंद जी ने की थी। यह मत संयास अथवा त्याग के जीवन पर बल देता था, जबकि गुरु नानक देव जी गृहस्थ जीवन के पक्ष में थे। उदासी मत के शेष सिद्धांत गुरु नानक देव जी के सिद्धांतों से मिलते थे। इस कारण बहुत-से सिख उदासी मत को मान्यता देने लग पड़े थे। ऐसी परिस्थितियों में गुरु अंगद साहिब ने उदासी मत का कड़ा विरोध किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो सिख उदासी मत में विश्वास रखता है, वह सच्चा सिख नहीं हो सकता।
प्रश्न 4.
गुरु अंगद देव जी तथा हुमायूँ में हुई भेंट की संक्षेप जानकारी दें।
(Give a brief account of the meeting between Guru Angad Dev Ji and Humayun.)
उत्तर-
1540 ई० में मुग़ल बादशाह हुमायूँ को शेरशाह सूरी के हाथों कन्नौज के स्थान पर कड़ी पराजय हुई थी। पराजय के पश्चात् हुमायूँ खडूर साहिब गुरु अंगद देव जी से आशीर्वाद लेने के लिए पहुँचा। उस समय गुरु जी समाधि में इतने लीन थे कि उन्होंने आँखें खोलकर नं देखा। हुमायूँ ने क्रोधित होकर अपनी तलवार म्यान से निकाल ली। उसी समय गुरु जी ने अपनी आँखें खोली और हुमायूँ से कहा कि, “यह तलवार शेरशाह सूरी के विरुद्ध लड़ाई करते समय कहाँ थी ?” ये शब्द सुनकर हुमायूँ अत्यंत लज्जित हुआ और उसने गुरु जी से क्षमा माँग ली।

प्रश्न 5.
संगत के बारे में आप क्या जानते हैं ? (What do you know about Sangat ?)
उत्तर-
संगत संस्था की स्थापना गुरु नानक देव जी ने की थी। संगत संस्था से अभिप्राय एकत्रित रूप में मिलकर बैठने से था। यह संगत सुबह-शाम गुरु जी के उपदेशों तथा सतनाम का जाप करने के लिए एकत्रित होते थी। गुरु अंगद देव जी ने इस संस्था को अधिक संगठित किया। संगत में बिना किसी जाति-पाति अथवा धर्म के भेद-भाव के कोई भी आ सकता था। संगत को ईश्वर का रूप समझा जाता था।
प्रश्न 6.
पंगत अथवा लंगर से आपका क्या भाव है ? (What do you mean by Pangat or Langar ?)
अथवा
लंगर प्रथा के बारे में आप क्या जानते हैं ?
(What do you know about Langar system ?)
अथवा
पंगत अथवा लंगर व्यवस्था पर एक नोट लिखें।
(Write a note on Pangat or Langar.)
उत्तर-
पंगत (लंगर) संस्था की स्थापना भी गुरु नानक देव जी ने की थी। इसके अंतर्गत धर्मों तथा वर्गों के लोग बिना किसी भेदभाव के एक जगह बैठकर खाते थे। गुरु अंगद देव जी ने इसे जारी रखा और गुरु अमरदास जी ने इस संस्था को अधिक विकसित किया। इस संस्था ने समाज में जाति-प्रथा और असमानता की भावनाओं को समाप्त करने में बड़ी सहायता की।
प्रश्न 7.
संगत एवं पंगत के महत्त्व पर एक संक्षिप्त नोट लिखो।
(Write a short note on importance of Sangat and Pangat.)
अथवा
संगत तथा पंगत से आपका क्या अभिप्राय है ?
(What do you mean by Sangat and Pangat ?)
उत्तर-
1540 ई० में मुग़ल बादशाह हुमायूँ को शेरशाह सूरी के हाथों कन्नौज के स्थान पर कड़ी पराजय हुई थी। पराजय के पश्चात् हुमायूँ खडूर साहिब गुरु अंगद देव जी से आशीर्वाद लेने के लिए पहुँचा। उस समय गुरु जी समाधि में इतने लीन थे कि उन्होंने आँखें खोलकर नं देखा। हुमायूँ ने क्रोधित होकर अपनी तलवार म्यान से निकाल ली। उसी समय गुरु जी ने अपनी आँखें खोली और हुमायूँ से कहा कि, “यह तलवार शेरशाह सूरी के विरुद्ध लड़ाई करते समय कहाँ थी ?” ये शब्द सुनकर हुमायूँ अत्यंत लज्जित हुआ और उसने गुरु जी से क्षमा माँग ली।
पंगत (लंगर) संस्था की स्थापना भी गुरु नानक देव जी ने की थी। इसके अंतर्गत धर्मों तथा वर्गों के लोग बिना किसी भेदभाव के एक जगह बैठकर खाते थे। गुरु अंगद देव जी ने इसे जारी रखा और गुरु अमरदास जी ने इस संस्था को अधिक विकसित किया। इस संस्था ने समाज में जाति-प्रथा और असमानता की भावनाओं को समाप्त करने में बड़ी सहायता की।

प्रश्न 8.
गुरुगद्दी प्राप्त करने के पश्चात् गुरु अमरदास जी को जिंन आरंभिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उनका संक्षेप वर्णन कीजिए।
(What problems did Guru Amar Das Ji face in the early years of his pontificate ?)
उत्तर-
- गुरुगद्दी पर विराजमान होने के पश्चात् गुरु अमरदास जी को सबसे पहले गुरु अंगद देव जी के पुत्रों दासू तथा दातू के विरोध का सामना करना पड़ा। उन्होंने गुरु पुत्र होने के नाते गुरुगद्दी पर अपना अधिकार जताया।
- गुरु नानक देव जी के बड़े पुत्र बाबा श्रीचंद भी गुरुगद्दी पर अपना अधिकार समझते थे। उन्होंने भी गुरु अमरदास जी का विरोध करना आरंभ कर दिया।
- गुरु अमरदास जी की बढ़ती हुई ख्याति देख कर गोइंदवाल साहिब के मुसलमान सिखों से ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने सिखों के लिए अनेक समस्याएँ उत्पन्न कर दी।
प्रश्न 9.
सिख धर्म के विकास में गुरु अमरदास जी के योगदान के बारे में बताओ।
(Give the contribution of Guru Amar Das Ji for the development of Sikh religion.)
अथवा
सिख धर्म के विकास में गुरु अमरदास जी द्वारा की गई तीन मुख्य सेवाओं का वर्णन करो।
(Write down the three services done by Guru Amar Das Ji for the development of Sikh religion.)
अथवा
गुरु अमरदास जी के कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। (From an estimate of the works of Guru Amar Das Ji.)
अथवा
सिख धर्म के विकास में गुरु अमरदास जी के तीन कार्य बताएँ। (Write any three works of Guru Amar Das Ji for the spread of Sikhism.)
अथवा
सिख पंथ के विकास में गुरु अमरदास जी के योगदान का अध्ययन करें। (Study the contribution of Guru Amar Das Ji to the growth of Sikhism.)
उत्तर-
- गुरु अमरदास जी ने सर्वप्रथम गोइंदवाल साहिब में बाऊली का निर्माण किया। शीघ्र ही यह सिखों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान बन गया।
- उन्होंने लंगर संस्था का अधिक विस्तार किया।
- उन्होंने सिख पंथ के प्रचार के लिए मंजी प्रथा की स्थापना की।
- गुरु साहिब ने सिख मत को उदासी मत से अलग रखकर लुप्त होने से बचा लिया।
- गुरु अमरदास जी ने समाज में प्रचलित कुरीतियों का जोरदार शब्दों में खंडन किया।
प्रश्न 10.
सिख इतिहास में गोइंदवाल साहिब की बाऊली के निर्माण का क्या महत्त्व है ?
(What is importante of the construction of the Baoli of Goindwal Sahib in Sikh History ?)
अथवा
गोइंदवाल साहिब को सिख धर्म का केंद्र क्यों कहा जाता है ? (Why is Goindwal Sahib called the centre of Sikhism-?)
उत्तर-
गुरु अमरदास जी का सिख पंथ के विकास की ओर पहला कदम गोइंदवाल साहिब में एक बाऊली का निर्माण करवाना था। इस पवित्र बाऊली का निर्माण कार्य 1552 ई० से 1559 ई० तक चला। इस बाऊली के निर्माण के पीछे गुरु साहिब के दो उद्देश्य थे। पहला, सिखों को हिंदुओं से अलग तीर्थ स्थान देना चाहते थे। दूसरा, वह वहाँ के लोगों की पानी की कठिनाई को दूर करना चाहते थे। बाऊली के निर्माण से सिखों को एक पवित्र तीर्थ स्थान मिल गया।

प्रश्न 11.
गुरु अमरदास जी के द्वारा किए गए सामाजिक सुधारों का संक्षेप में वर्णन करें। (Describe briefly the social reforms of Guru Amar Das Ji.)
अथवा
गुरु अमरदास जी के कोई तीन सामाजिक सुधारों का वर्णन करें।
(Describe any three social reforms of Guru Amar Das Ji.)
अथवा
गुरु अमरदास जी को समाज सुधारक क्यों कहा जाता है ?
(Why is.Guru Amar Das called a social reformer ?)
अथवा
गुरु अमरदास जी को समाज सुधारक किन कारणों के लिए कहा जाता है ? (Why is Guru Amar Das Ji called a social reformer ?)
उत्तर-
- गुरु अमरदास जी ने सती प्रथा का डटकर विरोध किया।
- गुरु साहिब ने बाल विवाह और पर्दा प्रथा का भी विरोध किया।
- उन्होंने समाज में प्रचलित जाति प्रथा की बड़े जोरदार शब्दों में आलोचना की।
- गुरु अमरदास जी नशीले पदार्थों के सेवन के विरुद्ध थे।
- उन्होंने सिखों के जन्म, विवाह और मृत्यु के अवसरों के लिए विशेष रस्में बनाईं।
प्रश्न 12.
गुरु अमरदास जी ने स्त्री जाति के कल्याण के लिए कौन-से सुधार किए ?
(What reforms were made by Guru Amar Das Ji for the welfare of women ?)
उत्तर-
- गुरु अमरदास जी ने नवजन्मी कन्याओं को मारने का विरोध किया।
- गुरु जी ने बाल विवाह का जोरदार शब्दों में खंडन किया।
- उन्होंने पर्दा प्रथा की भी निंदा की।
प्रश्न 13.
मंजी प्रथा क्या थी ? सिख धर्म के विकास में इसने क्या योगदान दिया ?
(What was Manji system ? How did it contribute to the development of Sikhism ?)
अथवा
मंजी प्रथा के बारे में आप क्या जानते हैं ? (What do you know about Manji system ?) .
अथवा
मंजी प्रथा पर एक नोट लिखें। (Write a note on Manji system.)
उत्तर-
गुरु अमरदास जी का एक और महान् कार्य मंजी प्रथा की स्थापना था। उनके समय में सिखों की संख्या इतनी बढ़ गई थी कि गुरु जी के लिए प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचना असंभव था। अतः गुरु साहिब ने अपने उपदेशों को दूर के प्रदेशों तक पहुँचाने के लिए 22 मंजियों की स्थापना की। प्रत्येक मंजी के मुखिया को मंजीदार कहते थे। मंजीदार अधिक-से-अधिक लोगों को सिख धर्म में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करते थे। इसके अतिरिक्त वे सिखों से धन एकत्रित करके गुरु साहिब तक पहुँचाते थे।

प्रश्न 14.
मंजीदार के प्रमुख कार्य क्या थे ? (What were the main functions of the Manjidar ?)
उत्तर-
- वे सिख धर्म के प्रचार के लिए अथक प्रयास करते थे ?
- वे गुरु साहिब के आदेशों को सिख संगतों तक पहुँचाते थे।
- वे लोगों को धार्मिक शिक्षा देते थे तथा गुरमुखी भाषा का अध्ययन करवाते थे।
प्रश्न 15.
गुरु अमरदास जी के मुग़लों के साथ कैसे संबंध थे ? (What type of relations did Guru Amar Das Ji have with the Mughals ?)
अथवा
मुगल बादशाह अकबर तथा गुरु अमरदास जी के मध्य संबंधों का उल्लेख कीजिए।
(Describe the relations between Mughal emperor Akbar and Guru Amar Das Ji.)
अथवा
मुगल सम्राट अकबर तथा गुरु अमरदास जी के बीच संबंधों का उल्लेख करें। (Explain the relations between the Mughal emperor Akbar and Guru Amar Das Ji.).
उत्तर-
गुरु अमरदास जी के मुग़लों के साथ संबंध मैत्रीपूर्ण थे। 1568 ई० में अकबर गोइंदवाल साहिब आया। उसने गुरु साहिब के दर्शन करने से पूर्व मर्यादानुसार लंगर खाया। वह गुरु साहिब के व्यक्तित्व और लंगर प्रबंध से बहुत प्रभावित हुआ। उसने लंगर प्रबंध को चलाने के लिए कुछ गाँवों की जागीर गुरु जी की सुपुत्री बीबी भानी जी के नाम लगा दी। अकबर की इस यात्रा के कारण गुरु अमरदास जी की प्रसिद्धि बहुत दूर-दूर तक फैल गई। इससे सिख धर्म का प्रसार और प्रचार बढ़ा।
प्रश्न 16.
गुरु रामदास जी का सिख धर्म को क्या योगदान था ?
(What was the contribution of Guru Ram Das Ji to Sikh religion ?)
अथवा
सिख मत के विकास में गुरु रामदास जी द्वारा दिये गए योगदान का वर्णन करो।
(Explain the contribution of Guru Ram Das Ji to the growth of Sikhism.)
उत्तर-
गुरु रामदास जी का गुरु काल 1574 ई० से 1581 ई० तक रहा। गुरु साहिब ने सर्वप्रथम रामदासपुरा (अमृतसर) की स्थापना की। इसके अतिरिक्त गुरु साहिब ने यहाँ पर दो सरोवरों अमृतसर और संतोखसर की खुदाई का कार्य भी आरंभ किया। गुरु साहिब ने सिख धर्म के प्रचार तथा उसके विकास के लिए धन एकत्रित करने के लिए मसंद प्रथा की स्थापना की। गुरु रामदास जी ने सिखों और उदासियों के मध्य लंबे समय से चले आ रहे मतभेदों को समाप्त किया। गुरु साहिब ने संगत और पंगत संस्थाओं को जारी रखा।

प्रश्न 17.
रामदासपुरा (अमृतसर) की स्थापना का सिख इतिहास में क्या महत्त्व है ?
[What is the importance of foundation of Ramdaspura (Amritsar) in Sikh History ?]
उत्तर-
गुरु रामदास जी की सिख पंथ को सबसे महत्त्वपूर्ण देन 1577 ई० में रामदासपुरा अथवा अमृतसर की स्थापना करना था। गुरुगद्दी प्राप्त करने के पश्चात् गुरु साहिब स्वयं यहाँ आ गए थे। इस शहर को बसाने के लिए गुरु साहिब ने यहाँ भिन्न-भिन्न व्यवसायों से संबंधित 52 अन्य व्यापारियों को बसाया। अमृतसर की स्थापना सिख पंथ के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। इससे सिखों को एक अलग तीर्थ स्थान मिल गया।
प्रश्न 18.
उदासी मत पर एक संक्षिप्त नोट लिखें। (Write a short note on Udasi sect.)
अथवा
उदासी प्रथा के बारे में आप क्या जानते हैं ? (What do you know about Udasi system ?)
अथवा
बाबा श्रीचंद जी पर एक संक्षिप्त नोट लिखें। (Write a brief note on Baba Sri Chand Ji.) .
उत्तर-
उदासी मत की स्थापना गुरु नानक देव जी के बड़े पुत्र बाबा श्रीचंद जी ने की थी। यह मत त्याग और वैराग्य पर बल देता था। यह मत योग तथा प्रकृति उपासना में भी विश्वास रखता था। बहुत-से सिख बाबा श्रीचंद जी के जीवन से प्रभावित होकर उदासी मत में सम्मिलित होने लग पड़े थे। इसलिए गुरु अंगद देव जी और गुरु अमरदास जी ने जोरदार शब्दों में उदासी मत का खंडन किया। उनका कहना था कि कोई भी सच्चा सिख उदासी नहीं हो सकता था। गुरु अमरदास जी के काल में उदासियों एवं सिखों के बीच समझौता हो गया।
वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Type Questions)
(i) एक शब्द से एक पंक्ति तक के उत्तर (Answer in One Word to One Sentence)
प्रश्न 1.
सिखों के दूसरे गुरु कौन थे ?
उत्तर-
गुरु अंगद देव जी।

प्रश्न 2.
गुरु अंगद देव जी का जन्म कब हुआ?
उत्तर-
1504 ई०।
प्रश्न 3.
गुरु अंगद देव जी का जन्म कहाँ हुआ?
उत्तर-
मत्ते की सराए (श्री मुक्तसर साहिब)।
प्रश्न 4.
गुरु अंगद देव जी की माता जी का नाम क्या था?
उत्तर-
सभराई देवी जी।।

प्रश्न 5.
गुरु अंगद देव जी के पिता जी का क्या नाम था ?
उत्तर-
फेरूमल जी।
प्रश्न 6.
गुरु अंगद देव जी का आरंभिक नाम क्या था?
उत्तर-
भाई लहणा जी।
प्रश्न 7.
गुरु अंगद देव जी ने गुरुगद्दी कब प्राप्त की?
उत्तर-
1539 ई०।

प्रश्न 8.
भाई लहणा जी को गुरु अंगद देव जी का नाम किसने दिया?
उत्तर-
गुरु नानक देव जी।
प्रश्न 9.
गुरु अंगद देव जी का विवाह किससे हुआ?
उत्तर-
बीबी खीवी जी।
प्रश्न 10.
गुरु अंगद देव जी के पुत्रों के नाम लिखो।
उत्तर-
दातू और दास।

प्रश्न 11.
गुरु अंगद देव जी की पुत्रियों के नाम लिखो।
उत्तर-
बीबी अमरो तथा बीबी अनोखी।
प्रश्न 12.
गुरु अंगद देव जी की धार्मिक गतिविधियों का केंद्र कौन-सा था?
उत्तर-
खडूर साहिब।
प्रश्न 13.
गुरुमुखी लिपि को किस गुरु साहिब ने लोकप्रिय बनाया?
उत्तर-
गुरु अंगद देव जी।

प्रश्न 14.
गोइंदवाल साहिब की नींव किस गुरु साहिब ने रखी?
अथवा
गोइंदवाल साहिब की स्थापना किस गुरु जी ने की थी?
अथवा
दूसरे गुरु साहिब ने किस नगर की स्थापना की थी?
उत्तर-
गुरु अंगद साहिब जी।
प्रश्न 15.
गोइंदवाल साहिब की नींव कब रखी गई थी?
उत्तर-
1546 ई०।
प्रश्न 16.
सिख पंथ के विकास में गुरु अंगद देव जी का कोई एक महत्त्वपूर्ण योगदान बताएँ।
अथवा
गुरु अंगद देव जी ने सिख धर्म के प्रसार के लिए क्या किया?
उत्तर-
उन्होंने गुरुमुखी लिपि को लोकप्रिय बनाया।

प्रश्न 17.
उदासी मत का संस्थापक कौन था?
उत्तर-
बाबा श्रीचंद जी।
प्रश्न 18.
उदासी मत से आपका क्या अभिप्राय है?
उत्तर-
इस मत में संन्यासी जीवन पर बल दिया जाता था।
प्रश्न 19.
कौन-से मुग़ल बादशाह ने गुरु अंगद साहिब जी से खडूर साहिब में मुलाकात की?
अथवा
किस मुगल बादशाह ने गुरु अंगद देव जी के साथ मुलाकात की?
उत्तर-
हुमायूँ।

प्रश्न 20.
मुगल बादशाह हुमायूँ ने किस गुरु साहिब जी से आशीर्वाद लिया था ?
उत्तर-
गुरु अंगद देव जी।
प्रश्न 21.
सिखों के तीसरे गुरु कौन थे ?
उत्तर-
गुरु अमरदास जी।
प्रश्न 22.
गुरु अमरदास जी का जन्म कब हुआ ?
उत्तर-
1479 ई० में।

प्रश्न 23.
गुरु अमरदास जी का जन्म कहाँ हुआ ?
उत्तर-
बासरके गाँव में।
प्रश्न 24.
गुरु अमरदास जी की माता जी का नाम बताएँ।
उत्तर-
सुलक्खनी जी।
प्रश्न 25.
गुरु अमरदास जी के पिता जी का क्या नाम था ?
उत्तर-
तेजभान जी।

प्रश्न 26.
गुरु अमरदास जी किस जाति से संबंधित थे ?
उत्तर-
भल्ला
प्रश्न 27.
बीबी भानी कौन थी ?
अथवा
बीबी दानी कौन थी ?
उत्तर-
गुरु अमरदास जी की सुपुत्री।
प्रश्न 28.
बाबा मोहरी जी किस गुरु साहिब के सुपुत्र थे ?
उत्तर-
बाबा मोहरी जी गुरु अमरदास जी के सुपुत्र थे।

प्रश्न 29.
गुरु अमरदास जी जिस समय गुरुगद्दी पर बैठे तो उस समय उनकी आयु क्या थी ?
उत्तर-
73 वर्ष।
प्रश्न 30.
गुरु अमरदास जी गुरुगद्दी पर कब विराजमान हुए ?
उत्तर-
1552 ई० में।
प्रश्न 31.
गुरु अमरदास जी का गुरुकाल बताएँ ।
उत्तर-
1552 ई० से 1574 ई०।

प्रश्न 32.
गोइंदवाल साहिब में बाऊली का निर्माण किसने करवाया ?
उत्तर-
गुरु अमरदास जी।
प्रश्न 33.
गोइंदवाल साहिब में पवित्र बाऊली का निर्माण कब किया गया ?
उत्तर-
1552 ई० में।
प्रश्न 34.
गोइंदवाल साहिब की बाऊली में कितनी सीढ़ियाँ बनाई गई थीं ?
उत्तर-
84.

प्रश्न 35.
गुरु अमरदास जी की कोई एक सफलता लिखें।
उत्तर-
गोइंदवाल साहिब में बाऊली का निर्माण।
प्रश्न 36.
मंजी प्रथा की स्थापना किस गुरु साहिब ने की ?
उत्तर-
गुरु अमरदास जी।
प्रश्न 37.
गुरु अमरदास जी ने कितनी मंजियों की स्थापना की ?
उत्तर-
22 मंजियों की।

प्रश्न 38.
मंजी प्रथा का उद्देश्य क्या था ?
उत्तर-
सिख मत का प्रचार करना।
प्रश्न 39.
मंजी प्रथा ने सिख धर्म के विकास में क्या योगदान दिया ?
उत्तर-
मंजी प्रथा ने सिख धर्म को लोकप्रिय बनाया।
प्रश्न 40.
गुरु अमरदास जी ने कितने शब्दों की रचना की ?
उत्तर-
907 शब्दों की।

प्रश्न 41.
आनंदु साहिब वाणी की रचना किस गुरु साहिब ने की थी ?
उत्तर-
गुरु अमरदास जी।
प्रश्न 42.
गुरु अमरदास जी का कोई एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक सुधार बताएँ।
उत्तर-
गुरु अमरदास जी ने सती प्रथा का खंडन किया।
प्रश्न 43.
गुरु अमरदास जी से भेंट करने कौन-सा मुग़ल बादशाह गोइंदवाल साहिब आया था ?
उत्तर-
अकबर।

प्रश्न 44.
मुग़ल बादशाह अकबर गोइंदवाल साहिब कब आया था ?
उत्तर-
1568 ई०।
प्रश्न 45.
गुरु अमरदास जी ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया ?
उत्तर-
गुरु रामदास जी।
प्रश्न 46.
गुरु अमरदास जी कब ज्योति-जोत समाए ?
उत्तर-
1574 ई०।

प्रश्न 47.
सिखों के चौथे गुरु कौन थे ?
उत्तर-
गुरु रामदास जी।
प्रश्न 48.
गुरु रामदास जी का गुरु काल कौन-सा था ?
उत्तर-
1574 ई० से 1581 ई०
प्रश्न 49.
गुरु रामदास जी का जन्म कब हुआ?
उत्तर-
1534 ई०।

प्रश्न 50.
गुरु रामदास जी का आरंभिक नाम क्या था?
अथवा
गुरु रामदास जी का पहला नाम क्या था ?
उत्तर-
भाई जेठा जी।
प्रश्न 51.
गुरु रामदास जी की माता जी का क्या नाम था?
उत्तर-
दया कौर।
प्रश्न 52.
गुरु रामदास जी के पिता जी का क्या नाम था?
उत्तर-
हरिदास।

प्रश्न 53.
गुरु रामदास जी का संबंध किस जाति से था ?
उत्तर-
सोढी।
प्रश्न 54.
सोढी सुल्तान किस गुरु साहिब को कहा जाता है ?
उत्तर-
गुरु रामदास जी को।
प्रश्न 55.
गुरु रामदास जी का विवाह किससे हुआ था ?
अथवा
गुरु रामदास जी की पत्नी का नाम लिखो।
उत्तर-
बीबी भानी जी से।

प्रश्न 56.
बीबी भानी कौन थी?
उत्तर-
गुरु रामदास जी की पत्नी।
प्रश्न 57.
गुरु रामदास जी के पुत्रों के क्या नाम थे ?
उत्तर-
पृथी चंद, महादेव तथा अर्जन देव जी।
प्रश्न 58.
पृथी चंद कौन था ?
उत्तर-
गुरु रामदास जी का ज्येष्ठ पुत्र।

प्रश्न 59.
गुरु रामदास जी कब गुरुगद्दी पर बैठे ?
उत्तर-
1574 ई०।
प्रश्न 60.
सिख पंथ के विकास के लिए रामदास जी द्वारा किए गए कोई एक कार्य का वर्णन कीजिए।
अथवा
गुरु रामदास जी की कोई एक महत्त्वपूर्ण सफलता का उल्लेख करें।
उत्तर-
रामदासपुरा शहर की स्थापना।
प्रश्न 61.
रामदासपुरा की स्थापना कब की गई थी ?
उत्तर-
1577 ई०।

प्रश्न 62.
रामदासपुरा किस नाम से प्रसिद्ध हुआ ?
उत्तर-
अमृतसर।
प्रश्न 63.
अमृतसर का पहला नाम क्या था ?
उत्तर-
रामदासपुरा।
प्रश्न 64.
अमृतसर नगर की नींव कब रखी गई थी ?
उत्तर-
1577 ई०।

प्रश्न 65.
अमृसतर की स्थापना किस गुरु साहिब जी ने की ?
उत्तर-
गुरु रामदास जी।
प्रश्न 66.
सिखों और उदासियों के बीच समझौता किस गुरु के समय में हुआ ?
उत्तर-
गुरु रामदास जी।
प्रश्न 67.
मसंद प्रथा किसने चलाई थी ?
अथवा
मसंद प्रथा किस गरु ने शुरू की ?
उत्तर-
गुरु रामदास जी।

प्रश्न 68.
मसंद प्रथा का कोई एक उद्देश्य बताओ।
उत्तर-
सिख धर्म का प्रचार करना।
प्रश्न 69.
‘चार लावां’ का उच्चारण किस गुरु साहिब ने किया ?
अथवा
विवाह के समय लावां की प्रथा किस गुरु साहिब ने आरंभ की थी?
उत्तर-
गुरु रामदास जी ने।
प्रश्न 70.
गुरु रामदास जी ने कितने शब्दों की रचना की ?
उत्तर-
679 शब्दों की।

प्रश्न 71.
चार लावों की रचना किस गुरु साहिब ने की थी ?
उत्तर-
गुरु रामदास जी ने।
प्रश्न 72.
गुरु रामदास जी कब ज्योति-ज्योत समाए थे ?
उत्तर-
1581 ई० में।
प्रश्न 73.
गुरु रामदास जी के उत्तराधिकारी कौन थे ?
उत्तर-
गुरु अर्जन देव जी।

(ii) रिक्त स्थान भरें (Fill in the Blanks)
प्रश्न 1.
सिखों के दूसरे गुरु ……………. थे।
उत्तर-
(अंगद देव जी)
प्रश्न 2.
गुरु अंगद देव जी का आरंभिक नाम ……………… था।
उत्तर-
(भाई लहणा जी)
प्रश्न 3.
गुरु अंगद देव जी का जन्म ………………. को हुआ।
उत्तर-
(1504 ई०)

प्रश्न 4.
गुरु अंगद देव जी के पिता जी का नाम ……… था।
उत्तर-
(फेरूमल)
प्रश्न 5.
गुरु अंगद देव जी …………… में गुरुगद्दी पर बैठे थे।
उत्तर-
(1539 ई०)
प्रश्न 6.
गुरमुखी लिपि को ………….. ने लोकप्रिय बनाया।
उत्तर-
(गुरु अंगद देव जी)

प्रश्न 7.
……………… उदासी मत के संस्थापक थे।
उत्तर-
(बाबा श्री चंद जी)
प्रश्न 8.
गुरु अंगद देव जी ने गोइंदवाल साहिब की स्थापना ……………… में की।
उत्तर-
(1546 ई०)
प्रश्न 9.
गुरु अंगद देव जी …………. में ज्योति-ज्योत समाए।
उत्तर-
(1552 ई०)

प्रश्न 10.
सिखों के तीसरे गुरु ……………….. थे।
उत्तर-
(गुरु अमरदास जी)
प्रश्न 11.
गुरु अमरदास जी का जन्म ………………. में हुआ।
उत्तर-
(1479 ई०)
प्रश्न 12.
गुरु अमरदास जी ………… जाति के साथ संबंधित थे।
उत्तर-
(भल्ला )

प्रश्न 13.
गुरु अमरदास जी …………….. में गुरुगद्दी पर बैठे।
उत्तर-
(1552 ई०)
प्रश्न 14.
गुरु अमरदास जी …………….. की आयु में सिखों के तीसरे गुरु बने।
उत्तर-
(73 वर्ष)
प्रश्न 15.
गुरु अमरदास जी ने …………. में बाऊली का निर्माण करवाया।
उत्तर-
(गोइंदवाल साहिब)

प्रश्न 16.
गुरु अमरदास जी ने गोइंदवाल साहिब में बाऊली का निर्माण …………. में आरंभ करवाया।
उत्तर-
(1552 ई०)
प्रश्न 17.
मंजी प्रथा की स्थापना ……………… ने की थी।
उत्तर-
(गुरु अमरदास जी)
प्रश्न 18.
मुग़ल बादशाह ……………. गोइंदवाल साहिब में गुरु अमरदास जी से मिलने आया था।
उत्तर-
(अकबर)
प्रश्न 19.
गुरु अमरदास जी और मुग़ल बादशाह …………. के मध्य मुलाकात हुई।
उत्तर-
(अकबर)

प्रश्न 20.
गुरु अमरदास जी …………….. में ज्योति-ज्योत समाए।
उत्तर-
(1574 ई०)
प्रश्न 21.
…………….. सिखों के चौथे गुरु थे।
उत्तर-
(गुरु रामदास जी)
प्रश्न 22.
गुरु रामदास जी का आरंभिक नाम ……………. था।
उत्तर-
(भाई जेठा जी)
प्रश्न 23.
गुरु रामदास जी …………… जाति से संबंधित थे। ।
उत्तर-
(सोढी)

प्रश्न 24.
गुरु रामदास जी का विवाह …………….. के साथ हुआ था।
उत्तर-
(बीबी भानी)
प्रश्न 25.
गुरु रामदास जी …………………… में गुरुगद्दी पर बैठे। .
उत्तर-
(1574 ई०)
प्रश्न 26.
गुरु रामदास जी ने …………….. में रामदासपुरा की स्थापना की।
उत्तर-
(1577 ई०)
प्रश्न 27.
………………. ने मसंद प्रथा की स्थापना की।
उत्तर-
(गुरु रामदास जी)

(ii) ठीक अथवा गलत (True or False)
नोट-निम्नलिखित में से ठीक अथवा गलत चुनें-
प्रश्न 1.
गुरु अंगद देव जी सिखों के तीसरे गुरु थे।
उत्तर-
गलत
प्रश्न 2.
गुरु अंगद देव जी का आरंभिक नाम भाई लहणा जी था।
उत्तर-
ठीक
प्रश्न 3.
गुरु अंगद देव जी के पिता जी का नाम तेज भान था।
उत्तर-
गलत
प्रश्न 4.
गुरु अंगद देव जी की माता जी का नाम सभराई देवी था।
उत्तर-
ठीक

प्रश्न 5.
गुरु अंगद देव जी का विवाह बीबी खीवी के साथ हुआ था।
उत्तर-
ठीक
प्रश्न 6.
गुरु अंगद देव जी 1539 ई० में सिखों के दूसरे गुरु बने।
उत्तर-
ठीक
प्रश्न 7.
गुरु अंगद देव जी ने फ़ारसी को लोकप्रिय बनाने के लिए महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।
उत्तर-
गलत
प्रश्न 8.
उदासी मत की स्थापना बाबा श्रीचंद जी ने की थी।
उत्तर-
ठीक

प्रश्न 9.
गुरु अंगद देव जी की मुग़ल बादशाह अकबर के साथ भेंट हुई थी।
उत्तर-
गलत
प्रश्न 10.
गुरु अंगद देव जी 1539 ई० में ज्योति-ज्योत समाए थे।
उत्तर-
गलत
प्रश्न 11.
गुरु अमरदास जी सिखों के तीसरे गुरु थे।
उत्तर-
ठीक
प्रश्न 12.
गुरु अमरदास जी का जन्म 1479 ई० को हुआ था।
उत्तर-
ठीक

प्रश्न 13.
गुरु अमरदास जी के पिता जी का नाम तेज़ भान था।
उत्तर-
ठीक
प्रश्न 14.
बीबी भानी गुरु अमरदास जी की पुत्री का नाम था।
उत्तर-
ठीक
प्रश्न 15.
गुरु अमरदास जी 1552 ई० में गुरुगद्दी पर विराजमान हुए।
उत्तर-
ठीक
प्रश्न 16.
गुरु अमरदास जी ने गोइंदवाल साहिब में बाऊली का निर्माण करवाया।
उत्तर-
ठीक

प्रश्न 17.
गुरु रामदास जी ने मंजी प्रथा की स्थापना की थी।
उत्तर-
गलत
प्रश्न 18.
गुरु अमरदास जी ने सती प्रथा का जोरदार शब्दों में खंडन किया।
उत्तर-
ठीक
प्रश्न 19.
गुरु रामदास जी सिखों के चौथे गुरु थे।
उत्तर-
ठीक
प्रश्न 20.
गुरु रामदास जी का आरंभिक नाम भाई जेठा जी था।
उत्तर-
ठीक

प्रश्न 21.
गुरु रामदास जी सोढी जाति से संबंधित थे।
उत्तर-
ठीक
प्रश्न 22.
गुरु रामदास जी की पत्नी का नाम बीबी भानी था।
उत्तर-
ठीक
प्रश्न 23.
गुरु रामदास जी 1574 ई० को गुरुगद्दी पर बिराजमान हुए।
उत्तर-
ठीक
प्रश्न 24.
रामदासपुरा की स्थापना 1577 ई० में की गई।
उत्तर-
ठीक
प्रश्न 25.
गुरु अमरदास जी ने मसंद प्रथा को आरंभ किया था।
उत्तर-
गलत

प्रश्न 26.
गुरु रामदास जी के समय सिखों और उदासियों के मध्य समझौता हो गया था।
उत्तर-
ठीक
प्रश्न 27. गुरु रामदास जी ने सिखों में चार लावाँ द्वारा विवाह करने की मर्यादा आरंभ की।
उत्तर-
ठीक
प्रश्न 28.
गुरु रामदास जी 1581 ई० में ज्योति-ज्योत समाए थे।
उत्तर-
ठीक
(iv) बहु-विकल्पीय प्रश्न (Multiple Choice Questions)
नोट-निम्नलिखित में से ठीक उत्तर का चयन कीजिए
प्रश्न 1.
सिखों के दूसरे गुरु कौन थे ?
(i) गुरु अमरदास जी
(ii) गुरु रामदास जी
(ii) गुरु अंगद देव जी
(iv) गुरु अर्जन देव जी।
उत्तर-
(iii)

प्रश्न 2.
गुरु अंगद देव जी का जन्म कब हुआ?
(i) 1469 ई० में
(ii) 1479 ई० में
(iii) 1501 ई० में
(iv) 1504 ई० में।
उत्तर-
(iv)
प्रश्न 3.
गुरु अंगद देव जी का जन्म कहाँ हुआ ?
(i) मत्ते की सराय
(ii) कीरतपुर साहिब
(iii) गोइंदवाल साहिब
(iv) हरीके।
उत्तर-
(i)
प्रश्न 4.
गुरु अंगद देव जी का आरंभिक नाम क्या था ?
(i) भाई जेठा जी
(ii) भाई लहणा जी
(iii) भाई गुरदित्ता जी
(iv) भाई दासू जी।
उत्तर-
(ii)

प्रश्न 5.
गुरु अंगद देव जी के पिता जी कौन थे ?
(i) त्याग मल जी
(ii) फेरूमल जी
(iii) तेजभान जी
(iv) मेहरबान जी।
उत्तर-
(ii)
प्रश्न 6.
गुरु अंगद देव जी की माता जी का क्या नाम था ?
(i) लक्ष्मी देवी जी
(ii) सभराई देवी जी
(iii) मनसा देवी जी
(iv) सुभाग देवी जी।
उत्तर-
(ii)
प्रश्न 7.
गुरु अंगद देव जी की पत्नी कौन थी ?
(i) बीबी खीवी जी
(ii) बीबी नानकी जी
(iii) बीबी अमरो जी
(iv) बीबी भानी जी।
उत्तर-
(i)
प्रश्न 8.
गुरु अंगद देव जी कब गुरुगद्दी पर बैठे ?
(i) 1529 ई० में
(ii) 1538 ई० में
(iii) 1539 ई० में ।
(iv) 1552 ई० में।
उत्तर-
(ii)

प्रश्न 9.
गुरु अंगद देव जी की धार्मिक गतिविधियों का केंद्र कौन-सा था ?
(i) गोइंदवाल साहिब
(ii) अमृतसर
(iii) खडूर साहिब
(iv) सुल्तानपुर लोधी।
उत्तर-
(iii)
प्रश्न 10.
किस गुरु साहिब ने गुरुमुखी लिपि को लोकप्रिय बनाया ?
(i) गुरु नानक देव जी ने
(ii) गुरु अंगद देव जी ने
(iii) गुरु अमरदास जी ने
(iv). गुरु गोबिंद सिंह जी ने।
उत्तर-
(ii)
प्रश्न 11.
उदासी मत का संस्थापक कौन था ?
(i) बाबा श्री चंद जी
(ii) बाबा लख्मी दास जी
(iii) बाबा मोहन जी
(iv) बाबा मोहरी जी।
उत्तर-
(i)
प्रश्न 12.
गुरु अंगद साहिब ने किस नगर की स्थापना की थी ?
(i) करतारपुर
(ii) तरनतारन
(iii) कीरतपुर साहिब
(iv) गोइंदवाल साहिब।
उत्तर-
(iv)

प्रश्न 13.
कौन-सा मुग़ल बादशाह गुरु अंगद साहिब को मिलने के लिए खडूर साहिब आया था ?
(i) बाबर
(ii) हुमायूँ
(iii) अकबर
(iv) जहाँगीर।
उत्तर-
(ii)
प्रश्न 14.
गुरु अंगद साहिब जी कब ज्योति-जोत समाए ?
(i) 1550 ई० में
(ii) 1551 ई० में
(iii) 1552 ई० में
(iv) 1554 ई० में।
उत्तर-
(iii)
प्रश्न 15.
सिखों के तीसरे गुरु कौन थे ?
(i) गुरु अंगद देव जी
(ii) गुरु रामदास जी
(iii) गुरु अमरदास जी
(iv) गुरु अर्जन देव जी।
उत्तर-
(iii)
प्रश्न 16.
गुरु अमरदास जी का जन्म कब हुआ ?
(i) 1458 ई० में
(ii) 1465 ई० में
(iii) 1469 ई० में
(iv) 1479 ई० में।
उत्तर-
(iv)

प्रश्न 17.
गुरु अमरदास जी का जन्म कहाँ हुआ ?
(i) खडूर साहिब
(ii) हरीके
(iii) बासरके
(iv) गोइंदवाल साहिब।
उत्तर-
(iii)
प्रश्न 18.
गुरु अमरदास जी के पिता जी का क्या नाम था ?
(i) तेजभान भल्ला
(ii) मेहरबान
(iii) मोहन दास
(iv) फेरूमल।
उत्तर-
(i)
प्रश्न 19.
बीबी भानी जी कौन थी ?
(i) गुरु अंगद देव जी की पुत्री
(ii) गुरु अमरदास जी की पत्नी
(iii) गुरु अमरदास जी की पुत्री
(iv) गुरु रामदास जी की पुत्री।
उत्तर-
(iii)
प्रश्न 20.
आनंदु साहिब की रचना किस गुरु साहिबान ने की थी ?
(i) गुरु नानक देव जी ने
(ii) गुरु अंगद देव जी ने
(iii) गुरु अमरदास जी ने
(iv) गुरु रामदास जी ने।
उत्तर-
(iii) गुरु अमरदास जी ने

प्रश्न 21.
किस गुरु साहिबान ने मंजी प्रथा की स्थापना की थी ?
(i) गुरु अंगद देव जी ने
(ii) गुरु अमरदास जी ने
(iii) गुरु रामदास जी ने
(iv) गुरु अर्जन देव जी ने।
उत्तर-
(i)
प्रश्न 22.
मंजी प्रथा की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था ?
(i) सिख धर्म का प्रचार करना
(ii) लंगर के लिए अनाज इकट्ठा करना
(iii) गुरुद्वारे का निर्माण करना ।
(iv) उपरोक्त सभी।
उत्तर-
(i)
प्रश्न 23.
गुरु अमरदास जी ने कुल कितनी मंजियों की स्थापना की ? (
(i) 20
(ii) 24
(iii) 26
(iv) 22
उत्तर-
(iv)
प्रश्न 24.
गुरु अमरदास जी ने निम्नलिखित में से किस बुराई का खंडन किया ?
(i) बाल विवाह.
(ii) सती प्रथा
(iii) पर्दा प्रथा
(iv) उपरोक्त सभी।
उत्तर-
(iv)

प्रश्न 25.
गुरु अमरदास जी की धार्मिक गतिविधियों का केंद्र कौन-सा था ?
(i) अमृतसर
(ii) गोइंदवाल साहिब
(iii) खडूर साहिब
(iv) लाहौर।
उत्तर-
(i)
प्रश्न 26.
गुरु अमरदास जी कब ज्योति-जोत समाए थे ?
(i) 1552 ई० में
(ii) 1564 ई० में
(iii) 1568 ई० में
(iv) 1574 ई० में।
उत्तर-
(iv)
प्रश्न 27.
सिखों के चौथे गुरु कौन थे ?
(i) गुरु रामदास जी
(ii) गुरु अमरदास जी
(iii) गुरु अर्जन देव जी
(iv) गुरु हरकृष्ण जी।
उत्तर-
(i)
प्रश्न 28.
गुरु रामदास जी का जन्म कब हुआ ?
(i) 1479 ई० में
(ii) 1524 ई० में
(iii) 1534 ई० में
(iv) 1539 ई० में।
उत्तर-
(iii)

प्रश्न 29.
गुरु रामदास जी का आरंभिक नाम क्या था ?
(i) भाई बाला जी
(ii) भाई जेठा जी
(iii) भाई लहणा जी
(iv) भाई मरदाना जी।
उत्तर-
(ii)
प्रश्न 30.
गुरु रामदास जी के पिता जी का क्या नाम था ?
(i) हरीदास जी
(i) अमरदास जी
(iii) तेजभान जी
(iv) फेरूमल जी।
उत्तर-
(i)
प्रश्न 31.
गुरु रामदास जी की माता जी का क्या नाम था ?
(i) दया कौर जी
(ii) रूप कौर जी
(iii) सुलक्खनी जी
(iv) लक्ष्मी जी।
उत्तर-
(i)
प्रश्न 32.
गुरु रामदास जी कौन-सी जाति से संबंधित थे ?
(i) बेदी
(ii) भल्ला
(iii) सोढी
(iv) सेठी।
उत्तर-
(iii)

प्रश्न 33.
गुरु रामदास जी का विवाह किसके साथ हुआ था ?
(i) बीबी दानी जी
(i) बीबी भानी जी
(iii) बीबी अमरो जी
(iv) बीबी अनोखी जी।
उत्तर-
(ii)
प्रश्न 34.
पृथी चंद कौन था ?
(i) गुरु रामदास का बड़ा भाई
(ii) गुरु अर्जन देव जी का बड़ा भाई
(iii) गुरु अर्जन देव जी का पुत्र
(iv) गुरु हरगोबिंद जी का पुत्र।
उत्तर-
(i)
प्रश्न 35.
गुरु रामदास जी गुरुगद्दी पर कब बैठे ?
(i) 1534 ई० में
(ii) 1552 ई० में
(iii) 1554 ई० में
(iv) 1574 ई० में।
उत्तर-
(iv)
प्रश्न 36.
रामदासपुरा अथवा अमृतसर की स्थापना किस गुरु साहिबान ने की थी ?
(i) गुरु अमरदास जी ने ।
(ii) गुरु रामदास जी ने
(iii) गुरु अर्जन देव जी ने
(iv) गुरु हरगोबिंद जी ने।
उत्तर-
(ii)

प्रश्न 37.
गुरु जी ने रामदासपुरा की नींव कब रखी थी ?
(i) 1574 ई० में
(ii) 1575 ई० में
(iii) 1576 ई० में
(iv) 1577 ई० में।
उत्तर-
(iv)
प्रश्न 38.
मसंद प्रथा का आरंभ किस गुरु ने किया था ?
(i) गुरु रामदास जी
(ii) गुरु अर्जन देव जी
(iii) गुरु अमरदास जी
(iv) गुरु तेग़ बहादुर जी।
उत्तर-
(i)
प्रश्न 39.
किस गुरु साहिबान के समय उदासियों और सिखों के बीच समझौता हुआ था ? ।
(i) गुरु अंगद देव जी
(ii) गुरु अमरदास जी
(iii) गुरु रामदास जी
(iv) गुरु अर्जन देव जी।
उत्तर-
(iii)
प्रश्न 40.
चार लावां की प्रथा किस गुरु साहिबान ने आरंभ की ?
(i) गुरु अमरदास जी ने
(ii) गुरु रामदास जी ने
(iii) गुरु अर्जन देव जी ने
(iv) गुरु हरगोबिंद जी ने।
उत्तर-
(ii)

प्रश्न 41.
कौन-सा मुगल बादशाह गुरु रामदास जी को मिलने आया था ?
(i) बाबर
(i) हुमायूँ
(iii) अकबर
(iv) औरंगज़ेब।
उत्तर-
(iii)
प्रश्न 42.
गुरु रामदास जी कब ज्योति-जोत समाए.?
(i) 1565 ई० में
(ii) 1571 ई० में
(iii) 1575 ई० में
(iv) 1581 ई० में।
उत्तर-
(iv)
Long Answer Type Question
प्रश्न 1.
सिख धर्म के विकास में गुरु अंगद देव जी द्वारा दिए गए योगदान पर चर्चा करें।
(Give description about Guru Angad Dev Ji’s contribution to the development of Sikhism.)
अथवा
सिख पंथ के विकास में गुरु अंगद देव जी ने क्या-क्या कार्य किए ? (What did Guru Angad Dev Ji do for the development of Sikh Panth ?)
अथवा
गुरु अंगद देव जी की किन्हीं छः ऐसी सफलताओं का वर्णन करें जिनके कारण सिख धर्म का विकास हुआ। (Write six achievements of Guru Angad Dev Ji for the development of Sikhism.)
अथवा
सिख पंथ के विकास में गुरु अंगद देव जी के कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। (Form an estimate of the works of Guru Angad Dev Ji for the spread of Sikhism.)
अथवा
गुरु अंगद देव जी पर एक संक्षिप्त नोट लिखें। (Write a short note on Guru Angad Dev Ji.) .
उत्तर-
गुरु अंगद देव जी 1539 ई० में सिखों के दूसरे गुरु बने। वह 1552 ई० तक गुरुगद्दी पर आसीन रहे। इस समय के दौरान गुरु अंगद देव जी ने सिख धर्म के विकास के लिए निम्नलिखित मुख्य काम किए—
1. गुरमुखी को लोकप्रिय बनाना—गुरु अंगद देव जी ने गुरमुखी लिपि को लोकप्रिय बनाने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने इसके रूप में एक नया निखार लाया। अब इस लिपि को समझना सामान्य लोगों के लिए सरल हो गया। इस लिपि के प्रसार के कारण सिखों में तीव्रता से विद्या का प्रसार भी होने लगा।
2. लंगर प्रथा का विस्तार-लंगर प्रथा के विकास का श्रेय गुरु अंगद देव जी को जाता है। लंगर का समूचा प्रबंध उनकी धर्म पत्नी माता खीवी जी करते थे। लंगर में सभी व्यक्ति बिना किसी ऊँच-नीच, जाति के भेदभाव के इकट्ठे मिलकर छकते थे। इस लंगर के लिए सारी माया गुरु जी के सिख देते थे। इस प्रथा के कारण सिखों में परस्पर सहयोग की भावना बढ़ी।
3. संगत का संगठन-गुरु अंगद देव जी ने गुरु नानक देव जी द्वारा स्थापित संगत संस्था को भी संगठित किया। संगत से अभिप्राय था-एकत्रित होकर बैठना। संगत में सभी धर्मों के लोग-स्त्री और पुरुष भाग ले सकते थे। यह संगत सुबह-शाम गुरु जी के उपदेशों को सुनने के लिए एकत्रित होती थी। इस संस्था ने सामाजिक असमानता को दूर करने तथा सिखों को संगठित करने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।
4. उदासी मत का खंडन-उदासी मत की स्थापना गुरु नानक देव जी के बड़े सुपुत्र बाबा श्रीचंद जी ने की थी। यह मत संन्यास अथवा त्याग के जीवन पर बल देता था। बहुत-से सिख उदासी मत को मान्यता देने लग पड़े थे। ऐसी परिस्थितियों में यह संकट उत्पन्न हो गया था कि कहीं सिख गुरु नानक देव जी के उपदेशों को भूल कर उदासी मत न अपना लें। अत: गुरु अंगद देव जी ने उदासी मत का कड़ा विरोध करके सिख मत के अस्तित्व को बनाए रखा।
5. गोइंदवाल साहिब की स्थापना—गुरु अंगद देव जी ने खर साहिब के समीप गोइंदवाल साहिब नामक एक नए नगर की स्थापना की। इस नगर का निर्माण कार्य एक श्रद्धालु सेवक अमरदास की देख-रेख में 1546 ई० में आरंभ हुआ। यह नगर शीघ्र ही सिखों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान बन गया।
6. उत्तराधिकारी की नियुक्ति-गुरु अंगद देव जी का सिख पंथ के विकास में सबसे महान् कार्य अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करना था। इसलिए उन्होंने अपने श्रद्धालु अमरदास जी का चुनाव किया।

प्रश्न 2.
गुरु अंगद देव जी ने गुरुमुखी लिपि को हरमन प्यारा बनाने के लिए क्या योगदान दिया ?
(What contribution was made by Guru Angad Dev Ji to improve Gurumukhi script ?)
अथवा
सिख धर्म के विकास में गुरु अंगद देव जी द्वारा गुरुमुखी को लोकप्रिय बनाने का क्या प्रभाव पड़ा ?
(What impact did the popularisation of Gurumukhi by Guru Angad Dev Ji leave on the growth of Sikhism ?)
उत्तर-
गुरु अंगद देव जी ने गुरुमखी लिपि को लोकप्रिय बनाकर सिख पंथ के विकास की ओर प्रथम महत्त्वपूर्ण पग उठाया। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया इस संबंध में इतिहासकारों में मतभेद हैं। डॉक्टर आई० बी० बैनर्जी का कथन है कि गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक देव जी द्वारा रचित राग आसा अंकित है। इसमें 35 अक्षरों पर आधारित एक पट्टी की रचना की गई है जिसमें गुरुमुखी के सभी 35 अक्षरों का प्रयोग किया गया है। इससे सिद्ध होता है कि गुरुमुखी लिपि का प्रचलन गुरु अंगद देव जी के समय से पूर्व हो चुका था।
यह ठीक है कि गुरुमुखी लिपि गुरु अंगद देव जी से पूर्व अस्तित्व में आ चुकी थी। इसे उस समय लंडा लिपि कहा जाता था। इसे पढ़कर कोई भी व्यक्ति बहुत सरलता से भ्रम में पड़ सकता था। इसलिए गुरु अंगद देव जी ने इसके रूप में एक नया निखार लाया। अब इस लिपि को समझना सामान्य लोगों के लिए भी बहुत सरल हो गया था। सिखों के सभी धार्मिक ग्रंथों की रचना इस लिपि में हुई। इस लिपि का नाम गुरुमुखी अर्थात् गुरुओं के मुख से निकली हुई होने के कारण यह सिखों को गुरु के प्रति अपने कर्तव्य का स्मरण दिलाती रही। इस प्रकार यह लिपि सिखों को अपनी अलग पहचान बनाए रखने में सहायक सिद्ध हुई। इस लिपि के प्रसार के कारण सिखों में तीव्रता से विद्या का प्रसार होने लगा। इसके अतिरिक्त इस लिपि के प्रचलित होने से ब्राह्मण वर्ग को कड़ा आघात पहुँचा क्योंकि वे संस्कृत को ही. धर्म की भाषा मानते थे। नि:संदेह गुरुमुखी लिपि का प्रचार सिख पंथ के विकास के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुआ।
प्रश्न 3.
संगत एवं पंगत के महत्त्व पर एक संक्षिप्त नोट लिखें। (Write a short note on the importance of Sangat and Pangat.)
अथवा
संगत एवं पंगत के बारे में आप क्या जानते हैं ? (What do you know about Sangat and Pangat ?)
उत्तर-
1. संगत-संगत संस्था से अभिप्राय एकत्रित रूप में मिलकर बैठने से था। यह संगत सुबह-शाम गुरु जी के उपदेशों को सुनने के लिए एकत्रित होती थी। इस संस्था की स्थापना गुरु नानक देव जी ने की थी। गुरु अंगद देव जी ने इस संस्था को अधिक संगठित किया। संगत में कोई भी स्त्री अथवा पुरुष बिना किसी जाति-पाति अथवा धर्म के भेद-भाव के सम्मिलित हो सकता था। संगत को ईश्वर का रूप समझा जाता था। संगत में जाने वाले व्यक्ति का काया कल्प हो जाता था। उसकी सभी मनोकामनाएँ पूर्ण होती थीं। वह भवसागर से पार हो जाता था। निस्संदेह यह संस्था सिख पंथ के विकास के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुई।
2. पंगत-पंगत (लंगर) संस्था की स्थापना गुरु नानक देव जी ने की थी। गुरु अंगद देव जी ने इसे जारी रखा और गुरु अमरदास जी ने इस संस्था को अधिक विकसित किया। मुगल सम्राट अकबर और हरिपुर के राजा ने भी गुरु अमरदास जी के दर्शन करने से पूर्व लंगर खाया था। लंगर प्रत्येक धर्म और जाति के लोगों के लिए खुला था। सिख धर्म के प्रसार में लंगर संस्था का योगदान बहुत महत्त्वपूर्ण था। इस संस्था ने समाज में जाति प्रथा और छुआछूत की भावनाओं को समाप्त करने में भी बड़ी सहायता की। इस संस्था के कारण सिखों में परस्पर भ्रातृत्व की भावना का विकास हुआ।

प्रश्न 4.
गुरुगद्दी प्राप्त करने के पश्चात् गुरु अमरदास जी को जिन आरंभिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उनका संक्षेप वर्णन कीजिए।
(What problems had Guru Amar Das Ji to face in the early years of his pontificate ?)
उत्तर-
गुरुगद्दी प्राप्त करने के पश्चात् गुरु अमरदास जी को जिन आरंभिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उनका संक्षेप वर्णन निम्नलिखित है—
1. दासू और दातू का विरोध-गुरु अमरदास जी को अपने गुरुकाल के आरंभ में, गुरु अंगद देव जी के पुत्रों दासू और दातू के विरोध का सामना करना पड़ा। उन्होंने गुरु जी को गुरु मानने से इंकार कर दिया तथा स्वयं को असली उत्तराधिकारी घोषित किया। सिखों ने उन्हें अपना गुरु मानने.से इंकार कर दिया। इस समय दातू ने भी माता खीवी जी के कहने पर अपना विरोध छोड़ दिया था।
2. बाबा श्रीचंद जी का विरोध-बाबा श्रीचंद जी गुरु नानक देव जी के ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण गुरुगद्दी पर अपना अधिकार समझते थे। बाबा श्रीचंद जी के अनेक समर्थक थे। गुरु अमरदास जी ने ऐसे समय में दृढ़ता से काम लेते हुए सिखों को स्पष्ट किया कि उदासी संप्रदाय के सिद्धांत गुरु नानक देव जी के उपदेशों के विपरीत हैं। उनके तर्कों से प्रभावित होकर सिखों ने बाबा श्रीचंद जी का साथ छोड़ दिया।
3. गोइंदवाल साहिब के मुसलमानों का विरोध-गोइंदवाल साहिब में गुरु अमरदास जी की बढ़ती हुई ख्याति देखकर वहाँ के मुसलमानों ने सिखों को परेशान करना आरंभ कर दिया। वे सिखों का सामान चोरी कर लेते। वे सतलुज नदी से जल भर कर लाने वाले सिखों के घड़े पत्थर मार कर तोड़ देते थे। सिख इस संबंध में गुरु जी से शिकायत करते। अमरदास जी ने सिखों को शाँत रहने का उपदेश दिया।
4. हिंदुओं द्वारा विरोध-इसका कारण यह था कि गुरु अमरदास जी के सामाजिक सुधारों से प्रभावित होकर बहुत-से लोग सिख धर्म में शामिल होते जा रहे थे। सिख धर्म में ऊँच-नीच का भेदभाव नहीं किया जाता था। बाऊली का निर्माण होने से सिखों को एक अलग तीर्थ स्थान भी मिल गया था। गोइंदवाल साहिब के उच्च जातियों के हिंदू यह बात सहन न कर सके। उन्होंने मुग़ल बादशाह अकबर के पास यह झूठी शिकायत की कि गुरु जी हिंदू धर्म के विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं। अकबर ने गुरु जी को निर्दोष घोषित किया।
प्रश्न 5.
गुरु अमरदास जी के समय होने वाले सिख धर्म के विकास का विवरण दीजिए।
(Give an account of the development of Sikhism Under Guru Amar Das Ji.)
अथवा
सिख धर्म के विकास में गुरु अमरदास जी द्वारा किये गये छः महत्त्वपूर्ण कार्यों का वर्णन करें।
(Give six contributions of Guru Amar Das Ji for the development of Sikhism.)
अथवा
गुरु अमरदास जी के कार्यों का मूल्याँकन कीजिए। (Form an estimate of the works of Guru Amar Das Ji.)
अथवा
सिख पंथ के विकास में गुरु अमरदास जी के कार्यों के बारे में आप क्या जानते हैं ? (What do you know about the works of Guru Amat Das Ji for the spread of Sikhism ?)
अथवा
सिख पंथ के विकास में गुरु अमरदास जी के योगदान का अध्ययन करें। (Study the contribution of Guru Amar Das Ji to the growth of Sikhism.)
उत्तर-
गुरु अमरदास जी 1552 ई० से 1574 ई० तक गुरुगद्दी पर रहे। इस समय के दौरान गुरु अमरदास जी ने सिख पंथ के संगठन के लिए निम्नलिखित प्रशंसनीय काम किए—
1. गोइंदवाल साहिब में बाऊली का निर्माण—गुरु अमरदास जी का सिख पंथ के विकास की ओर प्रथम पग गोइंदवाल साहिब में एक बाऊली का निर्माण करना था। इस बाऊली का निर्माण कार्य 1552 ई० से 1559 ई० तक चला। इस बाऊली तक पहुँचने के लिए 84 सीढ़ियाँ बनाई गई थीं। बाऊली के निर्माण से सिख पंथ को एक पवित्र तीर्थ स्थान मिल गया।
2. लंगर संस्था का विस्तार-गुरु अमरदास जी ने, गुरु नानक देव जी द्वारा स्थापित लंगर संस्था का और विस्तार किया। गुरु जी ने यह घोषणा की कि कोई भी यात्री लंगर छके बिना उनके दर्शन नहीं कर सकता। इस लंगर में विभिन्न धर्मों और जातियों के लोग सम्मिलित होते थे। यह संस्था सिख धर्म के प्रचार में बड़ी सहायक प्रमाणित हुई । इससे जाति-प्रथा को गहरा आघात पहुँचा।
3. मंजी प्रथा-मंजी प्रथा की स्थापना गुरु अमरदास जी के सबसे महत्त्वपूर्ण कार्यों में से एक थी। सिखों की संख्या में वृद्धि के कारण गुरु साहिब के लिए प्रत्येक सिख तक पहुँच पाना संभव नहीं था। उन्होंने अपने उपदेश दूर-दूर के क्षेत्रों में रहने वाले सिखों तक पहुँचाने के लिए 22 मंजियों की स्थापना की । मंजी प्रथा की स्थापना के परिणामस्वरूप सिख धर्म की प्रसिद्धि दूर-दूर तक फैल गई।
4. उदासी संप्रदाय का खंडन—गुरु अमरदास जी के समय में उदासी संप्रदाय सिख संप्रदाय के अस्तित्व के लिए ख़तरा बना हुआ था। बहुत-से सिख बाबा श्रीचंद जी से प्रभावित होकर उदासी संप्रदाय में सम्मिलित होने लगे थे। ऐसे समय गुरु अमरदास जी ने सिखों को समझाया कि सिख धर्म उदासी मत से बिल्कुल अलग है। इस प्रकार गुरु अमरदास जी ने सिख धर्म को हिंदू धर्म में विलीन होने से बचा लिया।
5. सामाजिक सुधार-गुरु अमरदास जी एक महान् समाज सुधारक थे। उन्होंने जाति प्रथा, सती प्रथा, बालविवाह तथा पर्दा प्रथा का जोरदार शब्दों में खंडन किया। उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया। इसके अतिरिक्त गुरु अमरदास जी ने सिखों के जन्म, विवाह तथा मृत्यु के अवसरों के लिए विशेष रस्में प्रचलित की। संक्षेप में गुरु अमरदास जी ने एक आदर्श समाज का निर्माण किया।
6. वाणी का संग्रह-गुरु अमरदास जी का अगला महत्त्वपूर्ण कार्य गुरु नानक देव जी तथा गुरु अंगद देव जी की वाणी का संग्रह करना था। गुरु साहिब ने स्वयं 907 शब्दों की रचना की। इस से आदि ग्रंथ साहिब के संकलन के लिए सामग्री एकत्र हो गई।

प्रश्न 6.
सिख इतिहास में गोइंदवाल साहिब की बाऊली के निर्माण का क्या महत्त्व है ?
(What is the importance of the construction of the Baoli of Goindwal Sahib in Sikh History ?)
उत्तर-
गुरु अमरदास जी का सिख पंथ के विकास की ओर पहला पग गोइंदवाल में एक बाऊली का निर्माण करना था। इस बाऊली का निर्माण-कार्य 1552 ई० में आरंभ किया गया था और यह 1559 ई० में संपूर्ण हुआ था। गोइंदवाल साहिब में बाऊली के निर्माण के पीछे गुरु अमरदास जी के दो उद्देश्य थे। पहला, वह सिखों को एक अलग तीर्थ स्थान देना चाहते थे ताकि उन्हें हिंदू धर्म से अलग किया जा सके। दूसरे, वह वहाँ के लोगों की पानी के संबंध में कठिनाई को दूर करना चाहते थे। इस बाऊली तक पहुँचने के लिए 84 सीढ़ियाँ बनाई गई थीं। बाऊली का निर्माण कार्य पूर्ण होने पर गुरु जी ने यह घोषणा की कि जो यात्री प्रत्येक सीढ़ी पर शुद्ध हृदय से जपुजी साहिब का पाठ करेगा तथा पाठ के पश्चात् बाऊली में स्नान करेगा वह 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाएगा। बाऊली का निर्माण सिख पंथ के विकास के लिए एक बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य प्रमाणित हुआ। इससे सिखों को एक पवित्र तीर्थ स्थान मिल गया। सिखों को हिंदुओं के तीर्थ स्थानों पर जाने की आवश्यकता नहीं थी। दूसरा बाऊली के निर्माण के कारण सिखों की साफ पीने के पानी की समस्या दूर हो गई। इससे पहले लोग ब्यास नदी से पानी लाते थे जोकि बरसात के दिनों में गंदा हो जाता था। बड़ी संख्या में सिखों के गोइंदवाल साहिब में पहुँचने पर गुरु अमरदास जी की ख्याति दूर-दूर तक फैल गई। इसके अतिरिक्त विभिन्न जातियों के लोगों के द्वारा बाऊली में स्नान करने से जाति प्रथा को एक गहरा धक्का लगा।
प्रश्न 7.
गुरु अमरदास जी के द्वारा किए गए सामाजिक सुधारों का संक्षेप में वर्णन करें। (Describe briefly the social reforms of Guru Amar Das Ji.)
अथवा
गुरु अमरदास जी के छः सामाजिक सुधारों का वर्णन करें।
(Describe six social reforms of Guru Amar Das Ji.)
अथवा
गुरु अमरदास जी को समाज सुधारक क्यों कहा जाता है ? (Why is Guru Amar Das called a social reformer ?)
अथवा
समाज सुधारक के रूप में गुरु अमरदास जी पर एक संक्षिप्त नोट लिखें। (Write a short note on Guru Amar Das Ji as a social reformer.)
उत्तर-
1. जातीय भेद-भाव तथा छुआ-छूत का खंडन-गुरु अमरदास जी ने जातीय एवं छुआ-छूत की प्रथाओं का जोरदार शब्दों में खंडन किया। उन्होंने संगतों को यह हुक्म दिया कि जो कोई उनके दर्शन करना चाहता है उसे पहले पंगत में लंगर छकना पड़ेगा। इस प्रकार गुरु अमरदास जी ने आपसी भ्रातृत्व का प्रचार किया।
2. लड़कियों की हत्या का खंडन-उस समय लड़कियों के जन्म को अच्छा नहीं माना जाता था। अतः कुछ लोग लड़कियों के जन्म लेते ही उन्हें मार देते थे। गुरु अमरदास जी ने इस कुप्रथा का जोरदार शब्दों में खंडन किया। उनका कथन था कि जो व्यक्ति ऐसा करता है वह घोर पाप का सहभागी बनता है । उन्होंने सिखों को इस अपराध से दूर रहने का उपदेश दिया।
3. बाल विवाह का खंडन-उस समय समाज में प्रचलित परंपराओं के अनुसार लड़कियों का विवाह छोटी आयु में ही कर दिया जाता था। इस कारण समाज में स्त्रियों की दशा बहुत दयनीय हो गई थी। गुरु अमरदास जी ने बाल विवाह के विरुद्ध प्रचार किया।
4. सती प्रथा का खंडन-उस समय समाज में प्रचलित कुप्रथाओं में से सबसे घृणा योग्य कुप्रथा सती प्रथा की थी। इस अमानवीय प्रथा के अनुसार यदि किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसे जबरन पति की चिता के साथ जीवित जला दिया जाता था। गुरु अमरदास जी ने शताब्दियों से चली आ रही इस कुप्रथा के विरुद्ध एक ज़ोरदार अभियान चलाया।
5. पर्दा प्रथा का खंडन-उस समय समाज में पर्दा प्रथा का प्रचलन भी काफ़ी बढ़ गया था। यह प्रथा स्त्रियों के शारीरिक तथा मानसिक विकास में एक बड़ी बाधा थी। इसलिए गुरु अमरदास जी ने इस प्रथा की जोरदार शब्दों में आलोचना की। उन्होंने यह आदेश दिया कि संगत अथवा लंगर में सेवा करते समय कोई भी स्त्री पर्दा न करे।
6. नशीली वस्तुओं का खंडन-उस समय कुछ लोग नशीली वस्तुओं का प्रयोग करने लग पड़े थे। गुरु अमरदास जी ने इन वस्तुओं के सेवन की जोरदार शब्दों में आलोचना की।

प्रश्न 8.
मंजी प्रथा क्या थी ? सिख धर्म के विकास में इसने क्या योगदान दिया? (What was the Manji System ? How did it contribute to the development of Sikhism ?)
अथवा
मंजी प्रथा के बारे में आप क्या जानते हैं ?
(What do you know about Manji System ?)
अथवा
मंजी प्रथा पर एक नोट लिखें। (Write a note on Manji System.)
उत्तर-
सिख धर्म के विकास में मंजी प्रथा ने प्रशंसनीय भूमिका निभाई। इस महत्त्वपूर्ण संस्था के संस्थापक गुरु अमरदास जी थे। मंजी प्रथा के आरंभ एवं विकास का संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित अनुसार है—
1. आवश्यकता-गुरु अमरदास जी के अथक प्रयासों तथा उनके जादुई व्यक्तित्व के कारण बड़ी संख्या में लोग सिख धर्म में सम्मिलित हो गए थे। क्योंकि सिखों की संख्या बहुत बढ़ गई थी तथा वे पंजाब के बाहर के प्रदेशों में फैले हुए थे इसलिए गुरु साहिब के लिए निजी रूप से इन तक पहुँचना कठिन हो गया। दूसरा, इस समय गुरु अमरदास जी बहुत वृद्ध हो चुके थे। अतः गुरु अमरदास जी ने मंजी प्रथा को आरंभ करने की आवश्यकता अनुभव की।
2. मंजी प्रथा से अभिप्राय-गुरु अमरदास जी अपने सिखों को उपदेश देते समय एक विशाल चारपाई पर बैठते थे। इसे मंजा कहा जाता था। अन्य सिख ज़मीन अथवा दरी पर बैठकर उनके उपदेश सुनते थे। गुरु जी ने अपने जीवन काल में 22 मंजियों की स्थापना की थी। इनके मुखी मंजीदार कहलाते थे। ये मंजीदार गुरु जी के प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए एक छोटी चारपाई का प्रयोग करते थे। इस कारण यह संस्था मंजी प्रथा कहलाने लगी।
3. मंजीदार के कार्य-मंजीदार अपने अधीन प्रदेश में गुरु साहिबान का प्रतिनिधित्व करता था। वह अनेक प्रकार के कार्यों के लिए उत्तरदायी था।
- वह सिख धर्म के प्रचार के लिए अथक प्रयास करता था।
- वह गुरु साहिब के हुक्मों को सिख संगत तक पहुँचाता था।
- वह लोगों को धार्मिक शिक्षा देता था।
- वह लोगों को गुरुमुखी भाषा पढ़ाता था।
- वह अपने प्रदेश की संगतों के साथ वर्ष में कम-से-कम एक बार गुरु जी के दर्शनों के लिए गोइंदवाल साहिब आते थे।
4. मंजी प्रथा का महत्त्व-सिख धर्म के विकास एवं संगठन में मंजी प्रथा ने बहुमूल्य योगदान दिया। मंजीदारों के प्रभाव से बड़ी संख्या में लोग सिख धर्म में सम्मिलित होने लगे। इसके दूरगामी प्रभाव पड़े। मंजीदार धर्म प्रचार के अतिरिक्त संगत से लंगर एवं अन्य कार्यों के लिए धन भी एकत्र करते थे। गुरु अमरदास जी ने इस धन को सिख धर्म के विकास कार्यों पर खर्च किया। इससे सिख धर्म की लोकप्रियता में काफ़ी वृद्धि हुई।
प्रश्न 9.
गुरु अमरदास जी के मुगलों के साथ कैसे संबंध थे ? (What type of relations did Guru Amar Das Ji have with the Mughals ?)
अथवा
मुगल बादशाह अकबर तथा गुरु अमरदास जी के मध्य संबंधों का उल्लेख कीजिए । (Describe the relations between Mughal emperor Akbar and Guru Amar Das Ji.)
अथवा
मुगल सम्राट अकबर तथा गुरु अमरदास जी के बीच संबंधों का उल्लेख करें। (Explain the relations between the Mughal emperor Akbar and Guru Amar Das Ji.)
उत्तर-
गुरु अमरदास जी के मुग़लों के साथ संबंध बहुत अच्छे थे। उस समय भारत में मुग़ल बादशाह अकबर का शासन था। गुरु अमरदास जी की ‘अरदास’ के फलस्वरूप अकबर को चित्तौड़ के अभियान में सफलता प्राप्त हुई थी। इसलिए गुरु साहिब का आभार. प्रकट करने के लिए अकबर 1568 ई० में गोइंदवाल साहिब आया था। उसने गुरु साहिब के दर्शन करने से पूर्व मर्यादानुसार अन्य संगत के साथ मिलकर लंगर खाया। वह गुरु साहिब के व्यक्तित्व और लंगर प्रबंध से बहुत प्रभावित हुआ। उसने लंगर प्रबंध को चलाने के लिए कुछ गाँवों की जागीर की पेशकश की। गुरु जी ने इस जागीर को स्वीकार करने से इसलिए इंकार कर दिया कि उनके सिख लंगर के लिए बहुत दान देते हैं। अकबर की इस यात्रा के कारण गुरु अमरदास जी की प्रसिद्धि बहुत दूर-दूर तक फैल गई तथा बहुत-से लोग सिख धर्म में सम्मिलित हो गए।

प्रश्न 10.
गुरु रामदास जी द्वारा सिख धर्म के विकास के लिए किए गए छः महत्त्वपूर्ण योगदानों की चर्चा करें।
(Give the six important contributions of Guru Ram Das Ji for the development of Sikhism.
अथवा
गुरु रामदास जी का सिख धर्म को क्या योगदान था ? (What was the contribution of Guru Ram Das Ji to Sikh religion ?)
अथवा
सिख मत के विकास में गुरु रामदास जी द्वारा दिये गए योगदान का वर्णन करो। (Explain the contribution of Guru Ram Das Ji to the growth of Sikhism.)
उत्तर-
1. रामदासपुरा की स्थापना-गुरु रामदास जी की सिख पंथ को सबसे महत्त्वपूर्ण देन रामदासपुरा अथवा अमृतसर की स्थापना करना था। रामदासपुरा की स्थापना 1577 ई० में हुई। इस शहर को बसाने के लिए गुरु साहिब ने यहाँ भिन्न-भिन्न व्यवसायों से संबंध रखने वाले 52 व्यापारियों को बसाया। इन व्यापारियों ने जो बाज़ार बसाय वह ‘गुरु का बाज़ार’ नाम से प्रसिद्ध हुआ। अमृतसर की स्थापना से सिखों को उनका मक्का मिल गया। यह शीघ्र ही सिखों का सर्वाधिक प्रसिद्ध धर्म-प्रचार केंद्र बन गया।
2. मसंद प्रथा का आरंभ-गुरु रामदास जी को रामदासपुरा में अमृतसर एवं संतोखसर नामक दो सरोवरों की खुदवाई के लिए धन की आवश्यकता पड़ी। इसलिए गुरु साहिब ने अपने प्रतिनिधियों को अलग-अलग स्थानों पर भेजा ताकि वे सिख मत का प्रचार कर सकें और संगतों से धन एकत्रित कर सकें। यह संस्था मसंद प्रथा के नाम से प्रसिद्ध हुई। मसंद प्रथा के कारण ही सिख मत का दूर-दूर तक प्रचार हुआ।
3. उदासियों से समझौता-गुरु रामदास जी के समय की एक महत्त्वपूर्ण घटना उदासी तथा सिख संप्रदाय के मध्य समझौता था। एक बार उदासी मत के संस्थापक बाबा श्रीचंद जी गुरु रामदास जी के दर्शनों के लिए अमृतसर आए। वह गुरु साहिब की नम्रता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उस दिन के पश्चात् सिख मत का विरोध नहीं किया। यह समझौता सिख पंथ के विकास के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण प्रमाणित हुआ।
4. कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण कार्य-गुरु जी के अन्य महत्त्वपूर्ण कार्यों में वाणी की रचना (679 शब्द) करना था। उन्होंने चार लावों द्वारा विवाह प्रथा को प्रोत्साहित किया। गुरु साहिब ने पहले से चली आ रही संगत, पंगत और मंजी नामक संस्थाओं को जारी रखा। गुरु साहिब ने समाज में प्रचलित कुरीतियों जैसे-जाति प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह आदि का भी ज़ोरदार शब्दों में खंडन किया।
5. अकबर के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध-गुरु रामदास जी के समय में भी सिखों के मुग़ल बादशाह अकबर से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित रहे। अकबर ने गुरु रामदास जी से लाहौर में मुलाकात की थी। उसने गुरु साहिब के कहने पर पंजाब के कृषकों का एक वर्ष के लिए लगान माफ कर दिया। फलस्वरूप गुरु साहिब की ख्याति में और वृद्धि हुई।
6. उत्तराधिकारी की नियुक्ति-गुरु रामदास जी ने 1581 ई० मे गुरु अर्जन देव जी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इस कारण सिख पंथ के विकास का कार्य जारी रहा।
प्रश्न 11.
रामदासपुरा (अमृतसर) की स्थापना का सिख इतिहास में क्या महत्त्व है ?
(What is the importance of the foundation of Ramdaspura (Amritsar) in Sikh History ?)
उत्तर-
गुरु रामदास जी की सिख पंथ को सबसे महत्त्वपूर्ण देन 1577 ई० में रामदासपुरा अथवा अमृतसर की स्थापना करना था। गुरुगद्दी प्राप्त करने के पश्चात् गुरु साहिब स्वयं यहाँ आ गए थे। इस शहर को बसाने के लिए गुरु साहिब ने यहाँ भिन्न-भिन्न व्यवसायों से संबंधित 52 अन्य व्यापारियों को बसाया। इन व्यापारियों ने जो बाज़ार बसाया वह ‘गुरु का बाजार’ नाम से प्रसिद्ध हुआ। शीघ्र ही यह एक प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र बन गया। गुरु साहिब ने रामदासपुरा में दो सरोवरों अमृतसर एवं संतोखसर की खुदवाई का विचार बनाया। पहले अमृतसर सरोवर की खुदवाई का कार्य आरंभ किया गया। अमृतसर की स्थापना सिख पंथ के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। इससे सिखों को एक अलग तीर्थ स्थान मिल गया जो शीघ्र ही उनका सर्वाधिक प्रसिद्ध धर्म-प्रचार केंद्र बन गया। इसे सिखों का मक्का कहा जाने लगा। इस के अतिरिक्त यह सिखों की एकता एवं स्वतंत्रता का प्रतीक भी बन गया।

प्रश्न 12.
उदासी मत पर एक संक्षिप्त नोट लिखें। , (Write a short note on Udasi Sect.)
अथवा
उदासी प्रथा के बारे में आप क्या जानते हैं ? (What do you know about Udasi System ?)
अथवा
बाबा श्रीचंद जी पर एक संक्षिप्त नोट लिखें। (Write a brief note on Baba Sri Chand Ji.)
उत्तर-
1. बाबा श्रीचंद जी-उदासी मत की स्थापना गुरु नानक देव जी के बड़े सुपुत्र बाबा श्रीचंद जी ने की थी। यह मत संन्यास अथवा त्याग के जीवन पर बल देता था जबकि गुरु नानक देव जी गृहस्थ जीवन के पक्ष में थे। उदासी मत के शेष सभी सिद्धांत गुरु नानक देव जी के सिद्धांतों से मिलते थे। इस कारण बहुत-से सिख उदासी मत को मान्यता देने लग पड़े थे। ऐसी परिस्थितियों में यह संकट उत्पन्न हो गया था कि कहीं सिख गुरु नानक देव जी के उपदेशों को भूलकर उदासी मत न अपना लें। इस संबंध में एक ठोस और शीघ्र निर्णय लिए जाने की आवश्यकता थी।
2. गुरु अंगद देव जी-गुरु अंगद देव जी ने उदासी मत का कड़ा विरोध किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि उदासी मत के सिद्धांत सिख धर्म के सिद्धांतों से सर्वथा विपरीत हैं एवं जो सिख उदासी मत में विश्वास रखता है, वह सच्चा सिख नहीं हो सकता।
3. गुरु अमरदास जी-गुरु अमरदास जी ने सिखों को समझाया कि सिख धर्म उदासी मत से बिल्कुल अलग है। उनका कहना था कि जहाँ सिख धर्म गृहस्थ मार्ग अपनाने तथा अपनी आजीविका के लिए सच्चा श्रम करने की शिक्षा देता है, वहाँ उदासी मत अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों से भाग जाने तथा संसार को त्याग कर मुक्ति की खोज में वनों में मारे-मारे फिरने की शिक्षा देता है। गुरु साहिब के अथक प्रयत्नों से सिखों ने उदासी मत से सदैव के लिए अपने संबंध तोड़ लिए।’
4. गुरु रामदास जी-गुरु रामदास जी के समय उदासियों एवं सिखों के मध्य समझौता हुआ। एक बार उदासी मत के संस्थापक बाबा श्रीचंद जी गुरु अमरदास जी के दर्शनों के लिए अमृतसर आए। श्रीचंद जी गुरु साहिब की नम्रता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उस दिन के पश्चात् सिख मत का विरोध करना बंद कर दिया। सिखों का उदासियों से यह समझौता सिख पंथ के लिए बहुत लाभप्रद प्रमाणित हुआ। इससे एक तो सिखों और उदासियों के बीच चला आ रहा परस्पर तनाव दूर हो गया। दूसरा, उदासियों ने सिख मत का प्रचार करने में प्रशंसनीय योगदान दिया।। इससे सिख धर्म की लोकप्रियता में वृद्धि हुई।
Source Based Questions
नोट-निम्नलिखित अनुच्छेदों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उनके अंत में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए।
1
भाई लहणा जी गुरु नानक देव जी से भेंट करने से पूर्व दुर्गा माता के भक्त थे। वे प्रतिवर्ष अपने साथ भक्तों का एक जत्था लेकर ज्वालामुखी (ज़िला काँगड़ा) देवी के दर्शन के लिए जाते थे, किंतु जिस सत्य की उन्हें तलाश थी, उसकी प्राप्ति न हो सकी। एक दिन खडूर साहिब में भाई जोधा जी जो गुरु नानक देव जी के एक श्रद्धालु सिख थे, के मुख से आसा दी वार’ का पाठ सुना। यह पाठ सुनकर भाई लहणा जी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने गुरु नानक देव जी के दर्शन करने का दृढ़ निश्चय किया। आगामी वर्ष जब भाई लहणा जी अपने जत्थे को साथ लेकर ज्वालामुखी की यात्रा के लिए निकले तो वे मार्ग में करतारपुर में गुरु नानक देव जी के दर्शन के लिए रुके। वे गुरु साहिब के महान् व्यक्तित्व
और मधुर वाणी को सुनकर इतने अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने अनुभव किया कि जिस मंज़िल की उन्हें वर्षों से तलाश थी, आज वह मंज़िल उनके सामने है।
- भाई लहणा जी गुरु नानक देव जी को मिलने से पहले किस देवी के भक्त थे ?
- भाई लहणा जी ने खडूर साहिब में किस के मुख से आसा दी वार’ का पाठ सुना था ?
- ‘आसा दी वार’ का पाठ सुनकर भाई लहणा जी ने क्या फैसला किया ?
- भाई लहणा जी गुरु नानक देव जी के शिष्य क्यों बन गए ?
- भाई लहणा जी गुरु नानक देव जी को कहाँ मिले थे ?
- करतारपुर में
- ज्वालामुखी में
- कीरतपुर में
- अमृतसर में।
उत्तर-
- भाई लहणा जी गुरु नानक देव जी को मिलने से पहले देवी दुर्गा के भक्त थे।
- भाई लहणा जी ने खडूर साहिब में भाई जोधा जी के मुख से ‘आसा दी वार’ का पाठ सुना था।
- ‘आसा दी वार’ का पाठ सुनकर भाई लहणा जी ने गुरु नानक देव जी के दर्शन करने का फैसला किया।
- वह गुरु नानक देव जी के व्यक्तित्व से तथा वाणी से बहुत प्रभावित हुए।
- करतारपुर में।

2
गुरु अंगद साहिब ने गुरमुखी लिपि को लोकप्रिय बनाकर सिख पंथ के विकास की ओर प्रथम महत्त्वपूर्ण पग उठाया। यह सही है कि यह लिपि गुरु अंगद देव जी से पूर्व अस्तित्व में आ चुकी थी, परंतु इसे पढ़कर कोई भी व्यक्ति बहुत सरलता से भ्रम में पड़ सकता था। इसलिए गुरु अंगद देव जी इसके रूप में एक नया निखार लाए। अब इस लिपि को समझना सामान्य लोगों के लिए भी बहुत सरल हो गया था। सिखों के सभी धार्मिक ग्रंथों की रचना इस लिपि में हुई। इस लिपि का नाम गुरमुखी [अर्थात् गुरुओं के मुख से निकली हुई] होने के कारण यह सिखों को गुरु के प्रति अपने कर्तव्य का स्मरण दिलाती रही। इस प्रकार यह लिपि सिखों की अपनी अलग पहचान बनाए रखने में सहायक सिद्ध हुई। इस लिपि के प्रसार के कारण सिखों में तीव्रता से विद्या का प्रसार होने लगा। इसके अतिरिक्त इस लिपि के प्रचलित होने से ब्राह्मण वर्ग को कड़ा आघात पहुँचा क्योंकि वे संस्कृत को ही धर्म की भाषा समझते थे।
- किस गुरु साहिबान ने गुरमुखी लिपि का प्रचलन किया ?
- गुरमुखी लिपि से पहले कौन-सी लिपि का प्रचलन था ?
- गुरमुखी से क्या भाव है ?
- गुरमुखी लिपि का क्या महत्त्व था ?
- सिखों के सभी धार्मिक ग्रंथों की रचना ……….. लिपि में हुई। ……….
उत्तर-
- गुरु अंगद देव जी ने गुरमुखी लिपि का प्रचलन किया था।
- गुरमुखी लिपि से पहले लंडे महाजनी लिपि का प्रचलन था।
- गुरमुखी लिपि से भाव है गुरुओं के मुख से निकली हुई।
- इसके प्रचार के कारण ब्राह्मण वर्ग को करारी चोट पहुँची क्योंकि वे केवल संस्कृत को ही पवित्र भाषा मानते
- गुरमुखी।
3
गुरु अमरदास जी का सिख पंथ के विकास की ओर पहला पग गोइंदवाल साहिब में एक बाऊली का निर्माण करना था। इस बाऊली का निर्माण कार्य 1552 ई० में आरंभ किया गया था और यह 1559 ई० में संपूर्ण हुआ था। इस बाऊली के निर्माण के पीछे गुरु साहिब के दो उद्देश्य थे। पहला, वह सिखों को एक अलग तीर्थ स्थान देना चाहते थे ताकि उन्हें हिंदू धर्म से अलग किया जा सके। दूसरा, वह वहाँ के लोगों की पानी के संबंध में कठिनाई को दूर करना चाहते थे। इस बाऊली तक पहुँचने के लिए 84 सीढ़ियाँ बनाई गई थीं। बाऊली का निर्माण कार्य पूर्ण होने पर गुरु जी ने यह घोषणा की कि जो यात्री प्रत्येक सीढ़ी पर शुद्ध हृदय से जपुजी साहिब का पाठ करेगा तथा पाठ के पश्चात् बाऊली में स्नान करेगा वह 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाएगा। बाऊली का निर्माण सिख पंथ के विकास के लिए एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण कार्य प्रमाणित हुआ।
- गोइंदवाल साहिब में बाऊली का निर्माण किस गुरु साहिब ने करवाया था ?
- गोइंदवाल साहिब में बाऊली का निर्माण कार्य कब आरंभ हुआ ?
- 1552 ई०
- 1559 ई०
- 1562 ई०
- 1569 ई०
- गोइंदवाल साहिब में बाऊली के निर्माण कार्य को कुल कितना समय लगा ?
- गोइंदवाल साहिब की बाऊली तक पहुँचने के लिए कुल कितनी सीढ़ियों का निर्माण किया गया ?
- बाऊली का निर्माण सिख पंथ के लिए कैसे महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुआ ?
उत्तर-
- गोइंदवाल साहिब में बाऊली का निर्माण गुरु अमरदास जी ने करवाया था।
- 1552 ई०।
- गोइंदवाल साहिब में बाऊली के निर्माण को कुल 7 वर्ष लगे।
- गोइंदवाल साहिब की बाऊली तक पहुँचने के लिए कुल 84 सीढ़ियाँ बनवाई गईं।
- इस कारण सिख धर्म को एक नया उत्साह मिला।

4
मंजी प्रथा की स्थापना गुरु अमरदास जी के सबसे महत्त्वपूर्ण कार्यों में से एक थी। गुरु अमरदास जी के समय सिखों की संख्या में भारी वृद्धि हुई थी। इसलिए गुरु साहिब के लिए प्रत्येक सिख तक पहुँच पाना संभव नहीं था। उन्होंने अपने उपदेश दूर-दूर के क्षेत्रों में रहने वाले सिखों तक पहुँचाने के लिए 22 मंजियों की स्थापना की। यहाँ यह बात स्मरणीय है कि गुरु जी ने इन मंजियों की स्थापना एक ही समय पर नहीं की थी अपितु यह क्रम उनके समस्त गुरुकाल के दौरान चलता रहा। प्रत्येक मंजी के मुखिया को मंजीदार कहते थे। मंजीदार का पद केवल बहुत ही पवित्र सिख को दिया जाता था। मंजीदार का प्रचार क्षेत्र किसी विशेष प्रदेश तक सीमित नहीं था। वह अपनी इच्छानुसार अपने प्रचार हेतु किसी भी स्थान पर जा सकते थे। ये मंजीदार अधिक-से-अधिक लोगों को सिखं धर्म में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करते थे तथा सिखों से धन एकत्र करके गुरु साहिब तक पहुँचाते थे।
- मंजी प्रथा की स्थापना किस गुरु साहिब ने की थी ?
- कुल कितनी मंजियों की स्थापना की गई थी ?
- मंजी का मुखिया कौन होता था ?
- मंजीदार का कोई एक मुख्य कार्य लिखें।
- मंजीदार का प्रचार क्षेत्र किसी विशेष ………. तक सीमित नहीं था।
उत्तर-
- मंजी प्रथा की स्थापना गुरु अमरदास जी ने की थी।
- कुल 22 मंजियों की स्थापना की गई थी।
- मंजी का मुखिया मंजीदार होता था।
- वे सिख धर्म का प्रचार करते थे।
- प्रदेश।
5
गुरु रामदास जी की सिख पंथ को सबसे महत्त्वपूर्ण देन रामदासपुरा अथवा अमृतसर की स्थापना करना था। गुरुगद्दी प्राप्त करने के पश्चात् गुरु साहिब स्वयं यहाँ आ गए थे। उन्होंने 1577 ई० में रामदासपुरा की स्थापना की। इस शहर को बसाने के लिए गुरु साहिब ने यहाँ भिन्न-भिन्न व्यवसायों से संबंधित 52 अन्य व्यापारियों को बसाया। इन व्यापारियों ने जो बाज़ार बसाया वह ‘गुरु का बाज़ार’ नाम से प्रसिद्ध हुआ। शीघ्र ही यह एक प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र बन गया। गुरु साहिब ने रामदासपुरा में दो सरोवरों अमृतसर एवं संतोखसर की खुदवाई का विचार बनाया। पहले अमृतसर सरोवर की खुदाई का कार्य आरंभ किया गया। इस कार्य की देखभाल के लिए बाबा बुड्डा जी को नियुक्त किया गया। बाद में अमृत सरोवर के नाम पर रामदासपुरा का नाम अमृतसर पड़ गया। अमृतसर की स्थापना सिख पंथ के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। इससे सिखों को एक अलग तीर्थ स्थान मिल गया जो शीघ्र ही उनका सर्वाधिक प्रसिद्ध धर्म-प्रचार केंद्र बन गया।
- रामदासपुरा की स्थापना किस गुरु साहिब ने की थी ?
- रामदासपुरा के पश्चात् इसे किस नाम से जाना जाने लगा ?
- रामदासपुरा में व्यापारियों के लिए बनाए गए बाज़ार का नाम क्या था ?
- रामदासपुरा की स्थापना का क्या महत्त्व था ?
- रामदासपुरा की स्थापना कब की गयी थी ?
- 1571 ई०
- 1573 ई०
- 1575 ई०
- 1577 ई०।
उत्तर-
- रामदासपुरा की स्थापना गुरु रामदास जी ने की थी।
- रामदासपुरा के पश्चात् इसे अमृतसर के नाम से जाना जाने लगा।
- रामदासपुरा में व्यापारियों के लिए बनाए गए बाज़ार का नाम ‘गुरु का बाज़ार’ था।
- इसके कारण सिखों को उनका सबसे पवित्र तीर्थ स्थान मिला।
- 1577 ई०।
![]()

![]()


![]()
![]()
![]()
![]()
![]()