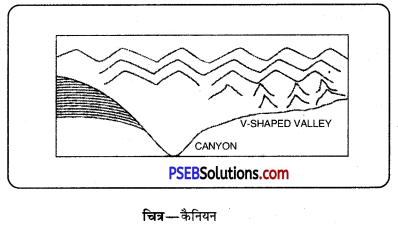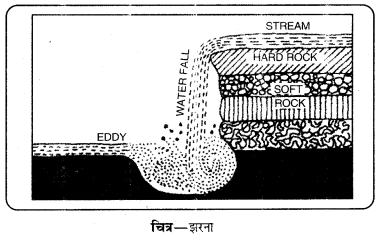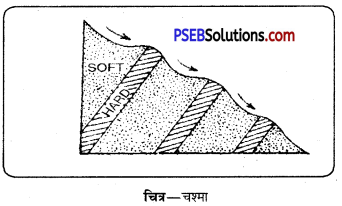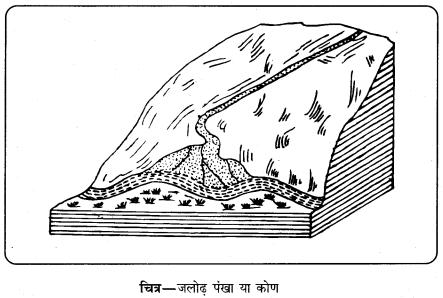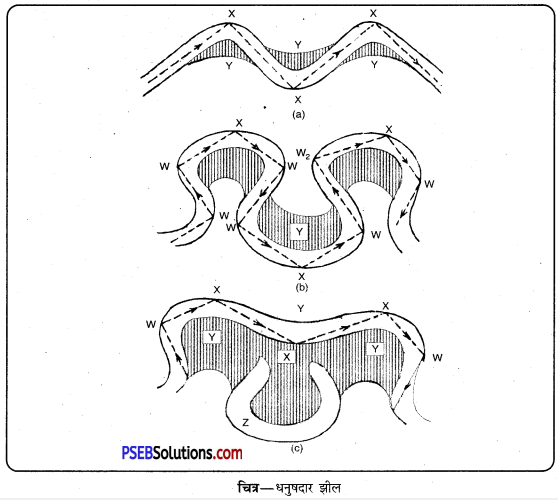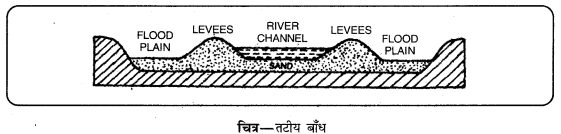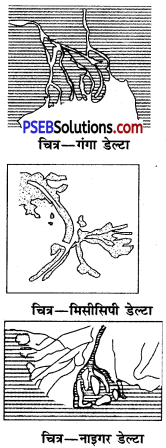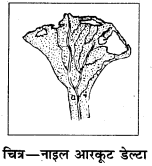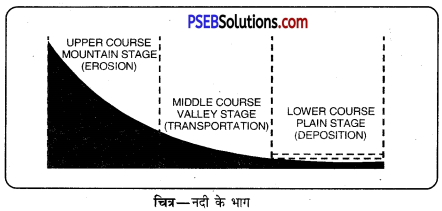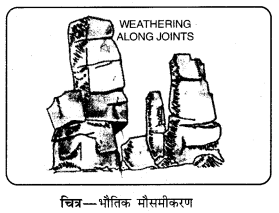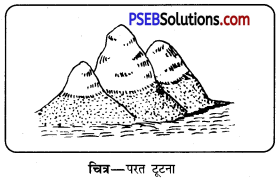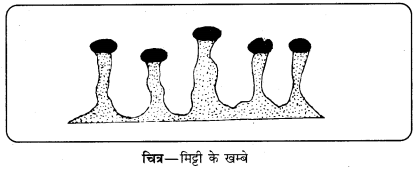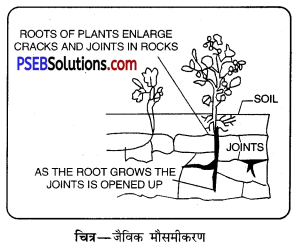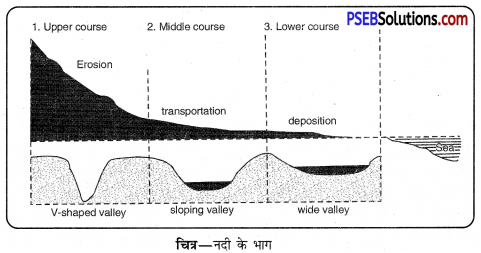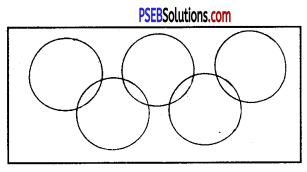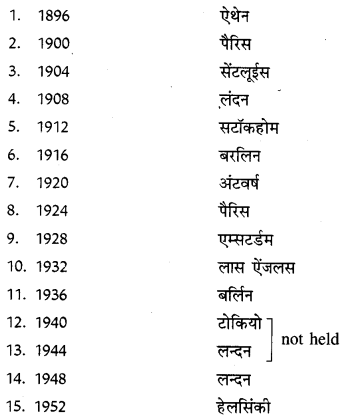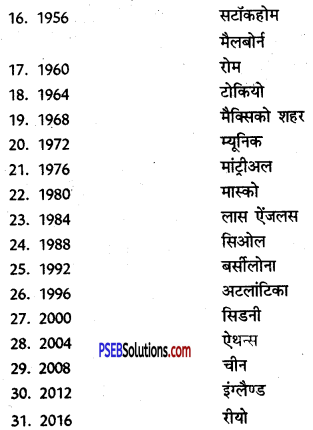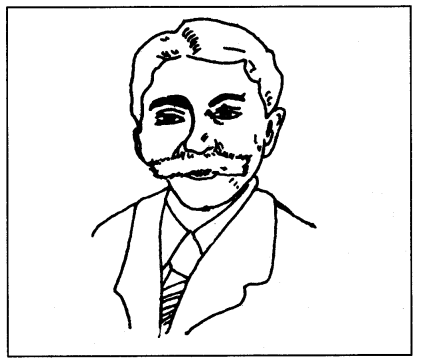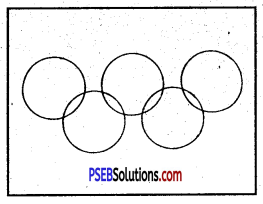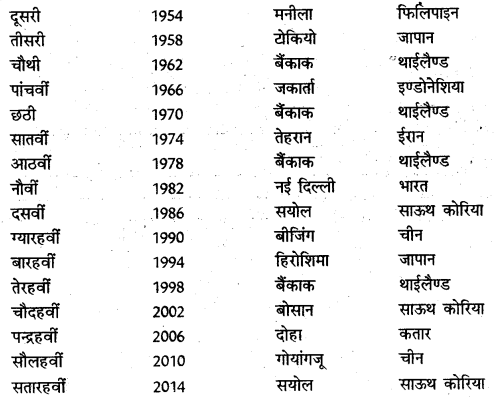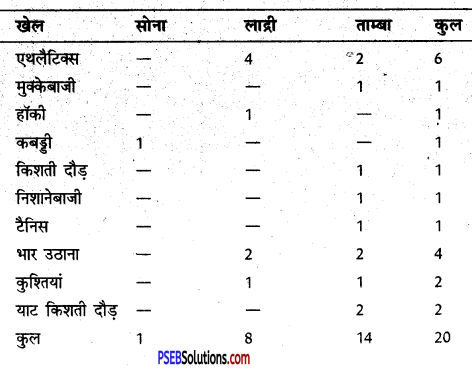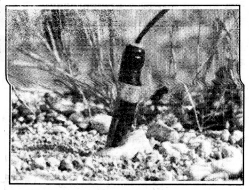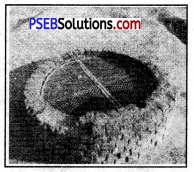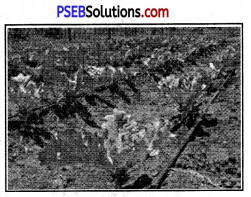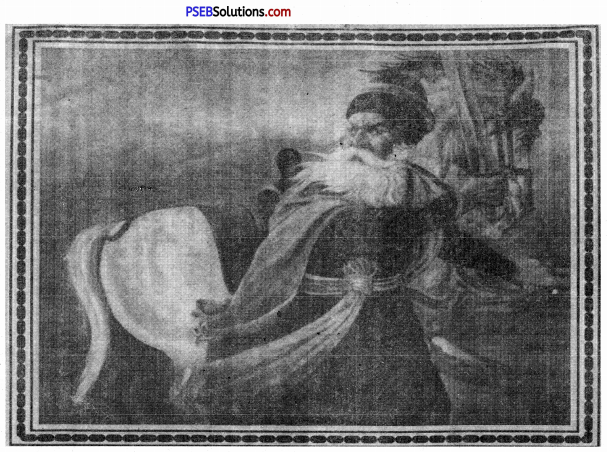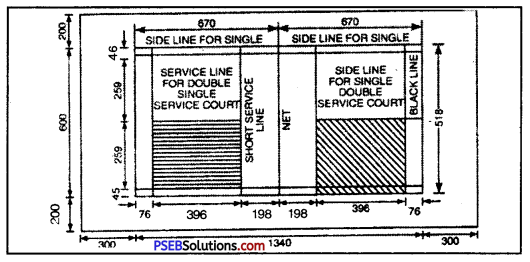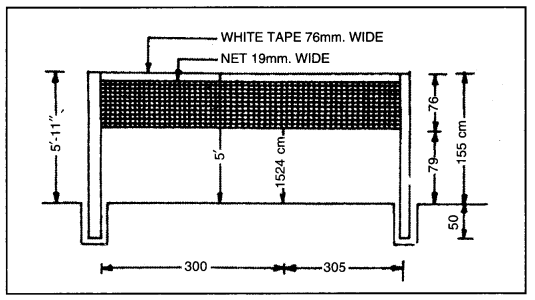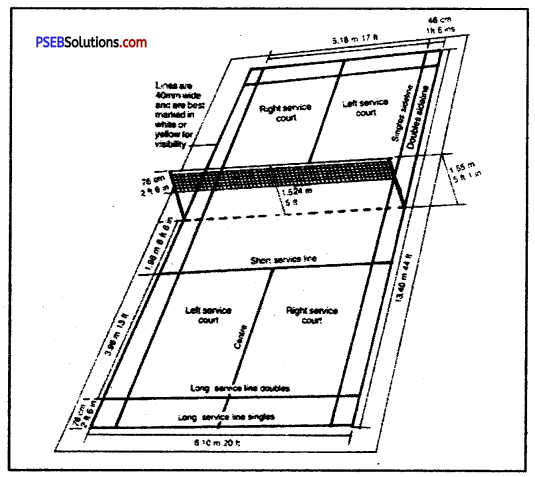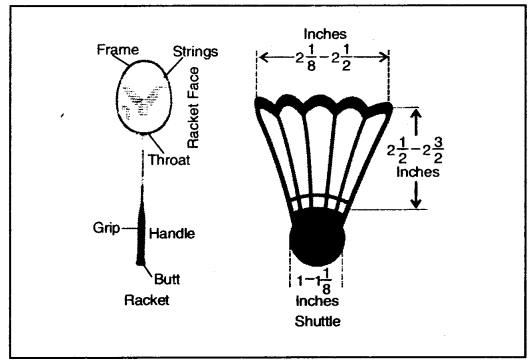Punjab State Board PSEB 12th Class Political Science Book Solutions Chapter 1 राजनीतिक व्यवस्था Textbook Exercise Questions and Answers.
PSEB Solutions for Class 12 Political Science Chapter 1 राजनीतिक व्यवस्था
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-
प्रश्न 1.
राजनीतिक व प्रणाली शब्द का अलग-अलग अर्थ स्पष्ट करते हुए राजनीतिक प्रणाली की कोई र विशेषताएं बताएं।
(Describe the word Political and System separately and also write any three features of Political System.)
अथवा राजनैतिक प्रणाली की परिभाषा लिखो। इसकी मुख्य विशेषताओं का विस्तार सहित वर्णन करो। (Define Political System. Write main characteristics of Political System.)
उत्तर-
आलमण्ड (Almond) तथा पॉवेल (Powell) के अनुसार, तुलनात्मक राजनीति से सम्बन्धित प्रकाशित पुस्तकों में राजनीतिक व्यवस्था (Political System) शब्दावली का अधिक-से-अधिक प्रयोग किया जा रहा है। पुरानी पाठ्य-पुस्तकें आमतौर पर राजनीतिक व्यवस्था के लिए ‘सरकार’, ‘राष्ट्र’ या ‘राज्य’ जैसे शब्दों का प्रयोग करती थीं। यह नवीन शब्दावली उस नए दृष्टिकोण का प्रतिबिम्ब है जो राजनीतिक व्यवस्था को एक नए ढंग से देखते हैं। आलमण्ड तथा पॉवेल आदि लेखकों का विचार है कि प्राचीन युग में प्रयोग होने वाले ये शब्द वैधानिक और संस्थात्मक अर्थों (Legal and Institutional Meanings) द्वारा सीमित है। आलमण्ड तथा पॉवेल का कहना है कि यदि वास्तव में राजनीति विज्ञान को प्रभावशाली बनाना है तो हमें विश्लेषण के अधिक व्यापक ढांचे की आवश्यकता है और वह ढांचा व्यवस्था विश्लेषण (System Analysis) का है। आलमण्ड तथा पॉवेल ने लिखा है, “राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा अधिक लोकप्रिय होती जा रही है क्योंकि यह किसी भी समाज के राजनीतिक क्रियाओं के सम्पूर्ण क्षेत्र की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती है।”
राजनीतिक व्यवस्था का अर्थ (Meaning of the Political System)-राजनीतिक व्यवस्था शब्द के दो भाग हैं-राजनीति तथा व्यवस्था। इन दोनों के अर्थ को समझने के बाद ही राजनीतिक व्यवस्था अथवा प्रणाली का अर्थ समझा जा सकता है। – 1. राजनीतिक (Political)-राजनीतिक शब्द सत्ता अथवा शक्ति का सूचक है। किसी भी समुदाय या संघ को राजनीतिक उस समय कहा ज सकता है जबकि उसकी आज्ञा का पालन प्रशासकीय कर्मचारी वर्ग द्वारा शारीरिक बल प्रयोग के भय से करवाया जात है । अरस्तु ने राजनीतिक समुदाय को अत्यधिक प्रभुत्व-समन्न तथा अन्तर्भावी र गठन’ (The most sovereign and inclusive association) परिभाषित किया है।” अरस्तु के मतानुसार, “राजनीतिक समुदाय के पास सर्वोच्च शक्ति होती है जो इसको अन्य समुदायों अथवा संघों से अलग करती है। अरस्तु के बाद अनेक विद्वानों ने इस बात को स्वीकार किया है कि राजनीतिक सम्बन्धों में सत्ता, शासन और शक्ति किसी-न-किसी प्रकार । निहित है।
आलमण्ड तथा पॉवेल (Almond and Powell) ने राजनीतिक समुदाय की इस शक्ति को कानूनी शारीरिक बलात् शक्ति (Legitimate Physical Coercive Powers) का नाम दिया है।
मैक्स वैबर (Max Webber) के अनुसार, “किसी भी समुदाय को उस समय राजनीतक माना जा सकतज उसके आदेशों को एक निश्चित भू-क्षेत्र में लगातार शक्ति के प्रयोग अथवा शक्ति-प्रयोग की धमकी द्वारा मनवाया । सकता हो।”
डेविड ईस्टन (David Easton) ने राजनीतिक जीवन को इस प्रकार परिभाषित किया है- “यह अन्तक्रियाओं का समूह अथवा प्रणाली है जो इस तथ्य से अलंकृत है कि यह एक समाज के लिए सत्तात्मक मूल्य निर्धारण से कम या अधिक सम्बन्धित है।” (“A set or system of interactions defined by the fact that they are more or less directly related to the authoritative allocation of values for a society.”) लॉसवैल तथा कॉप्लान (Lasswell and Kaplan) ने ‘घोर-हानि’ (Severe Deprivation) की बात की है। राबर्ट ए० डाहल (Robert A. Dahl) ने ‘शक्ति , शासन तथा सत्ता’ (Power, Rule and Authority) का वर्णन किया है।
विभिन्न विद्वानों के विचारों के आधार पर हम कह सकते हैं कि राजनीति का सम्बन्ध ‘शक्ति’, ‘शासन’ तथा ‘सत्ता’ से होता है और जिस समुदाय के पास ये गुण होते हैं उसे राजनीतिक समुदाय कहा जाता है।
2. व्यवस्था या प्रणाली (System)—व्यवस्था (System) शब्द का प्रयोग अन्तक्रियाओं (Interaction) के समूह ) का संकेत करने के लिए किया जाता है।
ऑक्सफोर्ड शब्दकोष (Concise Oxford Dictionary) के अनुसार, “प्रणाली एक पूर्ण समाप्ति है, सम्बद्ध वस्तुओं अथवा अंशों का समूह है, भौतिक या अभौतिक वस्तुओं का संगठित समूह है।” (A system is a complex whole, a set of connected things or parts, organised body of material or immaterial things.”)
वान बर्टलैंफी (Von Bertalanffy) के अनुसार, “प्रणाली (System) पारस्परिक अन्तक्रिया (Interaction) में बन्धे हुए तत्त्वों का समूह है।” (“System is a set of elements standing in interaction.”)
ए० हाल एवं आर० फैगन (A. Hall and R. Fagen) के अनुसार, “प्रणाली” पात्रों (Objects), पात्रों में पारस्परिक सम्बन्धों तथा पात्रों के लक्षणों के पारस्परिक सम्बन्धों का समूह है।” (“System is a set of objects together with relations between the objects and between their attitudes.”)
कालिन चैरे (Colin Cheray) के अनुसार, “प्रणाली” कई अंशों से मिलकर बनी एक समष्टि (Whole) कई लक्षणों का समूह है।” (“System is a whole which is compounded of many parts-an ensemble of attitudes.”)
आलमण्ड तथा पॉवेल (Almond and Powell) के अनुसार, “एक व्यवस्था से अभिप्राय भागों (Parts) की परस्पर निर्भरता और उसके तथा उसके वातावरण के बीच किसी प्रकार की सीमा से है।” (A system implies interdependence of parts of boundary of some kind between it and its environment.”)
विभिन्न विद्वानों की परिभाषाओं की विवेचना से स्पष्ट है कि व्यवस्था (System) एक पूर्ण इकाई होती है, जिसके कई भाग होते हैं और ये भाग एक-दूसरे पर निर्भर करते हैं और एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं। उदाहरणस्वरूप मानव शरीर एक व्यवस्था है। मानव शरीर के अनेक अंग हैं और ये सभी अंग अथवा भाग एक-दूसरे पर निर्भर करते हैं तथा एक-दूसरे को और सम्पूर्ण मानव शरीर को भी प्रभावित करते हैं। ___ एक व्यवस्था के अन्दर कुछ आधारभूत विशेषताएं होती हैं जैसे कि एकता, नियमितता, सम्पूर्णता, संगठन, सम्बद्धता (Coherence), संयुक्तता (Connection) तथा अंशों अथवा भागों का अन्योन्याश्रय (Interdependence of parts)।
इस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था उन अन्योन्याश्रित सम्बन्धों के समूह को कहा जा सकता है जिसके संचालन में सत्ता या शक्ति का भी हाथ है।
व्यवस्था में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं-
- व्यवस्था भिन्न-भिन्न अंगों या हिस्सों के जोड़ों से बनती है।
- व्यवस्था के भिन्न-भिन्न अंगों में परस्पर निर्भरता होती है।
- व्यवस्था के अंगों में एक-दूसरे को प्रभावित करने की समर्थता होती है।
- व्यवस्था की अपनी सीमाएं होती हैं।
- व्यवस्था में उप-व्यवस्थाएं (Sub-System) भी पाई जाती हैं।
- प्रत्येक व्यवस्था में सम्पूर्णता का गुण होता है।
- प्रत्येक व्यवस्था में एक इकाई के रूप में कार्य करने की योग्यता होती है।
![]()
प्रश्न 2.
राजनीतिक प्रणाली की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। (Describe the main characteristics of Political System.)
अथवा
आलमण्ड के अनुसार राजनीतिक प्रणाली की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। (Describe the characteristics of Political System according to Almond.)
अथवा
राजनीतिक प्रणाली की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या करें। (Explain main characteristics of Political System.)
उत्तर-
राजनीतिक व्यवस्था की विभिन्न परिभाषाओं से राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताओं का पता चलता है। आलमण्ड के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं अग्रलिखित हैं-
1. मानवीय सम्बन्ध (Human Relations)–जिस प्रकार राज्य के लिए जनसंख्या का होना अनिवार्य है, उसी प्रकार राजनीतिक व्यवस्था के लिए मनुष्यों के परस्पर स्थायी सम्बन्धों का होना आवश्यक है। बिना मानवीय सम्बन्धों के राजनीतिक व्यवस्था नहीं हो सकती। परन्तु सभी प्रकार के मानवीय सम्बन्धों को राजनीतिक व्यवस्था का अंग नहीं माना जा सकता। केवल उन्हीं मानवीय सम्बन्धों को राजनीतिक व्यवस्था का अंग माना जाता है जो राजनीतिक व्यवस्था की कार्यशीलता को किसी-न-किसी तरह प्रभावित करते हों।
2. औचित्यपूर्ण शक्ति का प्रयोग (Use of Legitimate Force)-राजनीतिक व्यवस्था का सबसे महत्त्वपूर्ण गुण शारीरिक दण्ड देने की शक्ति के प्रयोग करने के अधिकार के अस्तित्व को स्वीकार किया जाना है। इस गुण के आधार पर ही राजनीतिक व्यवस्था को अन्य व्यवस्थाओं से अलग किया जाता है। जिस प्रकार प्रभुसत्ता राज्य का अनिवार्य तत्त्व है और प्रभुसत्ता के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी तरह औचित्यपूर्ण शारीरिक दबाव शक्ति (Legitimate Physical Coercive Power) के बिना राजनीतिक व्यवस्था का अस्तित्व सम्भव नहीं है। प्रत्येक समाज में शान्ति और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए तथा अपराधियों को दण्ड देने के लिए शक्ति का प्रयोग किया जाता है, परन्तु शक्ति का प्रयोग औचित्यपूर्ण होना चाहिए। औचित्यपूर्ण शक्ति के द्वारा ही राजनीतिक व्यवस्था के सभी कार्य चलते हैं।
3. व्यापकता (Comprehensiveness)-आलमण्ड के विचारानुसार, व्यापकता का अर्थ है कि राजनीतिक व्यवस्था में निवेश तथा निर्गत (Inputs and Outputs) की वे सभी प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं जो शक्ति के प्रयोग या शक्ति प्रयोग की धमकी को किसी भी रूप में प्रभावित करती हैं। अन्य शब्दों में आलमण्ड के मतानुसार राजनीतिक व्यवस्था में केवल संवैधानिक अथवा कानूनी ढांचों जैसे कि-विधानमण्डल, न्यायपालिका, नौकरशाही आदि को ही सम्मिलित नहीं किया जाता बल्कि इसमें अनौपचारिक (Informal) संस्थाओं जैसे कि राजनीतिक दल, दबाव समूह, निर्वाचक मण्डल आदि के साथ-साथ सभी प्रकार के राजनीतिक ढांचों के राजनीतिक पहलुओं को भी शामिल किया जाता है।
4. उप-व्यवस्थाओं का अस्तित्व (Existence of Sub-System)-राजनीतिक व्यवस्था में कई उप-व्यवस्थाएं भी पाई जाती हैं, जिनके सामूहिक रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहा जाता है। इन उप-व्यवस्थाओं में परस्पर निर्भरता होती है तथा वे एक-दूसरे की कार्यविधि को प्रभावित करती हैं। जैसे-विधानपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, राजनीतिक दल, प्रशासनिक विभाग तथा दबाव समूह इत्यादि राजनीतिक व्यवस्था की उप-व्यवस्थाएं हैं। इन उप-व्यवस्थाओं की कार्यशीलता से राजनीतिक व्यवस्था की कार्यशीलता प्रभावित होती है।
5. अन्तक्रिया (Interaction)-राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों अथवा इकाइयों में अन्तक्रिया हमेशा चलती रहती है। राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों में व्यक्तिगत अथवा विभिन्न समूहों के रूप में सम्पर्क बना रहता है तथा वे एक-दूसरे को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। इकाइयों में अन्तक्रिया न केवल निरन्तर होती है बल्कि बहुपक्षीय होती है।
6. अन्तर्निर्भरता (Interdependence) अन्तर्निर्भरता राजनीतिक व्यवस्था का महत्त्वपूर्ण गुण है। आलमण्ड (Almond) के मतानुसार राजनीतिक व्यवस्था में अनेक उप-व्यवस्थाओं (Sub-systems) के राजनीतिक पहलू भी सम्मिलित हैं। उसके विचारानुसार राजनीतिक व्यवस्था की जब एक उप-व्यवस्था में परिवर्तन आता है तो इसका प्रभाव अन्य व्यवस्थाओं पर भी पड़ता है। उदाहरणस्वरूप आधुनिक युग में संचार के साधनों का बहुत विकास हुआ है। संचार के साधनों के विकास के साथ चुनाव विधि, चुनाव व्यवहार, राजनीतिक दलों की विशेषताओं, विधानमण्डल तथा कार्यपालिका की रचना तथा कार्यों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। इसी प्रकार श्रमिक वर्ग को मताधिकार देने में राजनीतिक दलों, दबाव समूहों, सरकारों के वैधानिक तथा कार्यपालिका अंगों पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है।
7. सीमाओं की विद्यमानता (Existence of Boundaries)-सीमाओं की विद्यमानता राजनीतिक व्यवस्था का महत्त्वपूर्ण गुण है। सीमाओं की विद्यमानता का अर्थ है कि प्रत्येक व्यवस्था किसी एक स्थान से शुरू होती है और किसी दूसरे स्थान पर समाप्त होती है। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था की कुछ सीमाएं होती हैं जो उसको अन्य व्यवस्थाओं से अलग करती हैं। राजनीतिक व्यवस्था की सीमाएं राज्य की तरह क्षेत्रीय सीमाएं नहीं होतीं। ये मानवीय सम्बन्धों तथा क्रियाओं की सीमाएं होती हैं। सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं की सीमाएं सदैव एक-जैसी अथवा निश्चित नहीं होतीं। प्राचीन तथा परम्परागत समाज में राजनीतिक व्यवस्था की सीमाएं इतनी स्पष्ट नहीं होती जितनी कि आधुनिक समाज में। जैसे-जैसे किसी व्यवस्था का आधुनिकीकरण तथा विकास होता है वैसे ही कार्यों के विशेषीकरण के कारण ये सीमाएं स्पष्ट होती जाती हैं। राजनीतिक व्यवस्था की सीमाओं में समयानुसार परिवर्तन आते रहते हैं। कई बार राजनीतिक व्यवस्था की सीमाएं किसी घटना के कारण बढ़ भी सकती हैं और कम भी हो सकती हैं।
8. खुली व्यवस्था (Open System)-राजनीतिक व्यवस्था एक खुली व्यवस्था होती है, “जिस कारण समय, वातावरण और परिस्थितियों के अनुसार उसमें परिवर्तन होता रहता है। यदि राजनीतिक व्यवस्था बन्द व्यवस्था हो तो उस पर परिस्थितियों का प्रभाव ही न पड़े और ऐसी व्यवस्था में राजनीतिक व्यवस्था टूट सकती है।”
9. अनुकूलता (Adaptability)-राजनीतिक व्यवस्था की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता अनुकूलता है। राजनीतिक व्यवस्था समय और परिस्थितियों के अनुसार अपने आपको परिवर्तित करने की विशेषता रखती है। उदाहरणस्वरूप भारत की राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप शान्ति के समय कुछ और होता है और संकटकाल में उसका स्वरूप बदल जाता है और संकटकाल समाप्त होने के बाद फिर परिवर्तित हो जाता है। वही राजनीतिक व्यवस्था स्थायी रह पाती है जो समय और परिस्थितियों के अनुसार बदल जाती है।
10. वातावरण (Environment) किसी भी व्यवस्था पर उसके वातावरण का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक तथा आवश्यक है। वातावरण से तात्पर्य है वे परिस्थितियां जो उसे चारों ओर से घेरे हुए हों। समाज के वातावरण या परिस्थितियों का राजनीतिक प्रणाली पर प्रभाव पड़ता है और उसे हम सामान्य रूप से राजनीतिक प्रणाली का वातावरण भी कह सकते हैं । व्यक्ति अपने समाज की आर्थिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक प्रवृत्तियों से बचे रहते हैं और इस प्रकार उनका राजनीतिक प्रणाली पर प्रभाव पड़ता है। समाज में स्थित सभी समुदाय या संस्थाएं कभी-न-कभी, किसी-न-किसी रूप में राजनीतिक प्रणाली के वातावरण में रहती हैं और कभी-कभी यह उसका अंग भी बन जाती हैं। जैसे कि कोई मजदूर संघ वैसे तो राजनीतिक प्रणाली का वातावरण है, परन्तु जब वे सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन करते हैं या सरकार पर कोई कानून बनाने के लिए जोर देते हैं तो वे राजनीतिक प्रणाली का अंग भी बन जाते हैं।
![]()
प्रश्न 3.
राजनीतिक प्रणाली के निकास कार्य लिखें। (Describe the output functions of Political System.)
अथवा
राजनीतिक प्रणाली के निवेश और निकास कार्यों का वर्णन करो।
(Write input and output functions of Political System.)
अथवा
राजनीतिक प्रणाली का अर्थ बताते हुए इसके निवेश कार्यों की व्याख्या करें।
(Describe the meaning of ‘Political System’ and also explain its ‘Input Functions’.)
उत्तर-
राजनीतिक प्रणाली की परिभाषा-इसके लिए प्रश्न नं० 1 देखें।
राजनीतिक प्रणाली के कार्य-आलमण्ड ने राजनीतिक व्यवस्था के दो प्रकार के कार्यों का वर्णन किया हैनिवेश कार्य (Input Functions) तथा निर्गत कार्य (Output Functions)।
(क) निवेश कार्य (Input Functions)-निवेश कार्य गैर-सरकारी उप-प्रणालियों, समाज तथा सामान्य वातावरण द्वारा पूरे किए जाते हैं। जैसे-दल, दबाव समूह, समाचार-पत्र आदि।
आलमण्ड ने राजनीतिक व्यवस्था के चार निवेश कार्य बतलाए हैं – (1) राजनीतिक समाजीकरण तथा भर्ती, (2) हित स्पष्टीकरण, (3) हित समूहीकरण, (4) राजनीतिक संचारण।
1. राजनीतिक समाजीकरण तथा भर्ती (Political Socialisation and Recruitment) आरम्भ में बच्चे राजनीति से अनभिज्ञ होते हैं और उसमें रुचि भी नहीं लेते परन्तु जैसे-जैसे वे बड़े होते जाते हैं उनके मन में भी धीरे-धीरे राजनीतिक वृत्तियां बैठती जाती हैं। वे राजनीति में भाग लेना आरम्भ करते हैं और अपनी भूमिका निभानी आरम्भ करते हैं। इसे ही राजनीतिक समाजीकरण कहते हैं।
आलमण्ड व पॉवेल के अनुसार, राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृतियां (Political Cultures) स्थिर रखी जाती हैं अथवा उनको परिवर्तित किया जाता है। इस प्रकार के सम्पादन के माध्यम से पृथक्-पृथक् व्यक्तियों को राजनीतिक संस्कृति में प्रशिक्षित किया जाता है तथा राजनीतिक उद्देश्य की ओर उनके उन्मुखीकरण (Orientations) निर्धारित किए जाते हैं। राजनीति संस्कृति के ढांचे में परिवर्तन भी राजनीतिक समाजीकरण के माध्यम से आते हैं। अतः राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया का उपयोग, परिवर्तन लाने अथवा यथास्थिति बनाए रखने, दोनों ही के लिए हो सकता है। यह प्रक्रिया निरन्तर चलती रहती है। कभी बन्द नहीं होती। राजनीतिक दल, हितसमूह व दबाव-समूह आदि राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा अधिक-से-अधिक लोगों को अपनी मान्यताओं के प्रति जागरूक कर, लोगों को इनकी ओर आकर्षित करते हैं। लोकतन्त्रात्मक व्यवस्थाओं में राजनीतिक समाजीकरण का महत्त्व और भी अधिक होता है क्योंकि राजनीतिक दलों का सफल होना अथवा न होना इसी पर निर्भर करता है।
राजनीतिक व्यवस्था में समाजीकरण के साथ-साथ भर्ती का काम भी चलता रहता है। पुरानी भूमिकाएं बदलती रहती हैं और उनका स्थान नई भूमिकाएं लेती रहती हैं। पदाधिकारी बदल दिए जाते हैं, मर जाते हैं और उनका स्थान स्वाभाविक रूप से नए व्यक्ति ले लेते हैं। आलमण्ड व पॉवेल के अनुसार, “राजनीतिक भर्ती से अभिप्राय उस कार्य से है जिसके माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था की भूमिकाओं की पूर्ति की जाती है।” (“We use the term political recruitment to refer to the function by means of which the rolls of political system are filled.”) राजनीतिक भर्ती सामान्य आधार पर भी हो सकती है और विशिष्ट आधार पर भी। पदाधिकारियों का चुनाव जब योग्यता के आधार पर किया जाता है तो उसे सामान्य आधार पर ही हुई भर्ती कहा जाता है। जब कोई भर्ती किसी विशेष वर्ग या कबीले या दल से की जाती है तो विशिष्ट आधार पर हुई भर्ती कही जाती है।
2. हित स्पष्टीकरण (Interest Articulation) अपने-अपने हितों की रक्षा करने के लिए प्रत्येक राजनीतिक प्रणाली के सदस्य अपनी प्रणाली की कुछ मांगें पेश किया करते हैं। जिस तरीके से इन मांगों को सही रूप प्रदान किया जाता है तथा जिस प्रकार से ये मांगें प्रणाली के निर्णयकर्ताओं को प्रस्तुत की जाती हैं उसे हित स्पष्टीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। आलमण्ड व पॉवेल के अनुसार, पृथक्-पृथक् व्यक्तियों तथा समूहों द्वारा राजनीतिक निर्णयकर्ताओं से मांग करने की प्रक्रिया को हम हित स्पष्टीकरण कहते हैं।” (“The process by which individuals and groups make demands upon the political decision makers we call interest articulation.”) राजनीतिक व्यवस्था में जिन अधिकारियों के पास नीति निर्माण व निर्णय लेने का अधिकार होता है, उनके सामने विभिन्न व्यक्ति तथा समूह अपनी मांगें पेश करते हैं अर्थात् अपने हित का स्पष्टीकरण करते हैं। राजनीतिक व्यवस्था में हित स्पष्टीकरण एक महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया होती है क्योंकि समाज के अन्तर्गत जब तक समूह या संघ अपने हित को स्पष्ट नहीं कर पाते, तब तक उनके हित की पूर्ति के लिए कानून या नीति निर्माण करना सम्भव नहीं। यदि समूह या संघ को अपने हित का स्पष्टीकरण करने का अवसर नहीं दिया जाता तो उसका परिणाम हिंसात्मक कार्यविधियां होता है। हित स्पष्टीकरण के कई साधन हैं। लिखित आवेदन-पत्रों, सुझावों, वक्तव्यों और कई बार प्रदर्शनियों द्वारा यह कार्य होता है। मजदूर संघ या छात्र संघ आदि हड़ताल भी करते हैं और कई बार हिंसात्मक तरीके भी अपनाते हैं। हित स्पष्टीकरण के समुचित एवं स्वस्थ साधन वर्तमान विशेषतः प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाओं की विशेषता होती है।
3. हित समूहीकरण (Interest Aggregration)-विभिन्न संघों के हितों की पूर्ति के लिए अलग-अलग कानून या नीति का निर्माण नहीं किया जा सकता। विभिन्न संघों या समूहों के हितों को इकट्ठा करके उनकी पूर्ति के लिए एक सामान्य नीति निर्धारित की जाती है। विभिन्न हितों को इकट्ठा करने की क्रिया को ही हित समूहीकरण कहा जाता है। आलमण्ड व पॉवेल के शब्दों में, “मांगों को सामान्य नीति स्थानापन्न (विकल्प) में परिवर्तित करने के प्रकार्य को हित समूहीकरण कहा जाता है।” (“The function of converting demands into general policy alternatives is called interest aggregation.”) यह प्रकार्य दो प्रकार से सम्पादित हो सकता है। प्रथम, विभिन्न हितों को संयुक्त और समायोजित करके तथा द्वितीय, एक देश नीति के प्रतिमान में निष्ठा रखने वाले व्यक्तियों की राजनीतिक भर्ती द्वारा। यह प्रकार्य राजनीतिक व्यवस्था में नहीं बल्कि सभी कार्यों में पाया जाता है। मानव अपने विभिन्न हितों को इकट्ठा करके एक बात कहता है। हित-समूह अपने विभिन्न उपसमूहों या मांगों का समूहीकरण करके अपनी मांग रखते हैं। राजनीतिक दल विभिन्न समुदायों या संघों की मांगों को ध्यान में रखकर अपना कार्यक्रम निर्धारित करते हैं। इस प्रकार हित समूहीकरण राजनीतिक व्यवस्था में निरन्तर होता रहता है।
4. राजनीतिक संचार (Political Communication) राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक संचार का बहुत महत्त्व है, क्योंकि इसके द्वारा ही अन्य सभी कार्य सम्पादित होते हैं। सभी व्यक्ति चाहे वे नागरिक हों या अधिकारी वर्ग से सम्बन्धित हों, सूचना पर ही निर्भर रहते हैं और उनके अनुसार ही उनकी गतिविधियों का संचालन होता है। इसलिए प्रजातन्त्र में प्रेस तथा भाषण की स्वतन्त्रता पर जोर दिया जाता है जबकि साम्यवादी राज्यों एवं तानाशाही राज्यों में उन पर प्रतिबन्ध लगाने की बात की जाती है। संचार के साधन निश्चय ही राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। संचार के बिना हित स्पष्टीकरण का काम हो ही नहीं सकता। आधुनिक प्रगतिशील समाज में संचार-व्यवस्था को जहां तक हो सका है, तटस्थ बनाने की कोशिश की गई है और इसकी स्वतन्त्रता एवं स्वायत्तता को स्वीकार कर लिया गया है।
लोकतन्त्रात्मक व्यवस्था में संचार-व्यवस्था बहुमुखी, शक्तिशाली, समाज एवं शासक वर्ग में तटस्थ, लोचशील और प्रसारात्मक होती है। आलमण्ड एवं पॉवेल (Almond and Powell) के शब्दों में, “विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं का परीक्षण करने के लिए, राजनीतिक संचार के निष्पादन (Performance) का विश्लेषण एवं तुलना अत्यन्त रुचिपूर्ण एवं उपयोगी माध्यम है।” (“The analysis and comparison of the performance of political communication is one of the most interesting and useful means of examining different political systems.”) तुलनात्मक अध्ययनों में राजनीतिक संचार पर चार दृष्टियों से विचार किया जाता है-सूचनाओं में समरसता (Homogeneity), गतिशीलता (Mobility), मात्रा (Volume) तथा दिशा (Direction)
(ख) निर्गत कार्य (Output Functions)–राजनीतिक व्यवस्था के निर्गत कार्य शासकीय क्रिया-कलापों में काफ़ी समानता रखते हैं। यद्यपि आलमण्ड ने स्वयं स्वीकार किया है कि निर्गत कार्य परम्परागत सक्ति पृथक्करण सिद्धान्त में वर्णित सरकारी अंगों के कार्यों से काफ़ी मिलते-जुलते हैं। फिर भी उसने इनको सरकारी कार्य-कलापों के स्थान पर निर्गत कार्य ही कहना अधिक उपयुक्त समझा है। डेविस व लीविस (Davis and Lewis) के शब्दों में, “इसका उद्देश्य संस्थाओं के विवरण पर अधिक बल देने के विचार को परिवर्तित करता है क्योंकि विभिन्न देशों में एक ही प्रकार की संस्थाओं के अलग-अलग प्रकार्य हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसके पीछे इन संस्थाओं द्वारा सम्पादित किए जाने वाले कार्य-कलापों की व्याख्या करने के लिए प्रकार्यात्मक अवधारणाओं का एक सैट प्रस्तुत करने की भावना भी उपस्थित है।”
जिस प्रकार सरकार के मुख्य कार्य तीन हैं-कानून-निर्माण, कानूनों को लागू करना और विवादों को निपटाना है, उसी प्रकार निर्गत कार्य तीन हैं
(1) नियम बनाना। (2) नियम लागू करना। (3) नियम निर्णयन कार्य।
1. नियम बनाना (Rule Making)-समाज में व्यक्तियों के रहने के लिए आवश्यक है कि उनके पारस्परिक सम्बन्धों को नियमित करने के लिए नियम होने चाहिएं। राजनीतिक व्यवस्था में नियम बनाने का कार्य मुख्यतः व्यवस्थापिकाओं तथा उप-व्यवस्थापन अभिकरणों द्वारा किया जाता है। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में इस कार्य को किया जाता है। आलमण्ड के विचारानुसार, ‘विधायन’ (Legislation) शब्द के स्थान पर ‘नियम निर्माण’ शब्द का प्रयोग उचित है क्योंकि ‘विधायन’ शब्द से कुछ विशेष संरचना तथा निश्चित प्रक्रिया का बोध होता है जबकि अनेक राजनीतिक व्यवस्थाओं में नियम निर्माण कार्य एक उलझी हुई (Diffuse) प्रक्रिया है जिसे सुलझाना तथा उसका विवरण देना कठिन होता है।
विधायन का काम औपचारिक तौर पर स्थापित संरचनाएं ही किया करती हैं जिन्हें संसद् अथवा कांग्रेस अथवा विधानपालिका कहा जाता है और जो सुनिश्चित एवं औपचारिक प्रक्रियाओं द्वारा ही काम करती हैं। परन्तु कुछ ऐसी राजनीतिक व्यवस्थाएं भी होती हैं जिनमें ऐसी औपचारिक संरचनाएं अथवा ऐसी औपचारिक प्रक्रियाएं होती ही नहीं। इस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था में नियम निर्धारण का कार्य एक अलग ढंग से किया जाता है। आधुनिक लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में नियम निर्धारण का कार्य प्रायः कई जगहों पर कई पात्रों द्वारा किया जाता है। एल० ए० हठ ने नियमों के ऐसे प्रकारों का वर्णन किया है-प्राथमिक तथा अनुपूरक। प्रारम्भिक समाज में कुछ ऐसे प्राथमिक नियम थे जो व्यक्तियों के यौन सम्बन्धों, बल प्रयोग, आज्ञा पालन आदि के कामों को नियमित करते थे। ये नियम अटल थे और इनको बदला नहीं जा सकता था।
ऐसे नियमों को लागू करने के लिए तथा उनके उल्लंघन किए जाने पर दण्ड के नियम बनाए गए जिन्हें अनुपूरक नियम कहते हैं। यदि इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो संविधान भी अनुपूरक नियमों का समूह है, प्राथमिक नियमों का नहीं। आलमण्ड एवं पॉवेल के मतानुसार, संविधानवाद की यह मान्यता है, “नियमों का निर्माण निश्चित प्रकार की सीमाओं के अन्तर्गत विशिष्ट संस्थाओं द्वारा निश्चित विधियों से होना चाहिए।” (“Rule must be made in certain ways and by specific institutions and within certain kinds of limitations.”)
2. नियम लागू करना (Rule Application)-राजनीतिक व्यवस्था का कार्य केवल नियम बनाना ही नहीं है, बल्कि उन नियमों को लागू करना भी है। नियमों को यदि सही ढंग से लागू नहीं किया जाता तो नियम बनाने का लक्ष्य ही समाप्त हो जाता है और उचित परिणामों की उम्मीद नहीं की जा सकती। राजनीतिक व्यवस्था में नियमों को लागू करने की ज़िम्मेदारी पूर्णतः सरकारी कर्मचारियों या नौकरशाही की होती है। यहां तक कि न्यायालयों के निर्णय भी कर्मचारी वर्ग द्वारा लागू किए जाते हैं। कभी-कभी नियम निर्माण करने वाली संरचनाओं द्वारा भी यह कार्य किया जाता है, परन्तु विकसित राजनीतिक व्यवस्थाओं के नियम प्रयुक्त संरचनाएं नियम निर्माण करने वाली संरचनाओं से पृथक् होती हैं।
3. नियम निर्णयन कार्य (Rule Adjudication)—समाज में जब कोई नियम बनाया जाता है, उसके उल्लंघन की भी सम्भावना सदैव बनी रहती है। अत: यह आवश्यक हैं-जो व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है उसे दण्ड अवश्य मिलना चाहिए। इसलिए नियमों में ही उसकी अवहेलना करने पर दण्ड देने का प्रावधान रहता है, परन्तु यह निर्णय करना पड़ता है कि नियमों को वास्तव में ही भंग किया गया है अथवा नहीं और अगर नियम भंग हुआ है तो किस सीमा तक तथा उसे कितना दण्ड दिया जाना चाहिए ? इसके अतिरिक्त कई बार नियमों के अर्थ पर विवाद उत्पन्न हो जाता है। ऐसी स्थिति में नियमों के अर्थ को भी स्पष्ट करना पड़ता है। प्रायः सभी आधुनिक लोकतन्त्रात्मक राज्यों में यह कार्य न्यायालयों द्वारा किए जाते हैं, परन्तु सर्वसत्तावादी (Totalitarian) प्रणालियों में गुप्त पुलिस केवल लोगों पर निगरानी रखने एवं उन पर दोषारोपण करने का ही काम नहीं करती बल्कि वह तो उन पर चलाया गया मुकद्दमा भी सुनती हैं और उन्हें सज़ा सुना कर स्वयं सजा को लागू भी करती है। व्यवस्था (System) को बनाए रखने के लिए नियम निर्णयन का कार्य बहुत महत्त्वपूर्ण है। अतः एक अच्छी राजनीतिक व्यवस्था में न्यायालयों को पूर्ण रूप से स्वतन्त्र रखा जाता है ताकि न्यायाधीशों का निष्पक्षता को कायम रखा जा सके और नागरिकों का विश्वास बना रहे।
निष्कर्ष (Conclusion) उपर्युक्त कार्य प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था को अवश्य करने पड़ते हैं। इन कार्यों के अतिरिक्त प्रत्येक देश की राजनीतिक व्यवस्था को विशेष परिस्थितियों में अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विशेष कार्य करने पड़ते हैं। सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं के कार्य समान नहीं होते क्योंकि देश की राजनीतिक व्यवस्था को अपने देश की परिस्थितियों और वातावरण के अनुसार नीतियों का निर्माण करना पड़ता है और उनके अनुसार कार्य करने पड़ते हैं।
![]()
प्रश्न 4.
निवेश-निकास प्रक्रिया के रूप में डेविड ईस्टन के राजनीतिक प्रणाली के मॉडल (रूप) की व्याख्या कीजिए।
(Explain David Easton’s model of Political system as input and output Process.)
अथवा
डेविड ईस्टन के विचारानुसार राजनीतिक प्रणाली के कार्यों की व्याख्या करो।
(Discuss the functions of Political System according to David Easton.)
अथवा
डेविड ईस्टन के अनुसार राजनीतिक प्रणाली के कार्यों का वर्णन कीजिए। (Discuss the functions of Political System with reference to the views of David Easton.)
उत्तर-
डेविड ईस्टन ने 1953 में ‘राजनीतिक प्रणाली’ (Political System) नामक पुस्तक प्रकाशित करवाई थी। उस पुस्तक में डेविड ईस्टन ने राजनीतिक प्रणाली की धारणा की विवेचना की थी। डेविड ईस्टन ने राजनीतिक प्रणाली को निवेशों (Inputs) को निकासों (Outputs) में बदलने की प्रक्रिया बताया है।
निवेश क्या हैं? (What are Inputs ?)-डेविड ईस्टन ने एक विशेष रूप में विचार अभिव्यक्त किया है। उसके मतानुसार, “निवेश उस कच्चे माल के समान है जो राजनीतिक प्रणाली नामक मशीन में पाये जाते हैं।” जिस तरह किसी मशीन में कच्चे माल के बिना कोई तैयार माल अथवा वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती है, उसी तरह निवेश रूपी कच्चा माल राजनीतिक प्रणाली रूपी मशीन में डालने के बिना राजनीतिक प्रणाली कोई सत्ताधारी निर्णय नहीं ले सकती है। ऐसे सत्ताधारी निर्णयों को डेविड ईस्टन ने निकास (Outputs) का नाम दिया है। निवेशों के दो रूप (Two Types of Inputs)-डेविड ईस्टन के अनुसार, निवेश दो प्रकार के होते हैं
(क) मांगों के रूप में निवेश (Inputs in the form of demands)-जब लोग राजनीतिक प्रणाली से कुछ मांगों की पूर्ति की मांग करते हैं तो मांगों के रूप में निवेश होते हैं। डेविड ईस्टन ने मांगों के रूप में निवेशों को चार प्रकार का माना है
1. वस्तुओं तथा सेवाओं के विभाजन के लिये मांगें (Demands for the allocation of goods and services)-व्यक्ति सरकार से उचित वेतन, कार्य करने के लिये निश्चित समय, शिक्षा प्राप्त करने की सुविधाएं, यातायात के साधन, स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाएं इत्यादि की मांग करते हैं। इनको डेविड ईस्टन ने वस्तुओं तथा सेवाओं को व्यवस्था की मांगें कहा है।
2. व्यवहार को नियमित करने के लिए मांगें (Demands for regulation of behaviour)—व्यक्ति राजनीतिक प्रणाली से सार्वजनिक सुरक्षा, सामाजिक व्यवहार सम्बन्धी नियमों के निर्माण आदि की मांगें करते हैं। कुशल और नियमित सामाजिक जीवन के लिये ऐसी मांगें प्रायः की जाती हैं।
3. राजीतिक प्रणाली में भाग लेने सम्बन्धी मांगें (Demands regarding participation in the political System)-लोग मांग करते हैं कि उनको मताधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार, राजनीतिक संगठन बनाने का अधिकार इत्यादि दिये जाएं। ये ऐसी मांगें हैं जिनके फलस्वरूप लोग राजनीतिक प्रणाली के कार्यों में भाग ले सकते हैं।
4. संचार तथा सूचना प्राप्त करने सम्बन्धी मांगें (Demands for Communication and Information)लोग राजनीतिक प्रणाली का संचार करने वाले विशिष्ट वर्ग से नीति निर्माण सम्बन्धी सूचनाएं प्राप्त करने, सिद्धान्त अथवा नियम निश्चित करने, संकट अथवा औपचारिक अवसरों पर राजनीतिक प्रणाली द्वारा शक्ति के दिखावे इत्यादि के लिये मांगें करते हैं। इन मांगों को डेविड ईस्टन ने संचार तथा सूचना प्राप्त करने सम्बन्धी मांगों का नाम दिया है।
(ख) समर्थन के रूप में निवेश (Inputs in the form of Support)-उपर्युक्त चार प्रकार के निवेश मांगों के रूप में हैं। ये ऐसे कच्चे माल के समान हैं जो राजनीतिक प्रणाली रूपी मशीन में पाया जाता है। कोई भी मशीन उस समय तक कार्य नहीं कर सकती जब तक उसको विद्युत् अथवा तेल अथवा किसी अन्य साधन द्वारा शक्ति न दी जाए। इसी तरह डेविड ईस्टन ने निवेशों के दूसरे रूप को समर्थन निवेश (Support Inputs) का नाम दिया है। ऐसे समर्थन
निवेशों के बिना राजनीतिक प्रणाली कार्य नहीं कर सकती है क्योंकि ये समर्थन निवेश ही राजनीतिक प्रणाली को ऐसी शक्ति देते हैं जिसके बल से राजनीतिक प्रणाली निवेश मांगों (Demand Inputs) सम्बन्धी योग्य कार्यवाही कर सकती है।
निकास क्या होते हैं? (What are Outputs ?) डेविड ईस्टन ने निकासों (Outputs) का बड़ा सरल अर्थ बताया है। लोगों द्वारा निवेशों के रूप में सरकार के पास कुछ मांगें पेश की जाती हैं। राजनीतिक प्रणाली अपने साधन तथा सामर्थ्य के अनुसार उन मांगों सम्बन्धी निर्णय लेती है। इन निर्णयों को डेविड ईस्टन ने निकास (Outputs) बताया है। निकास अनेक प्रकार के हो सकते हैं। जब सरकार मानवीय व्यवहार को नियमित करने के लिये कोई कानूनी निर्णय लेती है उनको भी निकास कहा जाता है। जब सरकार सार्वजनिक सेवाएं अथवा पदों की व्यवस्था करती है उसके ऐसे निर्णय भी निकास कहलाते हैं। संक्षेप में, राजनीतिक प्रणाली के सत्ताधारी निर्णयों को निकास (Outputs) का नाम दिया जाता है।
![]()
प्रश्न 5.
राज्य और राजनीतिक प्रणाली में मुख्य अन्तरों का वर्णन करो।
(Write main differences between State and Political System.)
अथवा
राज्य तथा राजनीतिक प्रणाली में अंतर बताओ।
(Make a distinction between State and Political System.)
उत्तर-
प्राचीनकाल में राज्य को राजनीतिशास्त्र का मुख्य विषय माना जाता था। गार्नर की भान्ति ब्लंटशली (Bluntschli), गैटेल (Gettell), गैरिस (Garies), गिलक्राइस्ट (Gilchrist), लॉर्ड एक्टन (Lord Acton) इत्यादि विद्वानों ने राज्य को ही राजनीतिशास्त्र का केन्द्र-बिन्दु माना। परन्तु आधुनिक विद्वान् इस परम्परागत विचार से सहमत नहीं होते। वे राज्य की अपेक्षा राजनीतिक व्यवस्था को आधुनिक राजनीति अथवा राजनीति शास्त्र का मुख्य विषय मानते हैं। आधुनिक विद्वानों का विचार है कि राजनीति शास्त्र के क्षेत्र को राज्य तक ही सीमित करना उसकी व्यावहारिकता को बिल्कुल नष्ट करने वाली बात है। इन विद्वानों में आलमण्ड तथा पॉवेल, चार्ल्स मेरियम (Charles Meriam), हैरल्ड लॉसवैल (Harold Lasswell), डेविड ईस्टन (David Easton), स्टीफन एल० वास्बी (Stephen L. Wasbi) इत्यादि के नाम मुख्य हैं। राज्य और राजनीतिक व्यवस्था में अन्तर पाए जाते हैं, परन्तु दोनों में अन्तर करने से पहले राज्य और राजनीतिक व्यवस्था का अर्थ स्पष्ट करना अति आवश्यक है।
राज्य का अर्थ (Meaning of State)-प्रो० गिलक्राइस्ट (Gilchrist) के अनुसार, “राज्य उसे कहते हैं जहां कुछ लोग एक निश्चित प्रदेश में एक सरकार के अधीन संगठित होते हैं। यह सरकार आन्तरिक मामलों में अपनी जनता की प्रभुसत्ता को प्रकट करती है और बाहरी मामलों में अन्य सरकारों से स्वतन्त्र होती है।” इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि जनसंख्या, निश्चित भूमि, सरकार तथा प्रभुसत्ता राज्य के चार मूल तत्त्व हैं जिनके बिना राज्य की स्थापना नहीं हो सकती। यदि इन चार तत्त्वों में से कोई भी तत्त्व विद्यमान नहीं है तो राज्य की स्थापना नहीं हो सकती।
राजनीतिक व्यवस्था का अर्थ (Meaning of Political System)-राजनीतिक व्यवस्था में सरकार की संस्थाओं के अतिरिक्त वे सभी औपचारिक अथवा अनौपचारिक संस्थाएं अथवा समूह अथवां संगठन सम्मिलित हैं जो किसीन-किसी तरह राजनीतिक जीवन को प्रभावित करते हैं। राजनीतिक व्यवस्था का सम्बन्ध केवल कानून बनाने और लागू करने से ही नहीं बल्कि वास्तविक रूप में बल प्रयोग द्वारा उनका पालन करवाने से भी है।
राज्य और राजनीतिक व्यवस्था में अन्तर (Difference between State and Political System)-राज्य और राजनीतिक व्यवस्था में मुख्य अन्तर निम्नलिखित हैं-
1. राज्य के चार अनिवार्य तत्त्व हैं जबकि राजनीतिक व्यवस्था के अनेक तत्त्व हैं (State has four essential elements whereas political system has many elements)-राज्य तथा राजनीतिक व्यवस्था में मुख्य अन्तर यह है कि राज्य के अनिवार्य तत्त्व चार हैं जबकि राजनीतिक व्यवस्था के तत्त्व अनेक हैं। जनसंख्या, निश्चित भूमि, सरकार तथा प्रभुसत्ता-राज्य के चार अनिवार्य तत्त्व हैं। इनमें से यदि एक तत्त्व भी न हो तो राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। परन्तु राजनीतिक व्यवस्था के निश्चित तत्त्व होते हैं जैसे कि इसमें राजनीतिक प्रभावों की खोज, वैधता की प्राप्ति, परिवर्तनशीलता, अन्य विषयों तथा अन्य राजनीतिक व्यवस्थाओं का प्रभाव तथा प्रतिक्रियाओं का अध्ययन इत्यादि सम्मिलित होता है।
2. राज्य कानूनी तथा संस्थात्मक ढांचे से सम्बन्धित होता है जबकि राजनीतिक व्यवस्था प्रक्रियाओं से सम्बन्धित होती है (State deals with legal and Institutional structure but political system deals with the processes)-राज्य का सम्बन्ध कानूनी तथा संस्थात्मक ढांचे से होता है जबकि राजनीतिक व्यवस्था का सम्बन्ध प्रक्रियाओं (Processes) से होता है। कई लेखकों ने प्रक्रियाओं से सम्बन्धित मॉडल (Models) पेश किए जिनका सम्बन्ध राजनीतिक व्यवस्था से है।
3. राजनीतिक व्यवस्था का क्षेत्र राज्य के क्षेत्र से अधिक व्यापक है (Scope of Political System is broader than the Scope of State)-राजनीतिक व्यवस्था का क्षेत्र राज्य के क्षेत्र से कहीं अधिक विशाल है। राज्य का मुख्य सम्बन्ध औपचारिक संस्थाओं से होता है जबकि राजनीति व्यवस्था में समाज में होने वाली प्रत्येक राजनीतिक प्रक्रिया, औपचारिक और अनौपचारिक भी शामिल की जाती हैं। राजनीतिक व्यवस्था की सीमाएं व्यावहारिक (Practical) तथा नीति (Policy) विज्ञान पर आधारित होने के कारण बड़ी विस्तृत होती हैं।
4. राज्य की मुख्य विशेषता प्रभुसत्ता है जबकि राजनीतिक व्यवस्था का मुख्य गुण वैध शारीरिक शक्ति है (Sovereignty is the main feature of State while legitimate Physical coercive force is the main feature of Political System)-आन्तरिक तथा बाहरी प्रभुसत्ता राज्य का सबसे महत्त्वपूर्ण तत्त्व है अर्थात् राज्य सर्वशक्तिमान् होता है और सभी नागरिकों तथा संस्थाओं को राज्य के आदेशों का पालन करना पड़ता है। परन्तु राजनीतिक व्यवस्था में प्रभुसत्ता की धारणा को कोई महत्त्व नहीं दिया जाता। आधुनिक राजनीतिक विद्वान् इस बात को नहीं मानते कि कोई भी राजनीतिक व्यवस्था आन्तरिक और बाहरी प्रभावों से बिल्कुल स्वतन्त्र होती है। आधुनिक वैज्ञानिक इस बात को स्वीकार करते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था आन्तरिक-समाज (Intra-Societal) और बाह्य-समाज (Extra-Societal) के वातावरण से अवश्य प्रभावित होती है। इसके साथ ही आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय युग में बाहरी प्रभुसत्ता का महत्त्व बहुत कम रह गया है। प्रत्येक देश की राजनीतिक व्यवस्था पर दूसरे देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है। आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक आन्तरिक प्रभुसत्ता की धारणा के स्थान पर वैध शारीरिक दण्ड देने की शक्ति (Legitimate Physical Coercive Force) शब्द का प्रयोग करते हैं अर्थात् उनके कथनानुसार राजनीतिक व्यवस्था के पास वैध शारीरिक दण्ड देने की शक्ति है।
5. राज्य एक परम्परागत धारणा है जबकि राजनीतिक व्यवस्था एक आधुनिक धारणा है (State is a traditional concept while Political System is a modern one)-राज्य एक परम्परागत धारणा है और परम्परागत राजनीति में प्रायः राज्य, राष्ट्र, सरकार, संविधान, कानून, प्रभुसत्ता और धारणाओं का इस्तेमाल होता रहा है। परन्तु आजकल राज्य शब्द तथा इसके साथ सम्बन्धित धारणाओं का प्रयोग बहुत घट गया है। आधुनिक युग में यदि कोई विद्वान् राजनीतिक व्यवस्था के स्थान पर राज्य शब्द का प्रयोग करता है तो उसे परम्परावादी कहा जाता है।
6. राजनीतिक व्यवस्था में आत्म-निर्भर अंगों का अस्तित्व होता है जबकि राज्य की धारणा में ऐसी कोई विशेषता नहीं है (Political system implies the existence of interdependent parts while the concept of State is devoid of such Character)-सरकार की संस्थाएं अर्थात् विधानमण्डल, न्यायपालिका, कार्यपालिका, राजनीतिक दल, हित समूह, संचार के साधन इत्यादि राजनीतिक व्यवस्था के भाग माने जाते हैं। जब किसी एक भाग में किसी कारण से महत्त्वपूर्ण परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव राजनीतिक व्यवस्था के अन्य भागों पर भी पड़ता है तथा सम्पूर्ण व्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ता है। परन्तु राज्य की धारणा में ऐसी कोई विशेषता नहीं पाई जाती।।
7. राज्य की क्षेत्रीय सीमाएं निश्चित होती हैं जबकि राजनीतिक व्यवस्था को क्षेत्रीय सीमाओं में नहीं बांधा GT HOAT (Boundaries of State are fixed whereas it is not possible to restrict the boundaries of Political System)-राज्य की क्षेत्रीय सीमाएं होती है। किसी भी राज्य के बारे में यह पता लगाया जा सकता है कि उसकी सीमाएं कहां से शुरू होती हैं और कहां समाप्त होती हैं। परन्तु राजनीतिक व्यवस्थाओं को क्षेत्रीय सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता है। राजनीतिक व्यवस्था की सीमाएं उसकी क्रियाओं की सीमाएं होती हैं। ये सीमाएं बदलती रहती हैं।
8. राज्य एक से होते हैं, राजनीतिक व्यवस्थाओं का स्वरूप विभिन्न प्रकार का होता है (States are the same everywhere, but political systems are Different)-सभी राज्य एक से होते हैं। वे छोटे हों या बड़े, उनमें चार तत्त्वों का होना अनिवार्य है-जनसंख्या, निश्चित भूमि, सरकार तथा प्रभुसत्ता। भारत, इंग्लैण्ड, जापान, चीन, श्रीलंका, बर्मा (म्यनमार), रूस आदि सभी राज्यों में ये चार तत्त्व पाए जाते हैं। परन्तु राजनीतिक व्यवस्थाओं का स्वरूप विभिन्न राज्यों में विभिन्न होता है।
9. राज्य स्थायी है, राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनशील (State is permanent while Political System is Dynamic)-राज्य स्थायी है जबकि राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनशील है। राज्य का अन्त तब होता है जब उससे प्रभुसत्ता छीन ली जाती है। फिर प्रभुसत्ता मिलने पर दोबारा राज्य की स्थापना हो जाती है, परन्तु राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनशील होती है। समय तथा परिस्थितियों के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था बदलती रहती है।
10. राजनीतिक व्यवस्था में निवेशों को निर्गतों में परिवर्तित करने की क्रिया का विशिष्ट स्थान है, परन्तु राज्य की धारणा कुछ विशेष कार्यों से सम्बन्धित है (The concept of political system involves the process of conversion of inputs into outputs, while the concept of state deals with some specific functions)—निवेशों (Inputs) को निर्गतों (Output) में परिवर्तन करने की क्रिया राजनीतिक व्यवस्था की एक . महत्त्वपूर्ण विशेषता है। निवेशों और निर्गतों में परिवर्तन की प्रक्रिया राजनीतिक व्यवस्था में निरन्तर चलती रहती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राजनीतिक व्यवस्था को नियम बनाने का कार्य (Rule Making Functions), नियम लागू करने (Rule application) तथा नियमों के अनुसार निर्णय करने से सम्बन्धित कार्य (Rule adjudication functions) भी करने पड़ते हैं। परन्तु राज्य को कुछ विशेष प्रकार के कार्य ही करने पड़ते हैं। राजनीतिक विद्वानों ने राज्य के कार्यों को अनिवार्य कार्य (Compulsory functions) और ऐच्छिक कार्यों (Optional functional) में बांटा है। इसके अतिरिक्त सांस्कृतिक, धार्मिक, नैतिक क्षेत्र और सामाजिक जीवन के कुछ पक्ष राज्य के अधिकार क्षेत्र से पृथक् माने जाते हैं। परन्तु जीवन के किसी पहलू को राजनीतिक व्यवस्था से अलग नहीं माना जा सकता यदि किसी भी रूप में उसका कोई पक्ष या कार्य राजनीति से सम्बन्धित हो।
11. राजनीतिक व्यवस्था राज्य की अपेक्षा अधिक विश्लेषणात्मक धारणा है (Concept of Political System is more analytical than State)-राज्य के वर्णनात्मक विचार हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है, परन्तु इसका विश्लेषण नहीं किया जा सकता। परन्तु राज्य के विपरीत राजनीतिक व्यवस्था एक विश्लेषणात्मक धारणा है। इसका अस्तित्व व्यक्तियों के मन में होता है। यह वास्तविक जीवन में प्राप्त होने वाली चीज़ नहीं है।
12. राजनीतिक व्यवस्था राज्य की अपेक्षा अधिक एकता तथा सामंजस्य लाने का साधन है (Political system is a better means of bringing integration and adoption than the State)-राज्य और राजनीतिक व्यवस्था में एक अन्य अन्तर यह है कि राजनीतिक व्यवस्था राज्य की अपेक्षा अधिक सामंजस्य उत्पन्न करती है। आलमण्ड तथा पॉवेल (Almond and Powell) के अनुसार, “राजनीतिक व्यवस्था स्वतन्त्र राज्यों में एकीकरण
और सामंजस्य उत्पन्न करने के लिए एक साधन है।”
13. राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक समाजीकरण तथा राजनीतिक संस्कृति का विशेष महत्त्व है, राज्य के लिए नहीं (Political Socialisation and Political culture have special importance in Political System, not for the State)राजनीतिक व्यवस्था की धारणा में राजनीतिक समाजीकरण और राजनीतिक संस्कृति की धारणाओं को विशेष महत्त्व दिया जाता है क्योंकि राजनीतिक समाजीकरण और राजनीतिक संस्कृति की क्रियाएं राजनीतिक व्यवस्था को निरन्तर प्रभावित करती रहती हैं और इसलिए राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन होते रहते हैं। परन्तु राज्य की धारणा में राजनीतिक समाजीकरण और राजनीतिक संस्कृति को कोई विशेष महत्त्व नहीं दिया जाता।
निष्कर्ष (Conclusion)-अन्त में हम यह कह सकते हैं कि राज्य एक परम्परागत धारणो है जबकि राजनीतिक व्यवस्था आधुनिक धारणा है और राजनीतिक व्यवस्था का क्षेत्र राज्य के क्षेत्र से बहुत अधिक व्यापक है।
![]()
लघु उत्तरीय प्रश्न-
प्रश्न 1.
राजनीतिक तथा प्रणाली शब्दों के अर्थों की व्याख्या करें।
अथवा
राजनीतिक (पोलिटिकल) शब्द का क्या अर्थ है ?
उत्तर-
राजनीतिक प्रणाली शब्द के दो भाग हैं-राजनीतिक तथा प्रणाली।
राजनीतिक शब्द का अर्थ-राजनीतिक शब्द सत्ता अथवा शक्ति का सूचक है। किसी भी समुदाय या संघ को राजनीतिक उस समय कहा जा सकता है जबकि उसकी आज्ञा का पालन प्रशासकीय कर्मचारी वर्ग द्वारा शारीरिक बल प्रयोग के भय से करवाया जाता है। अरस्तु ने राजनीतिक समुदाय को ‘अत्यधिक प्रभुत्व-सम्पन्न तथा अन्तर्भावी संगठन’ (The most sovereign and inclusive association) परिभाषित किया है। अरस्तु के मतानुसार राजनीतिक समुदाय के पास सर्वोच्च शक्ति होती है जो इसको अन्य समुदायों से अलग करती है। आल्मण्ड तथा पॉवेल ने राजनीतिक समुदाय की इस शक्ति को कानूनी शारीरिक बलात् शक्ति (Legitimate Physical Coercive Power) का नाम दिया है।
व्यवस्था या प्रणाली-प्रणाली शब्द का प्रयोग अन्तक्रियाओं के समूह का संकेत करने के लिए किया जाता है। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार, “प्रणाली एक पूर्ण समाप्ति है, सम्बद्ध वस्तुओं अथवा अंशों का समूह है, भौतिक या अभौतिक वस्तुओं का संगठित समूह है। आल्मण्ड तथा पॉवेल के अनुसार, “एक ब्यवस्था से अभिप्राय भागों की परस्पर निर्भरता और उसके तथा उसके वातावरण के बीच किसी प्रकार की सीमा से है।” एक प्रणाली के अन्दर कुछ आधारभूत विशेषताएं होती हैं जैसे कि एकता, नियमितता, सम्पूर्णता, संगठन, सम्बद्धता (Coherence), संयुक्तता (Connection) तथा अंशों अथवा भागों की पारस्परिक निर्भरता।
प्रश्न 2.
राजनीतिक प्रणाली का अर्थ लिखिए।
अथवा
राजनीतिक प्रणाली से आपका क्या भाव है ?
उत्तर-
राजनीतिक प्रणाली में सरकारी संस्थाओं जैसे विधानमण्डल, न्यायालय, प्रशासकीय एजेन्सियां ही सम्मिलित नहीं होती बल्कि इनके अतिरिक्त सभी पारस्परिक ढांचे जैसे रक्त सम्बन्ध,जातीय समूह, अव्यवस्थित घटनाएं जैसे प्रदर्शन, लड़ाई-झगड़े, हत्याएं, डकैतियां, औपचारिक राजनीतिक संगठन आदि राजनीतिक पहलुओं सहित सभी सम्मिलित हैं। इस प्रकार राजनीतिक प्रणाली का सम्बन्ध उन सब बातों, क्रियाओं, संस्थाओं से है जो किसी-न-किसी प्रकार से राजनीतिक जीवन को प्रभावित करती हैं। राजनीतिक प्रणाली का सम्बन्ध केवल कानून बनाने और लागू करने से ही नहीं बल्कि वास्तविक रूप से बल प्रयोग द्वारा उनका पालन करवाने से भी है।
![]()
प्रश्न 3.
राजनीतिक प्रणाली की परिभाषाएं दीजिए।
उत्तर-
राजनीतिक व्यवस्था की परिभाषाएं अलग-अलग राजनीति-शास्त्रियों ने अलग-अलग ढंग से दी हैं, फिर भी एक बात पर इन विद्वानों का एक मत है कि राजनीतिक व्यवस्था का सम्बन्ध न्यायसंगत शारीरिक दमन के प्रयोगों के साथ जुड़ा हुआ है। राजनीतिक व्यवस्था की इन सभी परिभाषाओं में न्यायपूर्ण प्रतिबन्धों, दण्ड देने की अधिकारपूर्ण शक्ति लागू करने की शक्ति और बाध्य करने की शक्ति आदि शामिल है।
- डेविड ईस्टन का कहना है, “राजनीतिक व्यवस्था अन्तक्रियाओं का समूह है जिसे सामाजिक व्यवहार की समग्रता में से निकाला गया है तथा जिसके द्वारा समाज के लिए सत्तात्मक मूल्य निर्धारित किए जाते हैं।”
- आल्मण्ड तथा पॉवेल का कथन है, “जब हम राजनीतिक व्यवस्था की बात कहते हैं तो हम इसमें उन समस्त अन्तक्रियाओं को शामिल कर लेते हैं, जो वैध बल प्रयोग को प्रभावित करती हैं।”
- रॉबर्ट डाहल के अनुसार, “राजनीतिक व्यवस्था मानवीय सम्बन्धों का वह दृढ़ मान है जिसमें पर्याप्त मात्रा में शक्ति, शासन या सत्ता सम्मिलित हो।”
- लॉसवेल और कॉप्लान के अनुसार, “राजनीतिक व्यवस्था गम्भीर वंचना है जो राजनीतिक व्यवस्था को अन्य व्यवस्थाओं से अलग करती है।”
प्रश्न 4.
राजनीतिक प्रणाली की कोई चार विशेषताओं का उल्लेख करें।
उत्तर-
राजनीतिक व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं-
- मानवीय सम्बन्ध-राजनीतिक व्यवस्था के लिए मनुष्य के परस्पर सम्बन्ध का होना आवश्यक है, परन्तु सभी प्रकार के मानवीय सम्बन्धों को राजनीतिक व्यवस्था का अंग नहीं माना जा सकता। केवल उन्हीं मानवीय सम्बन्धों को राजनीतिक व्यवस्था का अंग माना जाता हैं जो राजनीतिक व्यवस्था की कार्यशीलता को किसी-न-किसी तरह प्रभावित करते हों।
- औचित्यपूर्ण शक्ति का प्रयोग-औचित्यपूर्ण शारीरिक दबाव शक्ति के बिना राजनीतिक व्यवस्था का अस्तित्व सम्भव नहीं है। औचित्यपूर्ण शक्ति के द्वारा ही राजनीतिक व्यवस्था के सभी कार्य चलते हैं।
- अन्तक्रिया-राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों अथवा इकाइयों में अन्तक्रिया हमेशा चलती रहती है। राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों में व्यक्तिगत अथवा विभिन्न समूहों के रूप में सम्पर्क बना रहता है तथा वे एक-दूसरे को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। इकाइयों में अन्तक्रिया न केवल निरन्तर होती है, बल्कि बहपक्षीय होती है।
- सर्व-व्यापकता-सर्व-व्यापकता का भाव यह है कि विश्व में कोई ऐसा समाज नहीं होगा जहां राजनीतिक प्रणाली का अस्तित्व न हो। सांस्कृतिक एवं असांस्कृतिक समाजों में भी राजनीतिक प्रणाली का अस्तित्व अवश्य होता है। यह ठीक है कि हर समाज में राजनीतिक प्रणाली का स्वरूप एक समान नहीं होता, परन्तु राजनीतिक प्रणाली का स्वरूप प्रत्येक समाज में अवश्य होता है।
![]()
प्रश्न 5.
राज्य और राजनीतिक प्रणाली में चार मुख्य अन्तर लिखो। .
अथवा
राज्य व राजनैतिक प्रणाली में कोई चार अंतर बताइए।
उत्तर-
राज्य और राजनीतिक व्यवस्था में मुख्य अन्तर निम्नलिखित हैं-
- राज्य के चार अनिवार्य तत्त्व हैं जबकि राजनीतिक व्यवस्था के अनेक तत्त्व हैं। जनसंख्या, निश्चित भूमि, सरकार तथा प्रभुसत्ता राज्य के चार अनिवार्य तत्त्व हैं। इनमें से यदि एक तत्त्व भी न हो, तो राज्य की स्थापना नहीं की जा सकती है, परन्तु राजनीतिक व्यवस्था के निश्चित तत्त्व न होकर अनेक तत्त्व होते हैं।
- राज्य की मुख्य विशेषता प्रभुसत्ता है जबकि राजनीतिक व्यवस्था का मुख्य गुण वैध शारीरिक शक्ति है। आन्तरिक तथा बाहरी प्रभुसत्ता राज्य का सबसे महत्त्वपूर्ण तत्त्व है, परन्तु राजनीतिक व्यवस्था में प्रभुसत्ता की धारणा को कोई महत्त्व नहीं दिया जाता है। आधुनिक राजनीतिक विद्वान् आन्तरिक प्रभुसत्ता की धारणा के स्थान पर ‘वैध शारीरिक दण्ड देने की शक्ति’ शब्दों का प्रयोग करते हैं।
- राज्य स्थायी है जबकि राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनशील है। राज्य स्थायी है और इसका अन्त तब होता है जब उससे प्रभुसत्ता छीन ली जाती है। प्रभुसत्ता मिलने पर राज्य की स्थापना दुबारा हो जाती है, परन्तु राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनशील होती है। समय तथा परिस्थितियों के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था बदलती रहती है।
- राजनीतिक व्यवस्था का क्षेत्र राज्य के क्षेत्र से अधिक व्यापक है-राजनीतिक व्यवस्था का क्षेत्र राज्य के क्षेत्र से कहीं अधिक विशाल है।
प्रश्न 6.
फीडबैक लूप व्यवस्था किसे कहा जाता है ?
अथवा
डेविड ईस्टन की कच्चा माल फिर देने (Feed back loop) की प्रक्रिया का वर्णन करें।
अथवा
फीडबैक लूप (Feedback Loop) व्यवस्था से आपका क्या अभिप्राय है ।
उत्तर-
डेविड ईस्टन के अनुसार, निवेशों और निर्गतों में घनिष्ठ सम्बन्ध है। इन दोनों में निरन्तर सम्पर्क रहता है। फीड बैक का अर्थ है-निर्गतों के प्रभावों और परिणामों को पुनः व्यवस्था में निवेश के रूप में ले जाना। ईस्टन के अनुसार निर्गतों के परिणामों को निवेशों के साथ जोड़ने तथा इस प्रकार निवेश तथा निर्गतों के बीच निरन्तर सम्बन्ध बनाने के कार्य को फीड बैक लूप कहते हैं। यदि राजनीतिक व्यवस्था के व्यावहारिक रूप को देखा जाए तो आधुनिक युग में राजनीतिक संस्थाएं और राजनीतिक दल फीड बैक लूप व्यवस्था का कार्य करते हैं। इस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था में वह क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक एक राजनीतिक व्यवस्था इस पर डाले गए दबावों और मांगों को सहन करती है, परन्तु जब यह खतरनाक सीमा को पार कर जाती है तो राजनीतिक व्यवस्था में दबाव और मांगों को सहन करने की शक्ति नहीं रहती और इससे राजनीतिक व्यवस्था का पतन हो जाता है।
![]()
प्रश्न 7.
राजनीतिक प्रणाली के निकास कार्यों के बारे में लिखिए।
अथवा
राजनैतिक प्रणाली के किन्हीं तीन निकास कार्यों का वर्णन कीजिए।
उत्तर-
1. नियम बनाना-समाज में व्यक्तियों के रहने के लिए आवश्यक है कि उनके पारस्परिक सम्बन्धों को नियमित करने के लिए नियम होने चाहिए। राजनीतिक व्यवस्था में नियम बनाना मुख्यतः विधानपालिकाओं तथा उपव्यवस्थापन अभिकरणों द्वारा किया जाता है। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में इस कार्य को किया जाता है।
2. नियम लागू करना-राजनीतिक व्यवस्था का कार्य केवल नियम बनाना ही नहीं है, बल्कि उन्हें लागू करना है। नियमों को यदि सही ढंग से लागू नहीं किया जाता तो नियम बनाने का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है और उचित परिणामों की आशा नहीं की जा सकती। राजनीतिक व्यवस्था में नियमों को लागू करने की जिम्मेवारी पूर्णतया सरकारी कर्मचारियों या नौकरशाही की होती है।
3. नियम निर्णयन कार्य-समाज में जब भी कोई नियम बनाया जाता है, उसके उल्लंघन की भी सम्भावना सदैव बनी रहती है। अत: यह आवश्यक है कि जो व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है, उसे दण्ड मिलना चाहिए। प्रायः सभी आधुनिक लोकतन्त्रात्मक अच्छी राजनीतिक व्यवस्था में न्यायालयों को पूर्ण रूप से स्वतन्त्र रखा जाता है ताकि न्यायाधीशों की निष्पक्षता को कायम रखा जा सके जिससे नागरिकों का विश्वास बना रहे।
प्रश्न 8.
राजनैतिक प्रणाली के निवेश कार्यों का वर्णन करो।
अथवा
राजनैतिक प्रणाली के कोई तीन निवेश कार्य लिखिए।
उत्तर-
निवेश कार्य-निवेश कार्य गैर-सरकारी उप-प्रणालियों, समाज तथा सामान्य वातावरण द्वारा पूरे किए जाते हैं, जैसे-दल, दबाव समूह, समाचार-पत्र आदि। आल्मण्ड ने राजनीतिक व्यवस्था के चार निवेश कार्य बतलाए हैं-
1. राजनीतिक समाजीकरण तथा भर्ती-आरम्भ में बच्चे राजनीति से अनभिज्ञ होते हैं और उसमें रुचि भी नहीं लेते, परन्तु जैसे-जैसे वे बड़े होते जाते हैं उनके मन में धीरे-धीरे राजनीतिक वृत्तियां बैठती जाती हैं। वे राजनीति में भाग लेना आरम्भ करते हैं और अपनी भूमिका निभानी आरम्भ करते हैं। इसे ही राजनीतिक समाजीकरण कहते हैं। राजनीतिक व्यवस्था में समाजीकरण के साथ-साथ भर्ती का काम भी चलता रहता है। राजनीतिक भर्ती से अभिप्राय उस कार्य से है जिसके माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था की भूमिकाओं की पूर्ति की जाती है।
2. हित स्पष्टीकरण-अपने-अपने हितों की रक्षा करने के लिए प्रत्येक राजनीतिक प्रणाली के सदस्य अपनी प्रणाली में कुछ मांगें पेश किया करते हैं। जिस तरीके से इन मांगों को सही रूप प्रदान किया जाता है तथा जिस प्रकार से ये मांगें प्रणाली के निर्णयकर्ताओं को प्रस्तुत की जाती हैं, उसे हित स्पष्टीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है।
3. हित समूहीकरण-विभिन्न हितों को इकट्ठा करने की क्रिया को ही हित समूहीकरण कहा जाता है। यह प्रकार्य दो प्रकार से सम्पादित हो सकता है। प्रथम, विभिन्न हितों को संयुक्त और समायोजित करके तथा द्वितीय, एक देशी नीति के प्रतिमान में निष्ठा रखने वाले व्यक्तियों की राजनीतिक भर्ती द्वारा।
4. राजनीतिक संचार-राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक संचार का बहुत महत्त्व है, क्योंकि उसके द्वारा ही अन्य सभी कार्य सम्पादित होते हैं। संचार के साधन निश्चित ही राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। संचार के बिना हित स्पष्टीकरण का काम हो ही नहीं सकता।
![]()
प्रश्न 9.
“राजनीतिक प्रणाली” की सीमाएं क्या हैं ?
उत्तर-
प्रत्येक राज्य का वातावरण अन्य राज्यों से अलग होता है। इसी वातावरण में रहकर किसी राज्य की राजनीतिक व्यवस्था अपनी भूमिका निभाती है। वास्तव में राजनीतिक व्यवस्था निर्बाध रूप से कार्य नहीं कर सकती। उस पर आन्तरिक व बाहरी वातावरण का प्रभाव अवश्य पड़ता है। यही वातावरण राजनीतिक व्यवस्था की भूमिका या कार्यों को सीमित कर देता है। आल्पण्ड और पॉवेल के अनुसार प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था की अपनी सीमाएं होती हैं जो इसको अन्य प्रणालियों से अलग करती हैं। राजनीतिक प्रणाली की सीमाएं क्षेत्रीय नहीं बल्कि कार्यात्मक होती हैं और यह सीमाएं समय-समय पर बदलती रहती हैं। उदाहरणतया युद्ध के समय राजनीतिक प्रणाली की सीमाओं में विस्तार हो जाता है, लेकिन युद्ध समाप्त होते ही ये सीमाएं संकुचित हो जाती हैं।
प्रश्न 10.
कानून की दबावकारी शक्ति क्या होती है ?
अथवा
कानून की दबावकारी शक्ति से क्या अभिप्राय है ?
उत्तर-
प्रत्येक राज्य व्यवस्था के सुचारु रूप से संचालन के लिए कानूनों का निर्माण किया जाता है। कानूनों के पीछे राज्य की शक्ति होती है। प्रत्येक नागरिक बिना किसी भेदभाव के कानून के अधीन होता है। सभी व्यक्तियों के साथ एक-जैसी परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाता है। देश के प्रत्येक नागरिक के लिए राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करना अनिवार्य होता है। यदि कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है अथवा कानून का पालन नहीं करता तो उसे राज्य शक्ति द्वारा दण्डित किया जा सकता है। कानून नागरिकों को किसी कार्य को करने अथवा न करने पर बाध्य कर सकता है। ऐसा न करने पर दण्ड दिया जा सकता है। इसे कानून की बाध्यकारी शक्ति कहा जाता है।
![]()
प्रश्न 11.
राजनीतिक प्रणाली का हित स्पष्टीकरण कार्य क्या है ?
अथवा
राजनैतिक प्रणाली के हित स्पष्टीकरण के कार्य की व्याख्या कीजिए।
उत्तर-
हित स्वरूपीकरण या स्पष्टीकरण राजनीतिक प्रणाली का एक महत्त्वपूर्ण कार्य है। समाज में रहते सभी लोगों अथवा सभी वर्गों की मांगें तथा हित एक समान नहीं हो सकते। इसलिए यह अनिवार्य होता है कि विभिन्न वर्गों के लोग अपने हितों अथवा अपनी मांगों का स्पष्टीकरण करें ताकि सरकार उस सम्बन्धी योग्य निर्णय ले सके। जब राजनीतिक दल अथवा अन्य संगठन लोगों की मांगें सरकार तक पहुंचाते हैं तो वह हितों का स्पष्टीकरण कर रहे होते हैं। राजनीतिक दल तथा ऐसे अन्य संगठन राजनीतिक प्रणाली के अंग है। इसलिए उनके द्वारा किए कार्य राजनीतिक प्रणाली के कार्य माने जाते हैं। हित स्पष्टीकरण कार्य व्यापारिक संघों (Trade Unions) तथा अन्य दबाव समूहों (Pressure Groups) द्वारा भी किया जाता है।
प्रश्न 12.
राजनीतिक प्रणाली का राजनीतिक संचार कार्य लिखो।
उत्तर-
राजनीतिक संचार का भाव है सूचनाओं का आदान-प्रदान करना। राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक संचार का बहुत महत्त्व है, क्योंकि इसके द्वारा ही अन्य सभी कार्य सम्पादित होते हैं। सभी व्यक्ति चाहे वे नागरिक हों या अधिकारी वर्ग से सम्बन्धित हों, सूचना पर ही निर्भर रहते हैं और उनके अनुसार ही उनकी गतिविधियों का संचालन होता है। इसलिए प्रजातन्त्र में प्रेस तथा भाषण की स्वतन्त्रता पर जोर दिया जाता है जबकि साम्यवादी राज्यों एवं तानाशाही राज्यों में उन पर प्रतिबन्ध लगाने की बात की जाती है। संचार के साधन निश्चय ही राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। संचार के बिना हित स्पष्टीकरण का काम हो ही नहीं सकता। आधुनिक प्रगतिशील समाज में संचारव्यवस्था को जहां तक हो सका है, तटस्थ बनाने की कोशिश की गई है और इसकी स्वतन्त्रता एवं स्वायत्तता को स्वीकार कर लिया गया है।
![]()
प्रश्न 13.
राजनीतिक प्रणाली का हित समूहीकरण कार्य क्या है?
अथवा
हित समूहीकरण से क्या भाव है ? यह कार्य कौन करता है ?
उत्तर-
विभिन्न संघों के हितों की पूर्ति के लिए अलग-अलग कानून या नीति का निर्माण नहीं किया जा सकता। विभिन्न संघों या समूहों के हितों को इकट्ठा करके उनकी पूर्ति के लिए एक सामान्य नीति निर्धारित की जाती है। विभिन्न हितों को इकट्ठा करने की क्रिया को ही हित समूहीकरण कहा जाता है। आलमण्ड व पॉवेल के शब्दों में, “मांगों को सामान्य नीति स्थानापन्न (विकल्प) में परिवर्तित करने के प्रकार्य को हित समूहीकरण कहा जाता है।” (“The function of converting demands into general policy alternatives is called interest aggregation.”) यह प्रकार्य दो प्रकार से सम्पादित हो सकता है। प्रथम, विभिन्न हितों को संयुक्त और समायोजित करके तथा द्वितीय, एक देश नीति के प्रतिमान में निष्ठा रखने वाले व्यक्तियों की राजनीतिक भर्ती द्वारा । यह प्रकार्य राजनीतिक व्यवस्था में नहीं बल्कि सभी कार्यों में पाया जाता है। मानव अपने विभिन्न हितों को इकट्ठा करके एक बात कहता है। हित-समूह अपने विभिन्न उपसमूहों या मांगों का समूहीकरण करके अपनी मांग रखते हैं। राजनीतिक दल विभिन्न समुदायों या संघों की मांगों को ध्यान में रखकर अपना कार्यक्रम निर्धारित करते हैं। इस प्रकार हित समूहीकरण राजनीतिक व्यवस्था में निरन्तर होता रहता है।
प्रश्न 14.
निवेशों से आपका क्या भाव है ?
अथवा
निवेश समर्थन से क्या अभिप्राय है ?
उत्तर-
प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था का अपना राजनीतिक ढांचा होता है। राजनीतिक ढांचा तभी कार्य कर सकता है यदि इसके लिए उसे आवश्यक सामग्री प्राप्त हो। राजनीतिक व्यवस्था निवेशों के बिना नहीं चल सकती। डेविड ईस्टन ने निवेशों को दो भागों में बांटा है
1.निवेश मांगें- प्रत्येक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह अथवा संगठन राजनीतिक प्रणाली से कुछ मांगों की पूर्ति की आशा रखते हैं और इसीलिए वे राजनीतिक व्यवस्था के सामने कुछ मांगें प्रस्तुत करते हैं। डेविड ईस्टन के अनुसार ये मांगें चार प्रकार की हो सकती हैं-(1) राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेने की मांग (2) वस्तुओं और सेवाओं के वितरण की मांग (3) व्यवहार को नियमित करने के सम्बन्ध में मांग (4) संचारण और सूचना प्राप्त करने के सम्बन्ध में मांग।
2. निवेश समर्थन-डेविड ईस्टन के अनुसार समर्थन उन क्रियाओं को कहा जाता है जो राजनीतिक व्यवस्था की मांगों का मुकाबला करने की क्षमता प्रदान करती है। यदि किसी राजनीतिक व्यवस्था के पास किसी मांग के लिए समर्थन प्राप्त नहीं है अर्थात् उसके पास उसे पूरा करने की क्षमता नहीं है तो वह उसे पूरा नहीं कर सकती। समर्थन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं-(1) भौतिक समर्थन (2) वैधानिक समर्थन (3) सहभागी समर्थन (4) सम्मान समर्थन।
![]()
प्रश्न 15.
निकासों के अर्थों की व्याख्या कीजिए।
अथवा
निकासों से आपका क्या अभिप्राय है ?
उत्तर-
राजनीतिक व्यवस्था में मांगों तथा समर्थनों द्वारा आरम्भ की गई गतिविधियों के परिणामों को ही निर्गत या निकास कहा जाता है। यह आवश्यक नहीं है कि मांगों की पूर्ति के ही निकास होते हैं। निकास मांगों के अनुकूल भी हो सकते हैं और उनके विरुद्ध भी। निकास अग्रलिखित प्रकार के हो सकते हैं
- निकालना-यह लगान, कर, जुर्माना, लूट का माल और व्यक्तिगत सेवाओं के रूप में हो सकती है।
- व्यवहार का नियमन-व्यवहार का नियम जो मनुष्यों के सम्पूर्ण व्यवहारों तथा सम्बन्धों को प्रभावित करता है।
- वस्तुओं या सेवाओं का वितरण-निर्गत का एक अन्य रूप वस्तुओं, सेवाओं के अवसर और पदवियों का वितरण आदि है।
- सांकेतिक निर्गत-इसमें मूल्यों तथा आदर्शों का पुष्टिकरण, राजनीतिक चिह्नों का प्रदर्शन, नीतियों की घोषणा आदि को शामिल किया जाता है।
प्रश्न 16.
राजनीतिक प्रणाली के छः कार्य लिखें।
उत्तर-
इसके लिए प्रश्न नं० 7 एवं 8 देखें।
1. नियम बनाना-समाज में व्यक्तियों के रहने के लिए आवश्यक है कि उनके पारस्परिक सम्बन्धों को नियमित करने के लिए नियम होने चाहिए। राजनीतिक व्यवस्था में नियम बनाना मुख्यतः विधानपालिकाओं तथा उपव्यवस्थापन अभिकरणों द्वारा किया जाता है। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में इस कार्य को किया जाता है।
2. नियम लागू करना-राजनीतिक व्यवस्था का कार्य केवल नियम बनाना ही नहीं है, बल्कि उन्हें लागू करना है। नियमों को यदि सही ढंग से लागू नहीं किया जाता तो नियम बनाने का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है और उचित परिणामों की आशा नहीं की जा सकती। राजनीतिक व्यवस्था में नियमों को लागू करने की जिम्मेवारी पूर्णतया सरकारी कर्मचारियों या नौकरशाही की होती है।
3. नियम निर्णयन कार्य-समाज में जब भी कोई नियम बनाया जाता है, उसके उल्लंघन की भी सम्भावना सदैव बनी रहती है। अत: यह आवश्यक है कि जो व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है, उसे दण्ड मिलना चाहिए। प्रायः सभी आधुनिक लोकतन्त्रात्मक अच्छी राजनीतिक व्यवस्था में न्यायालयों को पूर्ण रूप से स्वतन्त्र रखा जाता है ताकि न्यायाधीशों की निष्पक्षता को कायम रखा जा सके जिससे नागरिकों का विश्वास बना रहे।
निवेश कार्य-निवेश कार्य गैर-सरकारी उप-प्रणालियों, समाज तथा सामान्य वातावरण द्वारा पूरे किए जाते हैं, जैसे-दल, दबाव समूह, समाचार-पत्र आदि। आल्मण्ड ने राजनीतिक व्यवस्था के चार निवेश कार्य बतलाए हैं-
1. राजनीतिक समाजीकरण तथा भर्ती-आरम्भ में बच्चे राजनीति से अनभिज्ञ होते हैं और उसमें रुचि भी नहीं लेते, परन्तु जैसे-जैसे वे बड़े होते जाते हैं उनके मन में धीरे-धीरे राजनीतिक वृत्तियां बैठती जाती हैं। वे राजनीति में भाग लेना आरम्भ करते हैं और अपनी भूमिका निभानी आरम्भ करते हैं। इसे ही राजनीतिक समाजीकरण कहते हैं। राजनीतिक व्यवस्था में समाजीकरण के साथ-साथ भर्ती का काम भी चलता रहता है। राजनीतिक भर्ती से अभिप्राय उस कार्य से है जिसके माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था की भूमिकाओं की पूर्ति की जाती है।
2. हित स्पष्टीकरण-अपने-अपने हितों की रक्षा करने के लिए प्रत्येक राजनीतिक प्रणाली के सदस्य अपनी प्रणाली में कुछ मांगें पेश किया करते हैं। जिस तरीके से इन मांगों को सही रूप प्रदान किया जाता है तथा जिस प्रकार से ये मांगें प्रणाली के निर्णयकर्ताओं को प्रस्तुत की जाती हैं, उसे हित स्पष्टीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है।
3. हित समूहीकरण-विभिन्न हितों को इकट्ठा करने की क्रिया को ही हित समूहीकरण कहा जाता है। यह प्रकार्य दो प्रकार से सम्पादित हो सकता है। प्रथम, विभिन्न हितों को संयुक्त और समायोजित करके तथा द्वितीय, एक देशी नीति के प्रतिमान में निष्ठा रखने वाले व्यक्तियों की राजनीतिक भर्ती द्वारा।
4. राजनीतिक संचार-राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक संचार का बहुत महत्त्व है, क्योंकि उसके द्वारा ही अन्य सभी कार्य सम्पादित होते हैं। संचार के साधन निश्चित ही राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। संचार के बिना हित स्पष्टीकरण का काम हो ही नहीं सकता।
![]()
अति लघु उत्तरीय प्रश्न
प्रश्न 1.
राजनीतिक प्रणाली से आप क्या समझते हैं ?
उत्तर-
राजनीतिक प्रणाली का सम्बन्ध उन सब बातों, क्रियाओं तथा संस्थाओं से है जो किसी-न-किसी प्रकार से राजनीतिक जीवन को प्रभावित करती हैं। राजनीतिक व्यवस्था का सम्बन्ध केवल कानून बनाने और लागू करने से ही नहीं बल्कि वास्तविक रूप से बल प्रयोग द्वारा उनका पालन करवाने से भी है।
प्रश्न 2.
राजनीतिक व्यवस्था की दो परिभाषाएं लिखो।
उत्तर-
- डेविड ईस्टन का कहना है, “राजनीतिक व्यवस्था अन्तक्रियाओं का समूह है जिसे सामाजिक व्यवहार की समग्रता में से निकाला गया है तथा जिसके द्वारा समाज के लिए सत्तात्मक मूल्य निर्धारित किए जाते
- आल्मण्ड तथा पॉवेल का कथन है, “जब हम राजनीतिक व्यवस्था की बात कहते हैं तो हम इसमें उन समस्त अन्तक्रियाओं को शामिल कर लेते हैं जो वैध बल प्रयोग को प्रभावित करती है।”
प्रश्न 3.
प्रणाली की दो मुख्य विशेषताएं बताइए।
उत्तर-
- प्रणाली भिन्न-भिन्न अंगों या हिस्सों के जोड़ों से बनती है।
- प्रणाली के भिन्न-भिन्न अंगों में परस्पर निर्भरता होती है।
![]()
प्रश्न 4.
राज्य और राजनीतिक प्रणाली में दो मुख्य अन्तर लिखो।
उत्तर-
- राज्य के चार अनिवार्य तत्त्व हैं जबकि राजनीतिक व्यवस्था के अनेक तत्त्व हैं। जनसंख्या, निश्चित भूमि, सरकार तथा प्रभुसत्ता राज्य के चार अनिवार्य तत्त्व हैं। परन्तु राजनीतिक व्यवस्था के निश्चित तत्त्व न होकर अनेक तत्त्व होते हैं।
- राज्य की मुख्य विशेषता प्रभुसत्ता है जबकि राजनीतिक व्यवस्था का मुख्य गुण वैध शारीरिक शक्ति है। आन्तरिक तथा बाहरी प्रभुसत्ता राज्य का सबसे महत्त्वपूर्ण तत्त्व है, परन्तु राजनीतिक व्यवस्था में प्रभुसत्ता की धारणा को कोई महत्त्व नहीं दिया जाता है। आधुनिक राजनीतिक विद्वान् आन्तरिक प्रभुसत्ता की धारणा के स्थान पर ‘वैध शारीरिक दण्ड देने की शक्ति’ शब्दों का प्रयोग करते हैं।
प्रश्न 5.
राजनीतिक प्रणाली में फीडबैक लूप व्यवस्था किसे कहा जाता है ?
उत्तर-
डेविड ईस्टन के अनुसार, निवेशों और निर्गतों में घनिष्ठ सम्बन्ध है। इन दोनों में निरन्तर सम्पर्क रहता है। फीड बैक का अर्थ है-निर्गतों के प्रभावों और परिणामों को पुनः व्यवस्था में निवेश के रूप में ले जाना। ईस्टन के अनुसार निर्गतों के परिणामों को निवेशों के साथ जोड़ने तथा इस प्रकार निवेश तथा निर्गतों के बीच निरन्तर सम्बन्ध बनाने के कार्य को फीड बैक लूप कहते हैं। यदि राजनीतिक व्यवस्था के व्यावहारिक रूप को देखा जाए तो आधुनिक युग में राजनीतिक संस्थाएं और राजनीतिक दल फीड बैक लूप व्यवस्था का कार्य करते हैं।
प्रश्न 6.
‘शासन की प्रक्रिया’ (The Process of Government) नामक पुस्तक किसने व कब लिखी ?
उत्तर-
‘शासन की प्रक्रिया’ नामक पुस्तक आर्थर बेंटले ने लिखी।
![]()
प्रश्न 7.
‘राजनीतिक प्रणाली’ (The Political System) नाम की पुस्तक किसने व कब लिखी ?
उत्तर-
राजनीतिक प्रणाली (The Political System) नाम की पुस्तक डेविड ईस्टन ने सन् 1953 में लिखी।
प्रश्न 8.
राजनीतिक प्रणाली के दो निकास (Output) कार्यों के बारे में लिखिए।
उत्तर-
- नियम बनाना-समाज में व्यक्तियों के रहने के लिए आवश्यक है कि उनके पारस्परिक सम्बन्धों को नियमित करने के लिए नियम होने चाहिएं। राजनीतिक व्यवस्था में नियम बनाना मुख्यतः विधानपालिकाओं तथा उप-व्यवस्थापन अभिकरणों द्वारा किया जाता है। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में इस कार्य को किया जाता है।
- नियम लागू करना-राजनीतिक व्यवस्था का कार्य केवल नियम बनाना ही नहीं है, बल्कि उन्हें लागू करना है। राजनीतिक व्यवस्था में नियमों को लागू करने की ज़िम्मेवारी पूर्णतया सरकारी कर्मचारियों या नौकरशाही की होती है।
प्रश्न 9.
राजनीतिक प्रणाली के दो निवेश कार्यों का वर्णन करो।
उत्तर-
- राजनीतिक समाजीकरण तथा भर्ती-जब लोग राजनीति में भाग लेना आरम्भ करते हैं और अपनी भूमिका निभानी आरम्भ करते हैं। इसे ही राजनीतिक समाजीकरण कहते हैं। राजनीतिक व्यवस्था में समाजीकरण के साथ-साथ भर्ती का काम भी चलता रहता है। राजनीतिक भर्ती से अभिप्राय उस कार्य से है जिसके माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था की भूमिकाओं की पूर्ति की जाती है।
- हित स्पष्टीकरण-अपने-अपने हितों की रक्षा करने के लिए प्रत्येक राजनीतिक प्रणाली के सदस्य अपनी प्रणाली में कुछ मांगें पेश किया करते हैं। जिस तरीके से इन मांगों को सही रूप प्रदान किया जाता है तथा जिस प्रकार से ये मांगें प्रणाली के निर्णयकर्ताओं को प्रस्तुत की जाती हैं उसे हित स्पष्टीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है।
![]()
प्रश्न 10.
राजनीतिक संचार से आपका क्या अभिप्राय है ?
उत्तर-
राजनीतिक संचार का भाव है सूचनाओं का आदान-प्रदान करना। राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक संचार का बहुत महत्त्व है, क्योंकि इसके द्वारा ही अन्य सभी कार्य सम्पादित होते हैं। सभी व्यक्ति चाहे वे नागरिक हों या अधिकारी वर्ग से सम्बन्धित हों, सूचना पर ही निर्भर रहते हैं और उनके अनुसार ही उनकी गतिविधियों का संचालन होता है। इसलिए प्रजातन्त्र में प्रेस तथा भाषण की स्वतन्त्रता पर जोर दिया जाता है जबकि साम्यवादी राज्यों एवं तानाशाही राज्यों में उन पर प्रतिबन्ध लगाने की बात की जाती है।
वस्तुनिष्ठ प्रश्न
प्रश्न I. एक शब्द/वाक्य वाले प्रश्न-उत्तर
प्रश्न 1.
राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा का जन्म कब हुआ?
उत्तर-
राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा का जन्म 20वीं शताब्दी में हुआ।
प्रश्न 2.
राजनीतिक प्रणाली शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस राजनीतिक विज्ञानी ने किया ?
उत्तर-
डेविड ईस्टन ने।
![]()
प्रश्न 3.
राजनीतिक प्रणाली के अधीन ‘राजनीतिक’ शब्द का अर्थ बताएं।
उत्तर-
किसी भी समुदाय या संघ को राजनीतिक उसी समय कहा जा सकता है जबकि उसकी आज्ञा का पालन प्रशासकीय कर्मचारी वर्ग द्वारा शारीरिक बल प्रयोग के भय से करवाया जाता है।
प्रश्न 4.
व्यवस्था शब्द का अर्थ लिखिए।
अथवा
प्रणाली शब्द का क्या अर्थ है ?
उत्तर-
व्यवस्था (प्रणाली) शब्द का प्रयोग अन्तक्रियाओं (interactions) के समूह का संकेत करने के लिए किया जाता है।
प्रश्न 5.
राजनीतिक प्रणाली का अर्थ लिखें।
उत्तर-
राजनीतिक प्रणाली का अर्थ उन अन्योन्याश्रित सम्बन्धों के समूह से लिया जाता है, जिसके संचालन में सत्ता या शक्ति का हाथ होता है।
![]()
प्रश्न 6.
राजनीतिक प्रणाली की कोई एक परिभाषा दें।
उत्तर-
डेविड ईस्टन का कहना है, “राजनीतिक व्यवस्था अन्तक्रियाओं का समूह है जिसे सामाजिक व्यवहार की समग्रता में निकाला गया है तथा जिसके द्वारा समाज के लिए सत्तात्मक मूल्य निर्धारित किए जाते हैं।”
प्रश्न 7.
राजनीतिक प्रणाली की कोई एक विशेषता लिखें।
उत्तर-
राजनीतिक व्यवस्था प्रत्येक समाज में पाई जाती है।
प्रश्न 8.
राजनीतिक प्रणाली का एक निवेश कार्य लिखें।
उत्तर-
राजनीतिक समाजीकरण और प्रवेश या भर्ती।
![]()
प्रश्न 9.
राजनीतिक प्रणाली का एक निकास कार्य लिखें।
उत्तर-
नियम निर्माण कार्य।
प्रश्न 10.
राजनीतिक प्रणाली एवं राज्य में कोई एक अन्तर लिखो।
उत्तर-
राजनीतिक व्यवस्था में आत्मनिर्भर अंगों का अस्तित्व होता है जबकि राज्य की धारणा में ऐसी कोई विशेषता नहीं है।
प्रश्न 11.
फीड बैक लूप व्यवस्था का अर्थ लिखें।
उत्तर-
फीड बैक लूप व्यवस्था का अर्थ है-निर्गतों के प्रभावों के परिणामों को पुन: व्यवस्था में निवेश के रूप में ले जाना।
![]()
प्रश्न 12.
राजनीतिक प्रणाली की धारण को लोकप्रिय बनाने वाले किसी एक आधुनिक लेखक का नाम लिखें।
उत्तर-
डेविड ईस्टन।
प्रश्न 13.
राजनीतिक व्यवस्था का वातावरण किसे कहते हैं ?
उत्तर-
समाज के वातावरण या परिस्थितियों का राजनीतिक प्रणाली पर जो प्रभाव पड़ता है, उसे हम सामान्य रूप से राजनीतिक प्रणाली का वातावरण कहते हैं।
प्रश्न 14.
‘नियम निर्माण कार्य’ से आप क्या समझते हैं ?
उत्तर-
परम्परावादी दृष्टिकोण के अनुसार विधानमण्डल को सरकार का एक महत्त्वपूर्ण अंग माना जाता है। इस अंग का मुख्य कार्य कानून बनाना है। इसी कार्य को ही आल्मण्ड ने राजनीतिक प्रणाली के नियम निर्माण के कार्य का स्वरूप बताया है।
![]()
प्रश्न 15.
‘नियम निर्णय कार्य’ क्या होता है ?
उत्तर-
समाज में जब भी कोई नियम बनाया जाता है, उसके उल्लंघन की भी सम्भावना सदैव बनी रहती है। अतः यह आवश्यक है कि जो व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है, उसे दण्ड मिलना चाहिए। प्रायः सभी आधुनिक लोकतन्त्रात्मक राज्यों में यह कार्य न्यायालयों द्वारा किए जाते हैं।
प्रश्न 16.
‘नियम लागू करने का कार्य’ किसे कहते हैं ?
उत्तर-
राजनीतिक व्यवस्था का कार्य केवल नियम बनाना ही नहीं है, बल्कि उन नियमों को लागू करना भी है। राजनीतिक व्यवस्था में नियमों को लागू करने की ज़िम्मेदारी पूर्णतः सरकारी कर्मचारियों या नौकरशाही की होती है। यहां तक कि न्यायालयों के निर्णय भी कर्मचारी वर्ग द्वारा लागू किए जाते हैं।
प्रश्न 17.
आल्मण्ड के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था की कोई एक विशेषता लिखिए।
उत्तर-
राजनीतिक व्यवस्था की सार्वभौमिकता।
![]()
प्रश्न 18.
राजनीतिक प्रणाली के कौन-से निकास कार्य हैं ?
उत्तर-
(1) नियम बनाना
(2) नियम लागू करना
(3) नियम निर्णयन कार्य।
प्रश्न 19.
राजनीतिक प्रणाली की सीमाएं क्या हैं ?
उत्तर-
राजनीतिक प्रणाली पर आन्तरिक व बाहरी वातावरण का प्रभाव अवश्य पड़ता है, जोकि राजनीतिक प्रणाली की भूमिका को सीमित कर देता है। इसकी सीमाएं क्षेत्रीय नहीं, बल्कि कार्यात्मक होती हैं।
प्रश्न 20.
राजनीतिक प्रणाली के किसी एक अनौपचारिक ढांचे का नाम लिखें।
उत्तर-
राजनीतिक दल।
![]()
प्रश्न 21.
राजनीतिक प्रणाली के किसी एक औपचारिक ढांचे का नाम लिखें। ।
उत्तर-
विधानपालिका।
प्रश्न 22.
राजनीतिक प्रणाली के दो कार्यों के नाम लिखो।
उत्तर-
(1) राजनीतिक समाजीकरण तथा भर्ती
(2) हित स्पष्टीकरण।
प्रश्न 23.
डेविड ईस्टन के अनुसार राजनैतिक समुदाय का क्या अर्थ है ?
उत्तर-
जो समूह सामूहिक क्रियाओं और प्रयत्नों द्वारा अपनी समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं, उन्हें राजनीतिक समुदाय कहा जाता है।
![]()
प्रश्न 24.
हित स्पष्टीकरण क्या होता है ?
उत्तर-
आल्मण्ड व पावेल के अनुसार अलग-अलग व्यक्तियों तथा समूहों द्वारा राजनीतिक निर्णयकर्ताओं से मांग करने की प्रक्रिया को हित स्पष्टीकरण कहते हैं।
प्रश्न 25.
राजनीतिक संचार से क्या अभिप्राय है ? .
उत्तर-
राजनीतिक संचार का भाव है, सूचनाओं का आदान-प्रदान करना।
प्रश्न 26.
हित समूहीकरण क्या होता है ?
उत्तर-
विभिन्न हितों को एकत्र करने की क्रिया को हित समूहीकरण कहते हैं।
![]()
प्रश्न 27.
राजनीतिक भर्ती से आप क्या समझते हैं ?
उत्तर-
राजनीतिक भर्ती से अभिप्राय उस कार्य से है, जिसके माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था की भूमिकाओं की पूर्ति की जाती है।
प्रश्न II. खाली स्थान भरें –
1. राजनीतिक व्यवस्था के दो भाग-राजनीतिक एवं ………………
2. राजनीतिक शब्द ……………….. का सूचक है।
3. व्यवस्था शब्द का प्रयोग …………….. के समूह का संकेत करने के लिए किया जाता है।
4. राजनीतिक समाजीकरण एक …………….. कार्य है।
5. नियम निर्माण एक ……………….. कार्य है।
उत्तर-
- व्यवस्था
- सत्ता
- अन्तक्रियाओं
- निवेश
- निर्गत ।
प्रश्न III. निम्नलिखित वाक्यों में से सही एवं ग़लत का चुनाव करें-
1. व्यवस्था भिन्न अंगों या हिस्सों से बनती है।
2. प्रत्येक व्यवस्था में एक इकाई के रूप कार्य करने की योग्यता होती है।
3. आल्मण्ड पावेल ने राजनीतिक समुदाय की शक्ति को कानूनी शारीरिक बलात् शक्ति का नाम दिया है।
4. मूल्यों के सत्तात्मक आबंटन की धारणा आल्मण्ड पावेल से सम्बन्धित है।
उत्तर-
- सही
- सही
- सही
- ग़लत।
![]()
प्रश्न IV. बहुविकल्पीय प्रश्न –
प्रश्न 1.
राजनीतिक व्यवस्था का मुख्य गुण है –
(क) शक्ति या सत्ता
(ख) संगठन
(ग) मानव व्यवहार
(घ) राबर्ट ई० रिग्स।
उत्तर-
(क) शक्ति या सत्ता
प्रश्न 2.
राजनीतिक व्यवस्था शब्द के दो भाग कौन-कौन से हैं ?
(क) राज्य एवं सरकार
(ख) अधिकार एवं कर्त्तव्य
(ग) राजनीतिक एवं व्यवस्था
(घ) स्वतन्त्रता एवं समानता।
उत्तर-
(ग) राजनीतिक एवं व्यवस्था
प्रश्न 3.
“राजनीतिक व्यवस्था अन्तक्रियाओं का समूह है, जिसे सामाजिक व्यवहार की समग्रता में से निकाला गया है, तथा जिसके द्वारा समाज के लिए सत्तात्मक मूल्य निर्धारित किए जाते हैं।” यह कथन किसका है।
(क) आल्मण्ड पावेल
(ख) डेविड ईस्टन
(घ) राबर्ट डहल।
(ग) लासवैल
उत्तर-
(ख) डेविड ईस्टन
![]()
प्रश्न 4.
राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता है
(क) मानवीय सम्बन्ध
(ख) औचित्यपूर्ण शक्ति का प्रयोग
(ग) व्यापकता
(घ) उपरोक्त सभी।
उत्तर-
(घ) उपरोक्त सभी।
प्रश्न 5.
राजनीतिक व्यवस्था का निवेश कार्य है
(क) हित स्पष्टीकरण
(ख) हित समूहीकरण
(ग) राजनीतिक संचारण
(घ) उपरोक्त सभी।
उत्तर-
(घ) उपरोक्त सभी।