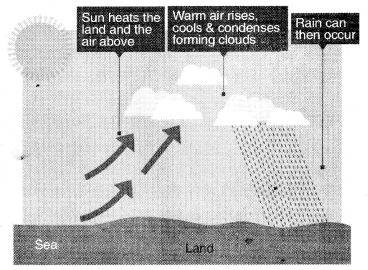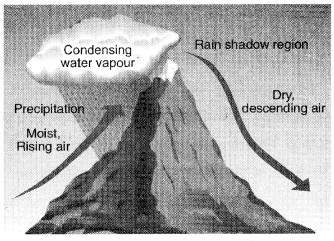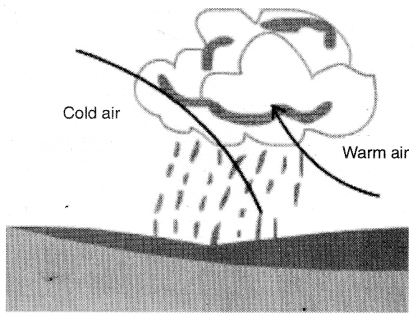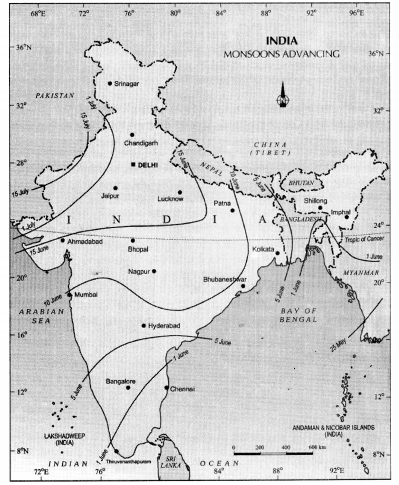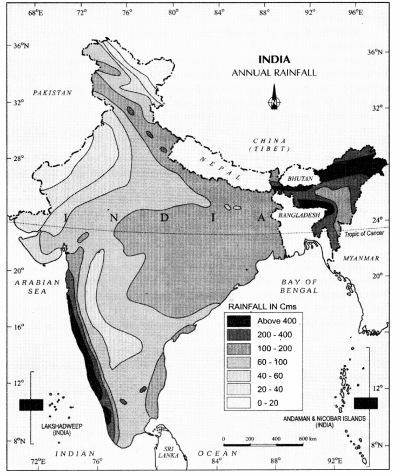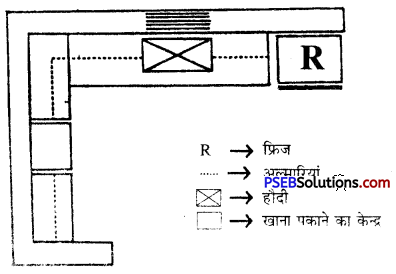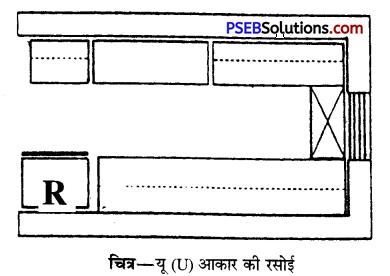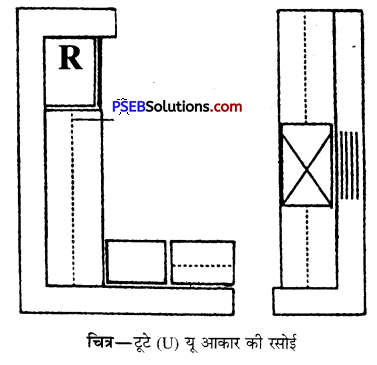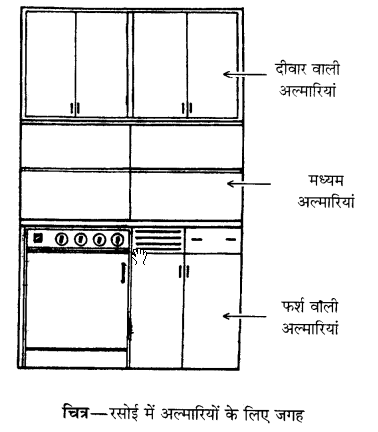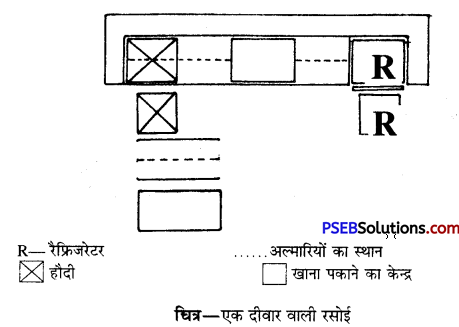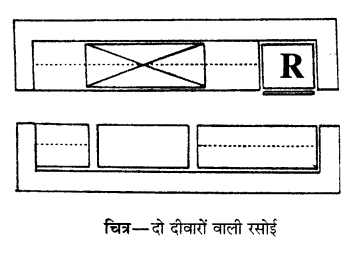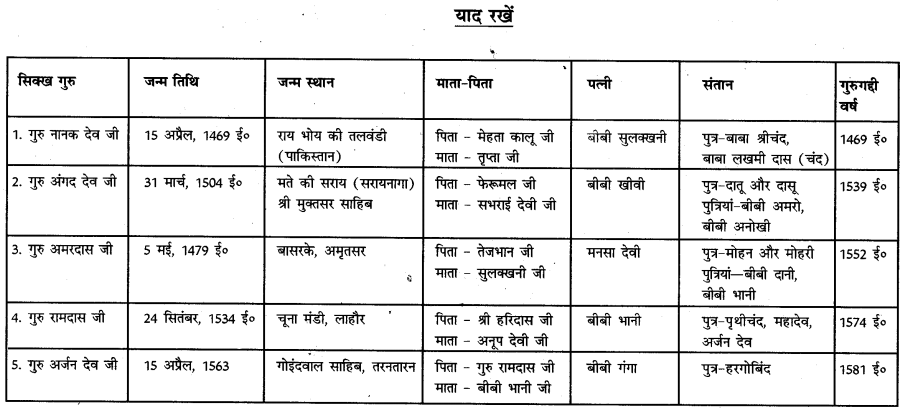Punjab State Board PSEB 11th Class Political Science Book Solutions Chapter 3 नागरिक और नागरिकता Textbook Exercise Questions and Answers.
PSEB Solutions for Class 11 Political Science Chapter 3 नागरिक और नागरिकता
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-
प्रश्न 1.
नागरिक की परिभाषा दीजिए।
(Give the definition of citizen.)
उत्तर-
नागरिक शब्द का अर्थ (Meaning of the word Citizen)-नागरिक शब्द अंग्रेज़ी के ‘सिटीजन’ (Citizen) शब्द का हिन्दी रूपान्तर है जिसका अर्थ है नगर निवासी। इस अर्थ में नागरिक वह व्यक्ति होता है जो किसी नगर की निश्चित परिधि के अन्दर निवास करता है। अतः इस अर्थ के अनुसार जो व्यक्ति गांवों में रहते हैं उन्हें हम नागरिक नहीं कह सकते। परन्तु नगारिक शास्त्र में ‘नागरिक’ शब्द का विशेष अर्थ है। नागरिक शास्त्र में उस व्यक्ति को नागरिक कहा जाता है जिसे राजनीतिक तथा सामाजिक अधिकार प्राप्त हों। भारत में 18वर्ष के पुरुष और स्त्री को मत देने का अधिकार प्राप्त है।
प्राचीन यूनान में छोटे-छोटे नगर-राज्य होते थे। जिन व्यक्तियों को शासन के कार्यों में भाग लेने का अधिकार होता था, उन्हीं को नागरिक कहा जाता था। समस्त जनता को शासन के कार्यों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त नहीं होता था। उन दिनों यूनान में दास प्रथा प्रचलित थी। दासों को नागरिकों की सम्पत्ति समझा जाता था। स्त्रियां, बच्चे, शिल्पकार और व्यापारी लोग नगर-निवासी होते हुए भी नागरिक नहीं समझे जाते थे।
परन्तु आजकल नागरिक शब्द का विस्तृत अर्थ लिया जाता है। आज राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को, जिसे सामाजिक तथा राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, नागरिक कहा जाता है।
नागरिक की परिभाषाएं (Definitions of Citizen)—विभिन्न लेखकों ने ‘नागरिक’ की विभिन्न परिभाषाएं दी हैं। जिनमें से कुछ मुख्य परिभाषाएं निम्नलिखित हैं-
1. अरस्तु (Aristotle) के अनुसार, “नागरिक उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसे राज्य के शासन-प्रबन्ध या न्याय-विभाग में भाग लेने का पूर्ण अधिकार हो।” (“He, who has the power to take part in the deliberative or judicial administration of any state, is a citizen.”) अरस्तु की परिभाषा वर्तमान राज्यों में लागू नहीं होती। आज राज्य इतने बड़े हैं कि सारी जनता राज्य के शासन तथा न्याय विभाग में भाग नहीं ले सकती। जनता का कुछ भाग ही शासन में भाग लेता है। आज नागरिक का विस्तृत अर्थ लिया जाता है।
2. वाटल (Vattal) के अनुसार, “नागरिक किसी राज्य के सदस्य होते हैं, जो कुछ कर्तव्यों द्वारा राजनीतिक समाज में बन्धे होते हैं तथा उससे प्राप्त होने वाले लाभ के बराबर के हिस्सेदार होते हैं।”
3. श्रीनिवास शास्त्री (Shriniwas Shastri) के अनुसार, “नागरिक राज्य का वह सदस्य है जो इसमें रह कर एक तरफ से अपनी उन्नति के विकास के लिए प्रयत्न करता है और दूसरी ओर सारे समाज की भलाई के लिए सोचता है।”
4. प्रो० लॉस्की (Laski) के अनुसार, “नागरिक वह व्यक्ति है जो संगठित समाज का सदस्य ही नहीं वरन् आदेशों को प्राप्त करने वाला तथा कतिपय कर्तव्यों का पालन करने वाला बुद्धिमान् व्यक्ति है।” ।
5. प्रो० ए० के० सीयू (A.K. Sew) के अनुसार, “नागरिक उस व्यक्ति को कहा जाता है जो राज्य के प्रति वफादार हो। जिसको राज्य राजनीतिक व सामाजिक अधिकार देता है और जिसमें मनुष्य की सेवा की भावना पाई जाती है।”

विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि आधुनिक दृष्टि से नागरिक वह व्यक्ति है, जो राज्य के प्रति निष्ठा रखता हो और जिसे सामाजिक तथा राजनीतिक अधिकार प्राप्त हों।
नागरिक की विशेषताएं (Characteristics of a Citizen)-नागरिक को मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं-
- नागरिक किसी राज्य के सदस्य को कहते हैं।
- नागरिक अपने राज्य में स्थायी रूप से रहता है या रह सकता है। राज्य उसे वहां से निकलने को नहीं कह सकता।
- नागरिक को राज्य की ओर से कुछ अधिकार मिले होते हैं, जिन्हें वह अपने और समाज कल्याण के लिए प्रयोग कर सकता है।
- नागरिक को कुछ कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। उसे राज्य के कानूनों का पालन करना पड़ता है।
- नागरिक राज्य के प्रति भक्ति की भावना रखता है और उसकी रक्षा के लिए वचनबद्ध होता है और यदि आवश्यकता पड़े, तो उसे अनिवार्य सैनिक सेवा भी करनी पड़ती है।
प्रश्न 2.
नागरिकता का क्या अर्थ है ? नागरिकता के प्रकार और इसको प्राप्त करने के ढंग बताएं।
(What is the meaning of Citizenship ? Define its kinds and methods of acquiring citizenship.)
अथवा
नागरिकता का क्या अर्थ है ? नागरिकता प्राप्त करने के तरीकों का वर्णन करो।
(What is the meaning of Citizenship ? Describe the methods of acquiring Citizenship.)
उत्तर-
नागरिकता का अर्थ एवं परिभाषाएं-नागरिकता की धारणा उतनी ही प्राचीन है, जितनी कि यूनानी नगर राज्य तथा संस्कृति । नागरिकता का अर्थ सदैव एक-जैसा नहीं रहा है बल्कि समय के अनुसार बदलता रहा है। यूनानी नगर-राज्य में नागरिकता का अधिकार सीमित व्यक्तियों को प्राप्त था। प्राचीन नगर-राज्य में नागरिकता उन्हीं व्यक्तियों को प्राप्त थी, जो नगर-राज्यों के शासन प्रबन्ध में हिस्सा लेते थे। स्त्रियों, गुलामों और विदेशियों को यह अधिकार प्राप्त नहीं था। अतः वे नागरिक नहीं थे।
अरस्तु (Aristotle) ने केवल “उस व्यक्ति को ही नागरिक की पदवी दी है जिसको किसी नगर की न्यायापलिका (Judiciary) या कार्यपालिका में भाग लेने का अधिकार हो।” अरस्तु श्रमिकों को नागरिकता प्रदान नहीं करता क्योंकि उसके मतानुसार श्रमिकों के पास नागरिक के अधिकारों के प्रयोग के लिए न तो योग्यता और न ही पर्याप्त अवकाश होता है। उसका नागरिकता सम्बन्धी विचार वास्तव में कुलीनतन्त्रात्मक है।
आधुनिक युग में नागरिकता की धारणा बहुत व्यापक है-आज नागरिकता केवल राज्य के प्रशासन में भाग लेने वाले को प्राप्त न होकर बल्कि निवास के आधार पर प्राप्त होती है। समस्त व्यक्ति बिना जाति-पाति, लिंग या ग्राम या नगर के निवास तथा सम्पत्ति के, भेदभाव के आधुनिक राज्यों के नागरिक माने जाते हैं। राज्य के प्रशासन में प्रत्यक्ष तौर पर भाग लेना अनिवार्य नहीं है।
नागरिकता की आधुनिक परिभाषाएं (Modern Definitions of Citizenship)—नागरिकता उस वैधानिक या कानूनी सम्बन्ध का नाम है जो व्यक्ति को उस राज्य के साथ जिसका वह सदस्य है, सम्बद्ध करता है।
लॉस्की (Laski) के शब्दों में, “अपनी सुलझी हुई बुद्धि को जनहितों के लिए प्रयोग करना ही नागरिकता है।” (“Citizenship is the contribution of one’s instructed judgement to public good.”)
गैटल (Gettel) के अनुसार, “नागरिकता व्यक्ति की उस अवस्था को कहते हैं जिसके कारण वह अपने राज्य में राष्ट्रीय और राजनीतिक अधिकारों का उपयोग कर सकता है और अपने कर्तव्यों के पालन के लिए तैयार रहता है।” (“Citizenship is that condition of individual due to which he can use national and political rights in his state and is ready to fulfil obligation.”)
बायड (Boyd) के अनुसार, “नागरिकता अपनी वफ़ादारियों को ठीक निभाना है।” (“Citizenship consists in the right ordering of loyalities.”) इस प्रकार किसी राज्य और उसके नागरिकों के उन आपसी सम्बन्धों को ही नागरिकता कहा जाता है जिससे नागरिकों को राज्य की ओर से सामाजिक और राजनीतिक अधिकार मिलते हैं तथा वे राज्य के प्रति कुछ कर्त्तव्यों का पालन करते हैं।
नागरिकता की विशेषताएं (Characteristics of Citizenship) उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर नागरिकता की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं-
- राज्य की सदस्यता (Membership of the State) नागरिकता की प्रथम विशेषता यह है कि नागरिक को किसी राज्य का सदस्य होना आवश्यक होता है। एक राज्य का सदस्य होते हुए भी वह किसी दूसरे राज्य में अस्थायी तौर पर निवास कर सकता है।
- सर्वव्यापकता (Comprehensive)-आधुनिक नागरिकता की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता सर्वव्यापकता है। यह न केवल नगर निवासी बल्कि ग्रामों के लोगों, स्त्रियों व पुरुषों को भी प्राप्त होती है। नागरिकता प्रदान करते समय ग़रीबअमीर, जाति-पाति आदि को नहीं देखा जाता।
- राज्य के प्रति भक्ति (Allegiance to the State)-नागरिकता की तीसरी विशेषता यह है कि नागरिक अपने राज्य के प्रति वफ़ादारी रखता है।
- अधिकारों का उपयोग (Use of Rights)-नागरिक को राज्य की ओर से कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। ये अधिकार राजनीतिक तथा सामाजिक दोनों प्रकार के होते हैं। साम्यवादी देशों में नागरिकों को आर्थिक अधिकार भी प्राप्त होते हैं।
- कर्तव्यों का पालन (Performance of Duties) नागरिकता की एक अन्य विशेषता यह है कि नागरिकों को राष्ट्र और समाज की उन्नति के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। राज्य के कानूनों का निष्ठापूर्वक पालन करना प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य होता है।
- सक्रिय योगदान (Active Participation)-आधुनिक नागरिकता की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता सामाजिक कल्याण के लिए सक्रिय योगदान देना है।
नागरिकता के प्रकार (Kinds of Citizenship)-नागरिकता दो प्रकार की होती है-जन्मजात और राज्यकृत। जन्मजात नागरिकता जन्म के नियम से नियमित होती है और जब विदेशियों को दूसरे देश की नागरिकता मिलती है, उसे राज्यकृत नागरिकता कहते हैं।
नागरिकता प्राप्त करने का ढंग (Methods to Acquire Citizenship)-
(क) जन्मजात नागरिकता की प्राप्ति (Acquisition of Natural born Citizenship)-जन्मजात नागरिकता दो तरीकों से प्राप्त होती है-
1. रक्त सम्बन्धी सिद्धान्त (Blood Relationship)—जन्मजात नागरिकता प्राप्त करने का प्रथम ढंग रक्त सम्बन्ध है। इस सिद्धान्त के अनुसार बच्चे की नागरिकता का निर्णय उसके माता-पिता की नागरिकता से होता है। बच्चे का जन्म किसी भी स्थान पर क्यों न हो, उसे अपने पिता की नागरिकता प्राप्त होती है। भारत में इसी सिद्धान्त को अपनाया गया है। एक भारतीय नागरिक का बच्चा कहीं भी पैदा हो, चाहे जापान में, चाहे अमेरिका में, वह भारतीय ही कहलाएगा। इसी तरह एक अंग्रेज़ का बच्चा कहीं भी पैदा हो चाहे फ्रांस में, चाहे भारत में, अंग्रेज़ ही कहलाएगा। एक जर्मन का बच्चा चाहे कहीं भी उत्पन्न हो, जर्मन ही कहलाएगा। फ्रांस, इटली, स्विट्ज़रलैंड तथा स्वीडन में भी इसी सिद्धान्त को अपनाया गया है।

2. जन्म-स्थान सिद्धान्त (Birth-place)-इस सिद्धान्त के अनुसार बच्चे की नागरिकता का निर्णय उसके जन्मस्थान के आधार पर किया जाता है। इस सिद्धान्त के अनुसार बच्चे को उसी देश की नागरिकता प्राप्त होती है जिस देश की भूमि पर उसका जन्म हुआ हो। बच्चे के पिता की नागरिकता को ध्यान में नहीं रखा जाता। अर्जेण्टाइना में यह सिद्धान्त लागू है। अर्जेण्टाइना में यदि कोई विदेशी सैर के लिए जाते हैं और उनकी सन्तान अर्जेण्टाइना में उत्पन्न होती है तो बच्चे को अर्जेण्टाइना की नागरिकता प्राप्त होती है। एक भारतीय की सन्तान को जिसका जन्म जापान में हुआ हो, जापानी नागरिक माना जाएगा।
दोहरा नियम (Double Principle)-कई देशों में दोनों सिद्धान्तों को अपनाया गया है। इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका में रक्त-सम्बन्धी सिद्धान्त तथा जन्म-स्थान सिद्धान्त दोनों प्रचलित हैं। दोहरे नियम के सिद्धान्त के अनुसार जो बच्चे अंग्रेज़ दम्पति से उत्पन्न हों, चाहे बच्चे का जन्म भारत में हो, चाहे जापान में, अंग्रेज़ कहलाता है और उसे अपने पिता की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त यदि किसी विदेशी के इंग्लैंड में सन्तान पैदा होती है, उसे भी इंग्लैंड की नागरिकता प्राप्त हो जाती है।
सिद्धान्तों के दोष (Defects of these Principles)-इन सिद्धान्तों के कई दोष हैं। जैसे कि एक व्यक्ति एक समय में दो राज्यों का नागरिक भी बन सकता है और यह भी हो सकता है कि व्यक्ति को किसी देश की नागरिकता प्राप्त ही न हो। इन दोनों दोषों की व्याख्या इस प्रकार है-
1. दोहरी नागरिकता (Double Citizenship)-कई बार एक बच्चे को दो राज्यों की नागरिकता भी मिल जाती है। यदि एक अंग्रेज़ दम्पति के अमेरिका में सन्तान उत्पन्न हो तो जो बच्चा जन्म लेगा उसे दोहरी नागरिकता प्राप्त होगी। रक्त-सम्बन्धी सिद्धान्त के अनुसार अंग्रेज़ दम्पति के बच्चे को इंग्लैंड की नागरिकता प्राप्त होगी और जन्म-स्थान सिद्धान्त के अनुसार अमेरिका की नागरिकता प्राप्त होगी। इसी तरह यदि एक जर्मन दम्पति के इंग्लैंड में बच्चा पैदा हो जाता है तो उस बच्चे को जर्मनी तथा इंग्लैंड की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। रक्त सम्बन्धी सिद्धान्त के अनुसार बच्चे को जर्मनी की नागरिकता प्राप्त होती है और जन्म-स्थान सिद्धान्त के अनुसार बच्चे को इंग्लैंड की नागरिकता प्राप्त होती है। दोहरी नागरिकता एक समस्या है। यदि दो देशों में युद्ध आरम्भ हो जाए तो समस्या उत्पन्न हो जाती है कि वह किस देश का नागरिक है। ऐसी दशा में नागरिक का बुरा हाल होता है क्योंकि दोनों देश उस नागरिक को शंका की नज़र से देखते हैं। इस समस्या को समाप्त करने के दो ढंग हैं
- प्रथम, यदि माता-पिता बच्चे के जन्म के पश्चात् अपने देश ले जाएं और रहना शुरू कर दें तो बच्चे को अपने पिता की नागरिकता प्राप्त हो जाती है।
- दूसरे विचार के अनुसार बच्चा वयस्क (Adult) हो कर अपनी नागरिकता का स्वयं निर्णय कर सकता है। वह दोनों में से किसी एक राज्य की नागरिकता को छोड़ सकता है।
2. नागरिकता विहीन या राष्ट्रीयता विहीन (Statelessness)-किसी समय ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि बच्चे को किसी भी देश की नागरिकता प्राप्त न हो। अर्जेण्टाइना (Argentina) में जन्म-स्थान सिद्धान्त और फ्रांस (France) में रक्त सिद्धान्त को अपनाया गया है। अर्जेण्टाइना के नागरिक नव-दम्पत्ति की जो सन्तान फ्रांस में उत्पन्न होगी वह न तो अर्जेण्टाइना और न ही फ्रांस की नागरिकता प्राप्त कर सकेगी। ऐसी स्थिति का हल करने के लिए देशीयकरण का साधन प्रयोग में लाया जा सकता है।
कौन-सा सिद्धान्त अच्छा है ? (Which Principle is better ?)-आम मत यह है कि जन्म-स्थान सिद्धान्त की अपेक्षा रक्त-सिद्धान्त अधिक अच्छा है। जन्म-स्थान सिद्धान्त में संयोगवश अप्रत्याशित अवसर अधिक है। इसके साथ-साथ रक्त-सिद्धान्त के अनुसार प्राप्त नागरिकता की दशा में नागरिक में अपने राज्य और देश के प्रति भक्ति, स्नेह और श्रद्धा की भावनाओं का अधिक प्रबल होना स्वाभाविक है। अतः रक्त सिद्धान्त ही उचित दिखाई पड़ता है।
(ख) राज्यकृत नागरिकता प्राप्त करने के तरीके (How the Naturalised Citizenship is Acquired ?)राज्यकृत नागरिक वे नागरिक होते हैं जिन्हें नागरिकता जन्म-जात सिद्धान्त से प्राप्त नहीं होती, बल्कि जिन्हें नागरिकता सरकार की तरफ से प्राप्त होती है। यदि कोई व्यक्ति अपने देश को छोड़ कर किसी दूसरे देश में जा कर बस जाता है और कुछ समय पश्चात् उस देश की नागरिकता को प्राप्त कर लेता है तो उस व्यक्ति को राज्यकृत नागरिक कहा जाता है। नागरिकता देना अथवा न देना राज्य पर निर्भर करता है। कोई भी व्यक्ति किसी राज्य को नागरिकता देने के लिए मज़बूर नहीं कर सकता। ऐसी नागरिकता प्रार्थना-पत्र देकर प्राप्त की जाती है। कई भारतीय विदेशों में जा कर बस गए हैं और उन्होंने वहां की नागरिकता प्राप्त कर ली है। नागरिकता की प्राप्ति निम्नलिखित ढंगों से की जा सकती है-
1. निश्चित समय के लिए निवास (Resident for Certain Period) यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश में जाकर बहुत समय के लिए रहे तो वह प्रार्थना-पत्र देकर वहां की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। सभी देशों में निवास की अवधि निश्चित है। इंग्लैंड और अमेरिका में निवास की अवधि पांच वर्ष है जबकि फ्रांस में दस वर्ष है। भारत में निवास की अवधि पांच वर्ष है।
2. विवाह (Marriage) विवाह करने से भी नागरिकता प्राप्त हो जाती है। यदि कोई स्त्री किसी दूसरे देश के नागरिक से शादी कर लेती है तो उसे अपने पति की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। भारत का नागरिक यदि इंग्लैंड की स्त्री से शादी कर लेता है तो उस स्त्री को भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। जापान में इसके उलट नियम है। यदि कोई विदेशी जापान की स्त्री से शादी कर लेता है तो उसे जापान की नागरिकता प्राप्त हो जाती है।
3. सम्पत्ति खरीदना (Purchase of Property)-सम्पत्ति खरीदने से भी नागरिकता प्राप्त हो जाती है। ब्राजील, पीरू और मैक्सिको में ऐसा नियम प्रचलित है। यदि कोई विदेशी पीरू में सम्पत्ति खरीद लेता है तो उसे वहां की नागरिकता प्राप्त हो जाती है।
4. गोद लेना (Adoption)-जब एक राज्य का नागरिक किसी दूसरे राज्य के नागरिक को गोद ले लेता है, तो गोद लिए जाने वाले व्यक्ति को अपने पिता की नागरिकता प्राप्त हो जाती है।
5. सरकारी नौकरी (Government Service)-कई राज्यों में यह नियम है कि यदि कोई विदेशी सरकारी नौकरी कर ले तो उसे वहां की नागरिकता मिल जाती है। उदाहरणस्वरूप यदि कोई भारतीय इंग्लैंड में सरकारी नौकरी कर लेता है तो उसे वहां की नागरिकता प्राप्त हो जाती है।
6. विद्वानों को (For Scholars)-कई देशों में विदेशी विद्वानों को नागरिक बनाने के लिए विशेष सुविधाएं दी जाती हैं। विदेशी विद्वानों के निवास की अवधि दूसरे विदेशियों की निवास अवधि से कम होती है। फ्रांस में वैज्ञानिकों या विशेषज्ञों के लिए वहां की नागरिकता प्राप्त करने के लिए एक वर्ष का निवास ही काफ़ी है।
7. विजय द्वारा (By Victory)-जब एक राज्य दूसरे राज्य को विजय करके अपने राज्य में मिला लेता है तो परास्त राज्य के नागरिकों को विजयी राज्य की नागरिकता मिल जाती है।
8. प्रार्थना-पत्र द्वारा (Through Application)-किसी देश के द्वारा निश्चित की गई कानूनी शर्ते पूरी करके प्रार्थना-पत्र देकर उस देश की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। ऐसे व्यक्ति को अच्छे चरित्र और देश के प्रति वफ़दारी रखने का प्रमाण देना पड़ता है।
9. गैर कानूनी बच्चे (Illegitimate Children) यदि कोई नागरिक किसी विदेशी स्त्री से अनुचित सम्बन्ध स्थापित कर लेता है, तो उसके बच्चे गैर-कानूनी कहलाते हैं। परन्तु यदि उन बच्चों के माता-पिता परस्पर शादी कर लेते हैं तो उन बच्चों को अपने पिता की नागरिकता प्राप्त हो जाती है।
10. राजनीतिक शरणागत (Political Asylum)-कई राज्यों में दूसरे देश के पीड़ित राजनीतिज्ञों को नागरिकता प्रदान करने की विशेष व्यवस्था है। चीन के संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो अपनी समाजवादी कार्यवाहियों और विचारों के कारण अपनी सरकार से पीड़ित हो तो चीन में शरण प्राप्त कर सकता है।
11. दोबारा नागरिकता की प्राप्ति (To accept Citizenship Again) यदि कोई नागरिक अपने देश की नागरिकता को छोड़ कर दूसरे राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसे दूसरे राज्य का नागरिक माना जाता है। परन्तु यदि वह चाहे तो अपने राज्य की नागरिकता कुछ शर्ते पूरी करके दोबारा प्राप्त कर सकता है।
संक्षेप में, नागरिकता कई तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। परन्तु कई देशों में जन्म-जात नागरिकों तथा राज्यकृत नागरिकों को एक समान अधिकार नहीं दिए जाते। जिन देशों में दोनों तरह के नागरिकों को समान अधिकार नहीं दिए जाते, वहां प्रायः राज्यकृत नागरिकों को कम अधिकार प्राप्त होते हैं । अमेरिका में राज्यकृत नागरिक राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते। राष्ट्रपति का चुनाव जन्म-जात नागरिक ही लड़ सकते हैं।
प्रश्न 3.
नागरिकता किस प्रकार खोयी जा सकती है ?
(How can citizenship be lost ?)
उत्तर-
जिस तरह नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है इसी तरह नागरिकता को खोया भी जा सकता है। प्रत्येक देश ने इसके लिए नियम बनाए हुए हैं। पर कई नियम प्रायः सभी देशों में एक समान हैं। नागरिकता को निम्नलिखित तरीकों से खोया जा सकता है-
1. लम्बे समय तक अनुपस्थिति (Long Absence)-कई देशों में यह नियम है कि यदि उनका नागरिक लम्बे समय तक बाहर रहे तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। उदाहरणस्वरूप यदि फ्रांस का कोई नागरिक लगातार 10 वर्ष से अधिक समय के लिए फ्रांस से अनुपस्थित रहे तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाती है।
2. विवाह (Marriage)-स्त्रियां विदेशी नागरिकों से शादी करके अपने देश की नागरिकता खो बैठती हैं। भारत का नागरिक जापानी स्त्री से शादी करके जापान की नागरिकता प्राप्त कर लेता है परन्तु स्त्री को अपने देश की नागरिकता छोड़नी पड़ती है।
3. विदेश में सरकारी नौकरी (Government Service Abroad)–यदि एक देश का नागरिक किसी दूसरे देश में सरकारी नौकरी कर लेता है तो उसकी अपने देश की नागरिकता समाप्त हो जाती है।

4. स्वेच्छा से नागरिकता का त्याग (Voluntary Renunciation of Citizenship)-कई देशों की सरकारें अपने नागरिकों को अपनी इच्छा के अनुसार किसी दूसरे देश का नागरिक बनने की आज्ञा प्रदान कर देती हैं। इस प्रकार के व्यक्ति अपनी जन्मजात नागरिकता त्याग कर अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं।
5. पराजय द्वारा (By Defeat)-जब एक देश दूसरे देश को जीत कर उसके क्षेत्र को अपने देश में मिला लेता है तो पराजित देश के नगारिक अपनी नागरिकता खो बैठते हैं और उन्हें विजयी देश की नागरिकता मिल जाती है।
6. सेना से भाग जाने से (Desertion from Army)- यदि कोई नागरिक सेना से भाग कर दूसरे देश में चला जाता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है।
7. दोहरी नागरिकता प्राप्त होने का अर्थ है एक देश की नागरिकता को छोड़ना (Acquisition of Double Citizenship means the loss of citizenship of one country)— a fost afara at at poest ost नागरिकता प्राप्त हो जाती है तब उसे एक राज्य की नागरिकता छोड़नी पड़ती है।
8. देश-द्रोह (Treason)-जब कोई व्यक्ति राज्य के विरुद्ध विद्रोह अथवा क्रान्ति करता है तो उसकी नागरिकता छीन ली जाती है। परन्तु देश-द्रोह के आधार पर उन्हीं नागरिकों की नागरिकता को छीना जा सकता है जो राज्यकृत नागरिक हों।
9. गोद लेना (Adoption) यदि कोई बच्चा किसी विदेशी द्वारा गोद ले लिया जाए, तो बच्चे की नागरिकता समाप्त हो जाती है और वह अपने नए मां-बाप की नागरिकता प्राप्त कर लेता है।
10. विदेशी सरकार से सम्मान प्राप्त करना (Acceptance of honour from Foreign Government)यदि कोई नागरिक अपने देश की आज्ञा के बिना किसी विदेशी सरकार द्वारा दिए गए सम्मान को स्वीकार कर लेता है, तो वह अपनी मूल नागरिकता से वंचित कर दिया जाता है।
11. विदेश में सम्पत्ति खरीदना (Purchase of Property in Foreign Land)–यदि किसी देश का नागरिक मैक्सिको या पीरू आदि देशों में सम्पत्ति खरीद ले तो वह उस देश का नागरिक बन जाएगा और उसकी अपने देश की नागरिकता समाप्त हो जाएगी।
12. न्यायालय के निर्णय द्वारा (Judgement by the Judiciary) कई देशों में यह नियम अपनाया गया है कि वहां की न्यायपालिका किसी भी नागरिक को दण्ड के रूप में देश-निकाले का आदेश दे सकती है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति की नागरिकता स्वयं समाप्त हो जाती है।
प्रश्न 4.
आदर्श नागरिक के अनिवार्य गुणों का वर्णन करें।
(Explain the qualities essential for ideal citizen.)
अथवा
एक अच्छे नागरिक के क्या गुण हैं ?
(What are the qualities of a good citizen ?)
उत्तर-
कोई भी देश उस समय तक उन्नति नहीं कर सकता जब तक कि उस देश के नागरिक अच्छे न हों। राज्य की उन्नति नागरिकों पर निर्भर है। अच्छे नागरिक से अभिप्राय ऐसे नागरिक से है जो अपने कर्तव्यों को पहचाने और उनका पालन करे, जो अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो और उनका पूरा-पूरा प्रयोग करे, जो औरों की स्वतन्त्रता का आदर उसी तरह से करे जैसा वह चाहता है कि अन्य लोग उसकी स्वतन्त्रता का आदर करें, जो केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए जीता है और जो मानव सभ्यता के विकास और प्रगति में अपना पूरा-पूरा योगदान देता है। लॉर्ड ब्राइस ने आदर्श नागरिक के लिए तीन गुण-बुद्धि, आत्मसंयम और उत्तरदायित्व पर जोर दिया है। डॉ० ई० एम० व्हाइट के अनुसार, “सामान्य बुद्धि, ज्ञान तथा कर्तव्य पालन अच्छी नागरिकता के गुण हैं।”
एक आदर्श नागरिक में निम्नलिखित गुण होने चाहिएं-
1. शिक्षा (Education)-अच्छा नागरिक बनने के लिए व्यक्ति का सुशिक्षित होना आवश्यक है। शिक्षा ही अच्छे जीवन का आधार मानी गई है। नागरिक को शिक्षा के द्वारा अपने अधिकारों तथा कर्त्तव्यों का ज्ञान होता है और ज्ञान प्राप्त होने पर ही वह अधिकारों का प्रयोग कर सकता है तथा कर्तव्यों का पालन कर सकता है। शिक्षा द्वारा व्यक्ति का मानसिक विकास भी होता है और उनमें उदारता व नैतिकता की भावनाएं जागृत होती हैं। शिक्षा प्राप्त करने पर उसकी बुद्धि का विकास होता है जिससे वह देश की समस्याओं को समझने, उन पर विचार करने तथा उनको सुलझाने में अपनी राय बनाने तथा प्रकट करने के योग्य बनता है। शिक्षा के बिना लोकतन्त्र सफलतापूर्वक नहीं चल सकता।
2. सामाजिक भावना (Social Spirit) एक अच्छे नागरिक में सामाजिक भावना का होना भी आवश्यक है। नागरिक व्यक्ति पहले है और वह भी सामाजिक। समाज के बिना उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति तथा जीवन का विकास नहीं हो सकता। अच्छे नागरिक केवल अपनी भलाई और स्वार्थ के लिए ही कार्य नहीं करते बल्कि मिल-जुल कर कार्य करते हैं और समस्त समाज के हित में कार्य करते हैं। यदि कोई व्यक्ति केवल अपना ही भला सोचता है तो वह एक अच्छा या आदर्श नागरिक नहीं कहा जा सकता। यदि कोई नागरिक केवल अपने ही कल्याण की बात सोचता रहे, दूसरों के साथ मिल-जुल कर चलने की बजाए सबसे अलग रहता हो, दूसरों के काम में हाथ न बंटाता हो, दूसरों के दुःख-सुख में भाग न लेता हो अर्थात् दूसरों से सम्बन्ध न रखता हो वह भी अच्छा नागरिक नहीं कहा जा सकता। लॉस्की (Laski) के अनुसार, “शिक्षित बुद्धि को सार्वजनिक हित में प्रयोग करना ही नागरिकता है।” (“Citizenship is the contribution of one’s instructed judgement to public good.”)
3. कर्त्तव्यपरायणता (Dutifulness)-अच्छे नागरिकों को अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहना और ईमानदारी से पालन करना आवश्यक है। जिस किसी के प्रति भी उनका कोई कर्त्तव्य है, उसे पूरी तरह से निभाएं। एक लेखक का कहना है, “अच्छी नागरिकता कर्त्तव्यों को उचित ढंग से निभाने में ही निहित है।” (“Citizenship consists in the right ordering of loyalities.”) यदि सब नागरिक अपने-अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करें तो अधिकार स्वयं प्राप्त हो जाएंगे और लड़ाई-झगड़े भी अपने आप बन्द हो जाएंगे। नागरिकों के कर्त्तव्य केवल राज्य के प्रति ही नहीं होते बल्कि परिवार, पड़ोस, मुहल्ले, शहर, प्रान्त तथा देश के प्रति भी हैं और इन सभी कर्तव्यों का उन्हें ईमानदारी से पालन करना चाहिए। जिस देश के नागरिक अपने कर्तव्यों का ठीक ढंग से पालन नहीं करते, वह देश कभी प्रगति नहीं कर सकता।
4. आत्मसंयम तथा सहनशीलता (Self-control and Tolerance)-एक अच्छे नागरिक को अपने ऊपर संयम होना चाहिए तथा उसमें सहनशीलता की भावना भी होनी चाहिए। देश में उसका सम्पर्क विभिन्न विचारों और मतों के व्यक्तियों से होता है, वे सब विचार उसे सुनने पड़ते हैं। विरोधी विचारों को सुन कर उसे जोश और गुस्सा नहीं आना चाहिए। इससे देश में लड़ाई-झगड़े ही बढ़ते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार प्रकट करने का पूर्ण अधिकार है। दूसरों की बातें उसे शान्ति से सुननी चाहिएं और दूसरों के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। दूसरों के विचारों पर प्रभाव दलीलों द्वारा ही डालना चाहिए। विचारों के अदल-बदल से ही समाज की प्रगति होती है। (“Conflict of ideas is more creative than the clash of arms.”) उसका हृदय भी उदार होना चाहिए तथा ऊंच-नीच, छुआछूत, जातिभेद आदि की भावनाएं नहीं होनी चाहिएं। उसे उच्च तथा उदार विचार रखते हुए दूसरों के साथ मिल-जुलकर समस्त समाज के कल्याण के कार्य करने चाहिएं।
5. प्रगतिशीलता (Progressive outlook)—अच्छे नागरिक की अच्छाई केवल यहां तक ही सीमित नहीं है कि वह सामाजिक ढांचे के प्रति श्रद्धा रखे और राजनीतिक व सामाजिक नियमों का पालन करे बल्कि अपने समाज की कुरीतियों और प्रतिक्रियावादी रूढ़ियों को शान्तिपूर्ण ढंग से बदलने के लिए क्रियात्मक प्रयत्न करे। वर्तमान से असन्तुष्टि और सुधार के लिए उमंग एक अच्छे नागरिक के गुण हैं। मानव-सभ्यता और ज्ञान में प्रगति और विकास लाना हर नागरिक का कर्त्तव्य होता है।

6. परिश्रम (Hard Work)-अपने हर कर्त्तव्य के पालन के लिए, अपनी आजीविका कमाने के लिए और मानवसभ्यता में विकास लाने के लिए परिश्रम अत्यावश्यक है। आलस्य और काम-चोरी एक अच्छे नागरिक के महान् शत्रु हैं। परिश्रम के द्वारा अन्य के गुणों को क्रियाशील और साकार किया जा सकता है। कार्लाइल Carlyle) के शब्द बहुत उचित है, “काम ही पूजा है।” (“Work is worship.”) पंडित नेहरू भी कहा करते थे कि, “आराम हराम है।” संसार भर के महान् व्यक्तियों की जीवन गाथाएं इस बात को सिद्ध करती हैं कि उनकी सफलता का प्रमुख कारण परिश्रम ही था। इस कथन के अनुसार, “परिश्रम ही सफलता की कुंजी है।” (“Hard work is the key to success.”)
7. अच्छा स्वास्थ्य (Good Health)-अच्छा नागरिक बनने के लिए स्वास्थ्य भी ठीक होना आवश्यक है। जिस देश के नागरिक कमज़ोर, दुबले-पतले तथा डरपोक होंगे, वह देश अधिक दिन स्वतन्त्र नहीं रह सकता। स्वस्थ नागरिक अपनी रक्षा भी करता है, साथ ही देश की भी। कमज़ोर व्यक्ति अधिक परिश्रम भी नहीं कर सकता। इसके साथ ही बीमार नागरिक विकास भी नहीं कर सकता क्योंकि स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर में (Sound mind in a sound body) ही रह सकता है। बीमार और कमज़ोर नागरिकों का स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो जाता है और उन्हें क्रोध भी जल्दी आने लगता है। बीमार नागरिक देश की समस्या पर अच्छी प्रकार से विचार नहीं कर सकता। स्पष्ट है कि अच्छे शरीर के बिना नागरिक कोई काम ठीक प्रकार से नहीं कर सकता, जिस देश के नागरिक अपने कर्तव्यों का ठीक ढंग से पालन नहीं करते वह देश कभी प्रगति नहीं कर सकता।
8. मत का उचित प्रयोग (Proper use of Vote)-प्रजातान्त्रिक सरकार में प्रत्येक नागरिक को अपना मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। वोट का उचित प्रयोग करके नागरिक अपने इस कर्त्तव्य को पूर्ण कर सकता है। नागरिकों को वोट का अधिकार प्रयोग करते समय धर्म, भाषा, जात-पात आदि से ऊंचा उठना चाहिए। उन्हें वोट उस उम्मीदवार को देना चाहिए जो देश सेवक, ईमानदार तथा योग्य हो। आदर्श नागरिक का यही गुण होता है कि वह वोट का प्रयोग देश के हित के लिए करता है। योग्य उम्मीदवारों को वोट देकर ही कुशल शासन की उम्मीद रखी जा सकती है। इसीलिए तो कहा जाता है कि प्रजातन्त्र प्रणाली में जैसे नागरिक होते हैं वैसी ही सरकार होती है।
9. कानूनों का पालन (Obedience to Law) आदर्श नागरिक कानूनों का पालन करता है। प्रायः यह देखा जाता है कि लोग कानून के पालन में लापरवाही कर जाते हैं। परन्तु यह राष्ट्रीय हित में नहीं है। एक अच्छा नागरिक कानूनों के प्रति पूरी निष्ठा रखता है।
10. निष्काम सेवा (Selfless Service) आदर्श नागरिक अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों की निष्काम सेवा करता है। लोक-कल्याण उसका उद्देश्य होता है।
11. स्वदेश भक्ति ! Patriotism)—प्रत्येक नागरिक को अपने देश और राज्य के प्रति वफ़ादार होना चाहिए। देशभक्ति की भावना जितनी अधिक नागरिकों में होगी, उतना ही अधिक उस देश का कल्याण होगा। देश की रक्षा और उन्नति के लिए नागरिक को तन-मन-धन सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अपने बड़े-से-बड़े लाभ को भी त्याग देना चाहिए यदि उससे अपने देश का थोड़ा भी अहित हो। देश-द्रोह सब से बड़ा अपराध है। देश का हित ही व्यक्ति का हित होना चाहिए। जिस देश के नागरिक सच्चे देश-भक्त होंगे, वह देश न तो कभी दूसरों का गुलाम बन सकता है और न ही किसी क्षेत्र में पिछड़ा हुआ रह सकता है।
12. प्रेम की भावना (Spirit of Love)-आदर्श नागरिक में प्रेम की भावना होती है। वह दूसरे मनुष्यों से प्रेम करता है और प्रत्येक से सद्व्यवहार करता है। वह ग़रीब तथा पिछड़ी जातियों के लोगों से नफरत नहीं करता। जो नागरिक दूसरे व्यक्तियों से लड़ता, झगड़ता रहता है वह अच्छा नागरिक नहीं है।
13. अनुशासन (Discipline) आदर्श नागरिक में अनुशासन का होना आवश्यक है। मनुष्यों की ज़िन्दगी नियमों के अधीन बंधी होती है। नियम का पालन करना ही अनुशासन है। आदर्श नागरिक सदैव समाज तथा राज्य के नियमों का पालन करता है। जिस राज्य के नागरिकों में अनुशासन की भावना नहीं होती, उस राज्य की समस्याएं दिन-प्रतिदिन बढ़ती जाती हैं और भविष्य की समस्याओं को हल करना अति कठिन हो जाता है। देश की उन्नति के लिए नागरिकों में अनुशासन का होना अति आवश्यक है।
14. अच्छा चरित्र (Good Character)-अच्छा चरित्र भी एक नागरिक का बहुत बड़ा गुण है। चरित्रवान् व्यक्ति में बहुत से गुण अपने आप आ जाते हैं। जीवन में उन्नति करने और नाम कमाने में चरित्र का बड़ा प्रभाव पड़ता है। यदि किसी देश के नागरिक बेईमान, धोखेबाज़, व्यभिचारी और शराबी होंगे तो वह देश कभी उन्नति नहीं कर सकता। हमारी भारतीय संस्कति में भी चरित्र को सब से अधिक मूल्यवान् माना गया है। चरित्रवान् व्यक्ति में आज्ञा पालन, अनुशासन का होना अति आवश्यक है।
15. सचेतता (Vigilance)—एक आदर्श नागरिक के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने अधिकारों के लिए सचेत रहे। आलस्य तथा लापरवाही आदर्श नागरिक के शत्रु हैं। लॉस्की (Laski) ने सर्वसिद्ध बात कही है, “निरन्तर सतर्कता स्वतन्त्रता का मूल्य है।” (“Eternal vigilance is the price of liberty.”) अपनी स्वतन्त्रता के प्रति उदासीनता एक नागरिक के लिए आत्म-हत्या के समान है। भले ही देश में प्रजातन्त्रीय शासन हो और नागरिकों के अधिकार संविधान द्वारा सुरक्षित हों, परन्तु ये सब बातें महत्त्वहीन होंगी यदि नागरिक अपनी जागरूकता का प्रदर्शन करने में कोई भी ढील करेंगे।
16. आत्मनिर्भरता (Self-sufficient)-आदर्श नागरिक यथासम्भव आत्मनिर्भर होता है। आत्मनिर्भरता व्यक्ति को स्वावलम्बी बना कर एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिवर्तित करती है जो किसी भी परिस्थिति में अपने पथ से विचलित नहीं हो सकता। ऐसे व्यक्ति समाज के लिए वरदान होते हैं।
17. रचनात्मक दृष्टिकोण (Constructive Attitude)-आदर्श नागरिक का दृष्टिकोण रचनात्मक होता है। वह आलोचना केवल आलोचना के लिए ही नहीं करता बल्कि सरकारी नीति का संशोधन करने तथा उसे लागू करने में आलोचना द्वारा सरकार की सहायता करता है। उसका कार्य केवल अवगुण ढूंढना नहीं होता बल्कि उसे दूर करने के लिए सुझाव भी देना होता है।
18. अन्तर्राष्ट्रीयता की भावना (Spirit of Internationalism)-आदर्श नागरिक में अन्तर्राष्ट्रीयता की भावना का होना आवश्यक है। नागरिक को अपने देश से ही प्यार नहीं होना चाहिए बल्कि मानव जाति से प्यार होना चाहिए। आदर्श नागरिक दूसरे राज्य के नागरिकों को अपना भाई मानते हैं और उनसे मित्रता का व्यवहार करते हैं। आदर्श नागरिक का यह गुण है कि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति की स्थापना के लिए प्रयत्नशील रहता है। वह देश के हित से बढ़ कर विश्व के हित के लिए कार्य करता है।
निष्कर्ष (Conclusion)-उपर्युक्त चर्चा से स्पष्ट हो जाता है कि केवल मात्र नागरिक होना ही काफ़ी नहीं है बल्कि एक अच्छा नागरिक होना आवश्यक है। लॉर्ड ब्राइस (Lord Bryce) ने आदर्श नागरिक के गुण “बुद्धि, आत्म संयम और सच्चाई” (Intelligence, self-control and conscience) कहे हैं। डॉ० विलियम ने “नागरिकता को वफ़ादारियों का उचित क्रम बताया है।” (“Citizenship consists in the right ordering of loyalities.”)
उपर्युक्त गुणों का विकास कोई कठिनाई की बात नहीं है। इन गुणों के विकास के लिए दृढ़ निश्चय और अभ्यास की ज़रूरत है। एक बार गुणों के पनपने के बाद सारी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं और इन गुणों का प्रयोग स्वाभाविक सा हो जाता है।
लघु उत्तरीय प्रश्न-
प्रश्न 1.
नागरिक किसे कहते हैं ?
उत्तर-
‘नागरिक’ का शाब्दिक अर्थ है किसी नगर का निवासी, परन्तु नागरिक शास्त्र में ‘नागरिक’ शब्द का विशेष अर्थ है। नागरिक शास्त्र में उस व्यक्ति को नागरिक कहा जाता है जिसे राजनीतिक तथा सामाजिक अधिकार प्राप्त हों। विभिन्न लेखकों ने नागरिक की विभिन्न परिभाषाएं की हैं-
- अरस्तु के अनुसार, “नागरिक उस व्यक्ति को कहा जाता है, जिसे राज्य के शासन प्रबन्ध विभाग तथा न्यायविभाग में भाग लेने का पूर्ण अधिकार है।”
- वाटल के अनुसार, “नागरिक किसी राज्य के सदस्य होते हैं, जो कुछ कर्त्तव्यों द्वारा राजनीतिक समाज में बन्धे होते हैं तथा इससे प्राप्त होने वाले लाभ के बराबर के हिस्सेदार होते हैं।”

प्रश्न 2.
नागरिक की कोई चार विशेषताएं बताइए।
उत्तर-
नागरिक के लिए निम्नलिखित बातों का होना आवश्यक है-
- नागरिक किसी राज्य का सदस्य होता है।
- नागरिक अपने राज्य में स्थायी रूप से रह सकता है।
- नागरिक को सामाजिक अधिकार प्राप्त होते हैं।
- नागरिक को कुछ कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है।
प्रश्न 3.
नागरिक और विदेशी में चार अन्तर बताएं।
उत्तर-
नागरिक तथा विदेशी में निम्नलिखित अन्तर पाए जाते हैं-
- स्थिति के आधार पर-नागरिक राज्य का सदस्य होता है, जिस कारण उसे निश्चित नागरिकता तथा कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं परन्तु विदेशी राज्य का सदस्य नहीं होता। वह कुछ उद्देश्यों के लिए राज्य में रहता है। उसका उद्देश्य व्यापार-प्रसार या अपनी सरकार का प्रतिनिधित्व करना हो सकता है।
- राज्य भक्ति के आधार पर-नागरिक को अपने राज्य के प्रति वफादार होना पड़ता है, परन्तु विदेशी उस राज्य के प्रति वफादारी नहीं दिखाता जहां कि वह रहता है बल्कि वह उस राज्य के प्रति वफादार रहता है, जहां से वह आया है।
- अधिकारों के आधार पर-नागरिक को सामाजिक और राजनीतिक दोनों प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं, परन्तु विदेशियों को केवल सामाजिक अधिकार प्राप्त होते हैं। विदेशियों को वोट डालने, चुनाव लड़ने, सरकारी पद सम्भालने इत्यादि अधिकार प्राप्त नहीं होते।
- युद्ध के समय विदेशियों को राज्य की सीमा से बाहर जाने के लिए कहा जा सकता है, परन्तु नागरिक को देश से नहीं निकाला जा सकता।
प्रश्न 4.
नागरिकता का अर्थ तथा परिभाषाएं लिखें।
उत्तर-
आज नागरिकता केवल राज्य के प्रशासन में भाग लेने वाले को प्राप्त न होकर बल्कि विकास के आधार पर प्राप्त होती है। समस्त व्यक्ति बिना जात-पात, लिंग या ग्राम या नगर के निवास तथा सम्पत्ति के भेद-भाव के बिना आधुनिक राज्यों के नागरिक माने जाते हैं। राज्य के प्रशासन में प्रत्यक्ष तौर पर भाग लेना अनिवार्य नहीं है। नागरिकता उस वैधानिक या कानूनी सम्बन्ध का नाम है जो व्यक्ति को उस राज्य के साथ, जिसका वह नागरिक है, सम्बद्ध करता है।
लॉस्की के शब्दों में, “अपनी सुलझी हुई बुद्धि को जन-हितों के लिए प्रयोग करना ही नागरिकता है।”
गैटेल के अनुसार, “नागरिकता व्यक्ति की उस अवस्था को कहते हैं जिसके कारण वह अपने राज्य में राष्ट्रीय और राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग कर सकता है और कर्त्तव्य के पालन के लिए तैयार रहता है।”
बायड के अनुसार, “नागरिकता अपनी वफ़ादारियों को ठीक निभाना है।”
इस प्रकार किसी राज्य और उसके नागरिकों के आपसी सम्बन्धों को ही नागरिकता कहते हैं जिससे राज्य की ओर से नागरिकों को कुछ सामाजिक व राजनीतिक अधिकार मिलते हैं तथा वे राज्य के प्रति कुछ कर्त्तव्यों का पालन करते हैं।
प्रश्न 5.
नागरिकता की चार प्रमुख विशेषताएं बताओ।
उत्तर-
नागरिकता की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं
- राज्य की सदस्यता-नागरिकता की प्रथम विशेषता यह है कि नागरिक को किसी राज्य का सदस्य होना आवश्यक होता है। एक राज्य का सदस्य होते हुए भी वह किसी दूसरे राज्य में अस्थायी तौर पर निवास कर सकता है।
- सर्वव्यापकता-आधुनिक नागरिकता की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता सर्वव्यापकता है। यह न केवल नगर निवासी बल्कि ग्रामों के लोगों, स्त्रियों व पुरुषों को भी प्राप्त होती है। नागरिकता प्रदान करते समय ग़रीब-अमीर, जाति-पाति आदि को नहीं देखा जाता।
- राज्य के प्रति भक्ति-नागरिकता की तीसरी विशेषता यह है कि नागरिक अपने राज्य के प्रति वफ़ादारी रखता है।
- नागरिक को राज्य की ओर से कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं।
प्रश्न 6.
जन्मजात नागरिकता प्राप्त करने के ढंग लिखें।
उत्तर-
जन्मजात नागरिकता दो तरीकों से प्राप्त होती है-
1. रक्त सम्बन्धी सिद्धान्त-जन्मजात नागरिकता प्राप्त करने का प्रथम ढंग रक्त सम्बन्ध है। इसके अनुसार बच्चे की नागरिकता का निर्णय उसके माता-पिता की नागरिकता से होता है। बच्चे का जन्म किसी भी स्थान पर क्यों न हो, उसे अपने पिता की नागरिकता प्राप्त होती है। एक भारतीय नागरिक का बच्चा दुनिया के किसी भी देश में पैदा हो, वह भारतीय ही कहलाएगा। फ्रांस, इंग्लैंड, इटली, जर्मनी, स्विट्ज़रलैण्ड तथा स्वीडन में भी इसी सिद्धान्त को अपनाया गया है।
2. जन्म स्थान सिद्धान्त-इस सिद्धान्त के अनुसार बच्चे की नागरिकता का निर्णय उसके जन्म स्थान के आधार पर किया जाता है। इस सिद्धान्त के अनुसार बच्चे को उसी देश की नागरिकता प्राप्त होती जहां उसका जन्म होता है। बच्चे के पिता की नागरिकता को ध्यान में नहीं रखा जाता है। यह सिद्धान्त अर्जेन्टाइना में प्रचलित है। एक भारतीय की सन्तान को जिसका जन्म जापान में हुआ हो तो जापानी नागरिक माना जाएगा।
प्रश्न 7.
राज्यकृत नागरिकता से आपका क्या अभिप्राय है ?
उत्तर-
राज्यकृत नागरिक वे नागरिक होते हैं जिन्हें नागरिकता जन्मजात सिद्धान्त से प्राप्त नहीं होती बल्कि सरकार की तरफ से प्राप्त होती है। यदि कोई व्यक्ति अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में बस जाता है और कुछ समय पश्चात् उस देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो वह राज्यकृत नागरिक कहलाता है। नागरिकता देना अथवा न देना राज्य पर निर्भर करता है। कोई व्यक्ति, किसी राज्य को नागरिकता देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। ऐसी नागरिकता प्रार्थना-पत्र देकर प्राप्त की जा सकती है। कई भारतीय विदेशों में जाकर बस गए हैं और उन्होंने वहां की नागरिकता प्राप्त कर ली है।

प्रश्न 8.
नागरिकता प्राप्त करने के चार ढंग लिखो।
उत्तर-
नागरिकता प्राप्ति के मुख्य ढंग निम्नलिखित हैं-
- निश्चित समय के लिए निवास- यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश में जाकर बहुत समय के लिए रहे तो वह प्रार्थना-पत्र देकर वहां की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। सभी देशों में निवास की अवधि निश्चित है। इंग्लैण्ड और अमेरिका में निवास की अवधि 5 वर्ष है। फ्रांस में 10 वर्ष और भारत में 5 वर्ष है।
- विवाह-विवाह करने से भी नागरिकता प्राप्त हो जाती है। यदि कोई स्त्री किसी दूसरे देश के नागरिक से विवाह कर लेती है तो उसे अपने पति की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। परन्तु जापान में इसके उलट नियम है। जापान में यदि कोई पुरुष जापानी लड़की से शादी कर ले तो उसे जापान की नागरिकता प्राप्त हो जाती है।
- सम्पत्ति द्वारा सम्पत्ति खरीदने से भी नागरिकता प्राप्त हो जाती है। ब्राज़ील, पीरू और मैक्सिको में ऐसा नियम प्रचलित है कि यदि कोई विदेशी वहां सम्पत्ति खरीद लेता है तो उसे वहां की नागरिकता प्राप्त हो जाती है।
- जब एक राज्य का नागरिक किसी दूसरे राज्य के नागरिक को गोद ले लेता है, तो गोद लिए जाने वाले व्यक्ति को अपने पिता के देश की नागरिकता प्राप्त हो जाती है।
प्रश्न 9.
नागरिकता किन चार कारणों द्वारा छीनी जा सकती है ?
उत्तर-
नागरिकता को निम्नलिखित कारणों से छीना जा सकता है-
- लम्बे समय तक अनुपस्थिति-कई देशों में यह नियम है कि यदि उनका नागरिक लम्बे समय तक बाहर रहे तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। यदि फ्रांस का कोई नागरिक 10 वर्ष से भी अधिक लम्बे समय तक फ्रांस से अनुपस्थित रहे तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाती है।
- विवाह-स्त्रियां विदेशी नागरिकों से विवाह करके अपनी नागरिकता खो बैठती हैं। भारत का नागरिक जापानी स्त्री से विवाह करके जापान की नागरिकता प्राप्त कर लेता है। परन्तु स्त्री को अपनी नागरिकता छोड़नी पड़ती है।
- विदेश में सरकारी नौकरी-यदि एक देश का नागरिक दूसरे देश में सरकारी नौकरी कर लेता है तो उसकी अपने देश की नागरिकता समाप्त हो जाती है।
- यदि कोई नागरिक सेना से भाग कर दूसरे देश में चला जाता है, तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है।
प्रश्न 10.
जन्मजात नागरिकता के जन्म स्थान सिद्धान्त का वर्णन करें।
उत्तर-
जन्मजात नागरिकता के जन्म स्थान सिद्धान्त के अनुसार बच्चे की नागरिकता का निर्णय उसके जन्म-स्थान के आधार पर किया जाता है। इस सिद्धान्त के अनुसार बच्चे को उसी देश की नागरिकता प्राप्त होती है जिस देश की भूमि पर उसका जन्म हुआ हो। बच्चे के पिता की नागरिकता को ध्यान में नहीं रखा जाता। अर्जेन्टाइना में यह सिद्धान्त लागू है। अर्जेन्टाइना में यदि कोई विदेशी सैर के लिए जाते हैं तो उनकी सन्तान अर्जेन्टाइना में उत्पन्न होती है तो बच्चे को अर्जेन्टाइना की नागरिकता प्राप्त होती है। एक भारतीय की सन्तान को जिसका जन्म जापान में हुआ हो, जापानी नागरिक माना जाएगा।
प्रश्न 11.
रक्त-सम्बन्धी सिद्धान्त के अनुसार नागरिकता कैसे प्राप्त होती है ?
उत्तर-
इस सिद्धान्त के अनुसार बच्चे की नागरिकता का वर्णन उसके माता-पिता की नागरिकता से होता है। बच्चे का जन्म किसी भी स्थान पर क्यों न हो, उसे अपने पिता की नागरिकता प्राप्त होती है। भारत में इस सिद्धान्त को अपनाया गया है। एक भारतीय नागरिक का बच्चा कहीं भी पैदा हो, चाहे जापान में, चाहे अमेरिका में, वह भारतीय ही कहलायेगा। इसी तरह एक अंग्रेज़ का बच्चा कहीं भी पैदा हो चाहे फ्रांस में, चाहे भारत में, अंग्रेज़ ही कहलायेगा। एक जर्मन का बच्चा चाहे कहीं उत्पन्न हुआ हो, जर्मनी ही कलगाएगा। फ्रांस, इटली, स्विट्ज़रलैण्ड तथा स्वीडन में भी इस सिद्धान्त को अपनाया गया है।
प्रश्न 12.
आदर्श नागरिकता के चार गुण लिखें।
उत्तर-
एक आदर्श नागरिक में अग्रलिखित गुण होने चाहिएं-
- शिक्षा-अच्छा नागरिक बनने के लिए व्यक्ति का सुशिक्षित होना आवश्यक है। शिक्षा द्वारा नागरिक को अपने अधिकारों व कर्तव्यों का ज्ञान होता है। शिक्षा द्वारा व्यक्ति का मानसिक विकास भी होता है और उसमें उदारता व नैतिकता की भावनाएं जागृत होती हैं।
- सामाजिक भावना-एक अच्छे नागरिक में सामाजिक भावना का होना भी आवश्यक है। नागरिक समाज में पहले आया तथा राज्य में बाद में। समाज के बिना उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति तथा विकास नहीं हो सकता।
- कर्त्तव्यपरायणता-अच्छे नागरिकों को अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहना और उनका ईमानदारी से पालन करना अति आवश्यक है। यदि सब नागरिक अपने-अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करें तो सभी अधिकार स्वयं प्राप्त हो जाएंगे। जिस देश के नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन ठीक ढंग से नहीं करते वह देश कभी प्रगति नहीं करता।
- नागरिक परिश्रमी होना चाहिए।
प्रश्न 13.
आदर्श नागरिकता के मार्ग में आने वाली चार बाधाओं का वर्णन करें।
उत्तर-
आदर्श नागरिकता के मार्ग में निम्नलिखित बाधाएं आती हैं :-
- अनपढ़ता-शिक्षा एक अच्छे जीवन का आधार है। शिक्षा के बिना व्यक्ति को अपने अधिकारों व कर्तव्यों का ज्ञान नहीं होता और न ही देश की समस्याओं को समझ कर उनमें सहयोग देने योग्य बन पाता है। अशिक्षित व्यक्ति न तो अपने वोट का ठीक प्रयोग कर सकता है और न ही शासन में भाग ले सकता है।
- अकर्मण्यता या आलस्य-आलसी व्यक्ति भी एक अच्छा नागरिक नहीं बन पाता। ऐसा व्यक्ति अपना पेट भरने के अतिरिक्त किसी काम में रुचि नहीं लेता। आलसी व्यक्ति इतना परिश्रम एवं पुरुषार्थ भी नहीं करता जितना वह कर सकता है। अतः देश के उत्थान पर बुरा प्रभाव पड़ता है।
- ग़रीबी-ग़रीबी भी एक अच्छे नागरिक के मार्ग में बहुत बड़ी रुकावट है। ग़रीब व्यक्ति 24 घण्टे रोटी कमाने के चक्कर में लगा रहता है अतः उसके पास देश की समस्याओं पर विचार करने के लिए समय नहीं होता। ग़रीब व्यक्ति लालच में लाकर अपने मत का भी दुरुपयोग करता है।
- आदर्श नागरिकता के मार्ग में बेरोज़गारी एक बड़ी बाधा है।
प्रश्न 14.
आदर्श नागरिकता के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के चार उपाय लिखो।
उत्तर-
- शिक्षा का प्रसार-अनपढ़ता सभी बुराइयों की जड़ है अतः इसे समाप्त करने के लिए शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। जनता को शिक्षित करने के लिए अधिक संख्या में स्कूल-कॉलेज खोले होने जाने चाहिएं।
- आर्थिक सुधार-ग़रीबी को दूर करने और लोगों की आर्थिक दशा में सुधार करने से भी अच्छे नागरिकों की संख्या बढ़ेगी। सरकार को लोगों में परिश्रम करने व आलस्य छोड़ने का प्रचार करना चाहिए। सरकार को चाहिए कि वह अधिक मात्रा में उद्योग-धन्धे स्थापित करे और लोगों को रोज़गार प्रदान करे।
- सामाजिक भावना-नागरिकों में सामाजिक भावना के महत्त्व पर विचार किया जाना चाहिए। सामाजिक भावना के जागृत होने से ही व्यक्ति का स्वार्थ नष्ट होता है और वह अपने स्वार्थ की ओर ध्यान न देकर समाज के हितों का ध्यान रखने लगता है।
- बेरोजगारी को दूर करना चाहिए।
प्रश्न 15.
नागरिक कितने तरह के होते हैं ?
उत्तर-
नागरिक दो तरह के होते हैं-
- जन्मजात नागरिक (Natural Citizens)
- राज्यकृत नागरिक (Naturalised Citizens) ।
1. जन्मजात नागरिक (Natural Citizens)-पैदायशी या जन्मजात नागरिक वह है, जो जन्म से ही राज्य के नागरिक बनते हैं और स्वाभाविक रूप से ही नागरिकता प्राप्त करते हैं। ऐसे नागरिकों को जन्म स्थान या रक्त सिद्धान्त के आधार पर वहां की नागरिकता प्राप्त होती है।
2. राज्यकृत नागरिक (Naturalised Citizens)-राज्यकृत नागरिक जन्म से किसी अन्य देश का नागरिक होता है परन्तु राज्य में बस जाने के कारण और दूसरी शर्ते पूरी करने पर सरकार द्वारा उन्हें राज्य का नागरिक मान लिया जाता है।

प्रश्न 16.
भारतीय संविधान में नागरिकता के सम्बन्ध में किन नियमों का वर्णन किया गया है ?
उत्तर-
संविधान में भारतीय नागरिकता के सम्बन्ध में निम्नलिखित नियमों का वर्णन किया गया है-
- संविधान के लागू होने पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ है और भारत में रहता है, भारत का नागरिक है।
- ऐसे बच्चे जिनका जन्म विदेश में हुआ है परन्तु जिसके माता या पिता में से किसी का जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ है, तो वह भारत का नागरिक है।
- ऐसे व्यक्ति जो संविधान लागू होने के पांच वर्ष से भारत में रहते हैं भारत के नागरिक होंगे।
- पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के लिए संविधान में वर्णन किया गया है कि 19 जुलाई, 1948 से पूर्व आने वाले ऐसे व्यक्ति जिनका माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी या इनमें से कोई एक अथवा स्वयं अविभाजित भारत में जन्मे हों, तो उन्हें भारत का नागरिक माना जाएगा। 19 जुलाई, 1948 के बाद पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी को नागरिकता प्राप्त करने के लिए प्रार्थनापत्र देना होगा।
- विदेशों में बसने वाले ऐसे भारतीय जिनका स्वयं का, अथवा जिनके माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी में से किसी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ है और वे भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे भारतीय अपना नाम भारतीय दूतावास में दर्ज करा लें। ऐसा करने पर उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त हो जायेगी।
प्रश्न 17.
भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 की मुख्य व्यवस्थाएं लिखो।
अथवा भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है ?
उत्तर-
विदेशियों को भारतीय नागरिकता प्राप्ति के सम्बन्ध में भारतीय संसद् ने 1955 में ‘नागरिकता अधिनियम’ (Citizenship Acquisition Act) पारित किया। इस अधिनियम में निम्नलिखित व्यवस्थाएं हैं-
- भारत की नागरिकता प्राप्त करने का इच्छुक व्यक्ति किसी ऐसे देश का नागरिक नहीं होना चाहिए जो भारतीयों को नागरिकता प्रदान नहीं करता।
- भारत की नागरिकता प्राप्त करने का इच्छुक व्यक्ति नागरिकता के लिए प्रार्थना-पत्र देने की तारीख से पहले वह या तो एक वर्ष तक भारत में निवास करता रहा हो अथवा सरकारी सेवा में रहा हो।
- उपर्युक्त एक वर्ष से पहले के सात वर्षों के भीतर वह भारत में कुल मिलाकर कम-से-कम 4 वर्ष रहा हो या 4 वर्ष तक सरकारी सेवा में रहा हो।
- भारत की नागरिकता प्राप्त करने का इच्छुक व्यक्ति अच्छे चरित्र का व्यक्ति हो।
- संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई भाषाओं में से किसी एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए।
- भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेने के पश्चात् वह या तो भारत में निवास करने अथवा यहां किसी सरकारी सेवा में बने रहने का इरादा रखता हो।
- यदि किसी विदेशी ने विज्ञान, कला, दर्शन, साहित्य, विश्व-शान्ति अथवा मानव विकास के क्षेत्र में कोई विशेष योग्यता प्राप्त कर ली है तो उसे उपर्युक्त शर्तों को पूरा किए बिना भारत का नागरिक बनाया जा सकता है।
प्रश्न 18.
नागरिक और देशीय शब्द में अन्तर स्पष्ट करें।
उत्तर-
साधारण भाषा में नागरिक उस व्यक्ति को कहते हैं जो किसी नगर की निश्चित परिधि के अन्दर निवास करता है। अतः इस अर्थ के अनुसार जो व्यक्ति गांवों में रहते हैं, उन्हें नागरिक नहीं कहा जा सकता। परन्तु आधुनिक युग में नागरिक शब्द का यह अर्थ नहीं लिया जाता है। नागरिक उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसे राज्य में राजनीतिक तथा सामाजिक अधिकार प्राप्त होते हैं। भारत में 18 वर्ष के पुरुष और स्त्री को मत देने का अधिकार प्राप्त है। वह व्यक्ति नगर निवासी भी हो सकता है और ग्रामीण भी।
देशीय (National) राज्य का सदस्य होता है परन्तु उसे वे सारे अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं जोकि एक नागरिक को प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए देशीय को सामाजिक तथा आर्थिक अधिकार तो प्राप्त होते हैं परन्तु उसे राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। जब उसे राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो जाते हैं तो वह नागरिक बन जाता है। प्राय: यह अधिकार एक निश्चित आयु जैसे भारत में 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर मिल जाता है। भारत में 18 वर्ष की आयु से कम आयु वाले व्यक्ति देशीय हैं, इन्हें नागरिक नहीं कहा जा सकता है।
प्रश्न 19.
विदेशी कितने प्रकार के होते हैं ?
उत्तर-
विदेशी तीन प्रकार के होते हैं
- स्थायी विदेशी (Resident Aliens)—स्थायी विदेशी उन व्यक्तियों को कहा जाता है जो अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में बस जाते हैं। वे अपना व्यवसाय वहीं आरम्भ कर देते हैं। उनमें अपने देश वापिस जाने की इच्छा नहीं होती अर्थात् उनका निश्चय स्थायी रूप से वहीं रहने का होता है। जब उन्हें नागरिकता मिल जाती है तब वे उस राज्य के नागरिक बन जाते हैं। भारत के अनेक नागरिक कनाडा, इंग्लैंड तथा दक्षिणी अफ्रीका में जाकर स्थायी रूप से बस गए हैं।
- अस्थायी विदेशी (Temporary Aliens) अस्थायी विदेशी उन व्यक्तियों को कहा जाता है जो सैर करने के लिए या किसी उद्देश्य के लिए दूसरे राज्य में थोड़े समय के लिए जाते हैं और फिर अपने देश वापिस लौट आते
- राजदूत (Ambassadors)-एक राज्य के दूसरे राज्यों के साथ कूटनीतिक सम्बन्ध होते हैं। इन सम्बन्धों की स्थापना राजदूतों के आदान-प्रदान करके होती है। दूसरे देशों के राजदूत हमारे देश में आकर रहते हैं और हमारे देश के राजदूत दूसरे देशों में जाकर रहते हैं। परन्तु राजदूतों पर उनके देश का ही कानून लागू होता है। राजदूत भी विदेशी होते हैं। परन्तु राजदूतों को अन्य विदेशियों की अपेक्षा सरकार से बहुत सुविधाएं प्राप्त होती हैं।
अति लघु उत्तरीय प्रश्न-
प्रश्न 1.
नागरिक किसे कहते हैं ?
उत्तर-
‘नागरिक’ का शाब्दिक अर्थ है किसी नगर का निवासी, परन्तु नागरिक शास्त्र में ‘नागरिक’ शब्द का विशेष अर्थ है। नागरिक शास्त्र में उस व्यक्ति को नागरिक कहा जाता है जिसे राजनीतिक तथा सामाजिक अधिकार प्राप्त हों।
प्रश्न 2.
नागरिक की कोई दो परिभाषाएं दीजिए।
उत्तर-
- अरस्तु के अनुसार, “नागरिक उस व्यक्ति को कहा जाता है, जिसे राज्य के शासन प्रबन्ध विभाग तथा न्याय-विभाग में भाग लेने का पूर्ण अधिकार है।” ।
- वाटल के अनुसार, “नागरिक किसी राज्य के सदस्य होते हैं, जो कुछ कर्तव्यों द्वारा राजनीतिक समाज में बन्धे होते हैं तथा इससे प्राप्त होने वाले लाभ के बराबर के हिस्सेदार होते हैं।”
प्रश्न 3.
नागरिक की कोई दो विशेषताएं बताइए।
उत्तर-
नागरिक के लिए निम्नलिखित बातों का होना आवश्यक है-
- नागरिक किसी राज्य का सदस्य होता है।
- नागरिक अपने राज्य में स्थायी रूप से रह सकता है।

प्रश्न 4.
नागरिक और विदेशी में दो अन्तर बताएं।
उत्तर-
- नागरिक राज्य का सदस्य होता है, जिस कारण उसे निश्चित नागरिकता तथा कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं परन्तु विदेशी राज्य का सदस्य नहीं होता।
- नागरिक को अपने राज्य के प्रति वफादार होना पड़ता है, परन्तु विदेशी उस राज्य के प्रति वफादारी नहीं दिखाता।
प्रश्न 5.
नागरिकता का अर्थ लिखें।
उत्तर-
आज नागरिकता केवल राज्य के प्रशासन में भाग लेने वाले को प्राप्त न होकर बल्कि विकास के आधार पर प्राप्त होती है। समस्त व्यक्ति बिना जात-पात, लिंग या ग्राम या नगर के निवास तथा सम्पत्ति के भेद-भाव के बिना आधुनिक राज्यों के नागरिक माने जाते हैं। राज्य के प्रशासन में प्रत्यक्ष तौर पर भाग लेना अनिवार्य नहीं है। नागरिकता उस वैधानिक या कानूनी सम्बन्ध का नाम है जो व्यक्ति को उस राज्य के साथ, जिसका वह नागरिक है, सम्बद्ध करता है।
प्रश्न 6.
नागरिकता की कोई दो परिभाषा दें।
उत्तर-
लॉस्की के शब्दों में, “अपनी सुलझी हुई बुद्धि को जन-हितों के लिए प्रयोग करना ही नागरिकता है।” गैटेल के अनुसार “नागरिकता व्यक्ति की उस अवस्था को कहते हैं जिसके कारण वह अपने राज्य में राष्ट्रीय और राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग कर सकता है और कर्त्तव्य के पालन के लिए तैयार रहता है।” बायड के अनुसार “नागरिकता अपनी वफ़ादारियों को ठीक निभाना है।”
प्रश्न 7.
नागरिकता की दो प्रमुख विशेषताएं बताओ।
उत्तर-
- राज्य की सदस्यता-नागरिकता की प्रथम विशेषता यह है कि नागरिक को किसी राज्य का सदस्य होना आवश्यक होता है।
- सर्वव्यापकता-आधुनिक नागरिकता की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता सर्वव्यापकता है। यह न केवल नगर निवासी बल्कि ग्रामों के लोगों, स्त्रियों व पुरुषों को भी प्राप्त होती है।
प्रश्न 8.
नागरिकता प्राप्त करने के दो ढंग लिखो।
उत्तर-
- निश्चित समय के लिए निवास-यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश में जाकर बहुत समय के लिए रहे तो वह प्रार्थना-पत्र देकर वहां की नागरिकता प्राप्त कर सकता है।
- विवाह-विवाह करने से भी नागरिकता प्राप्त हो जाती है। यदि कोई स्त्री किसी दूसरे देश के नागरिक से विवाह कर लेती है तो उसे अपने पति की नागरिकता प्राप्त हो जाती है।
प्रश्न 9.
नागरिकता किन दो कारणों द्वारा छीनी जा सकती है ?
उत्तर-
- लम्बे समय तक अनुपस्थिति-कई देशों में यह नियम है कि यदि उनका नागरिक लम्बे समय तक बाहर रहे तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाती है।
- विवाह-स्त्रियां विदेशी नागरिकों से विवाह करके अपनी नागरिकता खो बैठती हैं।
प्रश्न 10.
आदर्श नागरिकता के दो गुण लिखें।
उत्तर-
- शिक्षा-अच्छा नागरिक बनने के लिए व्यक्ति का सुशिक्षित होना आवश्यक है।
- सामाजिक भावना-एक अच्छे नागरिक में सामाजिक भावना का होना भी आवश्यक है। नागरिक समाज में पहले आया तथा राज्य में बाद में। समाज के बिना उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति तथा विकास नहीं हो सकता।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न-
प्रश्न I. एक शब्द/वाक्य वाले प्रश्न-उत्तर-
प्रश्न 1. नागरिक को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं ?
उत्तर-नागरिक को अंग्रेज़ी में सिटीज़न (Citizen) कहते हैं।
प्रश्न 2. सिटीजन का क्या अर्थ लिया जाता है ?
उत्तर-सिटीज़न का अर्थ है-नगर-निवासी।
प्रश्न 3. आदर्श नागरिक के कोई दो गुण लिखें।
उत्तर-
- सामाजिक भावना से परिपूर्ण
- प्रगतिशील तथा परिश्रमी।
प्रश्न 4. आदर्श नागरिक के मार्ग में आने वाली कोई दो बाधाएं लिखें।
उत्तर-
- अनपढ़ता
- सांप्रदायिकता।
प्रश्न 5. आदर्श नागरिकता के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के कोई दो उपाय लिखें।
उत्तर-
- शिक्षा का प्रसार
- समान अधिकारों की प्राप्ति।
प्रश्न 6. “नागरिक वह व्यक्ति है, जिसको राज्य के कानून सम्बन्धी विचार-विमर्श और न्याय प्रबन्ध में भाग लेने का अधिकार है।” यह कथन किसका है?
उत्तर- अरस्तु।
प्रश्न 7. ‘अपनी सुलझी हुई बुद्धि को जनहितों के लिए प्रयोग करना ही नागरिकता है।’ यह कथन किसका है?
उत्तर-लॉस्की।
प्रश्न 8. किन्हीं दो साधनों के नाम लिखें, जिनसे राज्यकृत नागरिकता प्राप्त की जा सकती है?
उत्तर-
- विवाह
- सरकारी नौकरी ।
प्रश्न 9. किन्हीं दो साधनो का नाम लिखें, जिनसे नागरिकता समाप्त हो सकती है?
उत्तर-
- लंबी अनुपस्थिति
- पराजय द्वारा।
प्रश्न 10. नागरिकता के उदारवादी सिद्धान्त का समर्थन किसने किया?
उत्तर-टी० एच० मार्शल।
प्रश्न 11. नागरिकता के स्वेच्छातंत्रवादी सिद्धान्त का समर्थन किसने किया?
उत्तर-राबर्ट नॉजिक।
प्रश्न 12. नागरिकता के बहुलवादी सिद्धान्त का समर्थन किसने किया?
उत्तर-डेविड हैल्ड ने।

प्रश्न 13. नागरिक की कोई एक विशेषता लिखें।
उत्तर-नागरिक को राज्य की ओर से कुछ अधिकार मिले होते हैं, जिन्हें वह अपने और समाज कल्याण के लिए प्रयोग करता है।
प्रश्न 14. नागरिकता की कोई एक विशेषता लिखें।
उत्तर-नागरिकता सर्वव्यापक होती है।
प्रश्न II. खाली स्थान भरें-
1. नागरिक शब्द को अंग्रेज़ी में …………. कहते हैं।
2. दीर्घ निवास नागरिकता प्राप्त करने का एक ……….. है।
3. पराजय द्वारा …………… समाप्त हो सकती है।
4. नागरिकता का उदारवादी सिद्धान्त …………… ने दिया।
5. नागरिकता का स्वेच्छातंत्रवादी सिद्धान्त …………. ने दिया।
6. नागरिकता का बहुलवादी सिद्धान्त …………… ने दिया।
उत्तर-
- सिटीज़न
- साधन
- नागरिकता
- टी० एच० मार्शल
- राबर्ट नॉजिक
- डेविड हैल्ड।
प्रश्न III. निम्नलिखित में से सही एवं ग़लत का चुनाव करें-
1. नागरिक को राज्य की ओर से कुछ अधिकार मिले होते हैं।
2. नागरिक कर्त्तव्यों का पालन नहीं करते।
3. नागरिक अपने राज्य के प्रति वफादारी रखता है।
4. ब्राजील में सम्पत्ति खरीदने से भी नागरिकता प्राप्त हो जाती है।
5. एक अच्छे नागरिक में सामाजिक भावना का होना आवश्यक नहीं है।
उत्तर-
- सही
- ग़लत
- सही
- सही
- गलत।
प्रश्न IV. बहुविकल्पीय प्रश्न-
प्रश्न 1.
“नागरिक वह व्यक्ति है जिसको राज्य के कानून संबंधी विचार-विमर्श और न्याय प्रबंध में भाग लेने का अधिकार है।” यह कथन किसका है ?
(क) अरस्तु
(ख) श्री निवास शास्त्री
(ग) प्लेटो
(घ) वाटल।
उत्तर-
(क) अरस्तु।
प्रश्न 2.
“अपनी सुलझी हुई बुद्धि को जनहित के लिए प्रयोग करना ही नागरिकता है”-यह कथन किसका है ?
(क) डेविस हैल्ड
(ख) लॉस्की
(ग) गैटल
(घ) श्री निवास शास्त्री।
उत्तर-
(ख) लॉस्की।

प्रश्न 3.
निम्न में से कौन-सा राज्यकृत नागरिकता प्राप्त करने का साधन है ?
(क) विवाह
(ख) सरकारी नौकरी
(ग) दीर्घ निवास
(घ) उपरोक्त सभी।
उत्तर-
(घ) उपरोक्त सभी।
प्रश्न 4.
निम्न में से कौन-सा नागरिकता खोने का साधन है ?
(क) दीर्घ निवास
(ख) सरकारी नौकरी
(ग) सेना में भर्ती
(घ) लंबी अनुपस्थिति।
उत्तर-
(घ) लंबी अनुपस्थिति।
![]()
![]()



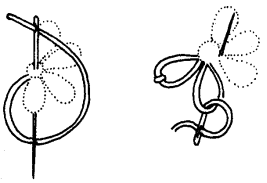

![]()
![]()